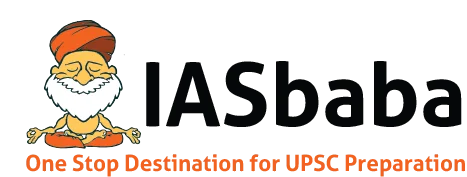IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
Archives
(PRELIMS & MAINS Focus)
पाठ्यक्रम:
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम
संदर्भ: राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष पूरे हुए।
पृष्ठभूमि: –
- देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) शुरू किया गया।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बदलना और आधुनिक बनाना है।
- तकनीकी वस्त्र पारंपरिक वस्त्रों से इस मायने में भिन्न हैं कि इन्हें कृषि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, मोटर वाहन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है।
- इस मिशन की परिकल्पना भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने, इसके मजबूत वस्त्र उद्योग का लाभ उठाकर नए आर्थिक अवसर सृजित करने, निर्यात क्षमता में वृद्धि करने तथा विविध क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी।
मिशन के प्रमुख घटक
- एनटीटीएम चार प्राथमिक घटकों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू को लक्षित करता है:
- अनुसंधान, नवाचार और विकास (आर एंड डी)
- उद्देश्य: नई सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाली अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करके नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- पहल: अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण, जिसका संचयी मूल्य अब तक 168 परियोजनाओं में लगभग 509 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
- परिणाम: इससे उन्नत, उच्च प्रदर्शन वाले वस्त्र उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है, जो उद्योग के मांग मानकों को पूरा करते हैं।
- प्रचार और बाजार विकास
- उद्देश्य: भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी वस्त्रों की बाजार पहुंच को बढ़ाना।
- पहल: प्रचार अभियान, बुनियादी ढांचे का विकास, और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय।
- परिणाम: प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों को अपनाने में वृद्धि, घरेलू उपयोग और वैश्विक बाजार मान्यता को मजबूती।
- निर्यात संवर्धन
- उद्देश्य: समर्पित निर्यात रणनीति विकसित करके भारत के तकनीकी वस्त्रों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना।
- पहल: निर्यात परिषद का गठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, तथा इस उप-क्षेत्र के लिए निर्यातोन्मुख नीतियां बनाना।
- परिणाम: भारतीय निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और व्यापक वैश्विक पहुंच।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास
- उद्देश्य: तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल से सुसज्जित एक मजबूत प्रतिभा पूल का निर्माण करना।
- पहल: शीर्ष संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर्नशिप और शैक्षणिक कार्यक्रम स्थापित करना।
- परिणाम: 50,000 व्यक्तियों को सशक्त बनाना, यह सुनिश्चित करना कि कार्यबल क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए तैयार है।
- अनुसंधान, नवाचार और विकास (आर एंड डी)
स्रोत: PIB
पाठ्यक्रम:
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम
संदर्भ : संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई को राज्य सरकारों की सहमति के बिना मामलों की जांच करने की शक्ति देने के लिए एक अलग या नया कानून बनाया जाना चाहिए।
पृष्ठभूमि: –
- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी अनुदान मांग रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आठ राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है।
मुख्य बिंदु
- समिति ने नोट किया कि आठ राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिससे भ्रष्टाचार और संगठित अपराध की जांच करने की उसकी क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई है।
- इस समस्या के समाधान के लिए, समिति का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले मामलों में राज्य की सहमति के बिना सीबीआई को व्यापक जांच शक्तियां प्रदान करने वाला एक अलग/नया कानून बनाया जा सकता है, जिसके लिए राज्य सरकारों से भी विचार प्राप्त किए जा सकते हैं।
- ये आठ राज्य – केरल, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मेघालय, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। इन सभी पर उन पार्टियों का शासन है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम की धारा 6 के तहत, सीबीआई को उन प्रांतों में मामलों की जांच करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता होती है, सिवाय उन मामलों के जहां सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या लोकपाल से आदेश जारी किए गए हों।
- संसदीय समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सीबीआई की विभिन्न इकाइयों में पार्श्विक प्रवेश (लैटरल एंट्री) शुरू करने को कहा है, क्योंकि एजेंसी ने बताया है कि उसे राज्य पुलिस से पर्याप्त और उपयुक्त नामांकन नहीं मिल रहे हैं, जो परंपरागत रूप से भर्ती का एक प्रमुख स्रोत रहा है।
- समिति ने कहा कि सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के लिए उपयुक्त नामांकन की कमी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे परिचालन दक्षता प्रभावित होती है।
सीबीआई के बारे में
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है।
- स्थापना: 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) के रूप में।
- 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसका नाम बदलकर सीबीआई कर दिया गया।
- कानूनी ढांचा: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के तहत काम करता है।
- निदेशक: प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता (एलओपी) वाली समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के विनीत नारायण निर्णय (1997) और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 में किए गए परिवर्तनों द्वारा स्थापित की गई थी।
- सीबीआई के कार्य:
- भ्रष्टाचार विरोधी मामले: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है।
- आर्थिक अपराध: बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय घोटाले, धन शोधन, साइबर अपराध आदि से संबंधित मामले।
- विशेष अपराध: आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों की जांच करता है।
- स्वप्रेरणा क्षेत्राधिकार: केवल केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर ही जांच की जा सकती है। राज्यों में, इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- हाई-प्रोफाइल मामले: राज्यों के अनुरोध पर या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के निर्देश पर मामलों को अपने हाथ में ले सकते हैं।
स्रोत: Hindustan Times
पाठ्यक्रम:
- प्रारंभिक परीक्षा – पर्यावरण
प्रसंग: असम में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्तपोषित सौर पार्क पर पर्यावरण छीनने का आरोप है।
पृष्ठभूमि:
- 26 मार्च को, जनजातीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारियों ने असम सरकार की 18,000 बीघा (2,396.5 हेक्टेयर) जनजातीय भूमि को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना के लिए हस्तांतरित करने की योजना के खिलाफ रैली निकाली।
मुख्य बिंदु
- ग्रीन ग्रैबिंग एक शब्द है जिसका उपयोग पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण या सतत विकास के नाम पर बाहरी संस्थाओं – चाहे वे सरकारें, निगम या गैर सरकारी संगठन हों – द्वारा भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के विनियोजन को वर्णित करने के लिए किया जाता है।
- जबकि पर्यावरणीय नीतियां और परियोजनाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन पर्यावरण पर कब्ज़ा करने की प्रक्रिया अक्सर शक्ति असंतुलन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से वंचित करने जैसे गहरे मुद्दों को छिपा देती है।
- ग्रीन ग्रैबिंग मूलतः भूमि हड़पने की व्यापक घटना का एक उपसमूह है। हालांकि, मुख्य रूप से कृषि या औद्योगिक हितों से प्रेरित पारंपरिक भूमि हड़पने के विपरीत, ग्रीन ग्रैबिंग को पर्यावरणीय उद्देश्यों का उपयोग करके उचित ठहराया जाता है।
प्रमुख चालक और तंत्र
- पर्यावरणीय तर्क एक बहाने के रूप में – प्रायः, पर्यावरण पर कब्ज़ा करने की आड़ में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:
- जैव विविधता संरक्षण: वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करना, जिससे स्वदेशी आबादी और स्थानीय हितधारकों का बहिष्कार हो सकता है।
- जलवायु परिवर्तन शमन
- पारिस्थितिक पर्यटन और सतत विकास: पारिस्थितिक पर्यटन या “हरित” आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं।
- संस्थागत और नीतिगत गतिशीलता – ग्रीन ग्रैबिंग नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं और वित्तीय तंत्रों के एक जटिल नेटवर्क में अंतर्निहित है। प्रमुख तंत्रों में शामिल हैं:
- कार्बन बाज़ार: कार्बन पृथक्करण पर मौद्रिक मूल्य लगाकर, सरकारें और निगम वन परियोजनाओं में ऐसे तरीकों से निवेश कर सकते हैं जो स्थानीय समुदायों को वंचित कर सकते हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: राज्य एजेंसियों और निजी फर्मों के बीच सहयोग से कभी-कभी भूमि स्वामित्व या उपयोग के अधिकारों को पुनः परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण सुधार के नाम पर नियंत्रण में बदलाव होता है।
- कानूनी सुधार: भूमि-उपयोग कानूनों या विनियमों में परिवर्तन से प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाया जा सकता है, जिससे “हरित” परियोजनाओं के लिए संसाधनों के विनियोजन को सरल बनाया जा सके।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- स्थानीय समुदायों का विस्थापन – जब पर्यावरण संरक्षण या वाणिज्यिक हरित पहलों के लिए भूमि का पुनर्वर्गीकरण किया जाता है, तो स्थानीय समुदाय विस्थापित हो जाते हैं।
- पारंपरिक अधिकारों की हानि: जो समुदाय पीढ़ियों से इन भूमियों का प्रबंधन करते रहे हैं और उन पर रहते आए हैं, उनके अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है या उन पर काफी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- आर्थिक हाशियाकरण: नए विनियामक ढांचे या स्वामित्व मॉडल बाहरी निवेशकों या सरकारी एजेंसियों का पक्ष लेते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और पारंपरिक प्रथाओं को बाधित कर सकते हैं।
- सामाजिक संघर्ष: भूमि अधिकारों को लेकर होने वाला संघर्ष अक्सर स्थानीय आबादी और बाहरी कारकों के बीच संघर्ष को जन्म देता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं।
स्रोत: Down To Earth
पाठ्यक्रम:
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – पर्यावरण
प्रसंग: तमिलनाडु सरकार ने डिंडीगुल जिले में कासमपट्टी (वीरा कोविल) पवित्र उपवन को आधिकारिक तौर पर जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित कर दिया है, जिससे यह मदुरै में अरिट्टापट्टी के बाद राज्य में दूसरा ऐसा स्थल बन गया है।
पृष्ठभूमि: –
- वीरा कोविल पवित्र उपवन लंबे समय से स्थानीय समुदायों द्वारा पूजनीय रहा है, जो उपवन के भीतर मंदिर में देवता ‘वीरानन’ की पूजा करते हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे, यह उपवन जलवायु विनियमन और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्य बिंदु
- जैवविविधता विरासत स्थल एक सुपरिभाषित – स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय जल या समुद्री क्षेत्र है- जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करता है:
- प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता: इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कई दुर्लभ, संकटग्रस्त या स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं।
- विकासवादी महत्व: इसमें ऐसी प्रजातियां या आनुवंशिक लक्षण हो सकते हैं जो अद्वितीय हों तथा विकासवादी इतिहास के भंडार के रूप में कार्य करते हों।
- सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य: कई बीएचएस सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक प्रथाओं से जुड़े हुए हैं, जहां स्थानीय समुदायों ने पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाया है।
- पारिस्थितिकीय सुभेद्यता: इन स्थलों में प्रायः ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं जो प्राकृतिक गड़बड़ी और बाहरी दबावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
- बीएचएस की अवधारणा पारंपरिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में उनकी भूमिका को मान्यता देने और समर्थन देकर संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया जाता है।
- भारत में जैव विविधता विरासत स्थलों के उदाहरण:
- नल्लूर इमली ग्रोव, कर्नाटक – सदियों पुराने इमली के पेड़ों वाला पहला बीएचएस में से एक।
- गुंडिया क्षेत्र, कर्नाटक – पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियों से समृद्ध।
- माजुली द्वीप, असम – अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप।
- अल्लापल्ली, महाराष्ट्र की महिमा – विविध प्रजातियों वाला एक संरक्षित प्राकृतिक वन।
- अरिट्टापट्टी, तमिलनाडु – 2022 में अधिसूचित, जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध।
स्रोत: The News Minute
पाठ्यक्रम:
- प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान और प्रौद्योगिकी
प्रसंग: नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के निकट से दूसरी बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है।
पृष्ठभूमि: –
- अंतरिक्ष यान 692,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से सूर्य की सतह से 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा।
मुख्य बिंदु
- पार्कर सोलर प्रोब (पीएसपी) नासा का एक अभूतपूर्व मिशन है, जिसे किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य के अधिक निकट जाकर सूर्य के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- 2018 में प्रक्षेपित यह यान नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका निर्माण और प्रबंधन जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा किया गया है।
मिशन के उद्देश्य
- कोरोना और सौर पवन का मानचित्रण: पार्कर का प्राथमिक उद्देश्य सौर कोरोना में भौतिक प्रक्रियाओं की जांच करना है। सूर्य के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश करके, जांच सौर वायु को चलाने वाले तापमान, चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा विशेषताओं पर डेटा एकत्र करती है।
- कण त्वरण को समझना: यह अध्ययन कि कण किस प्रकार प्रकाश की गति के आधे तक त्वरित हो जाते हैं, अंतरिक्ष मौसम की समझ को बढ़ाता है – एक ऐसी घटना जो पृथ्वी पर उपग्रहों, विद्युत ग्रिडों और संचार को प्रभावित कर सकती है।
- सौर गतिविधि के रहस्यों को उजागर करना: सूर्य के पहले से भी अधिक निकट पहुंचकर, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे कोरोनल हीटिंग के रहस्य (क्यों कोरोना सूर्य की सतह से काफी अधिक गर्म है) और सौर ज्वालाओं तथा कोरोनल द्रव्यमान निष्कासनों के पीछे के तंत्रों के बारे में लंबे समय से चले आ रहे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे।
मुख्य तकनीकी विवरण
- कक्षा और निकटता: शुक्र से कई गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करते हुए, पार्कर सोलर प्रोब की अण्डाकार कक्षा धीरे-धीरे इसके पेरिहेलियन (सबसे निकट दृष्टिकोण) को कम करती है, जिससे यह सौर सतह से लगभग 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजर सकता है। यह निकटता मानव निर्मित वस्तुओं के बीच एक रिकॉर्ड है।
- गति रिकॉर्ड: अपने निकटतम दृष्टिकोण पर, जांच 692,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चौंका देने वाली गति तक पहुँचती है, जो इसे इतिहास में सबसे तेज़ मानव निर्मित वस्तु बनाती है। यह रिकॉर्ड तोड़ने वाली गति कोरोना के सबसे कठोर हिस्सों में बिताए गए समय को कम करने के लिए आवश्यक है, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना है।
स्रोत: Space
Practice MCQs
दैनिक अभ्यास प्रश्न:
Q1.) ग्रीन ग्रैबिंग (Green Grabbing) शब्द का तात्पर्य है:
(a) हरित आवरण बढ़ाने के लिए जैविक खेती की एक विधि।
(b) औद्योगिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।
(c) पर्यावरण संरक्षण के नाम पर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का विनियोजन।
(d) बंजर भूमि पर पुनः वनरोपण करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीति।
Q2.) निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) नहीं है?
(a) माजुली द्वीप, असम
(b) अरित्तापट्टी, तमिलनाडु
(c) फूलों की घाटी, उत्तराखंड
(d) नल्लूर इमली ग्रोव, कर्नाटक
Q3.) नासा द्वारा प्रक्षेपित पार्कर सोलर प्रोब मुख्य रूप से अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
(a) मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की संभावना
(b) पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभाव
(c) सूर्य का कोरोना और सौर हवा
(d) मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट
Comment the answers to the above questions in the comment section below!!
ANSWERS FOR ’ Today’s – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs
ANSWERS FOR 28th March – Daily Practice MCQs
Q.1) – b
Q.2) – a
Q.3) – b