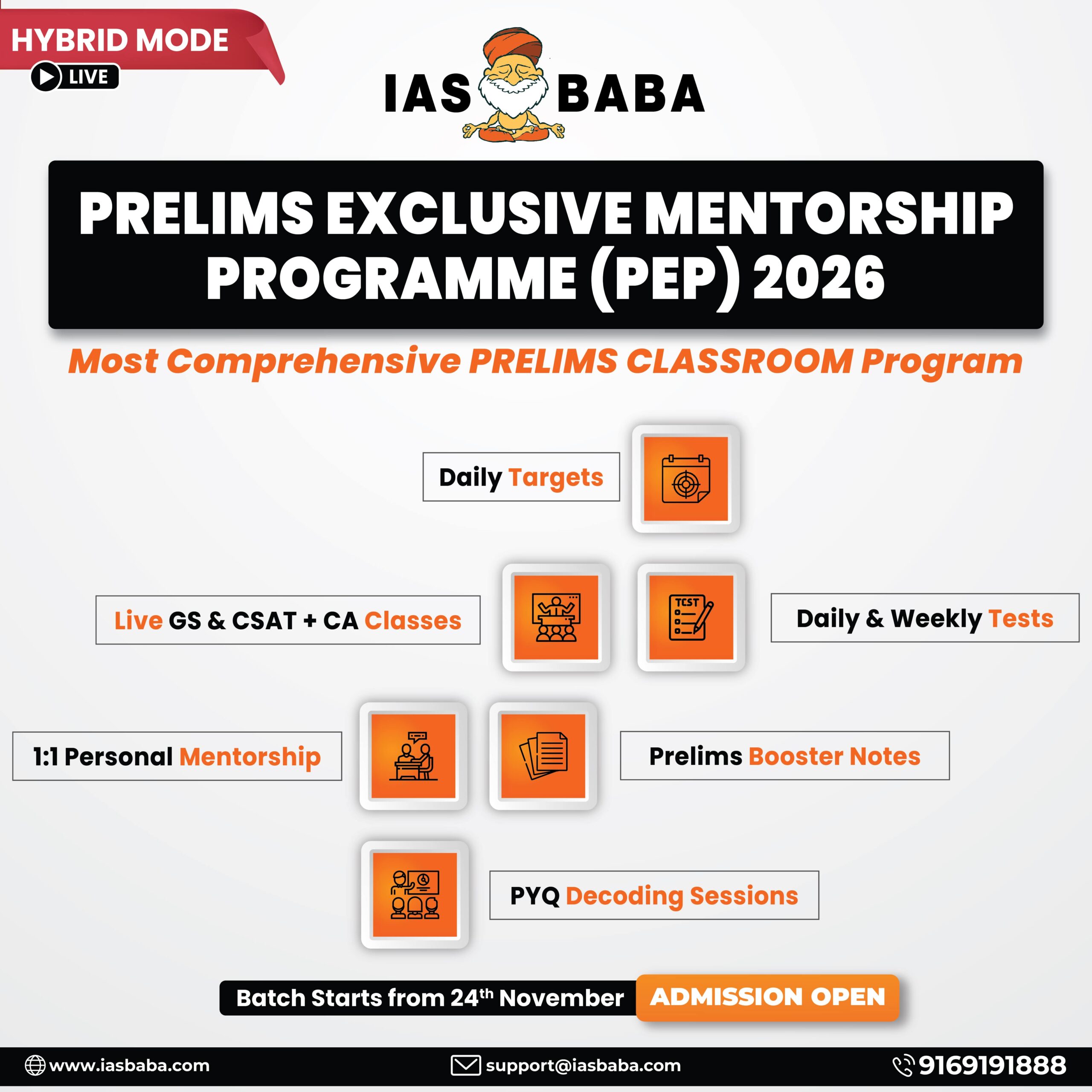IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रसंग:
- एक्सिओम स्पेस ने कहा कि चालक दल कक्षा में अपने अंतिम दिनों का पूर्ण उपयोग कर रहा है, तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को आगे बढ़ा रहा है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार दे सकते हैं तथा पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
एक्सिओम मिशन 4 के बारे में
- यह मिशन एक्सिओम स्पेस (निजी कंपनी), राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का सहयोग है।
- यह नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। 1970 और 1980 के दशक में अपनी-अपनी इंटरकॉसमॉस उड़ानों के बाद, यह भारत, पोलैंड और हंगरी के सरकारी प्रायोजित अंतरिक्ष यात्रियों वाला पहला आईएसएस मिशन है।
- चालक दल में अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के सदस्य शामिल हैं। चालक दल के सदस्य आईएसएस पर 14 दिन बिताएँगे और सूक्ष्म-गुरुत्व अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आउटरीच गतिविधियों में भाग लेंगे।
- शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले अंतिम भारतीय थे, जब उन्होंने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की थी।
महत्व
- इससे सूक्ष्मगुरुत्व में जैविक प्रक्रियाओं की समझ बढ़ेगी तथा लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए रणनीति विकसित होगी।
- इससे अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति और मजबूत होगी तथा वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में योगदान देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा।
- ये वैज्ञानिक प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति को बढ़ावा देंगे तथा भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेंगे।
स्रोत:
श्रेणी: भूगोल एवं पर्यावरण
प्रसंग:
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य में प्रजनन दर 1.7 है, जिस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आर्थिक मंदी, श्रमिकों की कमी, वृद्धों की देखभाल का बोझ और शहरी-ग्रामीण असमानताएं बढ़ सकती हैं।
प्रमुख शब्दावलियाँ:
- कुल प्रजनन दर (TFR): TFR उन बच्चों की औसत संख्या है जो एक महिला समूह अपने प्रजनन वर्षों (15 से 49 वर्ष की आयु) के अंत तक पैदा कर सकता है, अगर वे जीवन भर वर्तमान प्रजनन दरों का पालन करें, यह मानते हुए कि मृत्यु दर नहीं होगी। इसे प्रति महिला बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- प्रतिस्थापन स्तर: 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जहां प्रत्येक पीढ़ी बिना किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि या गिरावट के स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेती है।
भारत में प्रजनन दर के रुझान:
- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 1950 के दशक के 6.18 से गिरकर 2021 में 1.9 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से भी कम है। 2100 तक, भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) और गिरकर 1.04 (प्रति महिला बमुश्किल एक बच्चा) हो जाने का अनुमान है।
- केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में पहले प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली।
- भारत में वर्तमान में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 10.5% है। 2050 तक, यह संख्या बढ़कर 347 मिलियन या कुल जनसंख्या का 20.8% हो जाने की उम्मीद है।
भारत की प्रजनन दर में गिरावट के कारण:
- भारत में जन्म नियंत्रण/परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पुराने कार्यक्रमों में से एक है, लेकिन महिला साक्षरता, कार्यबल में भागीदारी और महिला सशक्तिकरण जैसे कारकों का प्रजनन दर में गिरावट पर अधिक प्रभाव पड़ा है।
- विवाह और प्रजनन के प्रति बदलते दृष्टिकोण, जिसमें विवाह और मातृत्व में देरी या परहेज शामिल है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन के बढ़ते मामले इस गिरावट में योगदान दे रहे हैं।
- गर्भपात की उपलब्धता और सामाजिक स्वीकृति ने संभवतः प्रजनन दर में गिरावट में योगदान दिया है।
स्रोत:
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- विभिन्न दलों के सांसद केंद्र सरकार से दलाई लामा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना 90वां जन्मदिन मनाया है।
भारत रत्न पुरस्कार के बारे में:
- यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी क्षेत्र में, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग की गणना किए बिना, उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी, 1954 को की थी।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(1) पुरस्कार विजेताओं को अपने नाम के आगे ‘भारत रत्न’ शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग करने से रोकता है। हालाँकि, उन्हें अपने बायोडेटा, विज़िटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि में ‘राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित’ या ‘भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता’ लिखने की अनुमति है।
- इस पुरस्कार के लिए सिफ़ारिशें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाणपत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार के साथ कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार गैर-भारतीयों के लिए भी खुला है, जैसा कि मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के मामले में हुआ है।
- प्रत्येक वर्ष अधिकतम तीन पुरस्कार दिए जा सकते हैं, अपवाद स्वरूप इस वर्ष 2024 और 1999 में क्रमशः पांच और चार व्यक्तियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ था।
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1964 में भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे।
दलाई लामा के बारे में:
- दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
- तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं, और पहले और दूसरे दलाई लामा को यह उपाधि मरणोपरांत दी गई थी। 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेनज़िन ग्यात्सो हैं।
- ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग के अवतार हैं, जो करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत हैं।
स्रोत:
श्रेणी: सुरक्षा और आपदा प्रबंधन
प्रसंग:
- भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 11 जुलाई को एक नाटकीय बचाव अभियान के तहत अमेरिकी ध्वज वाले नौकायन पोत ‘सी एंजेल’ को बचाया, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा प्वाइंट के दक्षिण-पूर्व में समुद्र की उथल-पुथल के बीच फंसा हुआ था।
भारतीय तटरक्षक बल के बारे में:
- इसे तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत अगस्त 1978 में किया गया था । यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज एवं बचाव तथा समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार, आईसीजी विभाग को दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल माना जाता है।
- यह समुद्री कानूनों, विनियमों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करता है जिन पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है। यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्र तटों पर अपतटीय विकास क्षेत्रों (ODA) की निगरानी के लिए नियमित गश्त करता है।
- यह सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है तथा प्रतिबंधित सूची में शामिल प्रतिबंधित वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के प्रवेश और निकास को रोकने के लिए तस्करी-रोधी अभियान चलाता है। यह विभिन्न समुद्री अभ्यासों और अभियानों में भाग लेता है और उनका संचालन करता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) के बारे में:
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ भारत का संबंध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से है, जब अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक दंडात्मक उपनिवेश की स्थापना की थी।
- 1942 में इन द्वीपों पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था और बाद में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर दौरे के बाद यह ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला भारत का पहला हिस्सा बन गया।
- दस डिग्री चैनल एक संकरी जलडमरूमध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह लगभग 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है।
- इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का निवास स्थान है: जो ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनली हैं।
- 2001 में, कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा समीक्षा के बाद पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमान (ANC) की स्थापना की गई। यह भारत की पहली संयुक्त/एकीकृत परिचालन कमान है, जिसमें तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल के बलों को एक ही कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया है।
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को घोषणा की कि बिहार में 7,89,69,844 मतदाताओं में से 74% से अधिक ने राज्य में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के हिस्से के रूप में अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में:
- विशेष गहन पुनरीक्षण में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोजित, मतदाता सूची पर्यवेक्षण के लिए ईसीआई को सशक्त बनाना।
- यह नये पंजीकरण, नाम हटाने और संशोधन की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी और विसंगतियों से मुक्त हो।
- इस प्रक्रिया के तहत, मतदाताओं, खासकर 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को अब जन्म प्रमाण पत्र या माता-पिता का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे। और, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत संदिग्ध मामलों को संदर्भित करने के अधिकार के साथ, शामिल करने/हटाने का निर्णय लेंगे।
- अकेले बिहार में ही, 1 लाख बीएलओ और 4 लाख स्वयंसेवकों की मदद से 8 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं का पुनर्सत्यापन किया जा रहा है। यह पूरा संशोधन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, 25 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है।
- मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान का आदेश देना भी शामिल है, और इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 329(बी) के अनुसार चुनावों के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है।
एसआईआर से संबंधित चिंताएं/चुनौतियां:
- पिछली प्रथा के विपरीत, अब साक्ष्य का भार मतदाताओं पर है, आपत्तिकर्ताओं पर नहीं (यह नियम 18, मतदाता पंजीकरण नियम का खंडन करता है)।
- केवल 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को ही कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है – यह एक अतार्किक कटऑफ है, जिसका कोई कानूनी उदाहरण नहीं है।
- सीमांचल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, आधार या ईपीआईसी के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र के बिना मतदाताओं को सूची से बाहर रखा जा सकता है।
- केवल बिहार में चुनाव से पहले आयोजित किया गया – जिसके कारण विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए हेरफेर का आरोप लगाया है।
आगे की राह:
- यद्यपि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फिर भी यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सबसे सुलभ पहचान पत्र है और इसे निवास सत्यापन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, तथा विरासत डेटा के साथ क्रॉस-सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
- ईसीआई को नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों से परामर्श करना चाहिए तथा एसआईआर नियमों और समय-सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- एआई-संचालित विसंगति पहचान का उपयोग संदिग्ध विलोपन/जोड़ (जैसे, एक इलाके से बड़ी संख्या में निष्कासन) को चिह्नित करने, ब्लॉकचेन-आधारित मतदाता लॉग को लागू करने और मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान छेड़छाड़ को रोकने के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
- हाशिए पर रहने वाले समूहों (जैसे, विकलांग और आदिवासी) के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, ताकि बहुभाषी हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जा सके, तथा सटीक नामांकन सुनिश्चित करने और बहिष्करण को न्यूनतम करने के लिए संशोधन के बाद नमूना सर्वेक्षण आयोजित किए जा सकें।
स्रोत:
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
मानसून के आरंभ में, भारी वर्षा – जो कुछ ही घंटों में 71 मिमी से अधिक मापी गई – के कारण मंडी , कुल्लू और चंबा जिलों में बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिसके कारण भूस्खलन हुआ, सड़कें बंद हो गईं और जान-माल का नुकसान हुआ।
इस क्षेत्र में कुल आर्थिक नुकसान 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा हुआ है, और पर्यावरणीय क्षति भी उतनी ही चिंताजनक है। भारी बारिश के कारण मिट्टी का कटाव, तलछट जमाव और कृषि भूमि को नुकसान हुआ है, जिससे स्थानीय समुदाय की दुर्दशा और भी बढ़ गई है।
ये सभी हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शा रहे हैं।
कारण
भारत के हिमालयी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड , तथा नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं।
इसके कारण हैं:
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय मौसम प्रणालियों को बदल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक तीव्र तूफान, अप्रत्याशित वर्षा, तेजी से ग्लेशियर पिघलना और बाढ़ में वृद्धि हो रही है।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडलीय नमी बढ़ रही है ( प्रति 1°C तापमान वृद्धि पर 7% की वृद्धि होती है)। इस अतिरिक्त नमी के कारण भारी वर्षा होती है।
- हिमालय के ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं, कुछ ग्लेशियरों की बर्फ की मोटाई सालाना 30 मीटर तक कम हो रही है। इसके पिघलने से नदियों के प्रवाह की मात्रा में सीधे तौर पर वृद्धि हो रही है, जिससे भारी मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।
- ग्लेशियरों के पिघलने और तीव्र वर्षा के कारण व्यास, यमुना और गंगा जैसी नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वे उफान पर आ जाती हैं, जिससे उनके किनारों का क्षरण होता है और बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं।
- पर्वतीय ढलानें वर्षा जल को तेजी से घाटियों में पहुंचा देती हैं, तथा अस्थिर ढलानें भूमि को भूस्खलन के लिए प्रवृत्त करती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और भी बढ़ जाता है।
प्रभाव
- प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं, जिससे संपर्क और आवश्यक सेवाएं बाधित हुईं।
- हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, भोजन की कमी और आजीविका के नुकसान का सामना कर रहे हैं।
- प्रभावित समुदायों में भविष्य की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि।
- बड़े पैमाने पर कृषि को नुकसान, पहले से ही कमजोर पहाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी का और अधिक बढ़ना।
- बार-बार विस्थापन से सरकारी संसाधनों और आपदा प्रतिक्रिया प्रणालियों पर दबाव पड़ता है।
- दूरदराज के गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और पूर्व चेतावनी तंत्र का अभाव है, जिससे उनकी भेद्यता बढ़ जाती है।
आगे की राह
- सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपदाओं के दौरान आवश्यक संपर्क बनाए रखने के लिए टिकाऊ पुलों, सभी मौसमों में उपयोग होने वाली सड़कों और प्रभावी बाढ़ अवरोधकों का निर्माण करना।
- बाढ़ और भूस्खलन की संवेदनशीलता को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे को डिजाइन करते समय स्थानीय भूवैज्ञानिक और जलविज्ञान संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखना।
- वनरोपण कार्यक्रम का विस्तार करना और ढलानों को स्थिर करना ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो और भारी बारिश के दौरान भूस्खलन को रोका जा सके।
- नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित जलाशयों का विकास करें और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
- उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियों को लागू करना तथा त्वरित सामुदायिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रभावों को कम करने के लिए समय पर चेतावनी प्रणालियां स्थापित करना।
- बाढ़ के जोखिम और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में निवासियों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करें, तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण करें।
- किसानों को बाढ़-सहिष्णु फसल किस्मों को अपनाने, फसल पैटर्न को संशोधित करने और अनियमित मौसम के बावजूद आजीविका को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण तकनीकों को लागू करने में सहायता करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना तथा सतत जल प्रबंधन को एकीकृत करना।
- अतिरिक्त जल को अवशोषित करके और पारिस्थितिक सततता बनाए रखकर प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करने के लिए आर्द्रभूमि, वन और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करें।
- जलवायु-जनित आपदाओं के विरुद्ध हिमालयी क्षेत्र में दीर्घकालिक लचीलापन निर्मित करने के लिए सरकारी स्तरों, वैज्ञानिक एजेंसियों और समुदायों के प्रयासों का समन्वय करना।
निष्कर्ष
हिमालयी क्षेत्र, उसके लोगों, विरासत और पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय सभी स्तरों पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। सक्रिय उपायों और सामुदायिक सहभागिता से, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सतत भविष्य सुनिश्चित करते हुए, संवेदनशीलता को लचीलेपन में बदलना संभव है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार योगदान दे रहा है? इन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन विकसित करने के लिए कौन-सी अनुकूली और शमन रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं? (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को 148 देशों में 131वें स्थान पर रखा गया है, जो आर्थिक विकास के बावजूद लैंगिक असमानता को उजागर करता है।
महिलाओं की स्थिति
- भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है , तथा आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा के मामले में इसका स्कोर विशेष रूप से निम्न है, जो सार्थक लैंगिक समानता के लिए आवश्यक स्तंभ हैं।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि जन्म के समय भारत का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक विषम है, जो लगातार बेटे को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा अब पुरुषों की तुलना में कम है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के अनुसार, 15 से 49 आयु वर्ग की लगभग 57% भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनकी सीखने, काम करने या सुरक्षित रूप से गर्भधारण करने की क्षमता कम हो जाती है।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर उपसूचकांक में भारत 143वें स्थान पर है । महिलाएं पुरुषों की तुलना में एक तिहाई से भी कम कमाती हैं, और महिला श्रम बल में भागीदारी अभी भी बहुत कम है।
- महिलाएं अनौपचारिक और जीविका संबंधी कार्यों में व्यस्त रहती हैं तथा निर्णय लेने के क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
- टाइम यूज सर्वे के अनुसार, भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग सात गुना अधिक अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं।
कारण
- प्रजनन स्वास्थ्य, निवारक देखभाल और पोषण में, विशेष रूप से निम्न आय और ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए दीर्घकालिक उपेक्षा।
- लगातार पुत्र प्राप्ति की प्राथमिकता के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन और भेदभाव हो रहा है।
- सामाजिक मानदंड महिलाओं को अवैतनिक घरेलू कार्य और देखभाल संबंधी कर्तव्यों तक ही सीमित रखते हैं।
- ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और निवारक देखभाल तक सीमित पहुंच।
- सुरक्षित कार्यस्थलों की कमी, लैंगिक वेतन अंतर और अनौपचारिक रोजगार पर निर्भरता के कारण महिला श्रम बल में भागीदारी कम है।
मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 2015 में अनुमान लगाया था कि लैंगिक अंतर को कम करने से 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
आगे की राह
- स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन में वृद्धि, विशेष रूप से प्राथमिक देखभाल के स्तर पर, महिलाओं की भलाई और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार के लिए आवश्यक है।
- बाल देखभाल केन्द्रों , वृद्ध देखभाल सेवाओं की स्थापना करना तथा मातृत्व लाभ का विस्तार करना।
- केन्द्र और राज्य सरकारों को समय-उपयोग सर्वेक्षण, लिंग बजट और देखभाल बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अपने आर्थिक और सामाजिक नीति ढांचे में अवैतनिक देखभाल कार्य को शामिल करना शुरू करना चाहिए।
- सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो महिलाओं को अर्थव्यवस्था का निर्माता मानें, न कि केवल लाभार्थी।
निष्कर्ष
वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट केवल एक रैंकिंग नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। लैंगिक समानता एक जनसांख्यिकीय और आर्थिक आवश्यकता है। भारत को अपनी विकास गाथा में महिलाओं को शामिल करने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे, अन्यथा कड़ी मेहनत से अर्जित विकासात्मक उपलब्धियों को गँवाने का जोखिम उठाना पड़ेगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
भारत में लैंगिक असमानता के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए तथा इन मुद्दों के समाधान के लिए एकीकृत उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)