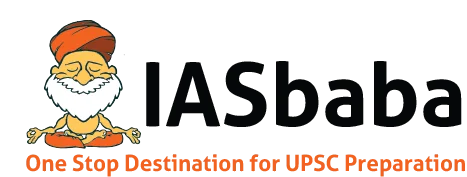IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
संदर्भ: दोहा, कतर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) और रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों के बीच युद्धविराम समझौता
दोनों पक्षों ने “स्थायी युद्धविराम” के लिए प्रतिबद्धता जताई और शरणार्थियों और विस्थापितों की स्वैच्छिक वापसी सहित वार्ता जारी रखने का संकल्प लिया। यह समझौता वर्षों से चल रहे भीषण संघर्ष, खासकर 2025 की शुरुआत में गोमा और बुकावु जैसे प्रमुख शहरों पर नए सिरे से एम23 आक्रमण के कब्जे के बाद हुआ है।
इस सफलता के बावजूद, कई कारकों के कारण युद्धविराम को नाजुक माना जा रहा है:
- अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव: विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना शांति प्रक्रिया लड़खड़ा सकती है, क्योंकि कतर के आश्चर्यजनक हस्तक्षेप तक पिछले मध्यस्थता प्रयास विफल रहे थे।
- जमीनी हकीकत: हिंसा और अविश्वास कायम है, एम23 ने धमकी दी है कि जब तक कुछ शर्तें पूरी नहीं होतीं, वे लड़ाई फिर से शुरू कर देंगे, और कुछ विद्रोहियों ने कहा है कि वे अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेंगे।
- नियंत्रण और प्रशासन: एम23 और उसके सहयोगी उत्तर और दक्षिण किवु प्रांतों में विशाल भूभाग पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा करने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- गहरी जड़ें जमाए हुए शिकायतें: यह संघर्ष नृजातीय, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के अतिव्यापी होने से उपजा है, जिसमें बाहरी तत्वों पर अपने हितों के लिए सशस्त्र समूहों का समर्थन करने का आरोप है। निरस्त्रीकरण और पुनः एकीकरण से जुड़े प्रमुख प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं।
- मानवीय संकट: लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, जिससे हजारों लोग गंभीर परिस्थितियों में हैं।
Learning Corner:
| विद्रोही समूह | देश/क्षेत्र |
|---|---|
| एम23 (23 मार्च आंदोलन) | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य |
| टीपीएलएफ (टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट) | इथियोपिया |
| तालिबान | अफ़ग़ानिस्तान |
| हूथी (अंसार अल्लाह) | यमन |
| पीकेके/वाईपीजी/कुर्द समूह | तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान |
| FARC (कोलंबिया की क्रांतिकारी सशस्त्र सेना) | कोलंबिया |
| आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) | इराक, सीरिया, वैश्विक |
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: भूगोल
संदर्भ: ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) घटनाओं के खिलाफ भारत की तैयारी
नेपाल में हाल ही में हुई जीएलओएफ घटना से काफी नुकसान हुआ तथा सेती नदी पर बने पुल के नष्ट होने से हिमालय में जीएलओएफ घटनाओं के बढ़ते खतरे पर बल मिला है।
भारत, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में, पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार, हिमनद झीलों की निगरानी और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने जैसे उपायों के माध्यम से इन जोखिमों को कम करने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) जीएलओएफ घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और सुदूर संवेदन डेटा सहित वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके शमन प्रयासों को बढ़ाने पर केंद्रित है।
इसके अलावा, साझा जलसंभरों और हिमनद झीलों से बढ़ते जोखिमों को देखते हुए, भारत और नेपाल के बीच सीमा पार सहयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने विनाशकारी GLOF घटनाओं का सामना किया है, और ऐसे जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु समाधान विकसित करने हेतु क्षेत्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत के प्रयासों में हिमनद झीलों और जलवायु पैटर्न पर शोध, तैयारी कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी और बेहतर जोखिम आकलन के लिए SAR इंटरफेरोमेट्री जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल है। हालाँकि, इन रणनीतियों की प्रभावशीलता पड़ोसी देशों के बीच निरंतर निगरानी और सहयोग पर निर्भर करेगी।
Learning Corner:
हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएँ
| प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| भूकंप (Earthquakes) | भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच विवर्तनिक टकराव के कारण यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय है | 2015 नेपाल भूकंप, 2005 कश्मीर भूकंप |
| भूस्खलन (Landslides) | तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, या भूकंपीय गतिविधि से उत्पन्न; खड़ी ढलानों पर अक्सर | केदारनाथ आपदा (2013), उत्तराखंड और सिक्किम में अक्सर होती है |
| हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) | हिमोढ़ दरार या गर्मी के कारण हिमनद झीलों से अचानक पानी का निकलना | चमोली आपदा (2021), सिक्किम में ल्होनक झील पर खतरा |
| आकस्मिक बाढ़ | बादल फटने या अचानक हिमनद पिघलने के कारण | लेह में अचानक बाढ़ (2010), हिमाचल में अचानक बाढ़ (2023) |
| हिमस्खलन | अचानक बर्फ का खिसकना, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में | 2022 गुलमर्ग हिमस्खलन, 2023 सियाचिन हिमस्खलन |
| बादल फटना (Cloudbursts) | तीव्र, स्थानीयकृत वर्षा (>100 मिमी/घंटा) विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनती है | केदारनाथ (2013), किन्नौर (2021), अमरनाथ (2022) |
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ: कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व माइक्रोस्कोप तकनीक विकसित की है जो दसियों एंगस्ट्रॉम तक आणविक गति का वास्तविक समय में अवलोकन करने में सक्षम बनाती है।
स्वतंत्र अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से चित्रण करने के बजाय, यह नई विधि प्रकाश के साथ उनकी अंतःक्रिया का विश्लेषण करके तथा ब्राउनियन गति – आणविक टकरावों के कारण होने वाली यादृच्छिक कंपन – का लाभ उठाकर, अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगाती है।
विधि के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
- पिकोसेकंड स्तर की गति के साथ नैनोस्केल गतिशीलता को ट्रैक करने के लिए स्ट्रीक कैमरा का उपयोग।
- अणुओं के समूह (एक साथ सैकड़ों अरबों) का अवलोकन, जिसमें स्वतंत्र आणविक गति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त परिशुद्धता हो।
- यह एक तीव्र इमेजिंग प्रक्रिया है, जो इसे जैव-चिकित्सा अनुसंधान, रोग निदान और नैनोमटेरियल निर्माण में अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है।
इस तकनीक में एक नमूने के माध्यम से एक लेज़र को निर्देशित किया जाता है, फिर एक डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस (डीएमडी) और स्ट्रीक कैमरा युक्त प्रणाली का उपयोग करके बिखरे हुए प्रकाश को कैप्चर किया जाता है। प्रकाश में परस्पर क्रिया पैटर्न और उतार-चढ़ाव आणविक आकार और गति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
यह अब विश्व की सबसे तेज एकल-अणु इमेजिंग तकनीक है, जो फ्लोरोसेंट लेबल या प्रत्यक्ष दृश्य अवलोकन की आवश्यकता के बिना, अभूतपूर्व गति और सटीकता से आणविक व्यवहार को देखने की नई संभावनाएं प्रदान करती है।
Learning Corner:
ब्राउनियन गति
ब्राउनियन गति से तात्पर्य किसी तरल पदार्थ (द्रव या गैस) में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक, अनियमित गति से है, जो तरल पदार्थ के तेज गति से चलने वाले अणुओं के साथ टकराव के परिणामस्वरूप होती है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- खोजकर्ता: रॉबर्ट ब्राउन (1827), जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे पानी में पराग कणों को अनियमित रूप से घूमते हुए देखा।
- व्याख्या: अल्बर्ट आइंस्टीन (1905), जिन्होंने गणितीय रूप से इसका मॉडल तैयार किया और इसे आणविक सिद्धांत से जोड़ा।
- पुष्टिकर्ता: जीन पेरिन, जिनके प्रयोगात्मक कार्य ने आइंस्टीन के समीकरणों को मान्य किया और परमाणुओं के अस्तित्व को स्थापित करने में मदद की।
वैज्ञानिक महत्व:
- आणविक गति का प्रमाण: ब्राउनियन गति ने पदार्थ के गतिज सिद्धांत के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान किया, जो पदार्थों की परमाण्विक प्रकृति का समर्थन करता है।
- सांख्यिकीय यांत्रिकी: यह आधुनिक सांख्यिकीय और क्वांटम भौतिकी के विकास में एक आधारशिला अवधारणा है।
अनुप्रयोग:
- कोलाइडल स्थिरता विश्लेषण (Colloidal stability analysis)
- शेयर बाजार मॉडलिंग (वित्तीय गणित में)
- रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रसार अध्ययन
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: इतिहास
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई उत्सव के दौरान चोल राजवंश को विकसित भारत (विकसित भारत) के सपने को साकार करने के लिए एक “प्राचीन रोडमैप” बताया।
- सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति: चोलों की शक्तिशाली नौसेना पर प्रकाश डाला गया तथा भारत की समुद्री एवं रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
- सांस्कृतिक एकता: सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए चोलों की प्रशंसा की गई, तथा इसे काशी-तमिल संगमम जैसी वर्तमान पहलों से जोड़ा गया ।
- लोकतांत्रिक परंपराएँ: भारत की स्वदेशी लोकतांत्रिक जड़ों पर जोर देने के लिए कुदावोलाई प्रणाली का हवाला दिया गया।
- जल प्रबंधन: सतत पर्यावरणीय प्रथाओं के मॉडल के रूप में चोलों की उन्नत सिंचाई प्रणालियों की सराहना की गई।
- कला और वास्तुकला: मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और साहित्य में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता दी गई।
- समकालीन कार्य: राजा राज चोल और राजेंद्र चोल प्रथम की मूर्तियों की घोषणा की गई, और सांस्कृतिक कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
Learning Corner:
चोल राजवंश
चोल राजवंश सबसे लम्बे समय तक शासन करने वाले और सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्यों में से एक था, जो मुख्यतः 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच फला-फूला।
उत्पत्ति और प्रारंभिक चोल
- प्रारंभिक चोलों का उल्लेख संगम साहित्य (लगभग 300 ईसा पूर्व-300 ईसवी) में मिलता है, जिसमें करिकाल चोल जैसे शासक उल्लेखनीय हैं।
- शाही चरण विजयालय चोल (850 ई.) के साथ शुरू हुआ, जिसने पल्लवों से तंजावुर पर कब्जा कर लिया और बाद में चोल साम्राज्य की नींव रखी।
महत्वपूर्ण शासक
- राजराजा प्रथम (985–1014 ई.)
- तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में साम्राज्य का विस्तार किया।
- प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)।
- प्रशासन और राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन किया गया।
- राजेंद्र प्रथम (1014–1044 ई.)
- साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक ले गए – श्रीलंका, अंडमान-निकोबार, मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की, और यहां तक कि श्रीविजय साम्राज्य (आधुनिक इंडोनेशिया) तक एक नौसैनिक अभियान भी भेजा।
- गंगईकोंडा चोलपुरम में नई राजधानी स्थापित की
प्रशासन और शासन
- कुशल राजस्व संग्रहण के साथ अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन।
- चुनावों के लिए ग्राम सभाओं और प्रसिद्ध कुदावोलाई प्रणाली का उपयोग ।
- भूमि अनुदान और मंदिर शिलालेखों का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है।
नौसेना शक्ति और विदेशी व्यापार
- चोलों ने प्राचीन भारत की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक का निर्माण किया।
- दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब दुनिया के साथ सक्रिय व्यापार बनाए रखा।
कला और वास्तुकला
- द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई।
- बृहदेश्वर, गंगईकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिर वास्तुशिल्प प्रतिभा को दर्शाते हैं।
- तमिल साहित्य और कांस्य मूर्तिकला, विशेष रूप से नटराज प्रतिमा को संरक्षण प्रदान किया।
पतन
- 12वीं शताब्दी के अंत में आंतरिक कलह और पांड्यों तथा होयसलों जैसी उभरती शक्तियों के कारण इसकी शुरुआत हुई ।
- अंतिम झटका 14वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मलिक काफूर के आक्रमण से लगा।
परंपरा
- दक्षिण पूर्व एशिया में तमिल संस्कृति और शैव धर्म के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई।
- अपने पीछे स्थापत्य कला, कला और साहित्यिक योगदान छोड़ गए।
स्रोत : द हिंदू
श्रेणी: अर्थव्यवस्था
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कपड़ा क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर जोर दिया है और इसे आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भरता के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित किया है।
मुख्य तथ्य:
- आर्थिक विकास: इस क्षेत्र का बाजार मूल्य 2014 में 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें यार्न, फैब्रिक और परिधान उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई है।
- रोजगार: कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में, कपड़ा उद्योग ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाता है, और 3,000 से अधिक स्टार्ट-अप का समर्थन करता है।
- सांस्कृतिक जुड़ाव: वस्त्रों को भारत की समृद्ध विरासत की अभिव्यक्ति माना जाता है। “खेत से रेशे से विदेश” मॉडल परंपरा और तकनीक के मिश्रण को दर्शाता है।
- नीतिगत समर्थन: प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, पीएलआई योजना, मित्र पार्क और समर्थ कौशल विकास योजना शामिल हैं। इस क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान 80% है।
- निर्यात लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य 2030 तक कपड़ा निर्यात को 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये करना है, जिसमें हाल ही में 7% की निर्यात वृद्धि हुई है।
- नवाचार एवं गुणवत्ता: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास, जीआई टैगिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर।
- सततता: यह क्षेत्र संसाधन-कुशल प्रथाओं के माध्यम से कपड़ा अपशिष्ट जैसी चुनौतियों का समाधान कर रहा है।
- विजन 2047: मोदी ने 2047 तक आत्मनिर्भर, विकसित भारत के निर्माण के लिए कपड़ा क्षेत्र को केंद्रीय भूमिका में रखने की परिकल्पना की है, जिससे किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को समान रूप से लाभ होगा।
Learning Corner:
कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकारी योजनाएँ
-
- वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (2021)
- मानव निर्मित रेशों (एमएमएफ) के उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य और तकनीकी वस्त्र
-
- वृद्धिशील उत्पादन के लिए 5 वर्षों तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना।
- पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क
- वस्त्र उद्योग के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू किया गया ।
- 7 प्रधानमंत्री मित्रा पार्कों को प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और मूल्य श्रृंखला एकीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
- 5एफ विजन से प्रेरित: खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन, फिर विदेश (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign)।
- समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना/ SAMARTH (Scheme for Capacity Building in Textile Sector)
- कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
- इसका लक्ष्य बेरोजगार युवा, विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर स्थित वर्ग के युवा हैं।
- इसमें प्लेसमेंट से संबद्ध कौशल कार्यक्रम शामिल हैं।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (2020-2024)
- इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र उद्योग में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है ।
- कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रदर्शन वाले वस्त्रों के अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी विकास को बढ़ावा देता है।
- एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (IWDP)
- ऊन क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है , विशेष रूप से हिमालयी और जनजातीय क्षेत्रों में।
- भेड़ प्रजनन, ऊन कतरन, ऊन प्रसंस्करण और विपणन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- सिल्क समग्र 2.0 (Silk Samagra 2.0)
- रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना ।
- अनुसंधान, बीज उत्पादन, पालन अवसंरचना और विपणन को समर्थन प्रदान करता है।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS)
- वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है ।
- उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनरी के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- पावरटेक्स इंडिया (PowerTex India)
- विद्युत करघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया ।
- करघा उन्नयन, सामान्य सुविधाओं और सौर ऊर्जा उपयोग के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।
- हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजनाएं (Handloom & Handicrafts Schemes)
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) शामिल हैं ।
- इसका उद्देश्य कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता, विपणन सहायता और बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
स्रोत: द हिंदू
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
विश्व बैंक ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से “भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की ।
इसका अनुमान है कि भारतीय शहरों को जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं के निर्माण के लिए 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शहरी आबादी 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाने की उम्मीद है और 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नए घरों की आवश्यकता होगी।
- निर्मित क्षेत्रों के तेज़ी से विकास से तापमान में वृद्धि होगी। तीव्र गर्मी की लहरें और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव पहले से ही शहरी केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में 3-4 डिग्री से अधिक की वृद्धि का कारण बन रहे हैं।
- इससे शहरों की पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो रही है, जिससे वे बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के पैटर्न जल-संबंधी या वर्षाजन्य बाढ़ के जोखिम के मुख्य चालक हैं, तथा 2070 तक जोखिम में 3.6 से 7 गुना तक की वृद्धि का अनुमान है।
- वर्षा या तूफानी जल से संबंधित बाढ़ से होने वाली वार्षिक अनुमानित हानि 2023 में 4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2070 तक 14-30 बिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है, जिससे 46.4 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।
- ग्लोबल वार्मिंग और शहरी ऊष्मा द्वीप घटना के कारण 2050 तक गर्मी से संबंधित मौतें दोगुनी होकर 3 लाख प्रति वर्ष हो सकती हैं।
- इसके अलावा, शहरी इलाकों में अचानक बाढ़ आना एक आम बात है। भारत में, अचानक बाढ़ अक्सर बादल फटने से जुड़ी होती है – यानी थोड़े समय में अचानक, तेज़ बारिश होना है। हिमालयी राज्यों को ग्लेशियरों के पिघलने से बनी ग्लेशियल झीलों के उफान पर आने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है, और पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।
शब्दावलियां
- शहरी ताप द्वीप (Urban Heat Island): शहरी ताप द्वीप एक स्थानीय और अस्थायी घटना है जो तब होती है जब शहर के कुछ हिस्सों में उसी दिन आसपास या आस-पास के इलाकों की तुलना में अधिक ताप भार होता है। यह परिवर्तन मुख्यतः उन स्थानों में गर्मी/ ऊष्मा के फंस जाने के कारण होता है जो अक्सर कंक्रीट के बने होते हैं। तापमान में यह परिवर्तन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है।
- हीट वेव: असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि, जो अक्सर उच्च आर्द्रता के साथ कई दिनों या हफ़्तों तक चलती है। भारत में, आईएमडी इसे मैदानी इलाकों में 40°C या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C या उससे अधिक तापमान के रूप में परिभाषित करता है, जो कम से कम 2 दिनों तक लगातार बना रहता है।
- तूफानी जल (Stormwater): वह जल जो वर्षा या पिघली हुई बर्फ से उत्पन्न होता है और सड़कों, छतों और खुली भूमि जैसी सतहों पर बहता है, तथा प्रायः जल निकासी प्रणालियों में प्रवेश कर जाता है।
- वर्षाजन्य बाढ़: तीव्र वर्षा के कारण शहरी जल निकासी प्रणालियों या भूमि अंतःस्यंदन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण आने वाली बाढ़ का एक प्रकार, जिसके परिणामस्वरूप नदी के अतिप्रवाह के बावजूद सड़कों और निचले इलाकों में सतही जल जमा हो जाता है।
- आकस्मिक बाढ़: भारी वर्षा, बादल फटने या बांध टूटने जैसी घटनाओं के 3 से 6 घंटे के भीतर आने वाली अचानक और तीव्र बाढ़। यह अत्यधिक स्थानीयकृत होती है, अक्सर शहरी क्षेत्रों या पहाड़ी इलाकों में होती है, और तेज़ी से जल संचय और विनाश का कारण बनती है।
जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने के लिए शहरों में अपनाई जाने वाली प्रथाएँ
- अहमदाबाद ने एक हीट एक्शन प्लान मॉडल विकसित किया है जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, स्वास्थ्य देखभाल की तैयारी में सुधार करना, हरित क्षेत्र को बढ़ाना और बाहरी श्रमिकों के लिए कार्यसूची में बदलाव करना है।
- कोलकाता ने शहर-स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली अपनाई है।
- इंदौर ने आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में निवेश किया है, जिससे स्वच्छता में सुधार हुआ है और हरित रोजगार को बढ़ावा मिला है।
- चेन्नई ने संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन के आधार पर जलवायु कार्य योजना अपनाई है, तथा अनुकूलन और निम्न-कार्बन वृद्धि दोनों को लक्ष्य बनाया है।
सिफारिशें
रिपोर्ट में 24 भारतीय शहरों का अध्ययन किया गया है, जिसमें चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम पर विशेष ध्यान दिया गया है, तथा पाया गया है कि समय पर अनुकूलन से भविष्य में मौसम संबंधी झटकों से होने वाले अरबों डॉलर के वार्षिक नुकसान को रोका जा सकता है।
उदाहरण के लिए, वार्षिक वर्षा बाढ़ से संबंधित नुकसान को टाला जा सकता है और 2030 तक यह 5 बिलियन डॉलर तथा 2070 तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अनुकूलन में निवेश से 2050 तक अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से 130,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
भारतीय शहरों की तत्काल मदद करने तथा सुभेद्य आबादी को सहारा देने के लिए, इस रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं:
- अत्यधिक शहरी गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए कार्यक्रमों को लागू करना, जिसमें जल का बेहतर विनियमन, हरित स्थान, ठंडी छतों की स्थापना और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियां शामिल हैं।
- लचीले बुनियादी ढांचे और नगरपालिका सेवाओं, ऊर्जा कुशल और लचीले आवास में निवेश करें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को आधुनिक बनाएं, और शहरी परिवहन को बाढ़ के प्रति लचीला बनाएं।
- निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के माध्यम से शहरी वित्त तक पहुंच में सुधार करना।
रिपोर्ट का अनुमान है कि शहरों में नए, लचीले और कम कार्बन उत्सर्जन वाले बुनियादी ढाँचे और सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के निवेश की ज़रूरत होगी। इन निवेशों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भूमिका अहम होगी।
निष्कर्ष
विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि मजबूत शहरी प्रशासन , वित्तीय नियोजन और स्थानीय स्वायत्तता के बिना भारत का शहरी परिवर्तन एक आपदा बन सकता है।
सतत विकास और समावेशी वृद्धि के लिए, भारत को शहरों को न केवल विकास इंजन के रूप में देखना चाहिए, बल्कि उन्हें लचीले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी देखना चाहिए, जिसके लिए बुनियादी ढांचे, संस्थानों और नवाचार में तत्काल निवेश की आवश्यकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“भारत में शहरी परिवर्तन जलवायु जोखिमों के तीव्र होने के साथ-साथ हो रहा है। इस संदर्भ में, भारतीय शहरों को लचीला और समृद्ध बनाने में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट यारलुंग जांग्बो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर एक विशाल जलविद्युत बांध का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।
यह परियोजना (167.8 बिलियन डॉलर) विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होने की उम्मीद है, तथा इससे भारत और बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण जलविज्ञान, पारिस्थितिकी और सामरिक चिंताएं उत्पन्न होंगी।
परियोजना का स्थान
- ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग ज़ंग्बो (या त्सांगपो) के नाम से जाना जाता है, जिस पर बांध “ग्रेट बेंड” पर बनाया जा रहा है, जहाँ नदी अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग में भारत में प्रवेश करने से पहले मेडोग काउंटी में यू-टर्न लेती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग कहा जाता है।
- इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 60,000 मेगावाट होगी, जो यांग्त्ज़ी नदी पर बने थ्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना अधिक है, जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है।
भारत के लिए प्रमुख चिंताएँ
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक बार चीन के ब्रह्मपुत्र मेगा बांध को “पानी बम” और “अस्तित्व के लिए खतरा” बताया था।
ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा है, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार है, और इसके इतिहास, संस्कृति और पारिस्थितिकी का केंद्र है। राज्य में नदी के प्रवाह में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण बाधा के दूरगामी परिणाम होंगे।
जल बम/ वॉटर बम का अर्थ
- “वॉटर बम” शब्द का प्रयोग हथियारबंद जल छोड़ने के लिए किया जाता है।
- यदि चीन अचानक बड़ी मात्रा में संग्रहित जल छोड़ दे, चाहे वह दुर्घटनावश हो, प्राकृतिक आपदा से हो, या जानबूझकर हो, तो इससे अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी और असम के कुछ हिस्सों जैसे निचले क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ सकती है ।
- तिब्बत भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और जिस क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है, उसे भूकंप-प्रवण और पारिस्थितिक रूप से अत्यंत सुभेद्य माना जाता है।
“अस्तित्वगत खतरे” का अर्थ
- सियांग क्षेत्र के मूल निवासी समुदाय मछली पकड़ने, कृषि और दैनिक जीवन के लिए नदी पर बहुत अधिक निर्भर हैं । बाढ़ या दीर्घकालिक कमी जैसी कोई भी बड़ी बाधा उनके अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान के लिए ख़तरा बन सकती है ।
- जल प्रवाह में अचानक परिवर्तन पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता और सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है। नदी के किनारे की वनस्पतियाँ और जीव-जंतु विलुप्त हो सकते हैं या उनके आवास नष्ट हो सकते हैं।
- लंबे समय में सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियाँ काफी हद तक सूख सकती हैं।
चीन का रुख
- चीनी विदेश मंत्रालय का दावा है कि यह परियोजना उसके संप्रभु अधिकारों के अंतर्गत है।
- डेटा साझाकरण, बाढ़ नियंत्रण और आपदा न्यूनीकरण के माध्यम से सहयोग का आश्वासन ।
भारत की प्रतिक्रिया
- भारत ने 19 जुलाई के समारोह के बाद कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की, लेकिन कहा कि वह नदी पर चीनी बुनियादी ढांचे के हस्तक्षेप पर नजर रख रहा है।
- चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले राज्यों के हितों को ऊपरी क्षेत्रों में गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे।
- राजनयिक सहभागिता में वृद्धि :
- मार्च में विदेश सचिव के नेतृत्व में हुई वार्ता में सीमा पार सहयोग पर चर्चा हुई थी।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा जून 2025 में फिर से शुरू हुई।
- चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जुलाई 2025 में पुनः शुरू किया जाएगा।
शमन के उपाय
- भारत को चीनी बांध परियोजना के बारे में वैज्ञानिक गणना करनी चाहिए, तथा भविष्य में किसी भी जानबूझकर की गई कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करना चाहिए।
- भारत प्रवाह में संभावित विविधताओं (बाढ़ की अवधि और कम प्रवाह) को अवशोषित करने के लिए ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियों पर भंडारण की योजना बना सकता है।
-
- अरुणाचल प्रदेश में 300 मीटर ऊंचे बांध के साथ अपर सियांग परियोजना को न केवल इसकी प्रचंड जलविद्युत क्षमता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि तिब्बत में चीनी परियोजनाओं के मद्देनजर इसे रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
- बांध का भंडारण नदी के प्रवाह में बदलाव के विरुद्ध एक बफर के रूप में काम कर सकता है।
- हालाँकि, बांध के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध के कारण परियोजना की प्रगति धीमी हो गई है।
- भविष्य में अतिरिक्त जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और अधिक अंतर्देशीय नहरें बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को गंगा बेसिन से जोड़ने के लिए दो संपर्क मार्गों का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त जल को जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचाना है।
- निरंतर आधार पर बहाव के प्रभावों का आकलन करने के लिए चीन से विस्तृत जलविज्ञान और परियोजना-संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- भारत को अन्य निचले तटवर्ती पड़ोसी देशों – भूटान, बांग्लादेश और यहां तक कि म्यांमार के साथ भी अग्रिम चेतावनी और आपदा तैयारी के लिए समन्वित प्रोटोकॉल विकसित करने पर बातचीत करनी चाहिए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बाँध से भारत के लिए गंभीर पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। भारत की जल सुरक्षा पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए और एक बहुआयामी प्रतिक्रिया रणनीति सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)