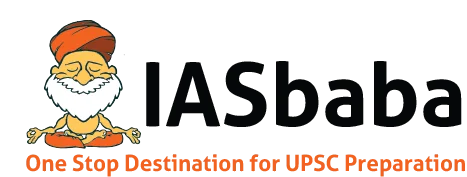IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: अर्थशास्त्र
प्रसंग: गिनी सूचकांक ने भारत को विश्व के अधिक समान समाजों में स्थान दिया है
- यह शहरी-ग्रामीण, लैंगिक, धन और डिजिटल असमानताओं की जमीनी हकीकत को दर्शाने में विफल रहा है।
- इसकी कार्यप्रणाली अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार, पहुंच संबंधी असमानताओं और असमानता को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंडों को नजरअंदाज करती है।
भारत में असमानता के रूप:
- धन असमानता:
- एक छोटे से हिस्से के पास देश की अधिकांश सम्पत्ति है।
- शीर्ष 10% लोगों के पास आय का अनुपातहीन हिस्सा है।
- अनौपचारिक नौकरियाँ और गैर-करयोग्य आय के कारण धन असमानता का आकलन करना कठिन हो जाता है।
- लैंगिक असमानता:
- कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 35.9% है।
- केवल 12.7% नेतृत्वकारी भूमिकाएं महिलाओं के पास हैं।
- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स कुल का मात्र 7.5% हैं।
- पितृसत्तात्मक मानदंडों के परिणामस्वरूप बालिकाओं के लिए संसाधन कम होते हैं तथा उत्तराधिकार भी कम मिलता है।
- डिजिटल असमानता:
- केवल 53.9% स्कूलों में इंटरनेट है, तथा 52.7% में कार्यशील कंप्यूटर हैं।
- केवल 25% ग्रामीण महिलाओं तथा 49% ग्रामीण पुरुषों के पास इंटरनेट की सुविधा है।
- प्रदूषण के मौसम में स्कूलों का बंद होना यह दर्शाता है कि इंटरनेट की असमान पहुंच शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है।
Learning Corner:
गिनी गुणांक
गिनी गुणांक (या गिनी सूचकांक) किसी जनसंख्या के भीतर आय या धन असमानता का एक सांख्यिकीय माप है।
परिभाषा:
- यह 0 से 1 (या 0% से 100%) तक होता है:
- 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है (सभी की आय समान है)।
- 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है (एक व्यक्ति के पास सारी आय है, अन्य के पास कुछ भी नहीं है)।
इसे कैसे मापा जाता है:
- लोरेंज वक्र पर आधारित, जो जनसंख्या के संचयी हिस्से के विरुद्ध आय के संचयी हिस्से को दर्शाता है।
- गिनी गुणांक समानता रेखा और लोरेंज वक्र के बीच के क्षेत्र और समानता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल का अनुपात है।
अनुप्रयोग:
- आय वितरण का आकलन करने के लिए अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और विश्व बैंक तथा यूएनडीपी जैसी संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है।
- विभिन्न देशों या समय के साथ असमानता की तुलना करने में सहायता करता है।
सीमाएँ:
- इसमें गैर-आय असमानताओं (जैसे, लिंग, डिजिटल पहुंच) को शामिल नहीं किया गया है।
- असमानता के स्थान के प्रति असंवेदनशील (चाहे वह आय पैमाने के शीर्ष पर हो या निम्नतम स्तर पर)।
- समान गिनी स्कोर बहुत भिन्न आर्थिक संरचनाओं को छिपा सकते हैं।
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: राजनीति
संदर्भ: 2024-25 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य 2030-31 तक भारत को तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है
मुख्य उद्देश्य:
- सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल आदि प्रमुख तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- उच्च उपज वाली, जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- आधुनिक कृषि पद्धतियों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- वित्तीय प्रोत्साहन और इनपुट सब्सिडी प्रदान करना।
- फसल-उपरांत प्रबंधन, बाजार संपर्क और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- फसल बीमा कवरेज का विस्तार करना।
- चावल की भूसी, कपास के बीज और वृक्ष-जनित तिलहन जैसे स्रोतों से द्वितीयक तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देना।
कार्यान्वयन एवं लक्ष्य:
- अवधि: 2024-25 से 2030-31
- बजट: ₹10,103 करोड़
- लक्ष्य: तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना
- लक्ष्य: अनुमानित घरेलू खाद्य तेल मांग का 72% पूरा करना
सहायता उपाय:
- बीज आपूर्ति समन्वय के लिए SATHI पोर्टल का शुभारंभ।
- उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी में वृद्धि तथा पीएम-आशा जैसी योजनाएं।
- घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए उच्च आयात शुल्क।
- पर्यावरणीय सततता और ग्रामीण रोजगार पर जोर।
Learning Corner:
भारत में तिलहन उत्पादन:
- भारत विश्व स्तर पर तिलहन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन खाद्य तेलों का शुद्ध आयातक बना हुआ है, जो अपनी घरेलू मांग का 50% से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है।
- उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहनों में शामिल हैं:
- मूंगफली, सोयाबीन, सरसों/रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, अलसी, नाइजर, कुसुम और अरंडी।
- मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है; जलवायु परिवर्तनशीलता, कम इनपुट उपयोग और सीमित सिंचाई के कारण उत्पादकता अक्सर कम होती है।
प्रमुख सरकारी योजनाएँ:
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-तिलहन) (2024-25 से 2030-31)
- इसका उद्देश्य भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है।
- 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- आवश्यक भाग:
- उच्च उपज वाले बीज, जलवायु-प्रतिरोधी किस्में
- वित्तीय प्रोत्साहन, इनपुट सब्सिडी
- फसल बीमा, बीज समन्वय के लिए SATHI पोर्टल
- कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन
- प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों (जैसे, चावल की भूसी, कपास के बीज) पर ध्यान केंद्रित करना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM – तिलहन और पाम ऑयल)
- तिलहन फसलों के लिए उत्पादकता और क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देता है।
- इनपुट, प्रशिक्षण और क्लस्टर प्रदर्शनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
मूल्य समर्थन योजना (PSS)
- पीएम-आशा के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित की जाती है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तिलहनों के लिए समर्थन सहित राज्य-नेतृत्व वाली पहलों को वित्तपोषित करने के लिए एक लचीली योजना।
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: भूगोल
संदर्भ: लद्दाख के गर्म झरने और जीवन की उत्पत्ति
वे क्यों महत्वपूर्ण हैं:
- अद्वितीय कार्बोनेट रसायन: सिलिका पर वैश्विक ध्यान के विपरीत, लद्दाख के गर्म झरने (विशेष रूप से पुगा घाटी में) तेजी से कैल्शियम कार्बोनेट (ट्रैवर्टीन) का निर्माण दर्शाते हैं, जो अमीनो एसिड और फैटी एसिड जैसे कार्बनिक अणुओं को संरक्षित करता है – जो प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्राकृतिक प्रयोगशाला: ये झरने प्रारंभिक पृथ्वी के सदृश वास्तविक दुनिया का वातावरण प्रदान करते हैं, जो यह अध्ययन करने के लिए आदर्श है कि जीवन कैसे बना होगा।
एक्सट्रीमोफाइल अंतर्दृष्टि (Extremophile Insights):
- कठोर परिस्थितियां (यूवी विकिरण, तापमान चरम) प्रारंभिक पृथ्वी और मंगल ग्रह के समान हैं।
- यहां सूक्ष्मजीव सुरक्षात्मक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि जीवन किस प्रकार विषम वातावरण में अनुकूलित होता है और जीवित रहता है।
खगोलीय जैविक महत्व:
- मंगल ग्रह के अनुरूप: मंगल ग्रह की जलतापीय प्रणालियों से समानताएं लद्दाख को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए मूल्यवान बनाती हैं।
- बायोमार्कर साक्ष्य: मंगल ग्रह पर बायोसिग्नेचर की खोज कहां और कैसे की जाए, इसकी पहचान करने में मदद करता है, तथा इसरो और नासा के मिशनों का मार्गदर्शन करता है।
मुख्य निष्कर्ष:
- कार्बोनेट जीवन के निर्माण खंडों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- खगोल जीव विज्ञान, सिंथेटिक जीव विज्ञान और मंगल अन्वेषण में नई दिशाओं का समर्थन करता है।
- पृथ्वी से परे जीवन की खोज में भारत के योगदान को मजबूत करता है।
Learning Corner:
हॉट स्प्रिंग्स/ गर्म झरने (Hot Springs):
- परिभाषा: गर्म झरना पृथ्वी की सतह पर भूतापीय रूप से गर्म भूजल का प्राकृतिक निर्वहन है।
- यह तब बनता है जब भूजल पृथ्वी में गहराई तक रिसता है, मैग्मा या गर्म चट्टानों से गर्म होता है, और वापस सतह पर आ जाता है।
- इसमें तापमान भिन्न-भिन्न हो सकता है – जो गुनगुने से लेकर उबलते जल तक हो सकता है।
- विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों, विशेषकर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- उल्लेखनीय भारतीय उदाहरण:
- मणिकरण (हिमाचल प्रदेश)
- तपोवन (उत्तराखंड)
- बकरेश्वर (पश्चिम बंगाल)
गीजर:
- गीजर एक विशेष प्रकार का गर्म झरना है जो समय-समय पर फूटता रहता है तथा हवा में भाप और गर्म पानी छोड़ता रहता है।
- यह तब होता है जब उबलते पानी और भाप से भरे भूमिगत कक्षों में दबाव बनता है।
- आवश्यक तत्व:
- तीव्र भूतापीय ऊष्मा
- प्रचुर भूजल
- संकीर्ण नलिकाओं के साथ एक अद्वितीय पाइपलाइन प्रणाली
- गर्म झरनों की तुलना में बहुत दुर्लभ।
- प्रसिद्ध गीजर:
- येलोस्टोन नेशनल पार्क (अमेरिका) में ओल्ड फेथफुल
- चिली में एल तातियो
- भारत में कोई महत्वपूर्ण वास्तविक गीजर नहीं है।
भूवैज्ञानिक महत्व:
- भूतापीय ऊर्जा क्षमता के संकेतक
- अद्वितीय सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करना
- पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थल
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रसंग: प्रलय मिसाइल और उसके हालिया परीक्षण
मुख्य अंश:
- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से संचालित।
- इसका उद्देश्य अधिकतम (500 किमी) और न्यूनतम (150 किमी) रेंज को मान्य करना है।
- सभी उप-प्रणालियों द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन के साथ सटीक सटीकता प्राप्त की गई।
तकनीकी सुविधा:
- प्रकार: ठोस ईंधन, अर्ध-बैलिस्टिक, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
- रेंज: 150-500 किमी.
- पेलोड: पारंपरिक वारहेड (350-1,000 किलोग्राम)।
- मिसाइल सुरक्षा से बचने के लिए उन्नत नेविगेशन और मध्य-मार्ग गतिशीलता।
परिचालन उपयोगिता:
- लक्ष्यों में कमांड सेंटर, एयरबेस और लॉजिस्टिक हब शामिल हैं।
- उच्च गतिशीलता और सामरिक परिशुद्धता के माध्यम से रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है।
- इससे भारत की पारंपरिक निवारक क्षमता मजबूत होगी, विशेषकर क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध।
विकास एवं प्रेरण:
- भारतीय उद्योग सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन किया गया।
- दोहरे परीक्षणों से चरण-1 परीक्षण पूरा हो गया है, जिससे सैन्य उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
Learning Corner:
प्रलय के समकक्ष भारतीय मिसाइलें:
| मिसाइल | प्रमुख विशेषताऐं | प्रलय से तुलना |
|---|---|---|
| प्रहार | 150 किमी रेंज, ठोस ईंधन SRBM, अत्यधिक गतिशील | कम दूरी और पेलोड; प्रलय बेहतर मार्गदर्शन और लंबी दूरी के साथ अधिक उन्नत है |
| शौर्य | 700–1,900 किमी रेंज, हाइपरसोनिक, परमाणु-सक्षम | लंबी दूरी और दोहरे उपयोग; शौर्य रणनीतिक है, जबकि प्रलय सामरिक और पारंपरिक है |
| ब्रह्मोस | 290–450 किमी रेंज, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हवा/समुद्र/जमीन से प्रक्षेपित | क्रूज मिसाइल (बैलिस्टिक नहीं); कम ऊंचाई, अधिक गतिशील; प्रलय बैलिस्टिक चाप पर अधिक तेज है |
प्रलय के समान विदेशी मिसाइलें:
| देश | मिसाइल | नोट्स |
|---|---|---|
| चीन | DF-12 (CSS-X-15) | सामरिक एसआरबीएम, ठोस ईंधन, प्रलय के समान रेंज और भूमिका |
| यूएसए | ATACMS (आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम) | अमेरिकी सेना द्वारा प्रयुक्त; ~300 किमी रेंज; गहन-सटीकता के लिए प्रयुक्त |
| रूस | इस्कंदर-एम | अत्यधिक सटीक, गतिशील एसआरबीएम; प्रलय जैसे युद्धक्षेत्र में प्रयुक्त |
| ईरान | फतेह-110 | कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल; समान दूरी और पारंपरिक पेलोड |
स्रोत : द हिंदू
श्रेणी: पर्यावरण
संदर्भ: काजीरंगा टाइगर रिजर्व: भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व (2024)
मुख्य डेटा:
- बाघ घनत्व: 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी (भारत में तीसरा)
- बाघों की आबादी: 1,307 वर्ग किमी में 148 बाघ
- 2022 से वृद्धि: बिश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग को शामिल करने के कारण 104 बाघों से बढ़कर (27 बाघ जोड़े गए)
शीर्ष तीन बाघ घनत्व (2024):
- बांदीपुर (कर्नाटक): 19.83 बाघ/100 वर्ग किमी
- कॉर्बेट (उत्तराखंड): 19.56 बाघ/100 वर्ग किमी
- काजीरंगा (असम): 18.65 बाघ/100 वर्ग किमी
यह क्यों मायने रखती है:
- उन्नत कैमरा ट्रैप और स्थानिक विश्लेषण ने सटीक अनुमान सुनिश्चित किया।
- पर्यावास संरक्षण, भूदृश्य संपर्कता, तथा अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में सफलता पर प्रकाश डाला गया।
- यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अंतर्गत संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
Learning Corner:
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
अवलोकन:
- स्थान: असम, भारत (गोलाघाट, नागांव और कार्बी आंगलोंग जिलों में फैला हुआ)
- स्थापना: 1905 (आरक्षित वन के रूप में), 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: 1985 से
मुख्य तथ्य:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रसिद्ध | विश्व में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी |
| अन्य जीव-जंतु | बाघ, हाथी, जंगली भैंसे, दलदली हिरण, जलीय पक्षी |
| फ्लोरा/ पादप | लंबी हाथी घास, दलदली भूमि, उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले वन |
| नदी प्रणाली | ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों के किनारे स्थित है |
| बाघ अभयारण्य की स्थिति | 2006 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया |
| बाघ घनत्व (2024) | प्रति 100 वर्ग किमी में 18.65 बाघ – भारत में तीसरा सबसे अधिक (बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद) |
| कवर किया गया क्षेत्र | ~1,307 वर्ग किमी (नए जोड़े गए बिश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग सहित) |
पारिस्थितिक महत्व:
- पूर्वी हिमालय की तलहटी में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करता है।
- बाढ़ के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण।
- विश्व के उन कुछ क्षेत्रों में से एक जहां अनेक महाशाकाहारी जानवर (गैंडा, हाथी, भैंस) प्राकृतिक रूप से सह-अस्तित्व में रहते हैं।
स्रोत: द हिंदू
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
हाल ही में, बिहार में 271 से अधिक लड़कियों को बचाया गया, जिनमें से 153 को ऑर्केस्ट्रा में तस्करी के लिए भेजा गया था, तथा शेष 118 को देह व्यापार में धकेल दिया गया था।
पटना उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया और बिहार सरकार को ऐसे ऑर्केस्ट्रा में नाबालिगों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
यह घटना गरीबी, विनियमन की कमी और सामाजिक-सांस्कृतिक शोषण से प्रेरित प्रणालीगत बाल तस्करी पर प्रकाश डालती है।
बाल तस्करी क्या है?
संयुक्त राष्ट्र पालेर्मो प्रोटोकॉल के अनुसार, बाल तस्करी में शोषण के लिए बच्चों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति शामिल है , जिसमें जबरन श्रम, यौन शोषण और दासता शामिल है।
बाल तस्करी के सामान्य रूप
सुभेद्य बच्चों को कई प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- यौन शोषण : इसमें बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण या बाल यौन शोषण सामग्री का उत्पादन शामिल हो सकता है।
- जबरन मजदूरी: जब बच्चे कृषि, कारखानों, खनन या घरेलू श्रमिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कठोर परिस्थितियों में काम करते हैं।
- भीख मांगना और छोटे-मोटे अपराध: बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर करना या चोरी जैसे अन्य अपराध करना।
- सशस्त्र संघर्ष में बच्चे: संघर्ष के दौरान बच्चों को लड़ाकों के रूप में भर्ती किया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है, या उन्हें घरेलू दासता में रखा जाता है।
- बाल विवाह: लड़कियों की शादी धन या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए तीसरे पक्ष से कर दी जाती है, जो अक्सर हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा होता है।
- अवैध गोद लेना: शोषण के लिए शिशुओं और बच्चों की अवैध गोद लेने के लिए तस्करी करना, जो अक्सर उनके माता-पिता या अभिभावकों को धोखे से या दबाव डालकर होता है।
कभी-कभी बाल तस्करी के शिकार एक साथ कई तरह के शोषण का शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चे का यौन शोषण भी हो सकता है।
डेटा:
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान बचाए गए पीड़ितों (18 वर्ष से कम) की संख्या नीचे दी गई है:
| क्र.सं. | वर्ष | बचाए गए पीड़ित (18 वर्ष से कम) |
| 1 | 2018 | 2484 |
| 2 | 2019 | 2746 |
| 3 | 2020 | 2151 |
| 4 | 2021 | 2691 |
| 5 | 2022 | 3098 |
कई मामले पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते क्योंकि या तो परिवार इसमें शामिल होते हैं या फिर बोलने से डरते हैं
बच्चे शोषण के प्रति संवेदनशील कैसे हो जाते हैं?
- बाल तस्करी पारिवारिक अव्यवस्था, माता-पिता की देखभाल की कमी, गरीबी, असमानता और अपर्याप्त बाल संरक्षण के वातावरण में पनपती है।
- तस्कर अक्सर अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चों या परित्यक्त बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं।
- संघर्ष, आर्थिक चुनौतियां और पर्यावरणीय आपदाएं बच्चों, विशेषकर अकेले या अलग-थलग पड़े प्रवासी बच्चों को तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती हैं।
- तस्कर बच्चों से संपर्क करने, उनका शोषण करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और डार्क वेब का भी इस्तेमाल करते हैं। वे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पहचान से बचते हैं और शोषणकारी सामग्री का प्रसार करते हैं। बच्चों द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग, अक्सर बिना उचित सुरक्षा उपायों के, उन्हें तस्करों के और भी ज़्यादा शिकार बना सकता है।
बिहार तस्करी का गढ़ क्यों बन गया है?
विनियमन और निरीक्षण का अभाव
-
ऑर्केस्ट्रा समूहों या नृत्य मंडलियों पर निगरानी रखने के लिए कोई सख्त नियामक ढांचा मौजूद नहीं है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियां तस्करी के मोर्चों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने में विफल रहती हैं।
- स्थानीय स्तर पर निगरानी का अभाव तस्करी नेटवर्क को फलने-फूलने में सक्षम बनाता है।
भूगोल
- नेपाल के साथ राज्य की छिद्रपूर्ण सीमा तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और उत्तर प्रदेश जैसे तस्करी-प्रवण राज्यों के साथ निर्बाध रेलवे संपर्क, बिहार के माध्यम से तस्करी के प्रवाह को सुगम बनाता है।
सांस्कृतिक आकांक्षाओं का शोषण
- पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संगीत और नृत्य को मूल्यवान माना जाता है।
- तस्कर नृत्य प्रशिक्षण , रंगमंच कैरियर या फिल्म के अवसरों के माध्यम से इन आकांक्षाओं का फायदा उठाते हैं और माता-पिता को सुनिश्चित आय और प्रसिद्धि का भरोसा दिलाते हैं।
‘ऑर्केस्ट्रा बेल्ट’ की उपस्थिति
- सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में – जिन्हें ‘ऑर्केस्ट्रा बेल्ट’ कहा जाता है – 12 साल की उम्र तक की लड़कियों को 10,000 रुपये जैसी मामूली रकम में ऑर्केस्ट्रा को बेचा जा रहा है।
- उन्हें अनुचित कपड़े पहनने और नशे में धुत पुरुषों के सामने अश्लील गानों पर नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है।
बाल तस्करी पीड़ितों और समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है?
इस अपराध के बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक विकास पर विनाशकारी परिणाम होते हैं।
- पीड़ितों को प्रायः आजीवन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, गंभीर आघात संबंधी विकारों, चिंता, अवसाद और सामाजिक एकीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- बाल तस्करी स्वस्थ सामाजिक संरचनाओं को कमजोर करती है तथा गरीबी और शोषण के चक्र को जारी रखती है।
- इससे बचपन नष्ट हो जाता है और तस्करी के शिकार बच्चे जब स्वयं माता-पिता बन जाते हैं तो वे हिंसा और शोषण के चक्र में फंस जाते हैं; इससे शिक्षा बाधित होती है और सामुदायिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
बाल तस्करी के खिलाफ कानून और मुद्दे
1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए)
- व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए अधिनियमित
- वेश्यालय चलाना, वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिगों को खरीदना या हिरासत में रखना जैसी गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है।
- पीड़ितों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए कानून प्रवर्तन को शक्तियां प्रदान करता है।
2.किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- कानून के साथ संघर्षरत या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसमें बाल तस्करी, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से निपटने के प्रावधान शामिल हैं।
- मामलों के निपटान के लिए बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना करता है।
3.यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
- बच्चों को यौन शोषण, हमले और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए एक व्यापक कानून।
- अपराधों की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और सुनवाई के लिए बाल-अनुकूल प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
- इसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है तथा कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
4.बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल बंधन सहित सभी प्रकार के बंधुआ और बलात् श्रम को समाप्त किया गया।
- बंधुआ मजदूरी की ओर ले जाने वाले किसी भी समझौते को शून्य एवं अमान्य घोषित करना।
- जिला मजिस्ट्रेटों को बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और पुनर्वास करने का अधिकार दिया गया है।
5.बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016)
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में तथा किशोरों (14-18 वर्ष) को खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर प्रतिबंध है।
- केवल विशिष्ट परिस्थितियों में पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति है।
- नियोक्ताओं के लिए दंड और प्रवर्तन के लिए तंत्र निर्धारित करता है।
6.भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत प्रावधान
- यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लेता है और इसमें बाल तस्करी, जबरन श्रम और यौन शोषण से संबंधित अपराध शामिल हैं।
- नाबालिगों की तस्करी और बार-बार अपराध करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
- कठोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के माध्यम से पीड़ित-केंद्रित न्याय पर जोर दिया गया।
7.कमियाँ
- कानून व्यापक हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता
- दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है
- अधिकांश मामले “लापता व्यक्ति” या “अपहरण” के रूप में दर्ज किए जाते हैं
- मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTUs) को अपर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त है
- कई राज्यों से संबंधित जांच अक्सर क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम और नौकरशाही देरी के कारण विफल हो जाती हैं।
- जब लड़कियों को बचाया जाता है, तो उनमें से कई को उन्हीं परिवारों के पास वापस भेज दिया जाता है, जिन्होंने उन्हें बेचा था।
तस्करी विरोधी प्रयासों की रोकथाम और प्रवर्तन के लिए प्रमुख उपाय
- स्कूल और समुदाय-आधारित रोकथाम
- छात्रों की उपस्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए ।
- यदि कोई बच्चा लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है , तो उसे अलर्ट और अनिवार्य रिपोर्टिंग शुरू कर देनी चाहिए।
- गांवों से बाहर जाने वाले या गांवों में आने वाले बच्चों पर नज़र रखने के लिए प्रवास रजिस्टर बनाए रखना चाहिए ।
- तस्करी के खतरों के बारे में परिवारों को जानकारी देने के लिए अभिभावक संवेदीकरण कार्यक्रम आवश्यक हैं।
- परिवहन सतर्कता को मजबूत करना
- रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को संवेदनशील गलियारों की निगरानी जारी रखनी चाहिए तथा स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- इस मॉडल को अंतर-राज्यीय बस मार्गों, स्थानीय टर्मिनलों और निजी वाहकों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।
- परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तस्करी के संकेतों को पहचानने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) में सुधार
- इस मॉडल को अंतर-राज्यीय बस मार्गों, स्थानीय टर्मिनलों और निजी वाहकों तक विस्तारित किया जाना चाहिए। परिवहन विभागों को अपने कर्मचारियों को तस्करी के संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
- श्रम और न्याय तंत्र को मजबूत करना
- श्रम विभाग को निरीक्षण, रिपोर्ट और कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- अभियोजन समयबद्ध होना चाहिए तथा पुनर्वास दीर्घकालिक एवं राज्य-पर्यवेक्षित होना चाहिए।
- बच्चों को ऐसे वातावरण में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उनका शोषण हुआ हो।
- पीड़ित मुआवजा योजनाओं को बिना किसी देरी के सक्रिय और कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।
रोकथाम की दिशा में कदम: “पिकेट” रणनीति (“PICKET” Strategy)
बाल तस्करी को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण:
- P – नीति (Policy): बाल शोषण के विरुद्ध स्पष्ट, शून्य-सहिष्णुता नीतियां।
- I – संस्थाएँ (Institutions): निगरानी, अभियोजन और पुनर्वास के लिए समर्पित इकाइयाँ
- C – अभिसरण (Convergence): साझा डिजिटल डेटा के साथ अंतर-एजेंसी सहयोग।
- K – ज्ञान (Knowledge): जमीनी स्तर पर जागरूकता और उत्तरजीवी-सूचित बुद्धिमत्ता।
- E – अर्थव्यवस्था (Economy): जब्ती और दंड के माध्यम से तस्करी को वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बनाना।
- T – प्रौद्योगिकी (Technology): पैटर्न और मार्गों का पता लगाने के लिए एआई, हीटमैप्स, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
भारत में बाल तस्करी केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढाँचों की व्यवस्थागत विफलता है। इस संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
हाल के दशकों में, भारत के औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र ने अपने रोजगार ढांचे में महत्वपूर्ण नकारात्मक परिवर्तन देखा है।
उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, विनिर्माण कार्यबल में ठेका श्रमिकों की हिस्सेदारी 1999-2000 में 20% से बढ़कर 2022-23 में 40.7% हो गई है, जो सभी उद्योगों में है।
संविदाकरण का दुरुपयोग उत्पादकता के लिए हानिकारक है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि को बनाए रखने के लिए औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।
संविदात्मक नौकरियाँ (Contractual jobs) क्या हैं?
- संविदात्मक नौकरियों में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध द्वारा परिभाषित एक विशिष्ट अवधि या परियोजना के आधार पर काम करना शामिल होता है।
- ये नौकरियाँ पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकती हैं, और उनकी अवधि में काफी अंतर हो सकता है।
- संविदात्मक कार्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना विशिष्ट आवश्यकताओं या परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा मिलती है।
संविदा मजदूरों के मुद्दे (Issues of contract labours)
संविदाकरण के पीछे प्राथमिक प्रेरणा कौशल या अनुकूलनशीलता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि श्रम लागत को कम करना और मूल श्रम कानूनों के तहत कानूनी दायित्वों को दरकिनार करना है।
भारत में ठेका मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें असमान वेतन, नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव और शोषण के प्रति संवेदनशीलता शामिल है।
ये मुद्दे कई कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, जैसे श्रम कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन, श्रमिकों में जागरूकता की कमी, तथा अनुबंध रोजगार की अंतर्निहित प्रकृति, जो अक्सर श्रमिक कल्याण की तुलना में लचीलेपन को प्राथमिकता देती है।
कुछ मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:
- ठेका श्रमिक नियमित श्रमिकों की तुलना में औसतन 14.5% कम कमाते हैं। बड़े उद्यमों में वेतन का अंतर बढ़कर 31% हो जाता है, जो व्यवस्थित शोषण का संकेत देता है। कुछ उद्योगों में, नियोक्ता नियमित कर्मचारियों की तुलना में ठेका श्रमिकों पर 50-85% कम खर्च करते हैं।
- ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे जाने के कारण, ये श्रमिक अक्सर औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे कानूनों के तहत प्रमुख सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाते हैं, जिससे वे अनुचित बर्खास्तगी और खराब कार्य स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- अल्पकालिक अनुबंधों के कारण श्रमिकों का उच्च टर्नओवर होता है और कौशल विकास या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में निवेश हतोत्साहित होता है, जिससे श्रमिकों की दीर्घकालिक रोजगार क्षमता और फर्म-स्तरीय नवाचार दोनों को नुकसान पहुंचता है।
उत्पादकता पर प्रभाव
संविदा कर्मचारियों को विशिष्ट भूमिकाओं या अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और ये कंपनियों को, खासकर अस्थिर बाज़ारों में, लचीला बने रहने में मदद करते हैं। ये दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना, परिचालन को तेज़ी से बढ़ाने या घटाने में मदद करते हैं।
हालाँकि, दीर्घकालिक प्रभाव इस प्रकार हैं:
- प्रिंसिपल-एजेंट समस्या दो पक्षों (इस मामले में, नियोक्ता (प्रिंसिपल) और ठेकेदार (एजेंट)) के बीच लक्ष्यों के गलत संरेखण को संदर्भित करती है । ठेकेदार नियोक्ता के गुणवत्ता मानकों की तुलना में अपने लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब पर्यवेक्षण और अकुशल श्रम उपयोग होता है ।
- संविदा कार्य में, श्रमिक अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं, जिससे नैतिक जोखिम पैदा हो सकता है , क्योंकि उन्हें पता है कि नियोक्ता और ठेकेदार के बीच जवाबदेही विभाजित है।
- संविदात्मक नौकरियाँ आमतौर पर अल्पकालिक होती हैं , जिससे टर्नओवर दर ऊँची हो जाती है। यह नियोक्ताओं को कौशल विकास या नवाचार में निवेश करने से रोकता है , जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- नियमित श्रम-गहन (आरएलआई) उद्यमों की तुलना में अनुबंध श्रम-गहन (सीएलआई) उद्यमों में श्रम उत्पादकता ( प्रति श्रमिक वास्तविक शुद्ध मूल्यवर्धन के रूप में मापी गई ) 31% कम है।
- छोटे उद्यमों (100 से कम श्रमिकों) में , अनुबंध श्रमिकों पर अधिक निर्भरता के कारण यह अंतर 36% तक बढ़ जाता है
- मध्यम उद्यमों (100-300 श्रमिक) में 23% का अंतर है , जबकि श्रम-प्रधान क्षेत्रों में सबसे खराब स्थिति है – जहां 42% उत्पादकता घाटा है।
- पूँजी-प्रधान उद्यम : पूँजी-प्रधान कंपनियाँ मानव श्रम की तुलना में मशीनों पर अधिक निर्भर करती हैं। ऐसी फर्मों में, ठेका श्रमिक तब भी उत्पादक हो सकते हैं क्योंकि उनका उपयोग सहायक भूमिकाओं में किया जाता है। ये कंपनियाँ 17% उत्पादकता वृद्धि दर्शाती हैं , लेकिन औपचारिक विनिर्माण में इनका योगदान केवल 20% है ।
कुछ अपवादों को छोड़कर, 80% औपचारिक उद्यम अत्यधिक संविदा /ठेका प्रथा के कारण पीड़ित हैं। यह दीर्घावधि में उत्पादकता , रोज़गार सुरक्षा और आर्थिक विकास को कमज़ोर करता है।
आवश्यक कदम
औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता लागू करना (2020)
-
केंद्र सरकार ने 2020 में औद्योगिक संबंधों पर एक श्रम संहिता पेश की, जिसका उद्देश्य नियुक्ति और बर्खास्तगी में अधिक लचीलापन प्रदान करना है। यह संहिता कंपनियों को बिना किसी तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के सीधे निश्चित अवधि के अनुबंधों पर गैर-नियमित कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देती है, हालाँकि यह बुनियादी वैधानिक रोजगार लाभों के प्रावधान को अनिवार्य करके अस्थायी कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लगाने का भी प्रयास करती है।
- हालांकि, श्रम संहिता के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा के बीच श्रमिक संघों ने चेतावनी दी है कि गैर-नियमित श्रमिकों को काम पर रखने में लचीलेपन में वृद्धि से अनौपचारिकीकरण में तेजी आ सकती है तथा औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की गुणवत्ता और अधिक खराब हो सकती है।
लंबी अवधि के निश्चित अनुबंधों को प्रोत्साहित करना:
- नीति निर्माता लंबी अवधि के अनुबंध अपनाने वाली कंपनियों को सामाजिक सुरक्षा योगदान में रियायत दे सकते हैं।
- इससे कम्पनियों को सरकारी कौशल कार्यक्रमों तक सब्सिडीयुक्त पहुंच भी मिल सकेगी।
- इससे कार्यबल में स्थिरता, कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा अनिश्चित रोजगार के संबंध में यूनियन की चिंताओं का समाधान होगा।
प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY):
- विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू किया गया।
- सरकार ने नये कर्मचारियों के लिए ईपीएस और ईपीएफ में नियोक्ता के 12% अंशदान का भुगतान किया।
- मार्च 2022 में बंद होने से पहले 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।
- औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा औपचारिक क्षेत्र में ठेका श्रम पर निर्भरता कम करने के लिए योजना को पुनर्जीवित तथा विस्तारित किया जाएगा।
Value Addition: भारत में संविदा श्रम को नियंत्रित करने वाले कानून
- संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970: यह संविदा श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करता है और कुछ मामलों में इसके उन्मूलन का प्रयास करता है। यह कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा और मजदूरी जैसे बुनियादी कल्याणकारी प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन कमजोर है।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं): यह नियोक्ताओं द्वारा सीधे निश्चित अवधि के रोजगार की अनुमति देता है और गैर-स्थायी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को अनिवार्य करता है, तथा तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के बिना अनुबंध भूमिकाओं को औपचारिक बनाने का प्रयास करता है।
- कारखाना अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 संविदा कर्मियों सहित सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं, लेकिन इनका प्रवर्तन अपर्याप्त है।
- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम निर्माण क्षेत्र में ठेका श्रमिकों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
निष्कर्ष
यदि संविदा श्रम का उपयोग उच्च-कौशल वाले क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के साथ रणनीतिक रूप से किया जाए, तो यह औद्योगिक लचीलेपन में योगदान दे सकता है। हालाँकि, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लागत-कटौती के साधन के रूप में इसका अत्यधिक उपयोग प्रतिकूल परिणाम दे सकता है।
समावेशी विकास और दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए भारत को शोषणकारी अनौपचारिकीकरण से वास्तविक औपचारिकीकरण की ओर बढ़ना होगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“भारत के औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में श्रम का बढ़ता हुआ संविदाकरण (contractualisation) श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक उत्पादकता दोनों को कमजोर करता है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)