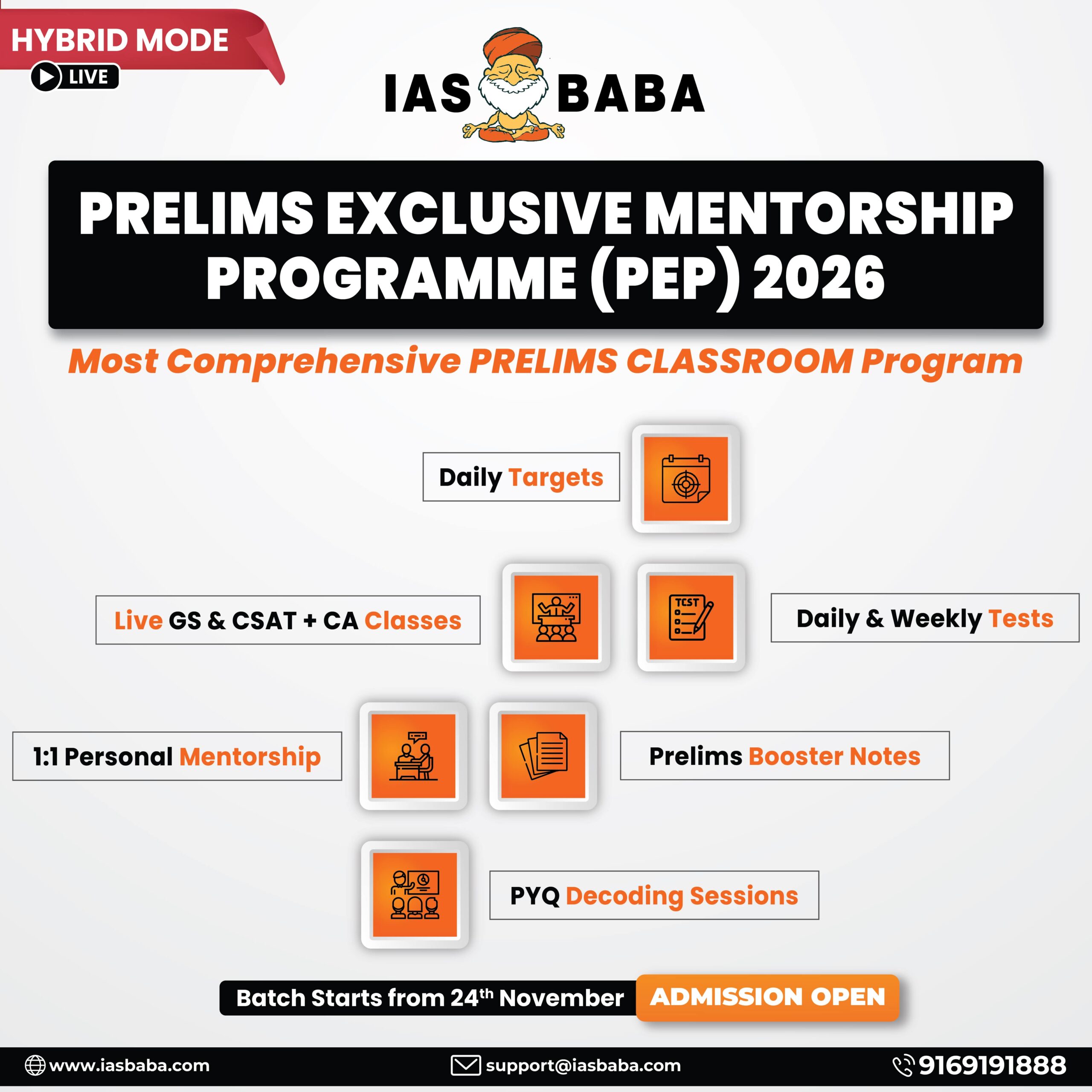IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: इतिहास
प्रसंग: तमिलनाडु में आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष
उत्पत्ति और विवरण
- 1925 में जाति और लिंग पदानुक्रम के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ।
- इसका नेतृत्व पेरियार ई.वी. रामासामी ने किया, जिन्होंने तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरासु (Kudi Arasu) का उपयोग उग्रवादी, गैर-ब्राह्मण विचारों को फैलाने के लिए किया।
राजनीतिक प्रभाव
- पेरियार ने कांग्रेस की जातिवादी राजनीति का मुकाबला करने के लिए जस्टिस पार्टी के साथ मिलकर उग्र गैर-ब्राह्मणवाद की वकालत की।
- उच्च जाति के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए एक वैकल्पिक सामाजिक सुधार एजेंडा पेश किया।
कट्टरपंथी सामाजिक सुधार
- आत्म-सम्मान विवाह को लोकप्रिय बनाया, महिलाओं के अधिकारों (पुनर्विवाह, संपत्ति) को बढ़ावा दिया, और सार्वजनिक बहस का विस्तार किया।
- कुडी अरासु ने जाति और लिंग पर कट्टरपंथी दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिससे हिंदू समाज में सुधार प्रभावित हुए।
जस्टिस पार्टी की भूमिका
- दक्षिण भारतीय उदारवादी महासंघ ने गैर-ब्राह्मणों को सशक्त बनाया और राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाया।
- हालाँकि, गैर-कुलीन गैर-ब्राह्मण अक्सर हाशिए पर ही रहे।
विरासत और मान्यता
- गैर-ब्राह्मण जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और गौरव को बढ़ावा दिया।
- इसकी विरासत ने जातिगत गतिशीलता, लैंगिक राजनीति और सामाजिक सुधार को नया रूप दिया, तथा समकालीन तमिल समाज में इसकी प्रासंगिकता बरकरार रखी।
Learning Corner:
ई.वी. रामास्वामी (पेरियार)
- जन्म: 17 सितंबर 1879, इरोड, तमिलनाडु
- इस नाम से जाना जाता है: पेरियार (“महान व्यक्ति”)
सामाजिक सुधार में भूमिका
- जाति पदानुक्रम, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और लैंगिक असमानता को चुनौती देने के लिए आत्म-सम्मान आंदोलन (1925) की स्थापना की।
- धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को खारिज करते हुए तर्कवाद, नास्तिकता और सामाजिक न्याय की वकालत की।
- अस्पृश्यता, वंशानुगत जातिगत विशेषाधिकारों और राजनीति एवं समाज में उच्च जातियों के प्रभुत्व का कड़ा विरोध किया।
राजनीतिक जुड़ाव
- प्रारम्भ में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी के साथ गठबंधन किया और राजनीति और शिक्षा में गैर-ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास किया।
- द्रविड़ विचारधारा को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसने बाद में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों को प्रभावित किया।
प्रमुख सुधार
- आत्म-सम्मान विवाह को बढ़ावा दिया (ब्राह्मण पुजारियों के बिना, समानता पर आधारित)।
- महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया: विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और बाल विवाह का विरोध।
- तर्कवादी और समतावादी विचारों को फैलाने के लिए पत्रकारिता (कुडी अरासु साप्ताहिक) और सार्वजनिक बहस का इस्तेमाल किया।
परंपरा
- “द्रविड़ आंदोलन के जनक” के रूप में सम्मानित।
- तमिल समाज, राजनीति और सामाजिक न्याय पर अमिट छाप छोड़ी।
- उनके विचार दक्षिण भारत में जाति, तर्कवाद और सामाजिक सुधार पर बहस को आकार देते रहे हैं।
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
संदर्भ: व्लादिवोस्तोक में एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत
मुख्य अंश
- केंद्रित , खुले, निष्पक्ष और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई ।
- विकास- केन्द्रित व्यापार एजेंडे का आह्वान किया गया, जिसमें शामिल हैं:
- खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान।
- विकासशील देशों के लिए प्रभावी विशेष एवं विभेदक उपचार।
- दो स्तरीय डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली की बहाली का आग्रह किया गया।
- पारदर्शी निर्यात उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया, दुरुपयोग और कृत्रिम कमी के खिलाफ चेतावनी दी गई।
- साझा समृद्धि के लिए निर्यात विविधीकरण, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और एमएसएमई एकीकरण पर जोर दिया गया।
व्यापक प्राथमिकताएँ
- भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (यूपीआई, ओएनडीसी) को प्रदर्शित किया गया तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षित डिजिटलीकरण पर एससीओ सहयोग का प्रस्ताव रखा गया।
- व्यापार से जुड़े भेदभाव का विरोध करते हुए, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जलवायु कार्रवाई की वकालत की।
- एवीजीसी क्षेत्र (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) को नौकरियों, निर्यात और रचनात्मक उद्योगों के संचालक के रूप में रेखांकित किया गया।
महत्व
- विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से नियम-आधारित, निष्पक्ष और समावेशी व्यापार को मजबूत करना।
- एससीओ के भीतर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और सतत विकास को बढ़ावा देता है।
Learning Corner:
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
- स्थापना: 1 जनवरी 1995 (GATT, 1947 का स्थान लेते हुए)।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- सदस्यता: 164 सदस्य (भारत सहित)।
उद्देश्य
- स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- व्यापार वार्ता और विवादों के निपटारे के लिए एक मंच प्रदान करना।
- सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) और राष्ट्रीय उपचार सिद्धांतों के माध्यम से गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना।
- विशेष एवं विभेदक उपचार (एस एंड डी टी) के माध्यम से विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना।
मूलभूत प्रकार्य
- विश्व व्यापार संगठन समझौतों (माल, सेवाओं और बौद्धिक संपदा पर – TRIPS, GATS, AoA) का प्रशासन करता है।
- व्यापार विवाद निपटान: दो स्तरीय प्रणाली संचालित होती है – पैनल और अपीलीय निकाय।
- निगरानी और पारदर्शिता: समीक्षाओं के माध्यम से सदस्यों की व्यापार नीतियों की देखरेख करना।
- क्षमता निर्माण: विकासशील/अल्पविकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण।
वर्तमान मुद्दे
- अपीलीय निकाय संकट: न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अमेरिकी विरोध के कारण 2019 से कार्य नहीं कर रहा है।
- कृषि वार्ता: खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी और सार्वजनिक भंडारण पर विवाद।
- डिजिटल व्यापार: ई-कॉमर्स और डेटा प्रवाह संबंधी नियमों पर विवाद।
- विकासशील देशों की चिंताएं: अधिक निष्पक्ष S&DT प्रावधानों की आवश्यकता।
महत्व
- एकतरफावाद को रोकते हुए नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है।
- वैश्विक व्यापार में पूर्वानुमान, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, जलवायु से जुड़े व्यापार मुद्दे और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रमुख मंच।
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: इतिहास
प्रसंग: “ब्रह्मपुत्र के कवि” भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी मनाई जा रही है।
- इसका नाम उनके प्रतिष्ठित गीत बिस्टिर्ना परोरे के नाम पर रखा गया है, जो एकता और सांस्कृतिक लचीलेपन का प्रतीक है।
- इसकी शुरुआत डिब्रूगढ़ के गुइजान में हुई, जिसमें हजारिका के गीतों की लाइव प्रस्तुति, लोक प्रदर्शन और मोरन, मोटोक, टी ट्राइब, सोनोवाल कछारी, देउरी और गोरखा जैसे समुदायों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे।
डॉ. भूपेन हजारिका की संगीत विरासत
- ओल मैन नदी से प्रेरित बिस्टिर्ना परोरे ने ब्रह्मपुत्र को मानव संघर्ष, न्याय और एकजुटता के रूपक में बदल दिया।
- उनके संगीत ने कई पीढ़ियों को एकजुट किया, असम की संस्कृति को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया तथा शांति और भाईचारे का प्रतीक बनाया।
महत्व
- यह हजारिका के अद्वितीय प्रभाव के प्रति जीवंत श्रद्धांजलि है।
- ब्रह्मपुत्र के किनारे असम की सांस्कृतिक विविधता, रचनात्मकता और सामूहिक भावना का जश्न मनाता है।
Learning Corner:
डॉ. भूपेन हजारिका
- जन्म: 8 सितंबर 1926, सदिया, असम
- ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में प्रसिद्ध
- पेशा: गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, फिल्म निर्माता और सांस्कृतिक प्रतीक।
योगदान
- असमिया लोक परंपराओं में निहित गीतों के माध्यम से लोगों के संघर्षों, आशाओं और एकता को आवाज दी।
- उनका प्रतिष्ठित गीत बिस्टिरना परोरे ने ब्रह्मपुत्र को न्याय, एकजुटता और लचीलेपन के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया (ओल मैन नदी से प्रेरित)।
- असमिया और पूर्वोत्तर संस्कृति को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर लाया गया।
- संगीत और फिल्मों के माध्यम से शांति, सार्वभौमिक भाईचारे और सामाजिक न्याय के विषयों की वकालत की।
- असमिया, बंगाली और हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिससे क्षेत्रीय संगीत राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गया।
मान्यताएं
- भारत रत्न (2019) – भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
- पद्म विभूषण (2012, मरणोपरांत), पद्म भूषण (2001)।
- भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार (1992) से सम्मानित।
परंपरा
- असम और पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक एकीकरणकर्ता के रूप में सम्मानित।
- उन्होंने सामाजिक रूप से जागरूक कला की एक विरासत छोड़ी जो न्याय, समानता और सांस्कृतिक गौरव के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रही है।
- उनकी शताब्दी असम और उसके बाहर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई जाती है।
स्रोत : पीआईबी
श्रेणी: इतिहास
प्रसंग: श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि
- प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा समानता, करुणा और सार्वभौमिक भाईचारे के उनके दृष्टिकोण को याद किया।
- सामाजिक सुधार और शिक्षा पर गुरु की शिक्षाओं की प्रगतिशील और समावेशी समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में प्रशंसा की गई।
- केरल के एक प्रतिष्ठित सुधारक और आध्यात्मिक नेता, उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और न्याय, सशक्तिकरण और नैतिक शक्ति को बढ़ावा दिया।
- उनकी विरासत समकालीन भारत में एकता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समानता को प्रेरित करती रहती है।
Learning Corner:
श्री नारायण गुरु (1855-1928)
प्रारंभिक जीवन
- 1855 में केरल के तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाझांती में एझावा समुदाय में जन्म।
- एक दार्शनिक, संत और समाज सुधारक जिन्होंने केरल में कठोर जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी।
प्रमुख शिक्षाएँ और दर्शन
- “मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर” (एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति) की वकालत की।
- सशक्तिकरण के मार्ग के रूप में शिक्षा, आध्यात्मिक उत्थान और सामाजिक समानता पर जोर दिया गया।
- जाति-आधारित भेदभाव और कर्मकाण्डीय प्रथाओं को अस्वीकार किया।
समाज सुधार
- अरुविप्पुरम (1888) में शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की , जिससे मंदिर में प्रवेश और पुरोहिताई में जातिगत एकाधिकार टूट गया।
- शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए 1903 में डॉ. पालपू और कुमारन आसन के साथ एसएनडीपी योगम (श्री नारायण धर्म परिपालन योगम) की स्थापना की।
- अंतर्जातीय भोजन और विवाह को बढ़ावा दिया, तथा पूजा में तर्कसंगत, नैतिक प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया।
परंपरा
- महात्मा गांधी जैसे बाद के नेताओं को इससे प्रेरणा मिली, जिन्होंने 1925 में उनसे मुलाकात की और उनके सुधारवादी दृष्टिकोण की प्रशंसा की।
- केरल के पुनर्जागरण और सामाजिक न्याय आंदोलन को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
- समानता, करुणा, सार्वभौमिक भाईचारे और शिक्षा-संचालित सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: अर्थशास्त्र
प्रसंग: भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह निम्न स्तर पर।
- 8% (2021-2024) से अधिक औसत जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत में पूंजी प्रवाह 15 साल के निचले स्तर पर है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कमज़ोर बना हुआ है, केवल 2021-22 में ही उल्लेखनीय निवेश हुआ है। मज़बूत जीडीपी वृद्धि वाली हालिया तिमाहियाँ भी महत्वपूर्ण पूंजी आकर्षित करने में विफल रहीं।
भुगतान संतुलन
- व्यापार घाटा जारी है, लेकिन सेवा निर्यात और धन प्रेषण ने चालू खाते को सहारा दिया है।
- हालाँकि, इन अदृश्य कारकों के कारण पूंजी निवेश में वृद्धि नहीं हुई है।
कम अंतर्वाह के कारण
- एफपीआई की निकासी और निजी इक्विटी/उद्यम निधियों के निकासी के कारण मजबूत बहिर्वाह।
- उच्च स्टॉक मूल्यांकन, वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, तथा सख्त सीमापार वित्तपोषण नियम, अंतर्वाह को और सीमित कर देते हैं।
आशय
- लगातार कम विदेशी पूंजी के कारण भविष्य में विकास के लिए वित्तपोषण के विकल्प सीमित हो सकते हैं।
- भारत को विस्तार के लिए पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करने के लिए निवेश माहौल और नीतिगत उपायों पर ध्यान देना होगा।
Learning Corner:
बाह्य व्यापार और भुगतान संतुलन (BoP) – विस्तृत नोट
बाह्य व्यापार की परिभाषा
बाह्य व्यापार किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी के आदान-प्रदान को कहते हैं। यह किसी देश के आर्थिक विकास, विदेशी मुद्रा अर्जन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बाह्य व्यापार के घटक
निर्यात
- घरेलू संस्थाओं द्वारा विदेशी देशों को बेची गई वस्तुएं या सेवाएं।
- प्रकार:
- व्यापारिक निर्यात: भौतिक वस्तुएं जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद।
- सेवा निर्यात: आईटी सेवाएं, पर्यटन, परामर्श, परिवहन।
आयात
- विदेशी देशों से खरीदी गई वस्तुएं या सेवाएं।
- प्रकार:
- व्यापारिक आयात: कच्चा तेल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स।
- सेवा आयात: परामर्श, पर्यटन, सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग।
दृश्य और अदृश्य व्यापार
- दृश्य व्यापार: केवल भौतिक वस्तुओं में व्यापार; व्यापारिक निर्यात और आयात के माध्यम से मापा जाता है।
- अदृश्य व्यापार: सेवाओं, आय और हस्तांतरण में व्यापार। इसमें शामिल हैं:
- सेवाएँ: आईटी, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन।
- आय: ब्याज, लाभांश, विदेशी निवेश से प्राप्त लाभ।
- स्थानान्तरण: अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धन, विदेशी सहायता, अनुदान, दान।
भुगतान संतुलन (बीओपी)
भुगतान संतुलन (BoP) किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन-देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों का उचित लेखा-जोखा रखा जाए।
बीओपी घटक:
चालू खाता
- माल, सेवाओं, आय और स्थानान्तरण से संबंधित सभी लेनदेन रिकॉर्ड करता है।
- उप-घटक:
- व्यापार संतुलन (BoT): व्यापारिक निर्यात और आयात के बीच का अंतर।
- BoT अधिशेष: निर्यात > आयात
- BoT घाटा: आयात > निर्यात
- शुद्ध सेवाएँ: सेवाओं में व्यापार (आईटी, पर्यटन, परिवहन, रॉयल्टी)।
- शुद्ध आय: विदेश में निवेश से आय (ब्याज, लाभांश, लाभ)।
- शुद्ध स्थानान्तरण: प्रेषण, विदेशी सहायता, अनुदान।
- व्यापार संतुलन (BoT): व्यापारिक निर्यात और आयात के बीच का अंतर।
महत्त्व:
- किसी देश की अल्पकालिक बाह्य आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
- चालू खाता घाटा विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भरता को दर्शाता है।
पूंजी खाता (वित्तीय खाता)
- सीमा पार वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है जो राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व को बदल देता है।
- अवयव:
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): विदेश में व्यापार/उद्योग में या विदेशियों द्वारा घरेलू व्यापार में निवेश।
- पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई): स्टॉक, बांड और प्रतिभूतियों में निवेश।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी): घरेलू संस्थाओं द्वारा विदेश से लिया गया ऋण।
- बैंकिंग पूंजी एवं एनआरआई जमा: बैंकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा निधियों का संचलन।
- अन्य निवेश: व्यापार ऋण, ऋण, मुद्रा जमा।
महत्त्व:
- चालू खाता घाटे के वित्तपोषण का समर्थन करता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता को प्रभावित करता है।
BoP पहचान और लेखांकन
- लेखांकन की दृष्टि से, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है:
- चालू खाते में किसी भी घाटे की भरपाई पूंजी खाते में अधिशेष या विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन से हो जाती है।
- लगातार असंतुलन से मुद्रा स्थिरता प्रभावित हो सकती है और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
भुगतान संतुलन का महत्व
- आर्थिक विकास: निर्यात से सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है।
- विदेशी मुद्रा भंडार: मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और आयात आवश्यकताओं को पूरा करना।
- निवेश का माहौल: पूंजी प्रवाह प्रौद्योगिकी, कौशल और वित्त को आकर्षित करता है।
- नीति निर्माण: सरकार को व्यापार, निवेश और मौद्रिक नीतियों की योजना बनाने में मदद करता है।
- वैश्विक एकीकरण: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी को बढ़ावा देता है।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
भारतीय शहर देश के आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन में सबसे आगे हैं। 2030 तक, ये 70% नए रोज़गार पैदा करेंगे, और 2050 तक भारत की शहरी आबादी एक अरब के क़रीब पहुँच जाएगी।
नये बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का सामना करने की आवश्यकता होगी।
इसलिए यह आवश्यक होगा कि जलवायु-अनुकूल शहरी डिजाइन और बुनियादी ढांचे में शीघ्र निवेश किया जाए, ताकि अरबों डॉलर के वार्षिक नुकसान को रोका जा सके और अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सके।
भारतीय शहरों के लिए प्रमुख जोखिम और समाधान
पानी की बाढ़
- बाढ़ भारतीय शहरों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है।
- तेजी से हो रहे आवास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के कारण, दो तिहाई से अधिक शहरी निवासियों को वर्षा या सतही बाढ़ का सामना करना पड़ेगा।
- अनुमानित आर्थिक नुकसान: 2030 तक 5 बिलियन डॉलर और 2070 तक 30 बिलियन डॉलर।
- इस जोखिम से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं:
-
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को नो-बिल्ड जोन के रूप में चिन्हित करना।
- शहरव्यापी जल निकासी प्रणालियों का विस्तार और उन्नयन।
- अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना।
- बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- उदाहरण:
- ब्राजील, जो अब 80% शहरी है, संरचनात्मक बाढ़ नियंत्रण से एकीकृत, प्रकृति-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो गया है।
- कोलकाता में शहर स्तर पर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली लागू की गई।
- चेन्नई में तूफानी जल प्रबंधन और बाढ़ की तैयारी को बढ़ाया जा रहा है, तथा संवेदनशील आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
अत्यधिक गर्मी
- शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के कारण शहर का रात्रिकालीन तापमान वर्ष भर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 3°C से 5°C तक बढ़ जाता है।
- 21वीं सदी में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है।
- शहर अहमदाबाद की हीट एक्शन प्लान को एक मॉडल के रूप में अपना सकते हैं।
- प्रमुख उपायों में शामिल हैं:
-
- वृक्ष आवरण और हरित छतरियों में वृद्धि।
- गर्मी को रोकने वाली छतों को ठंडी छतों से बदलना।
- बाहरी श्रमिकों के लिए कार्य घंटे समायोजित करना।
- प्रमुख शहरों में इन कार्यों को बढ़ाने से:
- प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु को टाला जा सकता है।
- गर्मियों के चरम महीनों के दौरान आर्थिक उत्पादकता की सुरक्षा करना।
खराब परिवहन बुनियादी ढांचा
- शहरी उत्पादकता के लिए परिवहन की दक्षता महत्वपूर्ण है।
- भारत की एक-चौथाई से अधिक शहरी सड़कें बाढ़ की चपेट में हैं।
- कुछ शहरों में, केवल 10-20% सड़कों के जलमग्न होने से आधे से अधिक परिवहन प्रणालियां बाधित हो सकती हैं।
- बाढ़-जोखिम मानचित्रण, बेहतर जल निकासी, वैकल्पिक मार्ग, तथा बाढ़ सुरक्षा और सड़क रखरखाव में निवेश, व्यवधानों को रोकने के लिए आवश्यक हैं।
- अपशिष्ट संग्रहण और अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण जैसी नगरपालिका सेवाओं के आधुनिकीकरण में बड़े निवेश की आवश्यकता है।
जलवायु-अनुकूल शहरों का निर्माण कैसे करें?
- जलवायु-जोखिम मूल्यांकन और शहरी नियोजन मानदंडों के प्रवर्तन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता का निर्माण करना।
- शहरी स्थानीय निकायों को जीआईएस मानचित्रण, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जलवायु मॉडलिंग जैसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना। शहरी-स्तरीय संस्थानों के लिए पर्याप्त स्टाफिंग, वित्त पोषण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता के लिए आवास, जल आपूर्ति, परिवहन और पर्यावरण विभागों में एकीकृत योजना की आवश्यकता है। विखंडित प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए एजेंसियों के बीच संयुक्त कार्य बल और डेटा-साझाकरण तंत्र स्थापित करना।
- जलवायु अनुकूलन लक्ष्यों के साथ अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के अभिसरण को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय समुदायों को पार्क, शहरी वन और आर्द्रभूमि जैसे हरित बुनियादी ढांचे के डिजाइन और रखरखाव में भागीदार होना चाहिए।
- गर्मी से निपटने, बाढ़ सुरक्षा और सतत जीवन शैली पर लक्षित अभियान शुरू करें।
- स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जलवायु अनुकूलन जागरूकता को एकीकृत किया जा सकता है।
- हरित भवन डिजाइन, ऊर्जा कुशल आवास और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित करें।
- शहरी जलवायु अनुकूलन निधि और आपदा न्यूनीकरण बजट के माध्यम से लचीले बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को प्राथमिकता दें।
- सतत गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा पहल में कॉर्पोरेट भागीदारी सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष
जलवायु-अनुकूल, कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों के लिए 2050 तक लगभग 10.95 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। इस निवेश से सालाना अरबों डॉलर के जलवायु-संबंधी नुकसानों को रोका जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप नए हरित रोज़गारों का सृजन, उन्नत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
इसलिए आज शीघ्र निवेश से आपदा से होने वाली हानि कम होगी, जीवन बचेंगे और भारतीय शहर समावेशी बनेंगे तथा निवेश के लिए वैश्विक रूप से आकर्षक बनेंगे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
भारत में जलवायु-अनुकूल शहरों के निर्माण में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और उनके समाधान के उपाय सुझाएँ। (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। इसने उद्योगों का आधुनिकीकरण किया, नई तकनीकों को अपनाया और भारत को वैश्विक बाज़ारों के साथ एकीकृत किया।
हालाँकि, हालिया रुझान एक चिंताजनक पैटर्न को उजागर करते हैं: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का आकर्षण जारी है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अल्पकालिक है, जिसमें विनिवेश बढ़ रहा है और भारतीय कंपनियाँ विदेशों में तेज़ी से निवेश कर रही हैं। यह विचलन भारत के निवेश माहौल को लेकर व्यवस्थागत चिंताएँ पैदा करता है।
एफडीआई क्षेत्र में वर्तमान रुझान
- वित्त वर्ष 2024-25 में सकल एफडीआई प्रवाह 81 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% अधिक है।
- कोविड के बाद निवेश प्रवाह में सालाना सिर्फ 0.3% की वृद्धि हुई, जबकि विनिवेश में सालाना 18.9% की वृद्धि हुई।
- कोविड के बाद से 308.5 अरब डॉलर के सकल निवेश के बावजूद, 153.9 अरब डॉलर स्वदेश वापस भेजे गए। भारतीय बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को समायोजित करने के बाद, शुद्ध प्रतिधारित पूंजी घटकर मात्र 0.4 अरब डॉलर रह गई ।
- विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 12% रह गई, जो अल्पकालिक और गैर-उत्पादक क्षेत्रों के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।
- निवेशक विनिर्माण या उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे दीर्घकालिक क्षेत्रों की तुलना में वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा वितरण और आतिथ्य को प्राथमिकता देते हैं।
- विदेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां: नियामक अक्षमता, नीतिगत अनिश्चितता और बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला देते हुए, बहिर्वाह वित्त वर्ष 2011-12 में 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 29.2 बिलियन डॉलर हो गया।
इस प्रकार, बड़े पैमाने पर बहिर्वाह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के दीर्घकालिक विकासात्मक प्रभाव को सीमित करता है। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि पूँजी लंबे समय तक नहीं टिकती, जिससे इसका दीर्घकालिक विकासात्मक प्रभाव सीमित हो जाता है।
दीर्घकालिक निवेश क्यों महत्वपूर्ण है?
एफडीआई प्रवाह से भारत को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:
- स्थायी निवेश में वृद्धि (कारखाने, संयंत्र, कार्यालय)।
- उत्पादन क्षमता का विस्तार (अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण)।
- नई प्रौद्योगिकियां लाना (जैसे, विनिर्माण में रोबोटिक्स)।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (प्रबंधन, दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण) को साझा करना।
हालाँकि, हालिया रुझान यह है कि:
- सकल विदेशी प्रवाह-जीडीपी अनुपात 2020-21 में 3.1% से लगातार घटकर 2024-25 में 2.1% हो गया और इसी अवधि में शुद्ध एफडीआई जीडीपी के 1.6% से गिरकर शून्य हो गया।
- भारत को विदेशी धन प्राप्त होता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा प्रत्यावर्तन (लाभ को स्वदेश ले जाना) और विनिवेश (पूंजी की निकासी) के माध्यम से शीघ्र ही बाहर निकल जाता है।
- भारतीय फर्मों द्वारा बाह्य एफडीआई वित्त वर्ष 2011-12 में 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 29.2 बिलियन डॉलर हो गया।
- कम्पनियां विदेशों में निवेश करने के कारणों के रूप में विनियामक अक्षमताओं, बुनियादी ढांचे की कमी और अप्रत्याशित नीतिगत ढांचे का हवाला देती हैं।
- पूंजी का बहिर्वाह रोजगार सृजन को सीमित करके, नवाचार को धीमा करके तथा औद्योगिक विकास को कम करके घरेलू अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है।
- अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च मूल्य विनिर्माण में कम निवेश से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता धीमी हो गई है।
- सरकारी सुधारों और बेहतर वैश्विक रैंकिंग के बावजूद, नियामक अस्पष्टता, कानूनी अनिश्चितता और असंगत शासन निवेशकों को हतोत्साहित कर रहे हैं।
- विदेशी कम्पनियों द्वारा धन वापस लेना तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में निवेश करना, दोनों ही व्यवस्थागत कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिन्हें भारत के निवेश वातावरण को स्थिर करने के लिए दूर किया जाना आवश्यक है।
आगे की राह
- भारत को अल्पकालिक कर-संचालित प्रवाह की तुलना में दीर्घकालिक, रणनीतिक पूंजी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- निवेशकों का विश्वास बनाने के लिए सरलीकृत एवं पारदर्शी विनियमन आवश्यक हैं।
- स्थिर कर व्यवस्था, सुसंगत नीतियां और कानूनी स्पष्टता निवेशकों का विश्वास बनाए रखेगी।
- परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में बुनियादी ढांचे के विकास से व्यावसायिक लागत कम होनी चाहिए।
- एफडीआई को किराया-प्राप्ति वाले क्षेत्रों के बजाय विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, एआई, अर्धचालक और स्वच्छ ऊर्जा की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए।
- कुशल कार्यबल के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश की आवश्यकता है।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और ज्ञान-संचालित निवेश को आकर्षित कर सकता है।
- राउंड-ट्रिपिंग को रोकने तथा वास्तविक उत्पादक अंतर्वाह की पहचान करने के लिए मजबूत निगरानी की आवश्यकता है।
- कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुबंध प्रवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों से विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- एफडीआई को हरित विकास, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल परिवर्तन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कहानी, जिसे कभी उदारीकरण की सफलता कहा जाता था, अब संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच बढ़ता अंतर, अल्पकालिक निवेशों का प्रभुत्व और भारत से बढ़ता विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कमजोर होते घरेलू आत्मविश्वास को दर्शाता है। सतत विकास के लिए, भारत को एफडीआई के प्रमुख आंकड़ों से हटकर गुणवत्ता, स्थायित्व और अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ निवेश के संरेखण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
सकल आँकड़ों के अनुसार, भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कहानी मज़बूत दिखाई देती है, लेकिन इसमें अल्पकालिकता, उच्च विनिवेश और भारतीय कंपनियों द्वारा बढ़ते बाहरी निवेश जैसी गहरी कमज़ोरियाँ छिपी हुई हैं। विस्तारपूर्वक बताइए। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-complex-turn-in-indias-fdi-story/article70022990.ece