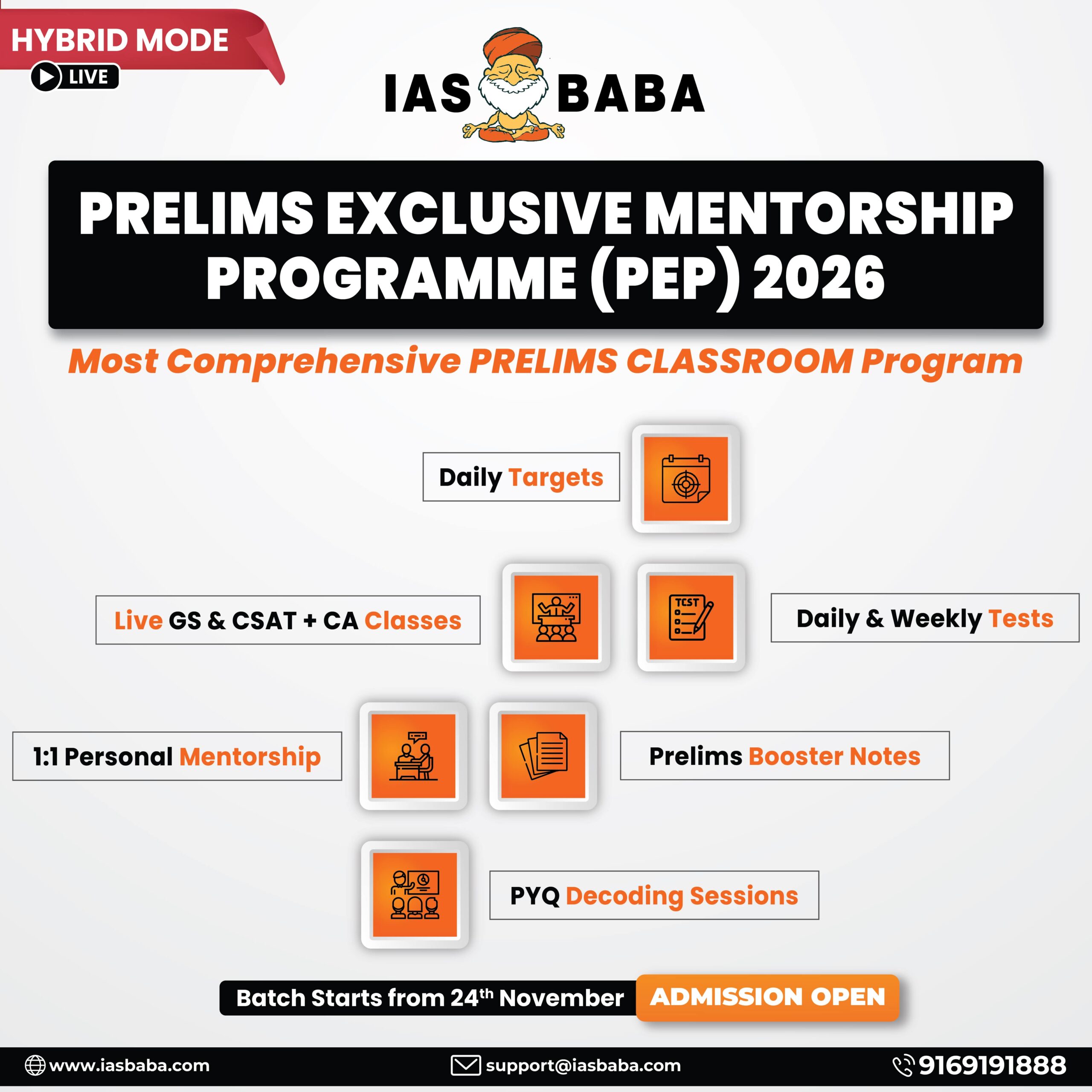IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
प्रसंग:
- पेरिस में चल रही वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की बैठकों में आतंकवाद को वित्तपोषित करने और समर्थन देने के साधन के रूप में राज्य प्रायोजन पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है , जिसमें पाकिस्तान में संचालित प्रतिबंधित संगठनों और उनके प्रतिनिधियों को वित्तपोषित करना भी शामिल है।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के बारे में:

- स्थापना: एफएटीएफ वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में विकसित देशों की जी-7 बैठक के दौरान की गई थी।
- उद्देश्य: प्रारंभ में, इसका उद्देश्य धन शोधन से निपटने के उपायों की जाँच और विकास करना था। अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद, FATF ने 2001 में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को भी इसमें शामिल कर लिया।
- सदस्य: यह 39 सदस्यों वाला एक निकाय है जो विश्व के सभी हिस्सों के अधिकांश प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 39 सदस्यों में से दो क्षेत्रीय संगठन हैं: जो यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद है।
- भारत और एफएटीएफ: भारत 2006 में ‘पर्यवेक्षक’ के दर्जे के साथ इसमें शामिल हुआ और 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया। भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) और यूरेशियन समूह (ईएजी) का भी सदस्य है।
- विशेष सिफ़ारिशें: अप्रैल 1990 में, FATF ने चालीस सिफ़ारिशों वाली एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य धन शोधन के विरुद्ध लड़ाई के लिए आवश्यक एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करना था। 2004 में, FATF ने नौवीं विशेष सिफ़ारिशें प्रकाशित कीं, जिसने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए (40+9 सिफ़ारिशें) सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को और मज़बूत किया।
- संरचना: FATF प्लेनरी, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी वर्ष में तीन बार बैठक होती है।
- सचिवालय: FATF सचिवालय पेरिस स्थित OECD मुख्यालय में स्थित है। यह सचिवालय FATF सदस्यों और वैश्विक नेटवर्क के मूलभूत कार्यों का समर्थन करता है।
- वित्तपोषण: एफएटीएफ सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए वित्तपोषण एफएटीएफ के वार्षिक बजट द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें सदस्य योगदान करते हैं।
- एफएटीएफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट:
- ग्रे लिस्ट: ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जिन्हें आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है । यह एक चेतावनी है कि वह देश काली सूची में जा सकता है।
- काली सूची: काली सूची में गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (एनसीसीटी) शामिल हैं जो आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- एफएटीएफ सूची में शामिल होने के निहितार्थ:
- एफएटीएफ (आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी आदि) से संबद्ध वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध
- ऐसे वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार
स्रोत:
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पिछले तीन महीनों में विभिन्न स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हुए कथित हमले को लेकर केरल, त्रिपुरा और मणिपुर सरकारों को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के बारे में:

- स्थापना: एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के तहत की गई थी।
- संशोधन: इसे मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया।
- उद्देश्य: यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप: इसकी स्थापना मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी।
- संरचना: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।
- सदस्यों की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं ।
- सदस्यों का कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
- प्रमुख कार्य:
- इसमें न्यायिक कार्यवाही के साथ सिविल न्यायालय की शक्तियां भी हैं।
- इसे मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
- यह मामले की घटना के एक वर्ष के भीतर जांच कर सकता है।
- बाध्यकारी नहीं: इसकी सिफारिशें मुख्यतः सलाहकारी प्रकृति की हैं।
स्रोत:
श्रेणी: इतिहास और संस्कृति
प्रसंग:
- मणिपुर सरकार ने निंगोल चाकोबा उत्सव से पहले मछली मेला आयोजित किया है और विभिन्न प्रकार की 1.5 लाख किलोग्राम मछली बेचने का लक्ष्य रखा है।
निंगोल चाकोबा महोत्सव के बारे में:

- मेइतेई कैलेंडर के हियांगेई चंद्र माह के दूसरे दिन मनाया जाता है ।
- मुख्य रूप से मैतेई लोगों द्वारा मनाया जाता है: यह त्यौहार मुख्य रूप से मैतेई लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन आजकल कई अन्य समुदाय भी इसे मनाने लगे हैं।
- उद्देश्य: यह समाज में शांति और सद्भाव लाने में परिवार की खुशी और पुनर्मिलन के महत्व पर जोर देता है।
- नामकरण: निंगोल का अर्थ ‘विवाहित महिला’ और चाकोबा का अर्थ ‘भोज के लिए निमंत्रण’ है; इसलिए यह वह त्यौहार है जिसमें विवाहित महिलाओं को उनके माता-पिता के घर भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- विशिष्टता: इस त्यौहार का मुख्य घटक विवाहित बहनों का अपने मायके जाकर भव्य भोज और खुशी से पुनर्मिलन करना तथा उसके बाद उपहार देना है।
मेइतेई समुदाय के बारे में:
- पृथक नृजातीय समूह: वे मणिपुर राज्य के प्रमुख जातीय समूह हैं।
- भाषा: वे मेइती भाषा (जिसे आधिकारिक तौर पर मणिपुरी कहा जाता है) बोलते हैं, जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और मणिपुर राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा है।
- वितरण: मैतेई मुख्य रूप से आधुनिक मणिपुर के इम्फाल घाटी क्षेत्र में बसे हैं, हालाँकि उनकी एक बड़ी आबादी असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम जैसे अन्य भारतीय राज्यों में भी बस गई है। पड़ोसी देशों म्यांमार और बांग्लादेश में भी मैतेई की उल्लेखनीय उपस्थिति है।
- कुल: वे कुलों में विभाजित होते हैं, जिनके सदस्य आपस में विवाह नहीं करते।
- अर्थव्यवस्था: सिंचित खेतों पर चावल की खेती उनकी अर्थव्यवस्था का आधार है।
स्रोत:
श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
प्रसंग:
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक ) की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में सचिव (नागरिक उड्डयन) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक ) योजना के बारे में:
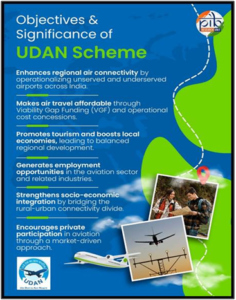
- लॉन्च: इस योजना को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016 के तहत डिजाइन किया गया था, जिसमें बाजार संचालित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- उद्देश्य: उड़ान का उद्देश्य विमानन को लोकतांत्रिक बनाना और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी हवाई पहुंच हो।
- नोडल मंत्रालय: यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- कार्यान्वयन प्राधिकरण: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- सब्सिडी का प्रावधान: उड़ान योजना के अंतर्गत सरकार एयरलाइनों के साथ साझेदारी में काम करती है, ताकि कम सेवा वाले और कम सेवा वाले मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।
- वीजीएफ मॉडल पर कार्य: सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) मॉडल के माध्यम से एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो चिन्हित मार्गों पर परिचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच के अंतर को कवर करती है।
- बोली का प्रयोग: विमानन कंपनियाँ हवाई मार्गों के लिए बोली लगाती हैं। जो कंपनी सबसे कम सब्सिडी मांगती है, उसे ठेका दे दिया जाता है। इस किराये के तहत, प्रत्येक उड़ान के लिए एयरलाइन को आधी, यानी कम से कम 9 या अधिकतम 40 सीटें बुक करनी होती हैं ।
- मूल्य की सीमा: इस योजना के तहत, ‘फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट’ द्वारा एक घंटे की यात्रा या हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 500 किलोमीटर की आधे घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया 2500 रुपये निर्धारित किया गया है।
स्रोत:
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- केंद्र की इच्छा के अनुरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अप्रत्याशित विचार परिवर्तन ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को फिर से ध्यान में ला दिया है।
कॉलेजियम प्रणाली के बारे में:
- प्रकृति: यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए भारत का न्यायिक तंत्र है। यह कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों, विशेष रूप से “तीन न्यायाधीशों के मामले” से विकसित हुआ है।
- विकास:
- प्रथम न्यायाधीश वाद (1981): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में, संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 में “परामर्श” शब्द का अर्थ “सहमति” नहीं है। इसने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को न्यायपालिका पर प्राथमिकता दी।
- द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश वाद को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में “परामर्श” का अर्थ वास्तव में सहमति है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यह सलाह देने से पहले, मुख्य न्यायाधीश को अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करना होगा।
- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार कर इसमें मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बाद न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल किया।
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम, 2014: इसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए लाया गया था। हालाँकि, पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक आधार:
- अनुच्छेद 124: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- अनुच्छेद 126: रिक्ति/अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी।
- अनुच्छेद 127: यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश (राष्ट्रपति की सहमति से) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 128: राष्ट्रपति की सहमति से, मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 217: मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- प्रक्रिया ज्ञापन ( एमओपी ) के बारे में:
- एमओपी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के नियमों और प्रक्रियाओं की सूची है। यह सरकार और न्यायपालिका द्वारा मिलकर तैयार किया गया एक दस्तावेज़ है। केंद्र सरकार ने 30 जून 1999 को एमओपी तैयार किया था।
- वर्तमान एमओपी में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सभी नियुक्तियों की अनुशंसा कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह अनुशंसा फिर केंद्र सरकार को भेजी जाती है। कानून मंत्री इसे प्रधानमंत्री को भेजेंगे, जो नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देंगे।
- संशोधित एमओपी : 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉलेजियम की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नया एमओपी तैयार करने का निर्देश दिया था। 2017 में, एमओपी को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद, सरकार ने मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसे नहीं अपनाया।
स्रोत:
(MAINS Focus)
(जीएस पेपर 3 - बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण)
संदर्भ (परिचय)
भारत अपनी क्षमता और घरेलू विनिर्माण में तेज़ी से वृद्धि के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनकर उभरा है। हालाँकि, इस प्रगति को बनाए रखने के लिए निर्यात का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ढाँचे के माध्यम से, विशेष रूप से अफ्रीका में, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का लाभ उठाना आवश्यक है।
मुख्य तर्क
- तीव्र सौर विस्तार: भारत का सौर उत्पादन 2024-25 में 1,08,494 गीगावाट घंटा तक पहुंच गया , जो जापान से आगे निकल गया तथा केवल चीन और अमेरिका से पीछे है। स्थापित सौर क्षमता 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 117 गीगावाट हो गई , तथा विनिर्माण क्षमता 100 गीगावाट (प्रभावी 85 गीगावाट) अनुमानित है।
- घटती लागत और प्रतिस्पर्धा: 2017 से, सौर ऊर्जा प्रति यूनिट कोयले की तुलना में सस्ती हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। फिर भी, पैमाने की अक्षमताओं, कच्चे माल की सीमित पहुँच और कमज़ोर उत्पादन लाइनों के कारण, भारतीय मॉड्यूल चीनी मॉड्यूल की तुलना में 1.5-2 गुना महंगे बने हुए हैं।
- घरेलू जलवायु प्रतिबद्धताएँ: भारत का 2030 का लक्ष्य 50% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन (लगभग 500 गीगावाट) से प्राप्त करना है , जिसमें 250-280 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करना शामिल है। हालाँकि, वार्षिक वृद्धि औसतन केवल 17-23 गीगावाट है, जो आवश्यक 30 गीगावाट/वर्ष की गति से कम है ।
- निर्यात और वैश्विक बाज़ार की संभावनाएँ: 2024 में अमेरिका को भारत का 4 गीगावाट का निर्यात अस्थायी था, जबकि चीन ने इसी अवधि में 236 गीगावाट का निर्यात किया। अपने बढ़ते उद्योग को बनाए रखने के लिए, भारत को स्थिर बाहरी बाज़ारों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ढाँचे के माध्यम से अफ्रीका एक आशाजनक गंतव्य प्रस्तुत करता है ।
- अफ्रीका के लिए अवसर: अफ्रीका में बिजली की कमी के कारण 96% कृषि योग्य भूमि सिंचित नहीं है । भारत, पीएम-कुसुम (ग्रामीण सौर ऊर्जा) और पीएम-सूर्य घर (शहरी रूफटॉप सौर ऊर्जा) योजनाओं की तर्ज पर किफायती सौर पंपसेट और विकेन्द्रीकृत सौर प्रणालियाँ प्रदान कर सकता है , जिससे ऊर्जा की पहुँच को विकासात्मक सहयोग के साथ जोड़ा जा सके।
आलोचनाएँ / चुनौतियाँ
- उच्च उत्पादन लागत: पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स और सेल्स पर आयात निर्भरता और उच्च रसद लागत के कारण भारतीय सौर मॉड्यूल वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हैं ।
- नीतिगत अनिश्चितता: आयात शुल्क में लगातार परिवर्तन , पीएलआई योजना में देरी , तथा असंगत राज्य स्तरीय सौर नीतियां दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
- कमजोर घरेलू मांग: पीएम-कुसुम और पीएम-सूर्य घर जैसी प्रमुख योजनाओं में कम वितरण और अपनाने की दर देखी गई है , जिससे सौर मॉड्यूल की घरेलू खपत सीमित हो गई है।
- सीमित तकनीकी गहराई: भारतीय निर्माता बड़े पैमाने पर असेंबली-आधारित उत्पादन पर निर्भर करते हैं, जिसमें उच्च दक्षता वाले सौर सेल (जैसे, TOPCon , HJT, पेरोव्स्काइट प्रौद्योगिकियां) में न्यूनतम अनुसंधान एवं विकास होता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: पैमाने, सब्सिडी और आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण के माध्यम से चीन का प्रभुत्व भारत के लिए स्थापित निर्यात बाजारों में प्रवेश करना कठिन बना देता है।
सुधार और आगे की राह
- वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करना: सौर ऊर्जा परिनियोजन, वित्त और क्षमता निर्माण में भारत-अफ्रीका साझेदारी को संस्थागत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का उपयोग करना ।
- प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएँ: उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार करके उसे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (पॉलीसिलिकॉन से मॉड्यूल तक) में शामिल करें। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करें।
- निर्यात केन्द्रों का निर्माण: निर्यात तत्परता और रसद दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों के पास सौर एसईजेड और हरित गलियारे स्थापित करना ।
- वित्तीय और नीतिगत स्थिरता: नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों के तहत डेवलपर्स के लिए स्थिर टैरिफ , पूर्वानुमानित नीति व्यवस्था और आसान ऋण सुनिश्चित करना ।
- नवाचार के माध्यम से घरेलू विस्तार: घरेलू उपयोग को बढ़ाने और प्रति इकाई लागत को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को कृषि (सौर पंपसेट , कोल्ड स्टोरेज) और शहरी आवास (रूफटॉप ग्रिड) के साथ एकीकृत करें ।
निष्कर्ष
भारत का सौर क्षेत्र - आत्मनिर्भरता से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर संक्रमण के कारण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है । नीतिगत कमियों को पाटकर, मूल्य-श्रृंखला की गहराई बढ़ाकर और आईएसए के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत सौर समाधानों का एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन सकता है , और औद्योगिक विकास को जलवायु न्याय के साथ जोड़ सकता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न:
"सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की सफलता अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित होनी चाहिए। भारत के लिए, विशेष रूप से अफ्रीका जैसे विकासशील क्षेत्रों में, एक प्रमुख सौर ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने की चुनौतियों और अवसरों का परीक्षण कीजिए।" (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द हिंदू
(जीएस पेपर 2 – शासन: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे)
संदर्भ (परिचय)
यद्यपि STEM में प्रतिभा पलायन को रोकना एक वैध लक्ष्य है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की महत्वाकांक्षा केवल औद्योगिक पाइपलाइनों के निर्माण से कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए। वास्तविक शैक्षणिक शक्ति अन्वेषण, स्वायत्तता, अंतःविषयकता और खुलेपन में निहित है – न कि केवल रणनीतिक STEM राष्ट्रवाद में।
मुख्य तर्क
- प्रतिभाओं के प्रत्यावर्तन की अपनी सीमाएँ हैं। भारतीय मूल के “स्टार फैकल्टी” को आकर्षित करने की प्रस्तावित योजना 12-14 प्राथमिकता वाले STEM क्षेत्रों को लक्षित करती है, और लौटने वालों को अनुदान और प्रयोगशालाएँ प्रदान करती है। फिर भी, लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि यह केवल एक शुरुआत है: ज़्यादा महत्वपूर्ण वह वातावरण है जो देश में निरंतर योगदान को सक्षम बनाता है।
- भारत में पहले से ही मज़बूत संस्थान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें और मज़बूत करने की ज़रूरत है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और अन्य संस्थानों ने बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय कार्य किया है। लेख में तर्क दिया गया है कि इन्हें निरंतर निवेश, पारदर्शी शासन और वास्तविक शैक्षणिक स्वायत्तता द्वारा मज़बूत किया जाना चाहिए ।
- उच्च शिक्षा को औद्योगिक आपूर्ति-शृंखला के तर्क तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह लेख विश्वविद्यालयों को केवल उद्योग के पोषक के रूप में देखने के विरुद्ध चेतावनी देता है और इस बात पर ज़ोर देता है कि नवाचार “अंतर्विषयक और अक्सर असुविधाजनक स्थानों में पनपता है” – उदाहरण के लिए, जहाँ समाजशास्त्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं, या इतिहासकार बहुसंख्यकवादी आख्यानों को चुनौती देते हैं।
- शैक्षणिक स्वतंत्रता और खुलापन ज़रूरी है। वापस लौटने वाले और वर्तमान संकाय सदस्यों को कठिन प्रश्न पूछने की आज़ादी होनी चाहिए। लेख में विद्वानों (जैसे, फ्रांसेस्का ओरसिनी) के निर्वासन का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि इससे “यह निराशाजनक संदेश जाता है कि भारत उन शैक्षणिक जाँच-पड़तालों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो आधिकारिक आख्यानों से मेल नहीं खातीं।”
- वैश्विक मानक भारत की पिछड़ी स्थिति को दर्शाते हैं। चीन की हज़ार प्रतिभा योजना (2008 में शुरू) के साथ-साथ उसके विश्वविद्यालयों में व्यापक सुधार भी हुआ – जिसके परिणामस्वरूप अब पाँच चीनी संस्थान क्यूएस टॉप 100 में शामिल हैं, यानी कुल 72वें स्थान पर। इसके विपरीत, भारत के 54 संस्थान अभी तक टॉप 100 में जगह नहीं बना पाए हैं; सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान, आईआईटी दिल्ली, 123वें स्थान पर है।
आलोचनाएँ / कमियाँ
- STEM और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अत्यधिक ज़ोर। STEM को लक्षित करना समझ में आता है, लेकिन उच्च शिक्षा को रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमताओं (AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक) तक सीमित करने से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के हाशिए पर जाने का खतरा है, जो नवाचार के नैतिक, चिंतनशील, सामाजिक आयामों के लिए आवश्यक हैं।
- संस्थागत स्वायत्तता कमज़ोर बनी हुई है। राजनीतिक हस्तक्षेप, पाठ्यक्रम नियंत्रण और संरक्षण से प्रेरित संकाय नियुक्तियाँ विश्वविद्यालयों को बाधित करती हैं।
- प्रतिधारण और आकर्षण के मुद्दे। भले ही वापस लौटने वाले शिक्षकों की भर्ती की जा सके, लेकिन बिना मज़बूत संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के, कई लोग भारत को एक दीर्घकालिक आधार के बजाय एक अस्थायी विकल्प के रूप में देख सकते हैं – जिससे उनके लिए एक घर बनाने की महत्वाकांक्षा कमज़ोर हो जाएगी।
- महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञानों की उपेक्षा। तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की चाह में, नैतिकता, दर्शन, सामाजिक अन्वेषण और अंतःविषयक विद्वत्ता की भूमिका की अनदेखी समग्र शिक्षा को कमज़ोर करती है।
- वैश्विक धारणा और रैंकिंग में अंतर। नामांकन और STEM स्नातकों की संख्या के बावजूद, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक अनुसंधान प्रभाव, नवाचार संस्कृति और संस्थागत प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं।
सुधार और आगे की राह
- शैक्षणिक स्वायत्तता और प्रशासन को मज़बूत बनाएँ। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम डिज़ाइन, संकाय नियुक्ति, शोध प्राथमिकताओं और संस्थागत निर्देशन में स्वतंत्रता होनी चाहिए – अत्यधिक राजनीतिक या नियामक नियंत्रण से मुक्त।
- मानविकी और अंतःविषयक अनुसंधान के साथ STEM को संतुलित करें। ऐसे वातावरण को बढ़ावा दें जहाँ तकनीक नैतिकता, समाज, संस्कृति और इतिहास से प्रेरित हो। ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें जो इंजीनियरिंग-विज्ञान को सामाजिक विज्ञान/मानविकी के साथ एकीकृत करते हैं ( जैसा कि “आईआईटी से एक सबक” लेख में तर्क दिया गया है)।
- संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें, न कि केवल स्टार फैकल्टी की भर्ती करें। सुनिश्चित करें कि लौटने वाले विद्वानों को उच्च-गुणवत्ता वाली प्रयोगशालाएँ, स्थिर वित्तपोषण, समकक्ष समुदाय, दीर्घकालिक अनुबंध और ऐसा वातावरण मिले जो अन्वेषण को महत्व देता हो।
- अनुसंधान निवेश और संस्कृति को बढ़ाएँ। अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाएँ (जो वर्तमान में वैश्विक समकक्षों की तुलना में कम है), उच्च-गुणवत्ता वाले पीएचडी को बढ़ावा दें, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करें, विशुद्ध रूप से अनुप्रयुक्त/औद्योगिक परिणामों के बजाय बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करें।
- वैश्विक जुड़ाव और खुलापन। शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा करें, विविध विचारों (विरोधियों सहित) का स्वागत करें, निर्वासन या विद्वानों पर राजनीतिक दबाव से बचें। घरेलू प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा और प्रतिष्ठा संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करें।
- सफलता के मानकों की निगरानी और सुधार करें। संकीर्ण मानकों (उद्योग के लिए स्नातक, प्लेसमेंट) से व्यापक मानकों की ओर बदलाव करें: शोध की गुणवत्ता, उद्धरण प्रभाव, अंतःविषयक आउटपुट, वैश्विक सहयोग, सामाजिक प्रासंगिकता।
निष्कर्ष
भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक दोराहे पर खड़ा है। प्रतिभा पलायन को रोकने और वैश्विक अनुसंधान क्षमता निर्माण का प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसके साथ एक गहन परिवर्तन भी आवश्यक है: एक संकीर्ण साधनात्मक मॉडल – “उद्योग पोषक के रूप में विश्वविद्यालय” – से हटकर , अन्वेषण, स्वायत्तता, अंतःविषयता और खुलेपन के एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ।
- तभी भारत न केवल अपनी रणनीतिक STEM आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, बल्कि ऐसे मस्तिष्कों का सही मायने में पोषण कर सकेगा जो प्रश्न करें, नवाचार करें, चिंतन करें और नेतृत्व करें , तथा ऐसे संस्थानों का निर्माण करें जो वैश्विक सम्मान प्राप्त करें और समाज की पूर्ण सेवा करें।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न: भारत की उच्च शिक्षा रणनीतिक STEM विकास पर अधिकाधिक केंद्रित हो रही है। इस दृष्टिकोण के अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस