IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए पीड़ित के माता-पिता को शामिल करना आवश्यक है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) के बारे में:
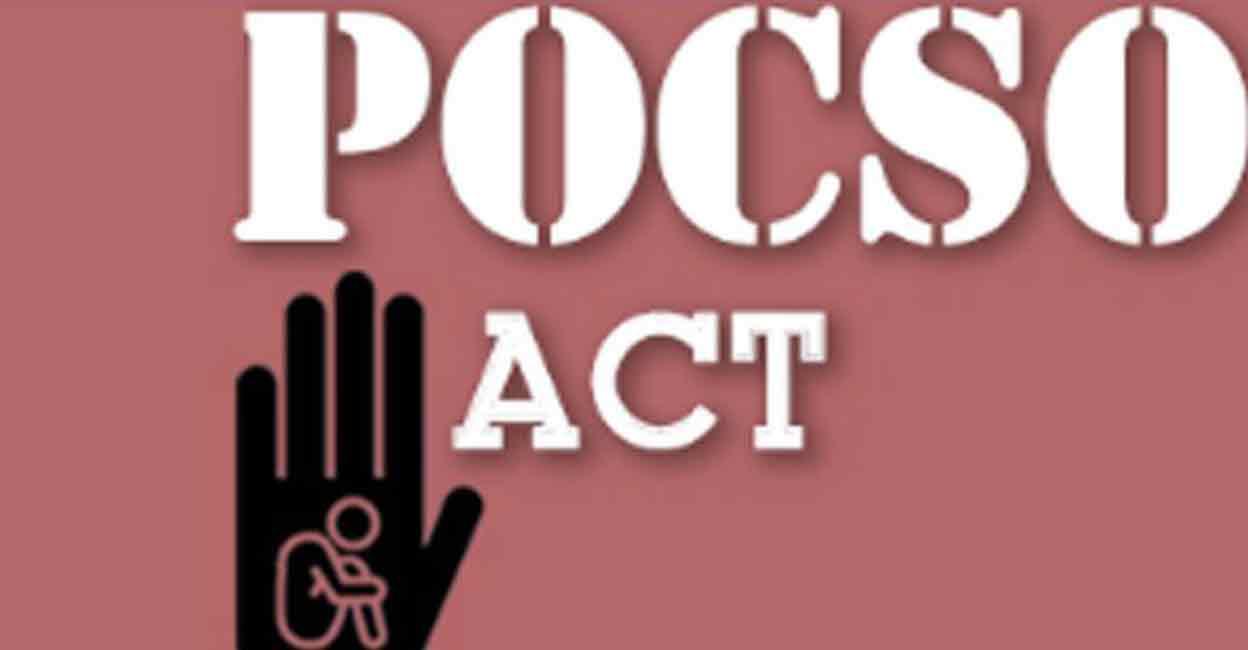
- अधिनियमन: पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को प्रभावी हुआ, जिसे 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत द्वारा अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- उद्देश्य: इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या जिनके लिए पर्याप्त रूप से दंड नहीं दिया गया है।
- बालक की परिभाषा: अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है। अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान है।
- अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:
- अधिनियम में यह मान्यता दी गई है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और ऐसा शोषण अपराध है, चाहे पीड़ित का लिंग कुछ भी हो।
- अब बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त सामान्य जागरूकता है, न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थाओं द्वारा भी, क्योंकि रिपोर्ट न करना POCSO अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है।
- बाल पोर्नोग्राफी सामग्री का भंडारण एक नया अपराध बना दिया गया है।
- इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता में ‘महिला की शील भंग करने’ की अमूर्त परिभाषा के विपरीत, ‘यौन उत्पीड़न’ के अपराध को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है (न्यूनतम सजा में वृद्धि के साथ)।
- आगे के संशोधन:
- 2019 में अधिनियम की समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किया गया, ताकि बच्चों पर यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया जा सके, ताकि अपराधियों को रोका जा सके और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोका जा सके।
- भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है।
- POCSO नियम, 2020 के बारे में:
- पोक्सो नियमों का नियम-9 विशेष न्यायालय को एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे की राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है।
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) या किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए धन का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है।
- पोक्सो नियम सीडब्ल्यूसी को जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराने का अधिकार देता है।
स्रोत:
श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी
प्रसंग:
- एक अध्ययन के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण से गोवा के नदी मुहाने के मत्स्य पालन के साथ-साथ मानव उपभोक्ताओं को भी खतरा है।
माइक्रोप्लास्टिक के बारे में:
- परिभाषा: इन्हें पाँच मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह हमारे महासागरों और जलीय जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है।
- निर्माण: सौर UV विकिरण, हवा, धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में, प्लास्टिक छोटे कणों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक (5 मिमी से छोटे कण) या नैनोप्लास्टिक (100 एनएम से छोटे कण) कहा जाता है।
- माइक्रोप्लास्टिक का वर्गीकरण:
- प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक: ये व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए सूक्ष्म कण होते हैं और कपड़ों व अन्य वस्त्रों से निकलने वाले माइक्रोफ़ाइबर होते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, प्लास्टिक छर्रों और प्लास्टिक रेशों में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स।
- द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक: ये पानी की बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। पर्यावरणीय कारकों, मुख्यतः सौर विकिरण और समुद्री लहरों के संपर्क में आने से ये टूटते हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक के अनुप्रयोग:
- चिकित्सा एवं औषधि उपयोग: रसायनों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने और छोड़ने की क्षमता के कारण लक्षित दवा वितरण में इसका उपयोग किया जाता है।
- औद्योगिक अनुप्रयोग: सफाई मशीनरी के लिए एयर-ब्लास्टिंग प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक वस्त्रों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
- सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद: चेहरे के स्क्रब, टूथपेस्ट और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में एक्सफोलिएटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है।
- माइक्रोप्लास्टिक्स से निपटने के लिए उठाए गए कदम:
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) संकल्प: यूएनईए संकल्प ने समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के विकास को अनिवार्य बना दिया।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) प्लास्टिक संधि: यूएनईपी माइक्रोप्लास्टिक सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर काम कर रहा है।
स्रोत:
श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा
प्रसंग:
- उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विशिष्ट आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का नया केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के बारे में:
- स्थापना: एनएसजी एक आतंकवाद-रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम – ‘राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986’ द्वारा अस्तित्व में आई।
- इसके गठन के पीछे की घटनाएं: इस तरह के बल के गठन का विचार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आया।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य ‘आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने के उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना’ है।
- विशेषज्ञता: एनएसजी को आतंकवाद विरोधी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें भूमि, समुद्र और हवा पर अपहरण विरोधी कार्य; बम निरोधक (आईईडी की खोज, पता लगाना और निष्क्रिय करना), विस्फोट के बाद जांच (पीबीआई) और बंधक बचाव मिशन शामिल हैं।
- विशिष्ट वर्दी: एनएसजी कर्मियों को अक्सर मीडिया में ब्लैक कैट कमांडो के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उनकी वर्दी पर काली पोशाक और काली बिल्ली का प्रतीक चिन्ह होता है।
- आदर्श वाक्य: ‘ सर्वत्र , सर्वोत्तम , सुरक्षा’ के आदर्श वाक्य को हमेशा से ही अपनाया गया है, तथा इसका मुख्य ध्यान तीव्र एवं त्वरित आक्रमण तथा युद्ध क्षेत्र से तत्काल पीछे हटने के मूल दर्शन पर केन्द्रित रहा है।
- मंत्रालय: यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एक कार्य-उन्मुख बल है जिसके दो पूरक तत्व हैं:
- सेना कर्मियों से युक्त विशेष कार्रवाई समूह (एसएजी) – एनएसजी की मुख्य आक्रामक या स्ट्राइक विंग है, और
- विशेष रेंजर समूह (एसआरजी) में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के जवान शामिल होते हैं। ये आमतौर पर वीआईपी सुरक्षा का काम संभालते हैं।
स्रोत:
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
प्रसंग:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत में दूषित पाई गई तीन तरल दवाओं के बारे में चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की है, जिसकी सूचना 8 अक्टूबर को संगठन को दी गई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में:
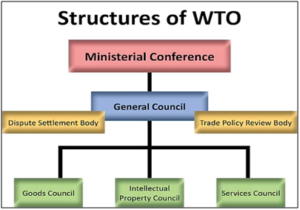
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का समन्वय करती है और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है।
- स्थापना: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसने 7 अप्रैल, 1948 को कार्य करना शुरू किया – यह तिथि अब हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाई जाती है।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
- प्रकृति: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है।
- उद्देश्य: विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देता है, मानदंड और मानक निर्धारित करता है, साक्ष्य-आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी और मूल्यांकन करता है।
- शासी निकाय: विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA), विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं। कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा इस सभा का मुख्य विषय होता है।
- सदस्यता: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्र-समूह जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।
स्रोत:
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि उसने ऑपरेशन चक्र V के तत्वावधान में डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में:

- परिभाषा: डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में साइबर अपराधी कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो का रूप धारण कर भोले-भाले पीड़ितों से उनकी मेहनत की कमाई ठग लेते हैं।
- पीड़ितों की प्रकृति: साइबर अपराधी आमतौर पर पीड़ितों पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी या साइबर अपराध जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं। वे अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिए सबूत गढ़ सकते हैं।
- काम करने का ढंग:
- साइबर अपराधी फोन या ईमेल के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं, शुरुआत ऑडियो कॉल से करते हैं और फिर हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशनों या अदालतों जैसे स्थानों से वीडियो कॉल करते हैं।
- वे अपने आप को वैध दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों की तस्वीरों को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- वे ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से फर्जी गिरफ्तारी वारंट, कानूनी नोटिस या आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज भी भेज सकते हैं।
- डिजिटल गिरफ्तारी में वृद्धि के कारण:
- भय और घबराहट: गिरफ्तारी की धमकी के डर से पीड़ित बिना सोचे-समझे ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं।
- जानकारी का अभाव: कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञता के कारण पीड़ितों के लिए वैध दावों और धोखाधड़ी के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
- सामाजिक कलंक: सामाजिक कलंक और परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का डर पीड़ितों को शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है।
- चालाकीपूर्ण तकनीकें: विश्वसनीय दिखने और पीड़ित की अनुपालना बढ़ाने के लिए एआई आवाजों, पेशेवर लोगो और नकली वीडियो कॉल का उपयोग।
साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत की पहल:
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित यह केंद्र साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है और साइबर अपराध रोकथाम संसाधन प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: एक समर्पित पोर्टल जनता को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कानून प्रवर्तन द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।
- वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली: 2021 में लॉन्च किए गए इस प्लेटफॉर्म ने वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग की अनुमति देकर 9.94 लाख शिकायतों में ₹3431 करोड़ से अधिक की सफलतापूर्वक बचत की है।
- साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला: दिल्ली स्थित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला और हैदराबाद स्थित साक्ष्य प्रयोगशाला ने डिजिटल साक्ष्यों के प्रबंधन और विश्लेषण में पुलिस की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- साइट्रेन के माध्यम से प्रशिक्षण : I4C का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइबर अपराध की जांच और अभियोजन के लिए कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है, जिसके तहत अब तक 98,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- जन जागरूकता अभियान: सरकार ने एसएमएस, सोशल मीडिया, साइबर दोस्त, संचार साथी पोर्टल और ऐप, तथा यहां तक कि मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से जागरूकता अभियान लागू किया है।
स्रोत:
(MAINS Focus)
(जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था - विकास, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति से संबंधित मुद्दे)
संदर्भ (परिचय)
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 99 महीने के निचले स्तर 1.54% (सितंबर 2025) पर पहुँच गई है —जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% के लक्ष्य से काफ़ी कम है। हालाँकि यह उत्साहजनक प्रतीत होता है, लेकिन यह माँग, नीतिगत अंशांकन और पूर्वानुमान सटीकता में गहरी संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर करता है, जिसके लिए नीतिगत स्तर पर सूक्ष्म पुनर्विचार की आवश्यकता है।
वर्तमान प्रवृत्ति को समझना
- अवमुद्रास्फीतिकारी चरण (Disinflationary Phase): वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के लिए औसत मुद्रास्फीति 2.2% रही , जो आरामदायक स्तर के भीतर है, लेकिन लक्ष्य मध्य बिंदु से नीचे है।
- क्षेत्रवार कमजोरी: कपड़े और जूते (2.3%) जैसी श्रेणियों में निरंतर मूल्य स्थिरता दिख रही है, जो कमजोर उपभोग का संकेत है।
- आपूर्ति-मांग असंतुलन: गिरती कीमतें यह दर्शाती हैं कि उत्पादकता में वृद्धि के बजाय आपूर्ति मांग से अधिक है।
- चीन के साथ तुलना: चीन के निर्यात-आधारित अतिआपूर्ति अवशोषण के विपरीत, भारत की बाह्य मांग टैरिफ तनाव के कारण सीमित बनी हुई है।
- नीतिगत निहितार्थ: लगातार कम मुद्रास्फीति निजी निवेश और वेतन वृद्धि को कम कर सकती है, जिससे समावेशी सुधार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
कम मुद्रास्फीति परिदृश्य चिंता का विषय क्यों है?
- कमजोर घरेलू मांग: उपभोक्ता विवेकाधीन खर्च की तुलना में बचत और ऋण चुकौती को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे विकास की गति धीमी पड़ रही है।
- राजकोषीय प्रोत्साहनों में कमी: जीएसटी कटौती और आयकर छूट से संरचनात्मक सुधार के बिना केवल अल्पकालिक मांग में वृद्धि हुई।
- सीमित रोजगार लोच: मजदूरी वृद्धि स्थिर हो गई है, जिससे क्रय शक्ति और उपभोग सुधार में कमी आई है।
- निजी निवेश में देरी: वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में अधिक परियोजनाओं की घोषणा के बावजूद, क्रियान्वयन में देरी से गुणक प्रभाव सीमित हो गया है।
- अपस्फीतिकारी चक्र का जोखिम: लगातार कम मुद्रास्फीति उत्पादन को हतोत्साहित कर सकती है और निवेशकों की भावना को कमजोर कर सकती है।
मौद्रिक नीति के निहितार्थ
- उदार रुख की आवश्यकता: मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे होने के कारण, आरबीआई को आगामी एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए।
- निवेश को प्रोत्साहित करना: कम उधारी लागत से ऋण प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, निजी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, तथा मांग मजबूत हो सकती है।
- जोखिमों को संतुलित करना: वर्तमान अवमुद्रास्फीति को देखते हुए, सख्ती का खतरा, हल्के मुद्रास्फीति जोखिम से अधिक है।
- समन्वित दृष्टिकोण: मौद्रिक सहजता को पीएम-गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी राजकोषीय पहलों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए ।
- विकास अभिविन्यास: सख्त मुद्रास्फीति नियंत्रण से हटकर मांग प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ।
पूर्वानुमान सटीकता और संस्थागत विश्वसनीयता
- बार-बार संशोधन: आरबीआई का मुद्रास्फीति अनुमान अप्रैल में 4% से घटकर सितंबर 2025 में 2.6% हो गया , जो पद्धतिगत कमियों को उजागर करता है।
- विश्वसनीयता चुनौती: पूर्वानुमान में तीव्र विचलन से मौद्रिक मार्गदर्शन में जनता और बाजार का विश्वास कमजोर होता है।
- डेटा एकीकरण की आवश्यकताएं: मॉडल में उच्च आवृत्ति उपभोग डेटा, मजदूरी प्रवृत्तियों और वैश्विक मूल्य आंदोलनों को शामिल किया जाना चाहिए।
- तकनीकी उन्नयन: एआई-संचालित नाउकास्टिंग मॉडल का उपयोग मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी में सटीकता बढ़ा सकता है।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: एमपीसी के भीतर एक समर्पित मुद्रास्फीति विश्लेषण इकाई की स्थापना से बेहतर पूर्वानुमान मानकों को संस्थागत रूप दिया जा सकता है।
सुधार और आगे की राह
- उन्नत पूर्वानुमान ढांचा: गतिशील मुद्रास्फीति आकलन के लिए वास्तविक समय डेटा, कमोडिटी रुझान और व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि को एकीकृत करें ।
- उदार मौद्रिक नीति: निवेश को पुनर्जीवित करने और उपभोग सुधार को समर्थन देने के लिए मध्यम दर में कटौती ।
- वेतन-आधारित विकास रणनीति: घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के उत्पादकता प्रोत्साहनों को वास्तविक वेतन वृद्धि के साथ जोड़ें।
- नीतिगत तालमेल: सुसंगत समष्टि-प्रबंधन के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्राधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करना ।
- पारदर्शिता और संचार: संस्थागत विश्वसनीयता बनाने के लिए त्रैमासिक मुद्रास्फीति ट्रैकर्स और सार्वजनिक डैशबोर्ड प्रकाशित करें ।
निष्कर्ष
भारत की मुद्रास्फीति की कमी की कहानी को व्यापक आर्थिक स्थिरता समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है और माँग अभी भी कमज़ोर है, ऐसे में आरबीआई की अगली चुनौती मूल्य स्थिरता और विकास में सुधार के बीच संतुलन बनाना है। सटीक पूर्वानुमान, समय पर मौद्रिक सहजता और मज़बूत नीतिगत समन्वय कम मुद्रास्फीति को टिकाऊ, समावेशी और निवेश-संचालित विकास के अवसर में बदल सकते हैं।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
भारत की अवमुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति के संदर्भ में, परीक्षण कीजिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक मूल्य स्थिरता को विकास और पूर्वानुमान सटीकता के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकता है। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द हिंदू
(जीएस पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा – साइबर सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और उभरते खतरे)
संदर्भ (परिचय)
छद्म पहचान के ज़रिए धोखाधड़ी और डिजिटल पहचान का दुरुपयोग करने वाले साइबर अपराधों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है । आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के तहत ये अपराध एक राष्ट्रीय चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि कई मामलों में आरोप नहीं लग पाते या दोषसिद्धि नहीं हो पाती, जो व्यवस्थागत प्रवर्तन की कमियों को दर्शाता है।
राष्ट्रीय रुझान
- तीव्र गति से मामलों में वृद्धि: भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टें 2021 में ~ 53,000 से बढ़कर 2023 में ~ 86,400 हो गईं, जो एक तीव्र वृद्धि को दर्शाती हैं।
- धारा 66डी का विस्तार: प्रतिरूपण-आधारित धोखाधड़ी (कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी) का हिस्सा 2019 में साइबर अपराधों के ~ 12% से बढ़कर 2023 में ~ 29% हो गया।
- राज्य संकेन्द्रण: कर्नाटक जैसे राज्यों में अत्यधिक मामले देखे गए हैं (उदाहरण के लिए 2023 में 70% से अधिक साइबर अपराध 66D के अंतर्गत थे), लेकिन यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि में भी प्रतिरूपण धोखाधड़ी के समान रुझान उभर रहे हैं।
- हाई-प्रोफाइल घोटाले: डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी – जहां पीड़ितों को फर्जी कानूनी धमकियों के माध्यम से धन हस्तांतरण करने के लिए मजबूर किया जाता है – में बड़ी वसूली और ऐतिहासिक सजाएं हुई हैं (उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में धारा 66डी से संबंधित एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई)।
- कानूनी दंड: धारा 66डी के तहत , कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है ।
कारण और संरचनात्मक कमजोरियाँ
- गुमनामी में आसानी और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग: धोखेबाज अधिकारी या विश्वसनीय संपर्कों का रूप धारण करने के लिए डीपफेक, नकली कॉल और क्लोन किए गए खातों जैसे उपकरणों का फायदा उठाते हैं।
- कम रिपोर्टिंग और जागरूकता: कई पीड़ित तुरंत प्रतिरूपण धोखाधड़ी को नहीं पहचानते या रिपोर्ट नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं।
- जांच क्षमता की कमी: पुलिस बलों में अक्सर समर्पित साइबर फोरेंसिक इकाइयों , डिजिटल साक्ष्य प्रोटोकॉल या कुशल कर्मचारियों की कमी होती है।
- डिजिटल विशेषज्ञता में न्यायिक अंतराल: न्यायालयों और अभियोजकों में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी साक्षरता का अभाव होता है, जिससे दोषसिद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।
- कानूनी-प्रक्रियात्मक अंतराल: आईटी अधिनियम, आईपीसी/बीएनएस और साक्ष्य कानूनों के अभिसरण से साइबर-प्रतिरूपण मामलों को संभालने में अस्पष्टता और देरी होती है।
- डेटा और निगरानी संबंधी अस्पष्टताएं: वर्तमान प्रणालियां गिग अर्थव्यवस्था या ग्रामीण धोखाधड़ी की कम रिपोर्टिंग करती हैं, जिससे छद्म पहचान वाले अपराध का पूरा स्तर छिप जाता है।
सुधार और नीतिगत उपाय
- डिजिटल जांच को मजबूत करना: जिला और राज्य स्तर पर साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को अनिवार्य बनाना , जिसमें चेन-ऑफ-कस्टडी, हैशिंग, मेटाडेटा आदि के लिए मानक प्रोटोकॉल हों।
- क्षमता निर्माण: राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिश के अनुसार , साइबर कानून, डिजिटल फोरेंसिक और साक्ष्य प्रबंधन में पुलिस, अभियोजकों और न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करना ।
- कानूनी अपडेट: डीपफेक, सिंथेटिक प्रतिरूपण, एआई-जनित पहचान धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से कवर करने के लिए धारा 66डी में संशोधन करें (या एक नया खंड पेश करें) ।
- विशेष साइबर न्यायालय: तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मुकदमों में तेजी लाने के लिए समर्पित साइबर अपराध पीठ या न्यायालय स्थापित करें ।
- जन जागरूकता एवं रोकथाम: डिजिटल साक्षरता अभियान का विस्तार करें; उपयोगकर्ताओं को छद्मवेशी रणनीति से बचाने के लिए गेम-आधारित घोटाला सिमुलेटर (जैसे शील्डअप!) जैसे उपकरणों का उपयोग करें।
- एकीकृत रिपोर्टिंग और निगरानी: ग्रामीण, गिग और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्रतिरूपण धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) का विस्तार करें ।
- अंतर-राज्यीय समन्वय: राज्यों के साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के संपर्क को मजबूत करना , जिससे प्रतिरूपण नेटवर्क की क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन ट्रैकिंग को सक्षम किया जा सके।
- पीड़ित सहायता एवं निवारण: प्रतिरूपण धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन, कानूनी सहायता और डिजिटल साक्ष्य पुनर्प्राप्ति सहायता प्रदान करना।
निष्कर्ष
छद्म पहचान के ज़रिए धोखाधड़ी—जिसे कभी विशिष्ट माना जाता था—अब भारत में एक व्यापक साइबर खतरा बन गया है, जो तकनीक और गुमनामी के कारण और भी बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए कानून, संस्थाओं, तकनीक और जन जागरूकता को समग्र रूप से मज़बूत करने की ज़रूरत है। तभी प्रवर्तन एजेंसियां छद्म पहचान के बदलते तरीकों पर लगाम लगा पाएंगी और बड़े पैमाने पर न्याय दिला पाएंगी।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
“भारत में साइबर प्रतिरूपण धोखाधड़ी बढ़ रही है, फिर भी दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है।” प्रवर्तन विफलताओं के कारणों पर चर्चा कीजिए और डिजिटल प्रतिरूपण अपराधों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय प्रस्तावित कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द हिंदू














