IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025 की पूर्व संध्या पर बोलते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय केवल सरकारी योजनाओं के “लाभार्थी” नहीं हैं, बल्कि “भारत की प्रगति के चालक” हैं। यह सम्मेलन ट्राइफेड जैसी संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अलग था।

ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) के बारे में:
- नोडल मंत्रालय: ट्राइफेड भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक संगठन है, जो जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित है।
- स्थापना: इसकी स्थापना अगस्त 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी।
- अधिदेश: इसका उद्देश्य देश के आदिवासियों द्वारा एकत्रित/खेती की गई लघु वन उपज (एमएफपी) और अधिशेष कृषि उपज (एसएपी) के व्यापार को संस्थागत बनाकर उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- उद्देश्य:
- जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक कल्याण का विकास करना।
- उत्पादन बढ़ाने के लिए जनजातीय समुदाय के लिए सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ कलात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्थिर आजीविका के लिए जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना।
- प्रक्रिया और गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करने तथा मंत्रालय को इनपुट प्रदान करने के लिए लक्षित समूहों की पहचान करना।
- स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान केंद्रित करना: इस दृष्टिकोण में जनजातीय लोगों को संवेदनशील बनाकर उनकी क्षमता का निर्माण करना, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करना, तथा उन्हें किसी विशेष गतिविधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन की संभावनाओं की खोज करना, जनजातीय उत्पादों के लिए स्थायी आधार पर विपणन के अवसर पैदा करना तथा एक ब्रांड का निर्माण करना शामिल है।
- खुदरा विपणन: ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम से जनजातीय उत्पादों का खुदरा विपणन करता रहा है। ट्राइफेड खुदरा दुकानों, आदिशिल्प , आदिचित्र , ऑक्टेव जैसी प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों और ई-मार्केटिंग के माध्यम से एक स्थायी बाजार को बढ़ावा देता है और उसका निर्माण करता है।
- एमएसपी का कार्यान्वयन: भारत सरकार ने ट्राइफेड को लघु वन उपज के लिए प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना को लागू करने का कार्य भी सौंपा है।
स्रोत:
श्रेणी: इतिहास और संस्कृति
प्रसंग:
- एक नई पुस्तक में दावा किया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) की स्थापना नहीं की थी , बल्कि इसकी स्थापना जापानी सेना के खुफिया विभाग और भारत के बाहर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा एक साझा दुश्मन – ब्रिटिशों से लड़ने के लिए की गई थी।

फर्स्ट आईएनए के बारे में:
- गठन: प्रथम इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) का गठन सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था।
- संरचना: इसमें लगभग 12,000 भारतीय युद्धबंदी शामिल थे जो जापानी सहायता से गठबंधन करके ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार थे। जापानियों ने अपने युद्ध प्रयासों में मदद के लिए भारतीयों सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्रवादियों से सहयोग मांगा।
- मोहन सिंह की भूमिका: कैप्टन मोहन सिंह को भारतीय युद्धबंदियों का उपयोग करके एक आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का काम सौंपा गया था। मोहन सिंह का नेतृत्व और भारतीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण का वादा भारतीय सैनिकों को आई.एन.ए. में शामिल होने के लिए प्रेरित किया ।
- प्रथम आई.एन.ए. के उदय के कारण : भारतीय सैनिकों और नागरिकों के आईएनए में शामिल होने के कारणों में राष्ट्रवाद, अंग्रेजों द्वारा विश्वासघात की भावना , नस्लीय भेदभाव और जापानियों का डर शामिल था ।
- प्रथम आईएनए का विघटन: हालाँकि, सेना के नेतृत्व और भूमिकाओं पर नियंत्रण को लेकर मतभेद और अविश्वास पैदा हो गया। कब्जे वाले क्षेत्रों में जापानी सैन्य प्रशासन की नीतियों को लेकर भी संघर्ष छिड़ा। मोहन सिंह ने बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ जापान के अभियान के लिए आईएनए सैनिक उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और दिसंबर 1942 तक प्रथम आईएनए को भंग कर दिया गया।
द्वितीय आईएनए के बारे में:
- एस.सी. बोस का सिंगापुर आगमन: जुलाई 1943 में, बोस सिंगापुर पहुंचे और आई.एन.ए. का नेतृत्व संभाला, तथा इसे केवल जापानी सैन्य लक्ष्यों का समर्थन करने के बजाय एक राष्ट्रवादी बल के रूप में पुनः स्थापित किया।
- द्वितीय आई.एन.ए. का गठन: आजाद हिंद फौज या द्वितीय आई.एन.ए. का गठन प्रथम आई.एन.ए. के अवशिष्ट सैनिकों को दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़ी संख्या में आए भारतीय नागरिक स्वयंसेवकों के साथ एकीकृत करके किया गया था, जो बोस के नेतृत्व और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ हथियार उठाने के आह्वान से उत्साहित थे।
- प्रथम आज़ाद हिंद फौज से अंतर: प्रथम आज़ाद हिंद फौज के विपरीत, जिसमें अनेक अधिकार केंद्र थे, बोस के नेतृत्व में द्वितीय आज़ाद हिंद फौज पूरी तरह से बोस के प्रति समर्पित थी। मिश्रित रेजिमेंटों और राजनीतिक प्रशिक्षण के माध्यम से जातीय और क्षेत्रीय निष्ठाओं को राष्ट्रीय भावनाओं के अंतर्गत समाहित कर लिया गया था। राष्ट्रवादी नेताओं के नाम पर रेजिमेंटों के नामकरण की प्रथा जारी रही, जिससे एकता की भावना को बढ़ावा मिला।
- संरचना: आईएनए को तीन ब्रिगेडों में विभाजित किया गया था – गांधी, आज़ाद और नेहरू। अपनी चरम शक्ति पर, आईएनए में लगभग 60,000 सैनिक थे, जिनमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व वाली महिला सैनिकों वाली रानी झाँसी रेजिमेंट भी शामिल थी।
- अपनी मुद्रा: आई.एन.ए. की अपनी मुद्रा, डाक टिकट और प्रतीक थे जो स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को दर्शाते थे।
- राष्ट्रीय ध्वज: सुभाष चंद्र बोस ने पहली राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज और टैगोर के गीत ‘जन गण मन अधिनायक’ को राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तुत किया। उछलते हुए बाघ के प्रतीक और ‘ इत्तेफाक , एतेमाद, कुर्बानी’ के आदर्श वाक्य वाले आज़ाद हिंद फौज के ध्वज ने राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया।
स्रोत:
श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी
प्रसंग:
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने हाल ही में कहा कि पश्चिम से आयातित कई पर्यावरण कानून सिद्धांत जैसे कि “अंतर-पीढ़ीगत समानता” मानव-केंद्रित हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने में शायद ही कोई मदद कर पाएंगे।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में:
- राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ( अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स) भारत का सबसे संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है।
- प्रमुख प्रजातियाँ: इसे प्रमुख घासभूमि प्रजाति माना जाता है, जो घासभूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है।
- विस्तार: इसकी जनसंख्या मुख्यतः राजस्थान और गुजरात तक सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी छोटी संख्या पाई जाती है।
- खतरे: बिजली की लाइनों से टकराने/बिजली का झटका लगने, शिकार (जो अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित है), व्यापक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप आवास की हानि और परिवर्तन आदि के कारण यह पक्षी लगातार खतरे में रहता है।
- धीमी प्रजनन प्रजातियाँ: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) धीमी प्रजनन वाली प्रजातियाँ हैं। ये कुछ अंडे देते हैं और लगभग एक साल तक चूज़ों की देखभाल करते हैं। ये लगभग 3-4 साल में परिपक्व हो जाता है।
- प्रजनन काल: वे ज्यादातर मानसून के मौसम में प्रजनन करते हैं, जब मादा खुले मैदान में एक अंडा देती है।
- शारीरिक विशेषताएँ: यह एक बड़ा पक्षी है जिसका शरीर क्षैतिज और लंबे, नंगे पैर होते हैं, जिससे यह शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है। दोनों लिंग लगभग एक ही आकार के होते हैं, सबसे बड़े पक्षी का वजन 15 किलो (33 पाउंड) होता है। इसे माथे पर काले मुकुट से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो पीली गर्दन और सिर के विपरीत है।
- जीवनकाल: इनका जीवनकाल आमतौर पर लगभग 12-15 वर्ष का होता है।
- आहार पद्धति: इनका आहार मौसम के अनुसार उपलब्ध भोजन पर निर्भर करता है। ये घास के बीज, टिड्डे और भृंग जैसे कीड़े, और कभी-कभी छोटे कृंतक और सरीसृप भी खाते हैं।
- संरक्षण स्थिति:
- IUCN लाल सूची: गंभीर रूप से लुप्तप्राय
- वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES): परिशिष्ट 1
- प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएमएस): परिशिष्ट I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- जीआईबी के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:
- प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम: इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के अंतर्गत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है।
- फायरफ्लाई बर्ड डायवर्टर: ये बिजली की लाइनों पर लगाए जाने वाले फ्लैप होते हैं। ये जीआईबी जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए रिफ्लेक्टर का काम करते हैं।
- प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड: इसे राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रजाति के लिए प्रजनन बाड़ों का निर्माण करने और इसके आवासों पर मानवीय दबाव को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए शुरू किया गया है।
स्रोत:
श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
प्रसंग:
- इथियोपिया सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की एक सप्ताह की अध्ययन यात्रा पूरी कर ली है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल, DAY-NRLM की कार्यान्वयन रणनीतियों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
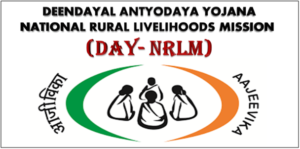
दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के बारे में:
- शुभारंभ: इसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के पुनर्गठित संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में, इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) कर दिया गया ।
- उद्देश्य: मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे वे स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ा सकें।
- कार्यान्वयन: यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- विश्व बैंक की भूमिका: विश्व बैंक भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) को वित्त पोषण, तकनीकी सहायता और प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है।
- एजेंडा: एनआरएलएम ने देश के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संघीय संस्थानों के माध्यम से कवर करने और 8-10 वर्षों की अवधि में आजीविका सामूहिकता के लिए उन्हें समर्थन देने का एजेंडा तैयार किया है।
- क्षमता निर्माण पर ध्यान: एनआरएलएम गरीबों की जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करने में विश्वास करता है और उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए क्षमताओं (सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त और सामूहिकता) के साथ पूरक बनाता है।
- योजना की मुख्य विशेषताएं:
- सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी: प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम 1 महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है।
- समुदाय के स्तर पर गरीबों की सहभागी पहचान की एक सुपरिभाषित, पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- सामुदायिक निधियां स्थायी संसाधन के रूप में: एनआरएलएम गरीबों की संस्थाओं को स्थायी संसाधन के रूप में रिवाल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्रदान करता है, ताकि उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जा सके।
- वित्तीय समावेशन: एनआरएलएम वित्तीय समावेशन के माँग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। माँग पक्ष पर, यह गरीबों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को उत्प्रेरक पूँजी प्रदान करता है। आपूर्ति पक्ष पर, मिशन वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करता है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय संवाददाताओं और ‘बैंक मित्र’ जैसे सामुदायिक सुविधा प्रदाताओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
स्रोत:
श्रेणी: भूगोल
प्रसंग:
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने गंभीर पारिस्थितिक जोखिमों के कारण कर्नाटक की 2000 मेगावाट की शरावती पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना (शरावती नदी पर) को स्थगित करने का निर्णय लिया।

शरावती पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना के बारे में:
- स्थान: यह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती नदी पर प्रस्तावित एक पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना है।
- विद्युत क्षमता: इसे 2,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- तालाकाले बांध और गेरुसोप्पा बांध, के बीच एक पंप स्टोरेज पावर प्लांट का निर्माण शामिल है। व्यस्ततम घंटों के दौरान पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाएगा और अधिकतम मांग के दौरान बिजली उत्पादन के लिए नीचे की ओर छोड़ा जाएगा।
- कालेश्वरम परियोजना पर आधारित : यह तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना की तर्ज पर बनाई गई है , इसका उद्देश्य बेंगलुरु को पेयजल की आपूर्ति करना भी है।
- चिंताएं: यह परियोजना शरावती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के अंतर्गत आती है, जो लुप्तप्राय शेर-पूंछ वाले मकाक, हॉर्नबिल, किंग कोबरा और पश्चिमी घाट की कई स्थानिक पौधों की प्रजातियों का घर है।
शरावती नदी के बारे में:
- स्थान: यह पश्चिमी कर्नाटक राज्य में स्थित एक नदी है। नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है।
- पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी : यह भारत की उन कुछ नदियों में से एक है जो पश्चिम दिशा में बहती है।
- मार्ग: पश्चिमी घाट से निकलकर यह नदी उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती है और उत्तर कन्नड़ जिले के निकट होन्नावर में अरब सागर में गिरती है ।
- कुल लम्बाई: नदी लगभग 128 किमी लम्बी है।
- क्षेत्रफल: नदी बेसिन का क्षेत्रफल 2,985 वर्ग किमी है।
- जोग जलप्रपात: अपने रास्ते में, शरावती नदी भारत के सबसे ऊँचे झरनों में से एक, जोग जलप्रपात बनाती है, जहाँ यह नदी 253 मीटर की ऊँचाई से गिरती है। इस नदी के मार्ग में विविध भूवैज्ञानिक विशेषताएँ हैं, जिनमें चट्टानी उभार, उपजाऊ मैदान और गहरी घाटियाँ शामिल हैं।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीहोल , हरिद्रावति, मविनाहोल , हिलकुंजी , येनहोल , हुर्लिहोल और नागोडिहोल शामिल हैं।
स्रोत:
(MAINS Focus)
(यूपीएससी जीएस पेपर III – सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध)
संदर्भ (परिचय)
10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट, जिसमें 13 लोग मारे गए, ने एक बार फिर आतंकवाद के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर किया है। पुलिस व्यवस्था से परे, यह सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक संयम और राज्य की वैधता पर केंद्रित एक व्यापक आतंकवाद-रोधी ढाँचे की माँग करता है।
मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए
- आतंकी खतरों का बदलता स्वरूप: यह विस्फोट एक चिंताजनक बदलाव का संकेत है, क्योंकि संगठित आतंकी घटनाएँ पहले ज़्यादातर संघर्ष क्षेत्रों तक ही सीमित थीं। राष्ट्रीय राजधानी को निशाना बनाकर किए गए हमले शांति को अस्थिर करने और नागरिकों की सुरक्षा की भावना को कम करने के नए प्रयासों का संकेत देते हैं।
- मजबूत कानूनी और संस्थागत तंत्र: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम का उपयोग , और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भागीदारी , आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचे को प्रदर्शित करती है।
- निवारक खुफिया जानकारी और समन्वय: प्रभावी खुफिया जानकारी जुटाने से कई संभावित हमलों को नाकाम किया गया है, जिनमें एक संभावित रासायनिक हमला भी शामिल है। आतंकवाद-रोधी अभियानों की सफलता अक्सर अंतर-एजेंसी समन्वय और वास्तविक समय में डेटा साझा करके अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने में निहित होती है।
- राजनीतिक और मीडिया ज़िम्मेदारी की आवश्यकता: राजनीतिक बयानबाज़ी और अटकलबाज़ी से भरी मीडिया कवरेज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकती है, जिससे अनजाने में आतंकवादी उद्देश्यों को बढ़ावा मिलता है। जनता की शांति और संस्थाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों का ज़िम्मेदाराना रवैया ज़रूरी है।
- आतंकवाद-निरोध का मूल आधार सामाजिक सद्भाव है: आतंकवादी समूह विभाजन और अलगाव का फायदा उठाते हैं। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में कट्टरपंथियों की भर्ती रोकने और लोकतांत्रिक वैधता को सुदृढ़ करने के लिए कट्टरपंथ से मुक्ति, अंतर-धार्मिक संवाद, समावेशी शासन और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करना आवश्यक है।
आलोचनाएँ / कमियाँ उजागर
- सुरक्षा कानूनों का अतिक्रमण: यूएपीए के कड़े प्रावधान, जैसे कि लंबे समय तक हिरासत और सीमित जमानत, अक्सर नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए आलोचना को आकर्षित करते हैं।
- अत्यधिक सुरक्षाकरण: कट्टरपंथ की सामाजिक जड़ों को संबोधित किए बिना बल पर अत्यधिक निर्भरता समुदायों को अलग-थलग कर सकती है।
- समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण का अभाव: आतंकवाद-निरोध अत्यधिक संस्थागत बना हुआ है, जिसमें जमीनी स्तर पर भागीदारी या पुनर्वास तंत्र न्यूनतम है।
- मीडिया सनसनीखेज: गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से दहशत बढ़ती है और अनजाने में भय फैलता है।
- राजनीतिक शोषण: आतंकवादी घटनाओं का राजनीतिकरण राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और नीति-आधारित समाधानों से ध्यान हटाता है।
उल्लिखित / सुझाए गए सुधार
- एकीकृत आतंकवाद निरोधक ढांचा: खुफिया, पुलिस, न्यायपालिका और समुदाय-आधारित रोकथाम तंत्र को जोड़ने वाला एक व्यापक मॉडल अपनाना।
- कट्टरपंथ से मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम: केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मॉडलों को आगे बढ़ाना, जिनमें परामर्श, शिक्षा और ऑनलाइन कट्टरपंथ निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
- पुलिस और फोरेंसिक आधुनिकीकरण: तकनीकी उन्नयन और तीव्र जांच के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना को मजबूत करना ।
- न्यायिक निगरानी और पारदर्शिता: दुरुपयोग को रोकने और मुकदमों में तेजी लाने के लिए यूएपीए मामलों के लिए स्वतंत्र समीक्षा तंत्र स्थापित करना।
- सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना: एकता और लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए अंतर-सामुदायिक शांति समितियों, स्थानीय आउटरीच अभियानों और नागरिक शिक्षा पहलों को संस्थागत बनाना।
निष्कर्ष:
आतंकवाद भय और विभाजन पर पनपता है; इसका सबसे प्रभावी प्रतिकार एकता और विश्वास है। भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र को मज़बूत सुरक्षा उपायों को करुणा और समावेशिता के साथ संतुलित करना होगा। आतंकवाद-रोधी नीति में सामाजिक सद्भाव को शामिल करके, राज्य अपनी वैधता और नागरिकों के न्याय में विश्वास, दोनों को मज़बूत करता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
आतंकवाद का उद्देश्य समाज में भय और विभाजन पैदा करना है। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि सामाजिक सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देना भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति का एक अभिन्न अंग कैसे बन सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत: द हिंदू
(यूपीएससी जीएस पेपर III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विकास और उनके अनुप्रयोग; विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे)
संदर्भ (परिचय)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( MeitY ) ने “नुकसान न पहुँचाएँ (Do No Harm)” के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए शासन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं । इनका उद्देश्य जोखिम-आधारित विनियमन और अनुकूली ढाँचों के माध्यम से नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करना है।
मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए
- संतुलित और अनुकूल नियामक दृष्टिकोण: सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक “हल्का” नियामक रुख अपनाया है, साथ ही एआई के नैतिक और सुरक्षा जोखिमों का भी समाधान किया है। एक अलग एआई कानून बनाने के बजाय, यह ढाँचा आईटी अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे मौजूदा अधिनियमों का लाभ उठाता है ।
- छह-स्तंभ शासन ढाँचा: ये दिशानिर्देश बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण, नीति और विनियमन, जोखिम न्यूनीकरण, जवाबदेही और संस्थानों के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। यह समग्र दृष्टिकोण एआई विकास को देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे (आधार, यूपीआई) और आर्थिक रणनीति के साथ एकीकृत करता है।
- जोखिम न्यूनीकरण और जवाबदेही पर ध्यान: एक भारत-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन मॉडल एआई के क्षेत्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। एक श्रेणीबद्ध दायित्व व्यवस्था जवाबदेही को कार्य और जोखिम स्तर से जोड़ती है। एआई घटना डेटाबेस और स्व-प्रमाणन प्रणालियों के निर्माण का उद्देश्य पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- एआई गवर्नेंस के लिए संस्थागत तंत्र: इस ढांचे में एक बहु-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है: निरीक्षण के लिए एक एआई गवर्नेंस समूह (एआईजीजी) , नीति संरेखण के लिए एक प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी) , और तकनीकी ऑडिट और अनुपालन के लिए एक एआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई) ।
- मानव-केंद्रित और समावेशी विकास: सभी के लिए एआई पर ज़ोर देते हुए , दिशानिर्देश कौशल विकास कार्यक्रमों, नागरिकों में एआई साक्षरता और कर छूट तथा एआई-संबंधित ऋणों के माध्यम से एमएसएमई को लक्षित सहायता प्रदान करने का आह्वान करते हैं। इसका लक्ष्य एआई पारिस्थितिकी तंत्र में समान पहुँच सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन को रोकना है।
आलोचनाएँ / कमियाँ उजागर
- समर्पित एआई कानून का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि मौजूदा ढांचे पर निर्भर रहने से स्पष्ट दायित्व, डेटा उपयोग मानदंडों और एआई दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की स्थापना में देरी हो सकती है।
- राज्य निगरानी का जोखिम: सार्वजनिक अवसंरचना में एआई का एकीकरण मजबूत डेटा संरक्षण प्रवर्तन के बिना गोपनीयता और स्वायत्तता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है।
- डीपफेक पर कमजोर निगरानी: यद्यपि सामग्री प्रमाणीकरण प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन गैर-अनुपालन के खिलाफ एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र की कमी प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है।
- विदेशी एआई प्रणालियों का सरकारी उपयोग: वैश्विक एआई मॉडल द्वारा संवेदनशील आधिकारिक डेटा को संसाधित किए जाने के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, जिससे रणनीतिक अनुमान और डेटा लीक होने का खतरा है।
- स्वैच्छिक अनुपालन मॉडल: स्व-नियमन और स्वैच्छिक ढांचे पर अत्यधिक निर्भरता जवाबदेही को सीमित कर सकती है, विशेष रूप से निजी अभिकर्ताओं के बीच।
उल्लिखित / सुझाए गए सुधार
- तकनीकी-कानूनी सुरक्षा उपाय: गोपनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को सीधे एआई प्रणाली डिजाइन में शामिल करना – नैतिक डिजाइन विकास को बढ़ावा देना।
- एआई सामग्री लेबलिंग: कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री के प्रकटीकरण को अनिवार्य करने के लिए आईटी नियमों में संशोधन करें, जिससे प्लेटफार्मों को डीपफेक और एआई-निर्मित मीडिया पर दृश्य लेबल प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।
- क्षमता और कौशल निर्माण: साक्षरता और जिम्मेदार उपयोग में सुधार के लिए नागरिकों, लोक सेवकों और कानून प्रवर्तन के लिए एआई प्रशिक्षण को मजबूत करना।
- सार्वजनिक-निजी सहयोग: औद्योगिक विकास को नैतिक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए संयुक्त एआई नवाचार सैंडबॉक्स और क्रॉस-सेक्टर साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत के नियामक रुख को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सुसंगत बनाने के लिए एआई मानकों और नैतिकता पर वैश्विक मंचों में भाग लेना।
निष्कर्ष:
भारत के एआई दिशानिर्देश ज़िम्मेदार नवाचार की दिशा में एक व्यावहारिक कदम हैं—जो एआई-संचालित विकास के वादे को दुरुपयोग के जोखिमों के साथ संतुलित करते हैं। “किसी को नुकसान न पहुँचाएँ” पर ज़ोर देकर, मानव-केंद्रित मूल्यों को बढ़ावा देकर, और एआई को शासन में सावधानीपूर्वक एकीकृत करके, भारत खुद को नैतिक, समावेशी और नवाचार-अनुकूल एआई विनियमन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
“भारत का नया एआई गवर्नेंस ढाँचा नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।” उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़ी नैतिक, कानूनी और संस्थागत चुनौतियों के आलोक में इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस











