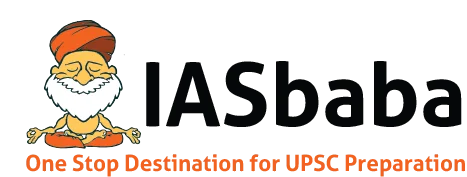IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
Archives
(PRELIMS MAINS Focus)
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
प्रसंग : भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन और भारत के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर पुनर्विचार करना ।
संदर्भ का दृष्टिकोण:
आईडब्ल्यूटी पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है:
- सिंधु जल संधि (1960) पर विभाजन के बाद नई भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के समय हस्ताक्षर किए गए थे।
- पाकिस्तान की निचली तटवर्ती स्थिति के कारण वह असुरक्षित था, जिसके कारण पश्चिमी मध्यस्थता से समझौता करना पड़ा।
- यह संधि कभी भी एक साधारण जल-बंटवारे का समझौता नहीं थी, बल्कि विश्व बैंक और पश्चिमी शक्तियों से जुड़ी शीत युद्ध युग की भूराजनीति का परिणाम थी।
जलवायु परिवर्तन एवं जल विज्ञान संबंधी प्रभाव:
- जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है: जिसमें ग्लेशियरों के पिघलने, नदियों के प्रवाह और भंडारण की आवश्यकताओं में परिवर्तन शामिल हैं।
- इस संधि में जल की उपलब्धता में परिवर्तन या चरम मौसम की घटनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है ।
- भंडारण क्षमता और जलविद्युत की आवश्यकता को पुनः वार्ता में शामिल किया जाता है।
संधि में विषमता:
- निचले तटवर्ती देश के रूप में पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर भारतीय परियोजनाओं पर वीटो शक्ति प्राप्त है।
- भारत को बेसिन का केवल 20% जल ही प्राप्त होता है।
- यह संधि पारस्परिक नहीं है, जिससे पाकिस्तान को अधिक लाभ मिलेगा और भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं में देरी होगी।
पुनर्वार्ता की रणनीतिक आवश्यकता:
- भारत को अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए तथा वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली शर्तों पर पुनः बातचीत करनी चाहिए ।
- संशोधित संधि में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए:
- भारत की जलवायु और विकासात्मक आवश्यकताएं,
- अन्य नदी प्रणालियों पर चीन और बांग्लादेश का प्रभाव,
- सिंधु बेसिन की वैज्ञानिक समझ (जैसे, हिमनद विज्ञान, जल विज्ञान) ।
Learning Corner:
सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty – IWT)
- हस्ताक्षरित: 1960
- पक्षकार: भारत और पाकिस्तान, विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता
- उद्देश्य: भारत (ऊपरी तटवर्ती) और पाकिस्तान (निचले तटवर्ती) के बीच सिंधु नदी प्रणाली का जल-बंटवारा
प्रमुख प्रावधान:
- पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब): पाकिस्तान को आवंटित, भारत को सीमित उपयोग की अनुमति (जल विद्युत जैसे गैर-उपभोग्य उपयोग)
- पूर्वी नदियाँ (रावी, व्यास, सतलुज): भारत को आवंटित
- स्थायी सिंधु आयोग: सहयोग और विवाद समाधान के लिए स्थापित
- विवाद तंत्र: इसमें वार्ता, तटस्थ विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शामिल है
स्रोत: THE INDIAN EXPRESS
श्रेणी: राजनीति
संदर्भ: भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के तहत चार स्वायत्त बोर्डों में से तीन में कोई अध्यक्ष नहीं हैं।
वर्तमान समस्याएँ:
- 4 में से 3 बोर्डों में अध्यक्ष नहीं हैं; अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है या उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है।
- बोर्ड तदर्थ तरीके से काम कर रहे हैं, निरीक्षण, निर्णय और पाठ्यक्रम अद्यतन को रोक रहे हैं।
- 18 में से 11 बोर्ड पद और 6 अंशकालिक पद रिक्त हैं।
- यहां तक कि कॉलेजों का वर्चुअल निरीक्षण भी गैर-तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता आश्वासन पर चिंताएं पैदा हो रही हैं।
- इस्तीफों को आधिकारिक रूप से स्वीकार न किये जाने से नेतृत्व शून्यता और भी बदतर हो गई है।
परिणाम:
- नये मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण और सीट नवीनीकरण में देरी हो रही है।
- शैक्षणिक परिवर्तन (जैसे, LGBTQ+ मुद्दों पर पाठ्यक्रम अद्यतन, नैतिकता) रुके हुए हैं।
- आयोग की कोई पूर्ण बैठक नहीं हुई है।
- नियामक निष्क्रियता के कारण छात्र और कॉलेज प्रभावित हो रहे हैं।
Learning Corner:
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)
पृष्ठभूमि:
- स्थापना: सितंबर 2020
- निम्न के द्वारा: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा)
- उद्देश्य: चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्रशासन में सुधार, पारदर्शिता और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से जुड़े भ्रष्टाचार को खत्म करना।
एनएमसी की संरचना:
- अध्यक्ष
- 10 पदेन सदस्य
- 22 अंशकालिक सदस्य
- 4 स्वायत्त बोर्ड (अत्यंत महत्वपूर्ण):
- स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB)
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB)
- मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (MARB)
- नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (EMRB)
प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है तथा वह विशिष्ट विनियामक कार्य करता है।
एनएमसी के प्रमुख कार्य:
- चिकित्सा संस्थानों, शिक्षा और पेशेवरों को विनियमित करना।
- स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम मानक तैयार करना।
- नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और सीटों की वृद्धि की अनुमति प्रदान करना।
- लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना।
- नैतिक आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना।
- अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) आयोजित करना (यह एक लाइसेंसिएट परीक्षा और पीजी प्रवेश परीक्षा के रूप में कार्य करेगा)।
- साक्ष्य-आधारित चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को बढ़ावा देना।
स्रोत: THE INDIAN EXPRESS
श्रेणी: अर्थशास्त्र
संदर्भ: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट (OBBBA) पारित किया है, जो गैर-वाणिज्यिक विदेशी प्रेषण पर 1% कर लगाएगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
कर का विवरण:
- शुरू में 5% प्रस्तावित था, बाद में घटाकर 1% कर दिया गया ।
- यह नियम नकदी, मनीऑर्डर, कैशियर चेक या मनी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अनौपचारिक स्थानान्तरण पर लागू होता है।
- छूट:
- 15 डॉलर से कम के स्थानान्तरण
- बैंक खातों या अमेरिका द्वारा जारी डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके स्थानान्तरण।
भारत पर प्रभाव:
- भारत में इसका सीमित प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि:
- अधिकांश धन प्रेषण औपचारिक चैनलों का उपयोग करते हैं, जो छूट प्राप्त हैं ।
- भारतीय धन प्रेषण को जनवरी 2026 से पहले अग्रिम रूप से भेजा जा सकता है।
- नया कर पहले के प्रस्तावों की तुलना में हल्का है ।
- सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अनुसार, मेक्सिको के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश होगा, लेकिन प्रभाव अभी भी मामूली होगा ।
Learning Corner:
भारत को प्रेषित धनराशि (2025)
भारत वैश्विक प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिसने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 135.46 बिलियन डॉलर प्राप्त किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। ये अंतर्वाह भारत के भुगतान संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं , जो देश की चालू खाता प्राप्तियों का 10% से अधिक है।
प्रमुख स्रोत देश:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (सबसे बड़ा योगदानकर्ता)
- यूनाइटेड किंगडम
- सिंगापुर
- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब
विकसित देश अब कुल अंतर्वाह में लगभग 45% का योगदान करते हैं, जबकि बदलते प्रवासन पैटर्न के कारण जीसीसी देशों की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई है।
रुझान और प्रमुख चालक:
- ओईसीडी देशों में उच्च-कुशल भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि
- प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि, अब 18 मिलियन से अधिक
- औपचारिक बैंकिंग चैनलों का सशक्त उपयोग
- डिजिटल धनप्रेषण प्लेटफार्मों का बढ़ता उपयोग
आर्थिक महत्व:
- व्यापार घाटे की भरपाई में मदद करता है
- विदेशी मुद्रा के एक स्थिर स्रोत के रूप में कार्य करता है
- अक्सर मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से अधिक होता है
- घरेलू उपभोग, ग्रामीण व्यय और वित्तीय समावेशन का समर्थन करता है
स्रोत : THE INDIAN EXPRESS
श्रेणी: संस्कृति
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद की यात्रा के दौरान एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासियों के बीच रामलीला की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए भगवान राम को “महासागरों से परे दिव्य कड़ी” कहा।
त्रिनिदाद और भारतीय जड़ें:
- त्रिनिदाद और टोबैगो की जनसंख्या लगभग 13 लाख है, जिसमें से एक बड़ा प्रतिशत भारत से जुड़ा है।
- 1838 और 1917 के बीच भारतीय गिरमिटिया मजदूर यहां पहुंचे, जिनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे।
- वे अपने साथ सांस्कृतिक परम्पराएं लेकर आए, विशेषकर रामलीला – तुलसीदास के रामचरितमानस का नाटकीय पुनर्कथन।
राम को समुद्र पार ले जाना:
- यद्यपि उनके पास बहुत कम संपत्ति थी, फिर भी प्रवासी लोग रामचरितमानस जैसे ग्रंथ अपने साथ ले गए या उसे स्मृति के रूप में संरक्षित कर लिया।
- यह परंपरा विदेशी धरती पर सांस्कृतिक निरन्तरता और पहचान का प्रतीक बन गयी।
- रामलीला का प्रदर्शन ग्रामीण परिवेश में किया जाता था, जिसमें प्रायः स्थानीय भोजपुरी गीत गाए जाते थे तथा समुदाय के सभी सदस्य इसमें भाग लेते थे।
पहचान का प्रतीक:
- भारतीय-त्रिनिदादवासियों के लिए, रामलीला एक सांस्कृतिक आधार और ‘भारतीयता ‘ का प्रतीक बनी हुई है, यहां तक कि पश्चिमी कैरेबियाई संदर्भ में भी।
- समुदाय भगवान राम की शिक्षाओं को आत्मसात करने और उनकी पुनर्व्याख्या करने में लगा हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय भारतीय पहचान मजबूत हो रही है।
Learning Corner:
रामलीला
रामलीला भगवान राम के जीवन और कहानी का पारंपरिक, नाटकीय पुनः मंचन है, जो मुख्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा महाकाव्य रामचरितमानस पर आधारित है। यह लोक रंगमंच का एक जीवंत रूप है जो विशेष रूप से उत्तरी भारत में लोकप्रिय है , जिसे नवरात्रि के दौरान प्रदर्शित किया जाता है , जिसका समापन दशहरा में रावण के पुतले के प्रतीकात्मक दहन के साथ होता है।
उत्पत्ति एवं महत्व:
- भक्ति आंदोलन से प्रेरित रामलीला ने 16वीं शताब्दी में राम के जीवन की भक्तिपूर्ण पुनर्कथन के साथ लोकप्रियता हासिल की ।
- यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें नाटक, संगीत और नैतिक शिक्षा का संयोजन होता है।
- यह धर्म, त्याग और निष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है।
भारत में लोक रंगमंच
लोक रंगमंच पारंपरिक प्रदर्शन कला का एक जीवंत और विविधतापूर्ण रूप है जो नैतिक, धार्मिक और सामाजिक संदेश देने के लिए कहानी कहने, संगीत, नृत्य, नाटक और अनुष्ठानों को जोड़ता है। स्थानीय संस्कृति और बोलियों में निहित, लोक रंगमंच ने ऐतिहासिक रूप से, खासकर ग्रामीण भारत में शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक सुधार के माध्यम के रूप में काम किया है।
मुख्य विशेषताएं:
- मौखिक परंपरा: बिना लिखित लिपि के पीढ़ियों से चली आ रही।
- सामुदायिक भागीदारी: दर्शकों की सक्रिय भागीदारी के साथ खुले स्थानों में प्रदर्शन किया जाता है।
- धार्मिक और पौराणिक विषय: अक्सर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर आधारित ।
- स्थानीय भाषा और मुहावरों का प्रयोग: ग्रामीण और अर्ध-साक्षर दर्शकों के लिए सुलभ।
क्षेत्रीय प्रपत्र:
| क्षेत्र | लोक रंगमंच का स्वरूप |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | रामलीला, नौटंकी |
| महाराष्ट्र | तमाशा |
| कर्नाटक | यक्षगान |
| आंध्र प्रदेश | बुराकाथा (Burrakatha) |
| पश्चिम बंगाल | जात्रा |
| राजस्थान | ख़याल, माच |
| पंजाब | भांड पाथेर, नक़ल (Naqal) |
| ओडिशा | प्रहलाद नाटक, दसकठिया |
सांस्कृतिक महत्व:
- स्थानीय परम्पराओं, भाषा और इतिहास को संरक्षित करता है।
- सामाजिक टिप्पणी और राजनीतिक व्यंग्य के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
- सामुदायिक बंधन और सामूहिक पहचान को प्रोत्साहित करता है।
स्रोत : THE INDIAN EXPRESS
श्रेणी: भूगोल
संदर्भ: भारत सरकार ने एल्युमीनियम और तांबा क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक विज़न दस्तावेज़ जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना, संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित करना और 2047 तक “विकसित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने के हिस्से के रूप में हरित विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
एल्युमीनियम विजन: मुख्य विशेषताएं
- लक्ष्य: 2047 तक उत्पादन को छह गुना बढ़ाकर 37 MTPA करना।
- कच्चे माल की सुरक्षा: बॉक्साइट उत्पादन को 150 MTPA तक बढ़ाना ।
- सततता: एल्युमीनियम पुनर्चक्रण दर को दोगुना करना; निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- नीतिगत समर्थन: सिद्ध भंडार, सुधार ढांचे और नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ उद्योग सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना ।
कॉपर/ तांबा विजन: मुख्य विशेषताएं
- लक्ष्य: 2047 तक घरेलू मांग में छह गुना वृद्धि ।
- क्षमता संवर्धन: 2030 तक 5 MTPA शोधन क्षमता जोड़ना ।
- पुनर्चक्रण पर ध्यान: आयात निर्भरता को कम करने के लिए द्वितीयक शोधन को बढ़ावा देना ।
- वैश्विक रणनीति: विदेशी खनिज परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना तथा विदेशी शोधन सुविधाएं स्थापित करना।
सामरिक महत्व
- स्वच्छ ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा: तांबा और एल्युमीनियम सौर ऊर्जा, ई.वी. और पावर ग्रिड के लिए आवश्यक हैं।
- आर्थिक विकास: निर्माण, परिवहन और मशीनरी क्षेत्रों को समर्थन मिलने की उम्मीद है ।
- सततता: जिम्मेदार खनन पर जोर और खदान बंद करने के 6 आर (पुनः प्राप्ति, पुनः प्रयोजन, पुनर्वास, पुनः वनस्पतिकरण, उपचार, त्याग) को अपनाना।
Learning Corner:
भारत में एल्युमिनियम और तांबा उत्पादक स्थान
भारत अलौह धातु संसाधनों, विशेष रूप से बॉक्साइट (एल्यूमीनियम के लिए) और तांबे के अयस्क में समृद्ध है। ये संसाधन विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जो देश के एल्यूमीनियम और तांबा उद्योगों की रीढ़ हैं।
एल्युमिनियम उत्पादन (बॉक्साइट भंडार पर आधारित)
प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य:
- ओडिशा
- सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार धारक और एल्यूमीनियम उत्पादक
- प्रमुख स्थल: पंचपटमाली (कोरापुट), कोडिंगमाली
- प्रमुख कम्पनियाँ: नाल्को, वेदांता
- छत्तीसगढ
- कबीरधाम एवं सरगुजा जिले में अभ्यारण्य
- भविष्य के विस्तार की कुंजी
- झारखंड
- उल्लेखनीय क्षेत्र: लोहरदगा , गुमला
- हिंडाल्को खनन और शोधन इकाइयों का संचालन करती है
- महाराष्ट्र
- कोल्हापुर जिला एक प्रमुख खनन क्षेत्र है
- गुजरात
- जामनगर और कच्छ क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है
एल्युमिनियम स्मेल्टर हब:
- अंगुल (ओडिशा) – नाल्को
- झारसुगुड़ा (ओडिशा) – वेदांता
- रेनुकूट (उत्तर प्रदेश) -हिण्डाल्को
- कोरबा (छ.ग.) -बालको
तांबा उत्पादन
प्रमुख तांबा अयस्क उत्पादक राज्य:
- राजस्थान
- तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक
- मुख्य बेल्ट: खेतड़ी-सिंघाना (झुंझुनू जिला)
- हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) प्रमुख ऑपरेटर है
- मध्य प्रदेश
- मलांजखंड (बालाघाट जिला) में भारत की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान है
- एचसीएल द्वारा संचालित
- झारखंड
- घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम जिला) में लंबे समय से भूमिगत खनन कार्य चल रहा है
तांबा प्रगलन इकाइयाँ:
- थूथुकुडी (तमिलनाडु) – स्टरलाइट कॉपर (2018 से बंद)
- दाहेज (गुजरात) – हिंडाल्को
- भरूच (गुजरात) – बिड़ला कॉपर
स्रोत: THE HINDU
(MAINS Focus)
प्रसंग
भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके चार स्वायत्त बोर्डों में से तीन नौ महीने से अधिक समय से अध्यक्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण निर्णय, मेडिकल कॉलेज निरीक्षण और अकादमिक प्रशासन में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे नियामक विश्वसनीयता और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
परिचय
पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की जगह सितंबर 2020 में एनएमसी का गठन किया गया था । इसमें चार प्रमुख स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं:
- यूजी और पीजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UG & PG Medical Education Board)
- मेडिकल मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (Medical Assessment and Rating Board (MARB)
- नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (Ethics and Medical Registration Board (EMRB)
- सलाहकार बोर्ड (अध्यक्ष: एनएमसी अध्यक्ष)
एनएमसी का महत्व:
- विनियमन की पारदर्शी, योग्यता-आधारित प्रणाली बनाना।
- भारतीय चिकित्सा शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करना।
- राज्यों और निजी/सार्वजनिक संस्थानों में मानकों में एकरूपता को बढ़ावा देना ।
- एमसीआई युग में देखे गए राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को कम करना।
हालाँकि, लगातार रिक्तियाँ, तदर्थ ऑपरेशन और प्रक्रियागत पक्षाघात ऐतिहासिक चिकित्सा शिक्षा सुधार के लक्ष्यों के लिए खतरा बन रहे हैं।
एनएमसी के सामने प्रमुख चुनौतियाँ
नेतृत्व शून्यता:
-
4 में से 3 स्वायत्त बोर्डों में अध्यक्षों का अभाव है ।
- 18 पूर्णकालिक पदों में से 11 रिक्त हैं; 6 अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
- यहां तक कि एनएमसी के अध्यक्ष और एक बोर्ड अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं – जिससे प्रशासनिक अस्पष्टता पैदा हो रही है।
खराब कार्यप्रणाली:
- बोर्ड तदर्थ तरीके से काम कर रहे हैं ।
- कॉलेज निरीक्षण, सीट अनुमोदन और पाठ्यक्रम सुधार जैसी नियमित गतिविधियां विलंबित या स्थगित हो जाती हैं ।
- आम सभा की बैठक 2023 के अंत से नहीं हुई है।
दोषपूर्ण निरीक्षण प्रणाली:
- सीसीटीवी और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके आभासी निरीक्षण किया जाता है।
- ये निरीक्षण कॉलेजों द्वारा स्वयं घोषित आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जो अक्सर अनियंत्रित या झूठे होते हैं।
- कई निरीक्षण गैर-तकनीकी कर्मियों द्वारा किए जाते हैं, जिससे वैधता पर सवाल उठते हैं।
चिकित्सा शिक्षा पर प्रभाव:
- नए मेडिकल कॉलेजों और सीटों की मंजूरी में देरी से छात्रों के प्रवेश पर असर पड़ रहा है।
- पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता, एलजीबीटीक्यू+ मुद्दे और चिकित्सा-कानूनी नैतिकता को शामिल करने जैसे सुधार अभी भी रुके हुए हैं।
शिथिलता के निहितार्थ
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव: डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयास (डब्ल्यूएचओ मानक: 1:1000) को नजरअंदाज किया जा रहा है।
- विनियामक विश्वसनीयता की हानि: कॉलेज एनएमसी की निगरानी को नजरअंदाज कर रहे हैं; विनियामकीय और भ्रष्टाचार की संभावना फिर से उभर रही है।
- जांच के बिना डिजिटल निर्भरता: सीसीटीवी और दस्तावेज़-आधारित निरीक्षण में कठोरता का अभाव है और इसमें हेरफेर किया जा सकता है।
- नीतिगत पक्षाघात: आम सभा की बैठकों के बिना, पाठ्यक्रम सुधार, अनुशासनात्मक कार्रवाई और नैतिक मानक कागज पर ही रह जाते हैं।
आगे की राह
- नियुक्तियों में तेजी लाना : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को योग्यता आधारित, समयबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से बोर्ड रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना : नौकरशाही संबंधी देरी को कम करना; विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली के लिए एनएमसी को सशक्त बनाना।
- पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित निरीक्षण : आभासी निगरानी को यादृच्छिक भौतिक ऑडिट के साथ संयोजित करना।
- हितधारक सहभागिता : समावेशी सुधारों के लिए मेडिकल कॉलेजों, संघों और नागरिक समाज से परामर्श करना।
- क्षमता निर्माण: एनएमसी कर्मचारियों को चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी, नैतिकता और डिजिटल मूल्यांकन प्रणालियों में प्रशिक्षित करना।
निष्कर्ष
एनएमसी को अगली पीढ़ी के चिकित्सा नियामक के रूप में देखा गया था, लेकिन अब इसकी प्रभावशीलता मजबूत नेतृत्व, प्रक्रियात्मक स्थिरता और जवाबदेही तंत्र पर निर्भर करती है। अमृत काल में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपनी संस्थागत अखंडता को पुनर्जीवित करना आवश्यक है।
Value Addition
डेटा बिंदु :
- 2024 तक, भारत में लगभग 1.4 मिलियन पंजीकृत डॉक्टर होंगे; ग्रामीण और टियर-2/3 भारत में अभी भी कमी है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर की सिफारिश करता है – भारत के कई राज्यों में इसमें कमी है।
मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न:
“किसी भी विनियामक निकाय की प्रभावशीलता न केवल उसके संरचनात्मक डिजाइन में निहित है, बल्कि इसकी परिचालन अखंडता में भी निहित है।” राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सामने हाल ही में आई चुनौतियों और भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रशासन के लिए उनके निहितार्थों का परीक्षण करें। (250 शब्द)
प्रसंग:
विश्व बैंक द्वारा 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच की गई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) भू-राजनीतिक तनावों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच नए सिरे से जांच के दायरे में आ गई है।
परिचय:
सिंधु जल संधि को अक्सर विश्व के सबसे सफल सीमापारीय /ट्रांसबाउंड्री नदी समझौतों में से एक माना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों के बाद भी कायम है। हालाँकि, बदलती जल-राजनीतिक वास्तविकताओं, बढ़ते जल तनाव और जलवायु परिवर्तनशीलता ने संधि की प्रासंगिकता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संरचना:
- 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को तथा पूर्वी नदियाँ (रावी, व्यास, सतलुज) भारत को आवंटित की गयीं।
- विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन पश्चिमी नदियों का उपयोग गैर-उपभोग्य प्रयोजनों (जल विद्युत, सिंचाई) के लिए कर सकता है।
- विश्व बैंक ने तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जो विवादों को सुलझाने में आज भी सक्रिय तंत्र है।
भारत की चिंताएं:
- दायित्वों में विषमता: ऊपरी तटवर्ती देश भारत के पास सीमित उपयोग अधिकार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास व्यापक अधिकार हैं।
- पाकिस्तान द्वारा कूटनीतिक दुरुपयोग: तकनीकी असहमतियों को बार-बार राजनीतिक और कानूनी मंचों तक ले जाना (जैसे, किशनगंगा और रातले परियोजनाओं पर मध्यस्थता)।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: 1960 में परिवर्तित वर्षा पैटर्न, हिमनदों का पीछे हटना और चरम मौसम की घटनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया।
- “संधि को स्थगित रखना”: भारत की वर्तमान स्थिति एक सुनियोजित रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है, जो संभावित वापसी या पुनः वार्ता का संकेत देती है।
रणनीतिक और पर्यावरणीय अनिवार्यताएँ:
- भारत की बढ़ती कृषि और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जल सुरक्षा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में ।
- संधि प्रावधानों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता :
- जलवायु लचीलापन
- तकनीकी प्रगति (जैसे, उपग्रह जल विज्ञान)
- सहकारी बेसिन प्रबंधन
- समतापूर्ण एवं उचित उपयोग या एकीकृत नदी बेसिन विकास के समकालीन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
क्षेत्रीय एवं भू-राजनीतिक संदर्भ:
- चीन की अपस्ट्रीम भूमिका एक अखिल हिमालयी जल नीति की आवश्यकता को उजागर करती है।
- बांग्लादेश की निचली तटवर्ती चिंताएं और नेपाल की अप्रयुक्त क्षमताएं यह सुझाव देती हैं कि भारत को व्यापक दक्षिण एशियाई जल-कूटनीति को भी आकार देना चाहिए ।
आगे की राह:
जबकि IWT ने उल्लेखनीय लचीलापन और स्थिरता का प्रदर्शन किया है, नई चुनौतियों के सामने इसकी कठोरता भारत की दीर्घकालिक जल संप्रभुता और जलवायु सुरक्षा को कमजोर करती है। पारस्परिक लाभ, न्यायसंगत उपयोग और आधुनिक वैज्ञानिक इनपुट के सिद्धांतों के आधार पर एक पुनर्निर्धारित या पुनर्गठित संधि आवश्यक है।
निष्कर्ष:
भारत को एक निष्क्रिय हस्ताक्षरकर्ता की भूमिका से आगे बढ़कर क्षेत्रीय जल प्रशासन को आकार देने वाला एक सक्रिय व्यक्ति बनना होगा, तथा जल कूटनीति को राष्ट्रीय हितों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जोड़ना होगा।
यूपीएससी उत्तर के लिए महत्वपूर्ण कीवर्ड:
- ऊपरी और निचले तटवर्ती अधिकार
- जल-कूटनीति
- जल संप्रभुता
- रणनीतिक संयम
- जलवायु लचीलापन
- असममित संधि ढांचा
- सीमापार जल प्रबंधन
- एकीकृत नदी बेसिन विकास
- ग्लेसिओ-हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तनशीलता
- निहित स्वार्थ और संधि का दुरुपयोग
- जल प्रशासन में सहकारी संघवाद
संवर्धन हेतु उद्धरण:
“जल संधियों में जल विज्ञान संबंधी वास्तविकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए, न कि केवल ऐतिहासिक बाध्यताएं।”
प्रश्न: “भारत की विदेश नीति में जल कूटनीति एक नया आयाम है।” इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में भारत की जल-कूटनीतिक गतिविधियों को आकार देने में सिंधु जल संधि की भूमिका का आकलन करें। (250 शब्द)