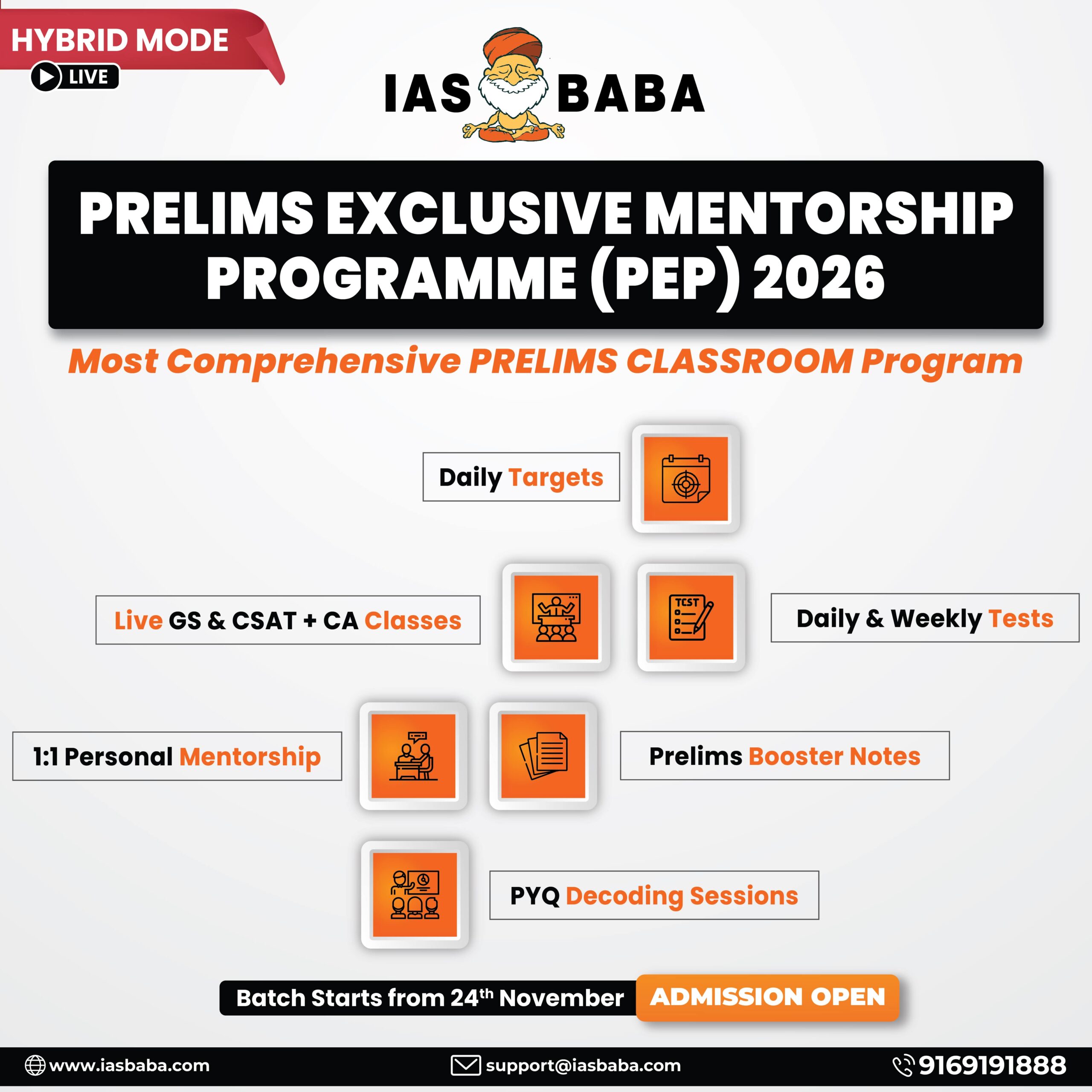IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रसंग: NIPGR (राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, दिल्ली) ने फॉस्फेट अवशोषण और उपज बढ़ाने के लिए जैपोनिका चावल में CRISPR-Cas9 जीन-संपादन का उपयोग किया।
प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष:
- संपादित चावल ने OsPHT1;2 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर जीन को लक्षित किया।
- जीन अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए दमनकारी जीन OsWRKY6 को हटा दिया गया।
- परिणाम:
- अनुशंसित फॉस्फेट उर्वरक के केवल 10% के साथ भी 40% अधिक उपज
- अधिक पुष्पगुच्छ, बीज, एवं जैवभार
- जड़ से टहनी तक बेहतर फॉस्फेट स्थानांतरण
कार्यप्रणाली:
- जड़ से प्ररोह (root-to-shoot) तक फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
- निरंतर जीन गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए रिप्रेसर बाइंडिंग साइट को हटा दिया गया।
- पौधों को पीसीआर, अनुक्रमण का उपयोग करके ऑफ-टारगेट प्रभावों के लिए परीक्षण किया गया।
- सख्त गैर-जीएमओ अनुपालन: कोई विदेशी डीएनए (जैसे, जीवाणु वेक्टर) का उपयोग नहीं किया गया है।
विनियामक एवं नैतिक पहलू:
- यदि कोई विदेशी डीएनए नहीं डाला गया है तो CRISPR-आधारित संपादन को GMO नहीं माना जाता है।
- भारत में मेंडेलियन पृथक्करण (Mendelian segregation) का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि केवल ट्रांसजीन रहित संपादित पौधों का ही प्रचार-प्रसार किया जाए।
- परिशुद्धता-प्रजनित फसलों (precision-bred crops) पर विनियामक बाधाओं को कम करने के लिए वार्ता चल रही है।
महत्व:
- उर्वरक निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है ।
- फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी में उपयोगी ।
- जीन संपादन, उपज या अनाज की गुणवत्ता से समझौता किए बिना खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का एक सतत समाधान हो सकता है।
Learning Corner:
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Institute of Plant Genome Research (NIPGR)
- स्थापना : 1998
- स्थान : नई दिल्ली
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान
- अधिदेश : फसल उत्पादकता और तनाव प्रतिरोध में सुधार के लिए पादप जीनोमिक्स और आणविक जीव विज्ञान में उन्नत अनुसंधान करना ।
प्रमुख कार्य और अनुसंधान क्षेत्र:
- प्रमुख भारतीय फसलों का जीनोम अनुक्रमण और विश्लेषण ।
- उपज, रोग प्रतिरोधकता, सूखा सहनशीलता और पोषक तत्व दक्षता जैसे गुणों के लिए जीन की खोज ।
- जीन संपादन के लिए CRISPR-Cas9 जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग ।
- कार्यात्मक जीनोमिक्स , ट्रांसजेनिक प्रौद्योगिकियों और जैव सूचना विज्ञान में अनुसंधान ।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ सहयोग।
CRISPR-Cas9 जीन संपादन तकनीक
CRISPR-Cas9 (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स – CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9) एक क्रांतिकारी जीनोम-संपादन उपकरण है जो वैज्ञानिकों को जीवों के भीतर डीएनए को सटीक रूप से संशोधित करने की अनुमति देता है।
मूल:
- यह बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र से व्युत्पन्न है, जो वायरल डीएनए को काटने के लिए CRISPR अनुक्रम और Cas9 एंजाइम का उपयोग करता है।
यह किस प्रकार कार्य करता है:
- एक गाइड आरएनए (gRNA) को लक्ष्य डीएनए अनुक्रम से मिलान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Cas9 एंजाइम आणविक कैंची की तरह कार्य करता है, जो वांछित स्थान पर DNA को काटने के लिए gRNA द्वारा निर्देशित होता है।
- कोशिका की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली का उपयोग डीएनए अनुक्रमों को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए किया जाता है ।
लाभ:
- अत्यधिक सटीक और कुशल
- पुरानी जीन-संपादन विधियों (जैसे TALENs या ZFNs) की तुलना में तेज़ और सस्ता
- पौधों, जानवरों और मनुष्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है
- विदेशी डीएनए (गैर-जीएमओ) को शामिल किए बिना लक्षित फसल सुधार को सक्षम बनाता है
अनुप्रयोग:
- कृषि : उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता या पोषक तत्व दक्षता वाली फसलों का विकास (उदाहरण के लिए, एनआईपीजीआर का फॉस्फेट-कुशल चावल)
- चिकित्सा : जीन थेरेपी, कैंसर उपचार, और सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवंशिक विकारों पर अनुसंधान
- अनुसंधान : मॉडल जीवों में जीन कार्य का अध्ययन
स्रोत: THE HINDU
श्रेणी: पर्यावरण
संदर्भ: हाल ही में एझिमाला, कन्नूर (केरल) में ग्रेट हॉर्नबिल के देखे जाने से इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है।
ग्रेट हॉर्नबिल का महत्व
- ग्रेट हॉर्नबिल (बुसेरोस बाइकोर्निस) एक बड़ा पक्षी है जो बीज फैलाने वाले और परिपक्व, स्वस्थ वनों के सूचक के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है।
- इसे सुभेद्य (VU) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तथा पर्यावास के नुकसान और शिकार के कारण इसकी आबादी घट रही है ।
एझिमाला में दिखाई देना क्यों महत्वपूर्ण है
- एझिमाला इस प्रजाति की विशिष्ट सीमा का हिस्सा नहीं है, जिससे पता चलता है कि यहां वन के अवशेष या पारिस्थितिक गलियारे मौजूद हैं।
- यह भू-दृश्य क्षेत्र की जैव विविधता की संभावना को इंगित करता है तथा पारिस्थितिकी बहाली के अवसरों पर प्रकाश डालता है।
संरक्षण संबंधी अनिवार्यताएं
- एझिमाला और आसपास के क्षेत्रों में वन खंडों और पारिस्थितिक गलियारों की रक्षा करना।
- पर्यावास निगरानी और पुनर्स्थापन सहित समुदाय आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना।
- वन्यजीव संरक्षण कानूनों को मजबूत करना और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने पर विचार करना।
- जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए ग्रेट हॉर्नबिल को एक प्रमुख प्रजाति के रूप में उपयोग करना।
व्यापक निहितार्थ
- वनों की कटाई और पर्यावास विखंडन को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- संरक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय भागीदारी के संयोजन के मूल्य पर जोर दिया गया है।
- यह दर्शाता है कि समय पर और निरंतर प्रयासों से वन्यजीवों का पुनरुद्धार संभव है।
Learning Corner:
ग्रेट हॉर्नबिल (Buceros bicornis)
ग्रेट हॉर्नबिल भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित हॉर्नबिल प्रजातियों में से एक है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- इसकी चोंच के ऊपर विशिष्ट आवरण (हेलमेट जैसी संरचना) होती है।
- काले, सफेद और पीले पंखों वाला बड़ा, रंगीन पक्षी।
- अपने आकार के बावजूद यह अपनी ऊंची आवाज और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है।
प्राकृतिक वास:
- घने सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों को पसंद करता है।
- यह सामान्यतः पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है।
पारिस्थितिक भूमिका:
- यह एक प्रमुख बीज प्रकीर्णक के रूप में कार्य करता है, तथा वन पुनर्जनन में सहायता करता है।
- स्वस्थ, परिपक्व वनों के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है।
संरक्षण की स्थिति:
- आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद्य (VU) के रूप में सूचीबद्ध ।
- खतरे:
- वनों की कटाई के कारण पर्यावास का नुकसान
- कैस्क और पंखों का शिकार
- घोंसले बनाने वाले पेड़ों का नुकसान
संरक्षण प्रयास:
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षण ।
- हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम जैसे समुदाय-नेतृत्व वाले कार्यक्रम आवास संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।
स्रोत: THE HINDU
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
संदर्भ : नॉर्मन टेबिट: मार्गरेट थैचर के प्रमुख सहयोगी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
अवलोकन
नॉर्मन टेबिट (1931-2025) एक प्रमुख ब्रिटिश कंज़र्वेटिव राजनेता और 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर की सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अपनी दृढ़ता और मज़दूर वर्ग के प्रति आकर्षण के लिए जाने जाने वाले, नॉर्मन ने ब्रिटिश रूढ़िवाद को नया रूप देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।
राजनीतिक कैरियर
- रोजगार, व्यापार और उद्योग राज्य सचिव तथा कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष सहित प्रमुख कैबिनेट भूमिकाओं का निर्वहन किया।
- ट्रेड यूनियन सुधारों का नेतृत्व किया, विशेष रूप से रोजगार अधिनियम 1982 के माध्यम से, जिससे यूनियन की शक्ति कम हुई और नियोक्ता अधिकारों को मजबूत किया गया।
- यह वाक्यांश “अपनी बाइक पर बैठो (get on your bike)” उन्हीं से संबद्ध है , जो आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत प्रयास का प्रतीक है।
यूरोप पर रुख
- एक मुखर यूरोसेप्टिक, उन्होंने बाद में ब्रुगेस समूह का नेतृत्व किया, जो गहन यूरोपीय एकीकरण का विरोध करता था।
सार्वजनिक छवि और विरासत
- अपने दृढ़ राजनीतिक रुख और निष्ठा के कारण उन्हें “थैचर का प्रवर्तक” उपनाम दिया गया।
- आव्रजन और राष्ट्रीय पहचान पर विवादास्पद विचारों के लिए जाने जाते हैं , जिसमें आत्मसात पर “क्रिकेट परीक्षण” भी शामिल है।
- 1992 में कॉमन्स से सेवानिवृत्त हुए, तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आजीवन सहकर्मी के रूप में बहस में योगदान देते रहे हैं।
Learning Corner:
थैचरवाद (Thatcherism)
थैचरवाद, 1979 से 1990 तक यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रहीं मार्गरेट थैचर से जुड़ी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा को दर्शाता है । यह ब्रिटिश राजनीति में मुक्त-बाज़ार पूंजीवाद, व्यक्तिवाद और राज्य के हस्तक्षेप में कमी की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- मुक्त बाजार अर्थशास्त्र :
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के निजीकरण पर जोर ।
- विनियमन को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना।
- मुद्रावाद :
- बेरोजगारी की बजाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- सार्वजनिक व्यय में कमी और मुद्रा आपूर्ति पर कड़ा नियंत्रण।
- कर सुधार :
- प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कराधान की ओर बदलाव ।
- धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर की शीर्ष दरें कम की गईं।
- ट्रेड यूनियन सुधार :
- सख्त कानून के माध्यम से संघ की शक्तियों में कटौती ।
- दुकानें बंद करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा हड़ताल करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- व्यक्तिगत जिम्मेदारी :
- आत्मनिर्भरता , उद्यमशीलता और घर के स्वामित्व की वकालत ।
- प्रसिद्ध कथन: “समाज जैसी कोई चीज़ नहीं है (There is no such thing as society)”
- यूरो-संदेहवाद:
- यूरोपीय समुदाय के भीतर गहन राजनीतिक एकीकरण का विरोध।
प्रभाव:
- ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ , जिसका कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों की नीतियों पर स्थायी प्रभाव पड़ा।
- सामाजिक और क्षेत्रीय विभाजन पैदा किया गया , आलोचकों ने बढ़ती असमानता और कल्याणकारी राज्य के क्षरण की ओर इशारा किया।
- यह ब्रिटेन में नवउदारवादी शासन का एक निर्णायक चरण बन गया और 1980 के दशक में वैश्विक नीतिगत बदलावों को प्रभावित किया।
स्रोत: TIMES OF INDIA
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
संदर्भ: 8 जुलाई 2025 को , प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस के ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया ।
सम्मान के बारे में:
- ब्राजील की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 1822 में ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस की स्थापना की गई थी ।
- यह पुरस्कार ब्राजील में असाधारण सेवा के लिए विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है।
- ग्रैंड कॉलर इस आदेश के अंतर्गत सर्वोच्च पद है और इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रदान किया जाता है ।
महत्व:
- यह पुरस्कार भारत-ब्राजील संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने में मोदी के योगदान को मान्यता देता है।
- प्रधान मंत्री मोदी ने यह सम्मान भारत के 1.4 अरब लोगों को समर्पित किया और दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता पर प्रकाश डाला।
Learning Corner:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान:
- नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कॉलर – ब्राज़ील (2025)
- यह सम्मान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत-ब्राजील संबंधों को मजबूत करने में मोदी के प्रयासों को मान्यता देता है।
- ऑर्डर ऑफ जायद – संयुक्त अरब अमीरात (2019)
- यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दिया गया, जो उनके रणनीतिक नेतृत्व और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया।
- लीजन ऑफ मेरिट – संयुक्त राज्य अमेरिका (2020)
- रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और हिंद-प्रशांत सुरक्षा को बढ़ावा देने में मोदी की भूमिका के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।
- ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू – रूस (2019)
- रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
- ऑर्डर ऑफ निशान इज्जुद्दीन – मालदीव (2019)
- द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए मालदीव द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान।
- किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां – बहरीन (2019)
- भारत और बहरीन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया।
- वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार – CERAWeek, USA (2021)
- ऊर्जा सततता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में नेतृत्व के लिए।
स्रोत : PIB
श्रेणी: राजनीति
संदर्भ: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने परिचालन और तकनीकी चुनौतियों के कारण दिल्ली-एनसीआर में जीवन-अंत वाले पुराने वाहनों (ईएलवी) को ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्देश को लागू करने की समय-सीमा बढ़ा दी है।
संशोधित समयरेखा:
- 1 नवंबर, 2025 से: दिल्ली और पांच एनसीआर जिलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में प्रतिबंध लागू होगा।
- 1 अप्रैल, 2026 से : प्रतिबंध एनसीआर के बाकी हिस्सों तक विस्तारित होगा ।
- 31 अक्टूबर, 2025 तक : ई.एल.वी. को ईंधन की आपूर्ति जारी रहेगी।
ईएलवी क्या हैं?
- 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन
- 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन
विस्तार का कारण:
- स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली से संबंधित समस्याएं:
- गड़बड़ियाँ, खराब कैमरा कवरेज, सेंसर त्रुटियाँ
- एनसीआर राज्यों में अपूर्ण डेटा एकीकरण
- नीतिगत खामियों से बचने के लिए , जैसे कि वाहन मालिकों द्वारा पड़ोसी शहरों में ईंधन भरवाना
- समन्वित कार्यान्वयन और तकनीकी उन्नयन की अनुमति देना
Learning Corner:
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management (CAQM)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली -एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- स्थापना: अक्टूबर 2020 (एक अध्यादेश के माध्यम से; बाद में अगस्त 2021 में कानून के माध्यम से अधिनियमित)
- क्षेत्राधिकार: दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
उद्देश्य:
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना ।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) सहित वायु गुणवत्ता सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना ।
- ईपीसीए (पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण) जैसे कई निकायों को प्रतिस्थापित करना।
कार्य:
- वायु गुणवत्ता से संबंधित पर्यावरण कानूनों की निगरानी और उनका क्रियान्वयन करना।
- प्रदूषणकारी उद्योगों और वाहनों को प्रत्यक्ष रूप से बंद करना या उनका विनियमन करना।
- बायोमास जलाने, धूल नियंत्रण और वाहन प्रदूषण उपायों की देखरेख करना ।
- पूसा बायो-डीकंपोजर और एएनपीआर प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन पर एनसीआर राज्यों के साथ समन्वय करना।
स्रोत: PIB
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
जून में हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के सैन्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5% तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया था (विशेष रूप से “2035 तक मुख्य रक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधी व्यय”)। पिछला व्यय लक्ष्य 2% था।
सैन्य व्यय का ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ क्या रहा है?
- शीत युद्ध काल में:
- 1960 में यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 6.1% था।
- बाद में इसे घटाकर 3% कर दिया गया।
- यह 1998 में 2.1% (लगभग 1,100 बिलियन डॉलर का कुल व्यय) के साथ अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार 2024 और 2025 में:
- वैश्विक सैन्य खर्च 2,718 अरब डॉलर रहा। इस वर्ष इसमें 9.4% की वृद्धि देखी गई, जो 1988 के बाद से साल-दर-साल सबसे ज़्यादा वृद्धि थी।
- इसका कारण रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-गाजा संघर्ष था।
- इसके अलावा, 2025 में, विश्व को भारत और पाकिस्तान, तथा इज़राइल और ईरान के बीच दो बड़े अतिरिक्त संघर्ष देखने को मिलेंगे। नाटो की प्रतिज्ञा के साथ, आने वाले वर्षों में वैश्विक सैन्य खर्च में और वृद्धि देखने को मिलेगी।
शीर्ष सैन्य व्ययकर्ता (2024)
| देश | व्यय ($ बिलियन ) |
| यूएसए | 997 |
| चीन | 314 |
| रूस | 149 |
| जर्मनी | 88.5 |
| भारत | 86.1 |
- नाटो (32 सदस्य): संयुक्त व्यय 1,506 बिलियन डॉलर (वैश्विक व्यय का 55%) ।
- शीर्ष 20 में जीडीपी % (युद्धग्रस्त राष्ट्रों को छोड़कर):
- सऊदी अरब: 7.3%
- पोलैंड: 4.2%
- अमेरिका: 3.4%
- अन्य: 1.3% – 2.6%
सैन्य व्यय में वृद्धि का प्रभाव
पुनःसैन्यीकरण की वर्तमान लहर से शीत युद्ध के बाद सैन्य व्यय में कमी से प्राप्त लाभों के पलट जाने का खतरा है।
वैश्विक शांति सूचकांक (2023) के अनुसार:
- 108 देशों में सैन्यीकरण बढ़ा।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संघर्षों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।
सैन्य-औद्योगिक परिसर प्रभाव:
- सैन्य खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को लाभ हो सकता है।
- फिर भी, जैसा कि अध्ययन दर्शाते हैं (उदाहरण के लिए, मासाको इकेगामी और जिजियान वांग द्वारा, 116 देशों पर आधारित), सैन्य खर्च में वृद्धि से घरेलू सरकारी स्वास्थ्य व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव मध्यम और निम्न आय वाले देशों पर अधिक पड़ता है।
उदाहरण: स्पेन:
- रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.24% खर्च किया जाता है।
- नाटो के नए 5% लक्ष्य को “अनुचित” बताते हुए इससे इनकार कर दिया गया।
- €300 बिलियन का अतिरिक्त बोझ कल्याणकारी व्यय में कटौती करेगा।
संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव
- संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम बजट केवल 44 अरब डॉलर का है, जिससे उसे विकास, मानवीय सहायता और शांति अभियानों के लिए धन जुटाना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र को छह महीनों में केवल 6 अरब डॉलर ही मिले हैं , और परिणामस्वरूप, वह बजट को घटाकर 29 अरब डॉलर करने की कोशिश कर रहा है।
- ऐसा सैन्य संघर्षों में वृद्धि के कारण है, क्योंकि राष्ट्र अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी सहायता में कटौती कर रहे हैं।
उदाहरण:
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका विदेशी सहायता में कटौती करना चाहता है।
- अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (USAID) को बंद कर दिया है। एक लैंसेट अध्ययन के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा, पोषण आदि में USAID की सहायता से पिछले दो दशकों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 91 मिलियन मौतें रोकी गई हैं।
सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रभाव
रक्षा व्यय में वृद्धि से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की प्रगति में बाधा आ रही है।
उदाहरण:
- विश्व में अत्यधिक चरम गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रति वर्ष केवल 70 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जो कि बहुत छोटी राशि है (अमीर देशों की आय का मात्र 0.1%)।
- वैश्विक स्तर पर पूर्ण गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रति वर्ष 325 बिलियन डॉलर या उच्च आय वाले देशों की आय का 0.6% आवश्यक है , जो अभी भी उनके सैन्य खर्च से बहुत कम है।
- 2021 में लगभग 4.5 बिलियन लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पूरी पहुंच नहीं थी।
- अध्ययनों से पता चलता है कि मधुमेह और कैंसर जैसी प्रमुख गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 1 डॉलर खर्च करने से 2030 तक लगभग 7 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है।
जो धनराशि सतत विकास के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उसे सेना में स्थानांतरित किया जा रहा है।
पर्यावरणीय प्रभाव
- सैन्य खर्च में वृद्धि से पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को नुकसान पहुँचता है। 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था , जिसमें भीषण गर्मी पड़ी थी।
- यदि नाटो देश अपने रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक बढ़ा देते हैं, तो इससे हर साल 200 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैसें बढ़ेंगी।
- जलवायु कार्रवाई के बजाय सैन्य पर अधिक खर्च करने से वैश्विक तापमान में वृद्धि और बढ़ेगी तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए धन की कमी होगी।
भारत पर प्रभाव
भारत का सैन्य बनाम स्वास्थ्य व्यय:
- सैन्य व्यय: सकल घरेलू उत्पाद का 2.3%
- स्वास्थ्य व्यय: सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.84%, जो है:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2.5% लक्ष्य से कम ।
- यह अधिकांश विकसित देशों द्वारा खर्च किये जाने वाले ~10% से बहुत कम है ।
सैन्यीकरण के प्रति जनता के समर्थन के कारण , यह जोखिम है कि स्वास्थ्य और कल्याण जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च कम हो सकता है ।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, सैन्य खर्च और सामाजिक क्षेत्र में निवेश के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। देशों को अपने सैन्य लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण से महत्वपूर्ण संसाधनों का दुरुपयोग न हो।
संयुक्त राष्ट्र और सतत विकास लक्ष्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने सहित वैश्विक शासन ढांचे को मजबूत करना, संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
रक्षा गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को चिन्हित करना तथा जलवायु संबंधी विचारों को राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में एकीकृत करना भी महत्वपूर्ण है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय को अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित ठहराया जाता है, फिर भी यह मानव विकास और पर्यावरणीय सततता के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
2025 गोल्डश्मिट सम्मेलन में प्रस्तुत एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि ग्लेशियरों के पिघलने से, विशेष रूप से पश्चिमी अंटार्कटिका में, भूमिगत मैग्मा कक्षों पर बर्फ के दबाव में कमी के कारण अधिक बार और विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं।
ग्लेशियर क्या हैं?
- ग्लेशियर बर्फ और हिम के विशाल, धीमी गति से बहने वाले पिंड हैं जो भूमि पर बनते हैं।
- ग्लेशियर गुरुत्वाकर्षण और बर्फ के आंतरिक विरूपण के कारण गति करते हैं। वे अपेक्षाकृत धीमी गति से गति कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ, यह गति भूदृश्य को आकार देती है।
- ग्लेशियरों को या तो अल्पाइन (पर्वतीय) ग्लेशियर या महाद्वीपीय ग्लेशियर (बर्फ की चादरें) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- ग्लेशियर उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां बर्फबारी कई वर्षों तक पिघलने या वाष्पित होने की अपेक्षा अधिक तेजी से जमा होती है, तथा अंततः बर्फ में तब्दील हो जाती है।
प्रमुख ग्लेशियरों के स्थान:
- एशिया: हिमालय (सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री), काराकोरम (बाल्टोरो)
- अंटार्कटिका: लैम्बर्ट ग्लेशियर (विश्व का सबसे बड़ा)
- आर्कटिक: ग्रीनलैंड बर्फ की चादर
- दक्षिण अमेरिका: पैटागोनियन ग्लेशियर (पेरिटो मोरेनो)
- यूरोप: आल्प्स (एलेत्श ग्लेशियर)
ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं?
1900 के दशक की शुरुआत से, विश्व भर के कई ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। इस घटना के मूल में मानवीय गतिविधियाँ हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग: बढ़ते तापमान से बर्फ पिघलने की गति बढ़ रही है।
- काला/ ब्लैक कार्बन जमाव: कालिख/ कार्बन एल्बिडो को कम करती है, जिससे ऊष्मा अवशोषण बढ़ता है।
- औद्योगिक प्रदूषण: वायुमंडलीय रसायन विज्ञान को बदल देता है, जिससे बर्फबारी और पिघलने की दर प्रभावित होती है।
- वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन: बर्फबारी में कमी और वर्षा में वृद्धि से बर्फ पिघलने में तेजी आती है।
यदि हम आने वाले दशकों में उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रूप से कमी भी कर लें, तो भी विश्व के शेष बचे एक तिहाई से अधिक ग्लेशियर वर्ष 2100 से पहले ही पिघल जायेंगे।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि उत्सर्जन में अनियंत्रित वृद्धि जारी रही, तो वर्ष 2040 तक आर्कटिक गर्मियों में बर्फ रहित हो सकता है, क्योंकि समुद्र और हवा का तापमान तेजी से बढ़ता रहेगा।
ग्लेशियरों और ज्वालामुखियों के बीच संबंध
- पिघलते ग्लेशियर भूमिगत मैग्मा कक्ष पर बर्फ द्वारा डाले गए दबाव को कम करते हैं
- इससे गैसों और मैग्मा का विस्तार होता है , जिसके परिणामस्वरूप विस्फोटक विस्फोट हो सकते हैं।
- सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र:
- पश्चिमी अंटार्कटिका : बर्फ के नीचे दबे लगभग 100 ज्वालामुखी, जो आने वाले दशकों में पिघल सकते हैं
- अन्य क्षेत्र : उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस
- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में होने वाले परिवर्तन भूमिगत स्तर तक पहुंच सकते हैं तथा मैग्मा प्रणालियों के साथ प्रतिक्रिया कर विस्फोटों को जन्म दे सकते हैं।
ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव
- अल्पकालिक शीतलन:
- राख, धूल और सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान कम हो जाता है।
- सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में पहुँचकर पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एरोसोल बनाता है। ये एरोसोल आने वाले सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है।
- अमेरिकी विज्ञान शिक्षा केन्द्र के अनुसार, एरोसोल समताप मंडल में तीन वर्षों तक रह सकते हैं, हवाओं के द्वारा इधर-उधर चले जाते हैं और विश्वभर में महत्वपूर्ण शीतलन पैदा करते हैं।
- दीर्घकालिक वार्मिंग:
- लगातार विस्फोटों से CO₂ और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं , जो वैश्विक तापमान में और वृद्धि करती हैं , तथा एक दुष्चक्र का निर्माण करती हैं :
- जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलने की दर भी बढ़ेगी, जिससे अधिक विस्फोट हो सकते हैं तथा वैश्विक तापमान में और वृद्धि हो सकती है।
आगे की राह
- वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और ग्लेशियर पिघलने की दर को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को मजबूत करना।
- विस्फोटों और जीएलओएफ की पूर्व चेतावनी के लिए हिमनद निगरानी प्रणालियों को उन्नत करना।
- ग्लेशियर समृद्ध ज्वालामुखी क्षेत्रों में अनुसंधान और आपदा तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।