IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
प्रसंग:
- दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई परिणामों के साथ समाप्त हुआ और इसका भारत और क्वाड पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

क्वाड के बारे में:
- सदस्य: क्वाड, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में भी जाना जाता है, एक रणनीतिक मंच है जिसमें चार देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- उद्देश्य: क्वाड का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
- औपचारिक समूह नहीं: क्वाड एक औपचारिक गठबंधन न होकर एक ढीला-ढाला समूह है। इसका कोई निर्णय लेने वाला निकाय, सचिवालय या नाटो या संयुक्त राष्ट्र जैसा कोई औपचारिक ढाँचा नहीं है। यह गठबंधन शिखर सम्मेलनों, बैठकों, सूचनाओं के आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यासों के माध्यम से कायम रहता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है: चारों देश स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को बनाए रखने, लोकतंत्र, मानवाधिकारों और कानून के शासन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में समान रुचि रखते हैं।
- चीन के प्रभाव का प्रतिकार: क्वाड को क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के एक तंत्र के रूप में देखा जाता है (‘मोतियों की माला/ पर्ल ऑफ़ स्ट्रिंग’ सिद्धांत के माध्यम से), हालांकि इसके सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह एक सैन्य गठबंधन नहीं है और उन अन्य देशों के लिए खुला है जो उनके मूल्यों और हितों को साझा करते हैं।
- अन्य प्रमुख क्षेत्र: क्वाड का उद्देश्य शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना और आपदा राहत एवं मानवीय सहायता क्षमताओं को बढ़ाना है। यह ‘क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल’ के माध्यम से जी20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण संबंधी मुद्दों का समाधान भी करता है।
- विकास:
- 2007: दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक के दौरान 2007 में क्वाड का गठन किया गया था। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ही सबसे पहले क्वाड बनाने का विचार रखा था।
- 2012: जापानी प्रधानमंत्री ने एशिया में ‘डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड’ की अवधारणा पर प्रकाश डाला, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- 2017: चीन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए, चारों देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित किया और इसके लक्ष्यों का विस्तार किया तथा एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने आसियान शिखर सम्मेलन 2017 से पहले मनीला में पहली ‘क्वाड’ वार्ता आयोजित की।
स्रोत:
श्रेणी: विविध
प्रसंग:
- बढ़ते वैश्विक तापमान के बीच, यूएनईपी की 2025 अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट: रनिंग ऑन एम्प्टी में पाया गया है कि विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त में एक बड़ा अंतर जीवन, आजीविका और संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल रहा है।
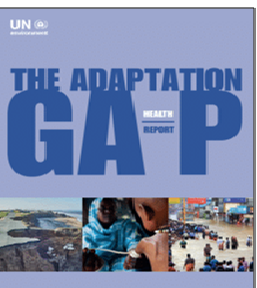
अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के बारे में :
- प्रकाशक: यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) – कोपेनहेगन जलवायु केंद्र का एक वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है जिसमें कई वैश्विक संस्थानों और विशेषज्ञों का योगदान है।
- उद्देश्य: अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन योजना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण पर वैश्विक प्रगति को ट्रैक करती है, तथा यह आकलन करती है कि विश्व जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को प्राप्त करने से कितनी दूर है।
- विकासशील देशों पर ध्यान केन्द्रित करना: यह मूल्यांकन करना कि क्या राष्ट्र – विशेष रूप से विकासशील देश – जलवायु प्रभावों के प्रति पर्याप्त तेजी से अनुकूलन कर रहे हैं, तथा यूएनएफसीसीसी और सीओपी30 के अंतर्गत वैश्विक वार्ताओं का समर्थन करने के लिए अनुकूलन वित्त अंतराल का परिमाणन करना।
- अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 के महत्वपूर्ण बिंदु:
- रिपोर्ट में विकासशील देशों में आवश्यक अनुकूलन वित्त की लागत को अद्यतन किया गया है, तथा मॉडल लागत के आधार पर 2035 में इसे 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष बताया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं में व्यक्त की गई अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, यह आंकड़ा बढ़कर 365 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष हो जाता है।
- इस बीच, विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त प्रवाह 2023 में 26 अरब अमेरिकी डॉलर था: जो पिछले वर्ष के 28 अरब अमेरिकी डॉलर से कम है। इससे विकासशील देशों में अनुकूलन वित्तपोषण की ज़रूरतें वर्तमान प्रवाह से 12-14 गुना ज़्यादा हो जाती हैं।
- यदि वर्तमान वित्तीय रुझान जारी रहे, तो 2019 के स्तर से 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का ग्लासगो जलवायु संधि का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा, जबकि जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य वित्तीय अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं है।
- निजी क्षेत्र और भी अधिक कर सकता है – यदि उसे लक्षित नीतिगत कार्रवाई और मिश्रित वित्तीय समाधानों का समर्थन प्राप्त हो तो वह प्रति वर्ष लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की क्षमता रखता है।
स्रोत:
श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
प्रसंग:
- भारत नवंबर 2025 में दिल्ली में अपनी पहली सहकारी कैब सेवा “भारत टैक्सी” शुरू करने के लिए तैयार है और इसका उद्देश्य निजी कैब सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।

भारत टैक्सी के बारे में:
- लॉन्च किया गया: इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ( NeGD ) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य देश में बढ़ती शहरी कैब सुविधा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत, अधिक न्यायसंगत प्रणाली का निर्माण करना है।
- सहकारी मॉडल पर आधारित: यह सहकारी कैब सेवा निजी एग्रीगेटर्स के लिए एक पारदर्शी, चालक-स्वामित्व वाला विकल्प प्रदान करती है, जहां चालक केवल ‘कर्मचारी’ के बजाय सदस्य और शेयरधारक बन जाते हैं।
- यात्रियों और ड्राइवरों के लिए वन-स्टॉप समाधान: भारत टैक्सी, निजी कैब सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों और ड्राइवरों, दोनों के सामने आने वाली दीर्घकालिक चुनौतियों का एक ठोस समाधान साबित होगी। यह मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर और पीछे बैठे यात्री सहित सभी हितधारकों की इस प्रणाली में आवाज़ हो।
- अन्य सरकारी सेवाओं के साथ एकीकरण: यह प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर और उमंग जैसी सरकारी डिजिटल सेवाओं के साथ एकीकृत है, जिससे निर्बाध सत्यापन और सेवा पहुंच सुनिश्चित होती है।
- प्रबंधन: सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहकारी नेताओं और चालक प्रतिनिधियों से मिलकर बनी भारत टैक्सी का प्रबंधन करती है। इसे आठ प्रमुख संस्थानों का समर्थन प्राप्त है, जो अपने सुदृढ़ प्रशासन, पारदर्शिता और इस पहल की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रसिद्ध हैं।
स्रोत:
श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी
प्रसंग:
- सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें सारंडा अभयारण्य के पूर्व के 310 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घटाकर 250 वर्ग किलोमीटर करने की मांग की गई थी ताकि आदिवासियों के वन अधिकारों की रक्षा के लिए उनके निवास वाले 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इससे बाहर रखा जा सके।

सारंडा अभयारण्य के बारे में:
- स्थान: यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य है, जो सारंडा वन प्रभाग के भीतर स्थित है, जिसे एशिया के सबसे बड़े साल (शोरिया रोबस्टा) वनों में से एक और झारखंड-ओडिशा सीमा पर एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है।
- नामकरण: दक्षिणी झारखंड में स्थित सारंडा क्षेत्र का अर्थ “सात सौ पहाड़ियों की भूमि” है
- क्षेत्रफल: इसका क्षेत्रफल लगभग 856 वर्ग किमी है, जिसमें से 816 वर्ग किमी आरक्षित वन है।
- कई राज्यों के बीच पारिस्थितिक गलियारा: यह सिंहभूम हाथी रिजर्व के भीतर स्थित है, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा बनाता है।
- विकास: इसे 1968 में बिहार वन अधिनियम के तहत एक खेल अभयारण्य घोषित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2022) ने झारखंड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसे अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
- वनस्पति: यहां साल, कुसुम, महुआ और दुर्लभ ऑर्किड का घना आवरण पाया जाता है।
- जीव-जंतु: यह एशियाई हाथियों, चार सींग वाले मृगों, सुस्त भालू, उड़ने वाली छिपकलियों और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।
- महत्वपूर्ण समुदाय: यह हो, मुंडा, ओरांव और कई पीवीटीजी का घर है, जो महुआ और राल जैसे वन उत्पादों पर निर्भर हैं।
- खनिज संसाधन: इसमें भारत के लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा मौजूद है, जो इसे सेल और निजी ऑपरेटरों के लिए एक प्रमुख खनन क्षेत्र बनाता है।
स्रोत:
श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
प्रसंग:
- डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने नई दिल्ली में दो परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन पोर्टल (क्लैंप) का शुभारंभ किया।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में:
- प्रकृति: कोयला शक्ति डैशबोर्ड एक अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खदान से लेकर बाजार तक संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला को एकीकृत इंटरफेस पर एकीकृत करता है।
- विकास: कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित, कोयला शक्ति – स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो कई हितधारकों के डेटा को एकीकृत करता है।
- उद्देश्य: कोयला शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन दक्षता को मजबूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय को बढ़ाना है।
- वास्तविक समय समन्वय प्रदान करता है : यह प्लेटफॉर्म कोयला कंपनियों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय समन्वय की सुविधा प्रदान करता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है और निर्बाध कोयला रसद सुनिश्चित होती है।
- डेटा-संचालित शासन: एक व्यापक निर्णय-समर्थन प्रणाली के रूप में, कोयला शक्ति डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाती है, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करती है, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करती है।
- आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप : यह पहल सरकार के आत्मनिर्भर भारत और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी नवाचार के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
क्लैम्प पोर्टल के बारे में:
- प्रकृति: कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन, पोर्टल (CLAMP) कोयला क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल समाधान है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- केंद्रीकृत भंडार: भूमि अभिलेखों के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करते हुए, यह पोर्टल डेटा एकीकरण सुनिश्चित करता है, जवाबदेही बढ़ाता है, और प्रक्रियागत देरी को न्यूनतम करता है।
- पारदर्शिता की ओर कदम: भूमि विवरण अपलोड करने से लेकर मुआवजे के भुगतान तक संपूर्ण कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाकर, CLAMP कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में भूमि प्रबंधन प्रथाओं में पारदर्शिता, दक्षता और अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाता है।
स्रोत:
(MAINS Focus)
(जीएस पेपर 2: शिक्षा से संबंधित मुद्दे; जीएस पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी - विकास और उनके अनुप्रयोग)
संदर्भ( परिचय)
शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव के साथ - साथ ' एआई रेडीनेस के लिए कौशल' पहल ने स्कूल स्तर पर एआई को एकीकृत करने में भारत की तत्परता, बुनियादी ढांचे और शैक्षिक प्राथमिकताओं पर बहस छेड़ दी है।
पक्ष में मुख्य तर्क
- एआई साक्षरता बनाम एआई कौशल: एक चरणबद्ध दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है - प्रारंभिक ग्रेड (कक्षा 3-8) एआई साक्षरता (अवधारणाओं को समझना, नैतिकता, जिम्मेदार उपयोग) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि वरिष्ठ ग्रेड (कक्षा 9-12) एआई कौशल जैसे कोडिंग, पायथन और डेटा एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं ।
- भविष्य के कार्यबल की तैयारी: प्रारंभिक अनुभव छात्रों को स्वचालन-संचालित नौकरी बाजारों के लिए तैयार करता है , तथा डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों का समर्थन करता है ।
- आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना: आधारभूत स्तर पर एआई को एकीकृत करने से बच्चों में विश्लेषणात्मक तर्क, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को मजबूत किया जा सकता है।
- विकासशील शिक्षाशास्त्र: शिक्षा को रटने वाली शिक्षा और संज्ञानात्मक मॉडल से रचनात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा की ओर स्थानांतरित करना होगा , जिससे प्रौद्योगिकी को कक्षाओं का मूल निवासी बनाया जा सके ।
- वैश्विक संरेखण: फिनलैंड, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों ने एआई नैतिकता और डिजिटल शिक्षा को सफलतापूर्वक शामिल किया है , जिससे पता चलता है कि जिम्मेदार परिचय संभव और लाभदायक है।
आलोचनाएँ और कमियाँ
- तीव्र तकनीकी परिवर्तन: एआई प्रौद्योगिकियां पाठ्यक्रम डिजाइन की तुलना में तेजी से विकसित होती हैं , जिससे अप्रचलन का खतरा रहता है (उदाहरण के लिए, शीघ्र इंजीनियरिंग जल्द ही गायब हो सकती है)।
- डिजिटल और भाषाई विभाजन: 50% से अधिक स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का अभाव है , और क्षेत्रीय भाषाओं में एआई उपकरण सीमित हैं, जिससे असमानता पैदा हो रही है।
- "अशिक्षा" का जोखिम: एआई-जनित प्रतिक्रियाओं पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों की सीखने और गंभीर रूप से सोचने की प्रेरणा को कम कर सकती है ।
- शिक्षक तैयारी: लगभग 9% स्कूलों में केवल एक शिक्षक है , और आधे स्कूलों में पूर्ण योग्यता का अभाव है । एआई साक्षरता और प्रशिक्षण के बिना , कार्यान्वयन विफल हो सकता है।
- नैतिक और मनोवैज्ञानिक चिंताएं: बच्चे चैटबॉट्स के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा कर सकते हैं या उन पर निर्भरता विकसित कर सकते हैं , जिससे डेटा का दुरुपयोग और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होने का खतरा हो सकता है ।
- बुनियादी ढांचे का अंतराल: बिजली या इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना स्कूल वास्तविक रूप से एआई-आधारित पाठ नहीं दे सकते हैं, जिससे शहरी-ग्रामीण विभाजन बढ़ रहा है ।
सुधार और सिफारिशें
- चरणबद्ध एवं प्रासंगिक परिचय:
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 3-5): सरल, वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके एआई जागरूकता और नैतिक समझ पर ध्यान केंद्रित करें ।
- मध्य स्तर (कक्षा 6-8): आलोचनात्मक सोच और नैतिक एआई उपयोग को विकसित करने के लिए व्यावहारिक, अनप्लग्ड परियोजनाओं का परिचय दें ।
- माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12): पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए एआई अनुप्रयोग, प्रोग्रामिंग, एनएलपी और डेटा एनालिटिक्स सिखाएं ।
- शिक्षक क्षमता निर्माण:
- सेवाकालीन एआई प्रशिक्षण का संचालन करना , ओपन-सोर्स एआई शिक्षण टूलकिट विकसित करना , तथा शैक्षणिक सहायता प्रणालियों को एकीकृत करना।
- समावेशी डिजिटल अवसंरचना:
- ग्रामीण और सरकारी स्कूलों तक एआई शिक्षा की पहुंच प्रदान करने के लिए पीएम ई-विद्या और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर (एनडीईएआर) का विस्तार करना ।
- बाल सुरक्षा और डेटा संरक्षण:
- नैतिक एआई इंटरैक्शन सुनिश्चित करने के लिए आयु-उपयुक्त एआई डिज़ाइन कोड , सख्त गोपनीयता नियम और डेटा गार्डरेल लागू करें ।
- स्थानीयकरण और पहुंच:
- विविध शिक्षार्थियों के लिए बहुभाषी एआई उपकरण विकसित करने के लिए भाषिणी मिशन और अन्य पहलों के साथ सहयोग करना ।
- नैतिक एआई शिक्षा:
- मूल्य-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप एआई नैतिकता, निष्पक्षता और जवाबदेही मॉड्यूल को एकीकृत करें ।
- सतत पाठ्यक्रम समीक्षा:
- तकनीकी विकास के आधार पर पाठ्यक्रम को समय-समय पर संशोधित और अद्यतन करने के लिए शिक्षा में एआई परिषद की स्थापना करें ।
निष्कर्ष
एआई शिक्षा का उद्देश्य केवल कोडर या इंजीनियर तैयार करना नहीं है , बल्कि ऐसे आलोचनात्मक विचारकों का पोषण करना है जो तकनीक का बुद्धिमानी और नैतिक रूप से उपयोग करने में सक्षम हों। चरणबद्ध, समावेशी और नैतिक रूप से आधारित दृष्टिकोण के साथ , भारत एक ऐसी एआई-तैयार पीढ़ी तैयार कर सकता है जो नवाचार को ज़िम्मेदारी के साथ जोड़कर एक तकनीकी रूप से सशक्त और मानव- केंद्रित भविष्य को आकार दे ।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न: “प्राथमिक स्तर से ही एआई शिक्षा शुरू करने से भविष्य के अवसरों का लोकतंत्रीकरण हो सकता है, लेकिन इससे डिजिटल असमानता बढ़ने का खतरा है।” भारत की शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द हिंदू
(जीएस पेपर 4: पत्रकारिता और लोक सेवा में नैतिकता)
संदर्भ (परिचय)
विनाशकारी उत्तर बंगाल बाढ़ (2025) , जिसने 30 से अधिक लोगों की जान ले ली और 110 बड़े भूस्खलन का कारण बनी , न केवल प्राकृतिक आपदाओं की त्रासदी को उजागर करती है, बल्कि संकट की स्थितियों में मानवीय पीड़ा को कवर करने वाले पत्रकारों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं और नैतिक जिम्मेदारियों को भी उजागर करती है।
आपदा पत्रकारिता में मूल नैतिक सिद्धांत
- शोषण पर सहानुभूति: आघात पर रिपोर्टिंग के लिए संवेदनशीलता ज़रूरी है। पत्रकारों को “ख़बरें” पाने के लिए पीड़ितों से दखलअंदाज़ी भरे सवाल पूछने या उनका भावनात्मक शोषण करने से बचना चाहिए । पीड़ितों की गरिमा को केंद्र में रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानी कहने का तरीका ताक-झांक वाला न हो जाए।
- मानवता और करुणा: सब कुछ खोने के बावजूद, कई बचे लोगों ने दया और एकजुटता दिखाई । नैतिक पत्रकारिता उस मानवता का प्रतिदान करती है – दुःख को बढ़ाने के बजाय लचीलेपन को स्वीकार करती है।
- सूचित सहमति: पीड़ितों को अपना दर्द साझा करने की कोई बाध्यता नहीं है। नैतिक आचरण के लिए साक्षात्कार या तस्वीरें लेने से पहले सूचित सहमति लेना आवश्यक है, खासकर जब व्यक्ति मानसिक संकट में हो ।
- दृश्य प्रतिनिधित्व के प्रति संवेदनशीलता: नैतिक पत्रकारों को ग्राफिक चित्रण के प्रति सतर्क रहना चाहिए – यह सुनिश्चित करते हुए कि दृश्य संवेदना और जागरूकता पैदा करें, सनसनी नहीं। दृश्यों को प्रभावित समुदायों की गोपनीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और भावनात्मक सीमाओं को संरक्षित करना चाहिए ।
- निष्पक्षता और करुणा: सच बोलने और भावनात्मक संयम के बीच संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है। तथ्य सटीक होने चाहिए, लेकिन लहज़ा करुणामय होना चाहिए , मानवीय संकटों के दौरान दोषारोपण या राजनीतिकरण से बचना चाहिए।
- सांस्कृतिक और प्रासंगिक सम्मान: आपदा क्षेत्र अक्सर आदिवासी, सीमावर्ती या अल्पसंख्यक समुदायों से आच्छादित होते हैं । नैतिक रिपोर्टिंग का अर्थ स्थानीय संवेदनशीलता को समझना , रूढ़िवादिता से बचना और हाशिए पर पड़ी आवाज़ों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
- नुकसान और पुनः आघात से बचना: पत्रकारों को मनोवैज्ञानिक सीमाओं को पहचानना चाहिए — दृश्य संकेतों और शारीरिक भाषा को पहचानकर यह जानना चाहिए कि कब सवाल करना बंद करना है। नैतिक संयम पत्रकार और पीड़ित दोनों को आगे के आघात से बचाता है।
क्षेत्र में नैतिक चुनौतियाँ
- पहुँच और सुरक्षा बनाम सूचना देने का कर्तव्य: रिपोर्टर अक्सर दूरदराज के, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खबरें लाने के लिए अस्थिर इलाकों में अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं । सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना एक बार-बार आने वाली नैतिक दुविधा है।
- सीमांत क्षेत्रों में मीडिया की अनुपस्थिति: नौकरशाही बाधाओं या प्रतिशोध के डर के कारण कई सीमावर्ती या उच्च-पहाड़ी समुदायों की खबरें रिपोर्ट नहीं की जातीं। यह मीडिया न्याय में विफलता को दर्शाता है , जहाँ कुछ जीवन राष्ट्रीय आख्यानों में अदृश्य रह जाते हैं।
- आर्थिक और संस्थागत दबाव: “प्रभावशाली कहानियों” की माँग सनसनीखेजता को बढ़ावा दे सकती है। नैतिक पत्रकारिता को व्यावसायिक दबाव का विरोध करना चाहिए और सत्यनिष्ठ, मानव- केंद्रित रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ।
- रिपोर्टर का भावनात्मक आघात: विनाश और मृत्यु की रिपोर्टिंग से अप्रत्यक्ष आघात होता है । नैतिक ढाँचे को पत्रकारों की भलाई तक विस्तारित किया जाना चाहिए , कवरेज के बाद मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सहकर्मी डीब्रीफिंग तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए।
सुधार और सर्वोत्तम प्रथाएँ
- नैतिक संहिता अपनाएं: आपदा कवरेज पर भारतीय प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों को लागू करें , जिसमें सटीकता, संयम और सहानुभूति पर जोर दिया जाए।
- क्षमता निर्माण: पत्रकारों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा , आघात-सूचित रिपोर्टिंग और नैतिक साक्षात्कार तकनीकों में प्रशिक्षित करना ।
- समुदाय-केंद्रित रिपोर्टिंग: घटना- आधारित पत्रकारिता से हटकर व्यक्ति-केंद्रित पत्रकारिता पर ध्यान केन्द्रित करें – लचीलापन, पुनर्प्राप्ति और सीखे गए सबक पर प्रकाश डालें ।
- सहयोगात्मक रिपोर्टिंग: प्रामाणिक, सुरक्षित और समग्र कवरेज सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्राधिकरणों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करें ।
- संस्थागत सहायता प्रणालियाँ: संवेदनशील रिपोर्टों और दृश्यों की नैतिक समीक्षा के लिए समाचार संगठनों के भीतर मीडिया नैतिकता प्रकोष्ठों की स्थापना करना ।
- नैतिक तकनीक का उपयोग: गलत सूचना से निपटने के लिए एआई सत्यापन उपकरणों का उपयोग करें , लेकिन आपदा से संबंधित दृश्यों या कहानियों में डेटा गोपनीयता और प्रासंगिक सटीकता सुनिश्चित करें ।
निष्कर्ष
नैतिक आपदा पत्रकारिता केवल दर्द की कहानियाँ सुनाने के बारे में नहीं है , बल्कि पीड़ितों के सम्मान को बहाल करने के बारे में भी है । सहानुभूति, सच्चाई और ज़िम्मेदारी को कायम रखते हुए , पत्रकार केवल दर्शक से मानवीय एकजुटता और जवाबदेही के वाहक बन जाते हैं । खंडहरों के बीच, केवल बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण की ही नहीं, बल्कि विश्वास और मानवता की भी आवश्यकता है ।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
“आपदा रिपोर्टिंग में सटीकता के साथ-साथ सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है।” भारत में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में, सत्य-कथन और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन बनाने में पत्रकारों की नैतिक ज़िम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
स्रोत: द हिंदू
(जीएस पेपर 1 – आधुनिक भारतीय इतिहास – “देश के भीतर स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और पुनर्गठन।”)
परिचय
1947 में स्वतंत्रता के समय , भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा -जैसे विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, आर्थिक पिछड़ापन, कमज़ोर संस्थाएँ और सामाजिक विखंडन । नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा काम विविधतापूर्ण और विभाजित राष्ट्र में राजनीतिक एकीकरण और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना था।
- एक संप्रभु और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण
- संविधान के निर्माण (1946-49) ने एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राजनीति की नींव रखी।
- संविधान सभा , जो आंशिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी , भारत की बहुलवादी विविधता को प्रतिबिंबित करती थी ।
- बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया ।
- इसने मौलिक अधिकारों , नीति निर्देशक सिद्धांतों और मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचे की गारंटी दी , जिससे विविधता के बीच एकता सुनिश्चित हुई।
- संविधान भारत के राजनीतिक एकीकरण का नैतिक और संस्थागत आधार बन गया।
- रियासतों का एकीकरण
- स्वतंत्रता के बाद, प्रत्यक्ष ब्रिटिश भारत के बाहर 500 से अधिक रियासतें अस्तित्व में थीं। उनका एकीकरण क्षेत्रीय एकता के लिए अत्यंत आवश्यक था ।
- सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन ने कूटनीति, अनुनय और रणनीतिक दृढ़ता के माध्यम से इस प्रक्रिया का नेतृत्व किया ।
- हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अधिकांश शासकों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय कर लिया था – इनमें से प्रत्येक का विलय जनमत संग्रह, सैन्य कार्रवाई या विलय के माध्यम से हुआ था ।
- बाद में, पांडिचेरी (1954) और गोवा (1961) ने भारत के क्षेत्रीय एकीकरण को पूरा किया ।
- पटेल की राजनीतिज्ञता ने उन्हें “भारत का लौह पुरुष” की उपाधि दिलाई, जो व्यावहारिक राष्ट्रवाद के माध्यम से एकता का प्रतीक था।
- भाषाई पुनर्गठन और संघीय संतुलन
- प्रारंभिक नेतृत्व ने विघटन के डर से भाषाई पुनर्गठन को स्थगित कर दिया।
- तेलुगु भाषी राज्य के लिए अनशन के दौरान पोट्टी श्रीरामलु की मृत्यु (1952) के कारण आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा ।
- फजल अली आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए ।
- इसने राजनीतिक मानचित्र को तर्कसंगत बनाया और क्षेत्रीय असंतोष को कम किया, तथा संघीय समायोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संरक्षित किया ।
- जैसा कि रजनी कोठारी ने कहा, इसने भारतीय संघ को कमजोर करने के बजाय मजबूत किया।
- शिक्षा और मानव पूंजी में सुधार
- औपनिवेशिक शिक्षा अभिजात्य और भारत की आवश्यकताओं से अलग थी।
- जन-आधारित, वैज्ञानिक और समतावादी शिक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश की गई ।
- एस. राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने व्यापक विश्वविद्यालय सुधार का आह्वान किया।
- मुदालियर आयोग (1952) ने माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक कौशल पर जोर दिया ।
- यूजीसी (1953) और आईआईटी (1950 से) की स्थापना ने एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा की नींव रखी ।
- संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो समावेशी विकास की ओर एक बदलाव है ।
- एक स्वतंत्र विदेश नीति को आकार देना
- उपनिवेशवाद-विरोध, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से निर्देशित था ।
- कांग्रेस के 1921 के प्रस्ताव और नेहरू के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर , भारत ने वैश्विक मामलों में रणनीतिक स्वायत्तता का लक्ष्य रखा।
- पंचशील समझौते (1954) में पारस्परिक सम्मान, अहिंसा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत शामिल थे ।
- अफ्रीकी-एशियाई एकजुटता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के माध्यम से भारत ने स्वयं को विकासशील विश्व की नैतिक और स्वतंत्र आवाज के रूप में प्रस्तुत किया।
- संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य को शांति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है ।
- राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर काबू पाना
- नये राष्ट्र को विभाजन हिंसा, शरणार्थियों की आमद, खाद्यान्न की कमी और भाषाई विविधता से निपटना पड़ा ।
- नेहरू, पटेल और अम्बेडकर के नेतृत्व में संवैधानिक लोकतंत्र कायम रहा , जबकि कई उत्तर-औपनिवेशिक राज्य अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे थे।
- लोकतांत्रिक चुनाव, स्वतंत्र प्रेस और धर्मनिरपेक्ष शासन भागीदारी के माध्यम से एकता के साधन बन गए ।
- नियोजन, शिक्षा और संस्थागत निर्माण पर जोर देने से प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्थिरता प्रदान हुई।
निष्कर्ष
भारत के प्रारंभिक दशक दूरदर्शी नेतृत्व, समावेशी संविधानवाद और व्यावहारिक शासन-कला से चिह्नित थे ।
- संवैधानिक लोकतंत्र, संघीय पुनर्गठन, शैक्षिक सुधार और गुटनिरपेक्ष कूटनीति के माध्यम से प्राप्त विविधता के साथ एकता के संश्लेषण ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय राष्ट्र न केवल जीवित रहा, बल्कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे लचीले लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ ।
- सामाजिक न्याय, सहभागी शासन और सहकारी संघवाद – जो भारत की स्वतंत्रता की सच्ची भावना है – के माध्यम से इस एकता को और गहरा करना चुनौती बनी हुई है ।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न: “स्वतंत्रता-पश्चात् भारत में राजनीतिक सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय एकता केवल राजनीतिक एकीकरण के माध्यम से ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी संविधानवाद और समावेशी राज्य-निर्माण के माध्यम से प्राप्त हुई।” चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस











