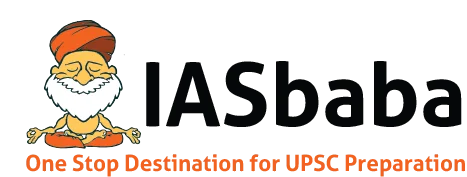IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
Archives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: अर्थशास्त्र
प्रसंग: अदृश्य निर्यातों – सेवाओं और निजी धन-प्रेषण हस्तांतरण – से भारत की विदेशी मुद्रा आय अब दृश्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक हो गई है।
संदर्भ का दृष्टिकोण:
प्रमुख बिंदु:
परिभाषा और बदलाव:
- दृश्य व्यापार से तात्पर्य भौतिक वस्तुओं के निर्यात से है।
- अदृश्य व्यापार में सेवाएं (जैसे आईटी, वित्त) और निजी स्थानान्तरण (जैसे धनप्रेषण) शामिल हैं।
- 2024-25 में भारत का अदृश्य निर्यात: 576.54 बिलियन डॉलर, जो 441.79 बिलियन डॉलर के वस्तु निर्यात से अधिक है ।
दृश्य /मूर्त बनाम अदृश्य /अमूर्त (Tangibles vs Intangibles):
- वस्तु निर्यात 66.29 बिलियन डॉलर (2003-04) से बढ़कर 441.79 बिलियन डॉलर (2024-25) हो गया।
- सेवाओं में उछाल और धन प्रेषण प्रवाह के कारण 2020 के बाद अदृश्य प्राप्तियों में तेजी से उछाल आया।
- कोविड के बाद वैश्विक सुधार के कारण 2021-23 के दौरान बड़ी वृद्धि हुई।
अदृश्य घटक:
- सेवा निर्यात: 2024-25 में 387.54 बिलियन डॉलर, मुख्यतः आईटी, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं से।
- निजी स्थानान्तरण (मुख्यतः एनआरआई धन प्रेषण): 135.43 बिलियन डॉलर , खाड़ी और पश्चिम में भारतीय प्रवासियों द्वारा संचालित।
आर्थिक महत्व:
- अदृश्य वस्तुएं, वस्तु व्यापार के विपरीत, भूराजनीति, टैरिफ और आपूर्ति झटकों के प्रति लचीली होती हैं।
- भारत वस्तु व्यापार घाटा बनाए रखता है (उदाहरण के लिए, 2024-25 में -278.1 बिलियन डॉलर) लेकिन इसे मजबूत अदृश्य अधिशेष (263.85 बिलियन डॉलर) के माध्यम से संतुलित करता है।
रणनीतिक लाभ:
- भारत का तुलनात्मक लाभ भौतिक वस्तुओं के बजाय कौशल, सेवाओं और मानव पूंजी के निर्यात में निहित है।
- इससे अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक व्यवधानों से बचाया गया है और वृहद आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है।
Learning Corner:
भुगतान संतुलन (Balance of Payments (BoP)
भुगतान संतुलन (बीओपी) एक देश और शेष विश्व के बीच एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष या एक तिमाही के दौरान सभी आर्थिक लेनदेन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है।
भुगतान संतुलन (बीओपी) के मुख्य घटक :
चालू खाता (Current Account)
यह माल, सेवाओं और स्थानान्तरण के दैनिक लेन-देन से संबंधित है।
- क) व्यापारिक व्यापार (दृश्य व्यापार):
भौतिक वस्तुओं (जैसे, तेल, मशीनरी) का निर्यात और आयात । - ख) सेवाएँ (अदृश्य व्यापार):
आईटी, बैंकिंग, पर्यटन जैसी अमूर्त सेवाओं का निर्यात और आयात । - ग) प्राथमिक आय:
निवेश और मजदूरी से आय, जैसे कि लाभांश, ब्याज और विदेश में अर्जित वेतन। - घ) द्वितीयक आय (स्थानान्तरण):
एकतरफा स्थानान्तरण जैसे अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धन, उपहार और दान।
चालू खाता शेष = निर्यात – आयात (माल, सेवाओं, आय और स्थानान्तरण का)
पूंजी खाता (Capital Account)
पूंजीगत हस्तांतरण और गैर-उत्पादित, गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों (लघु घटक) के अधिग्रहण/निपटान को रिकॉर्ड करता है ।
वित्तीय खाता
सीमाओं के पार निवेश प्रवाह पर नज़र रखता है।
- क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
- ख) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)
- ग) ऋण और बैंकिंग पूंजी
- घ) आरक्षित परिसंपत्तियाँ (जैसे आरबीआई द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार)
भूल चुक / त्रुटि (Errors and Omissions)
डेटा असंतुलन के कारण होने वाली विसंगतियों को ध्यान में रखने के लिए एक संतुलन मद।
बीओपी स्थिति:
- यदि अंतर्वाह > बहिर्वाह → भुगतान संतुलन अधिशेष
- यदि बहिर्वाह > अंतर्वाह → भुगतान संतुलन घाटा
भारत में अक्सर चालू खाता घाटा (वस्तु आयात पर निर्भरता के कारण) रहता है, लेकिन मजबूत पूंजी प्रवाह और अदृश्य प्राप्तियों के माध्यम से भुगतान संतुलन स्थिरता बनाए रखता है।
स्रोत: THE INDIAN EXPRESS
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
मुख्य तथ्य
- इस बात पर जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक जैसी 20वीं सदी की संस्थाएं अब 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।
- बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था के लिए आग्रह किया गया, जिसमें निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए।
- इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा, जो कि अधिकांशतः विकासशील देशों से है, अभी भी अल्प प्रतिनिधित्व वाला है।
- विकास, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पहुंच पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं में दोहरे मानदंडों और दिखावटीपन की आलोचना की गई ।
- ऐसे सुधारों का आह्वान किया गया जो ठोस परिणाम ला सकें – जैसे शासन, नेतृत्व की भूमिका और मताधिकार का पुनर्गठन।
- पुरानी वैश्विक प्रणालियों पर जोर देने के लिए ” नेटवर्क के बिना सिम कार्ड ” और ” 20वीं सदी के टाइपराइटर पर 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर ” जैसी उपमाओं का इस्तेमाल किया गया।
- नए ब्रिक्स सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत किया गया तथा समूह के विस्तार में ब्राजील के नेतृत्व की प्रशंसा की गई।
- वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा समावेशी वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के साथ काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई ।
- शिखर सम्मेलन में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्यों ने भाग लिया, जिसका ध्यान अधिक न्यायसंगत और सतत विश्व व्यवस्था के निर्माण पर केंद्रित था।
Learning Corner:
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (2025)
- 17 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई, 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया।
विषय/ थीम:
“बहुध्रुवीय विश्व के लिए वैश्विक शासन में सुधार”
मुख्य तथ्य:
- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्यों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेताओं ने भाग लिया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निम्न कार्यों के लिए आह्वान किया:
- वैश्विक संस्थाओं में वैश्विक दक्षिण (Global South) का अधिक प्रतिनिधित्व
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में तत्काल सुधार
- वैश्विक विकास, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पहुंच में दोहरे मानकों का अंत
- मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि 20वीं सदी की संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए पुरानी हो चुकी हैं।
- इंडोनेशिया के शामिल किए जाने का स्वागत किया गया तथा ब्रिक्स के विस्तार में ब्राजील के नेतृत्व की प्रशंसा की गई।
शिखर सम्मेलन के परिणाम:
- समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि
- ब्रिक्स सदस्यता के विस्तार का समर्थन किया
- समतापूर्ण एवं सतत वैश्विक विकास का आह्वान किया गया
- वैश्विक शासन संरचना में दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सुधार पर जोर दिया गया
महत्व:
- वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक समावेशी मंच बनाने की दिशा में बदलाव को चिह्नित किया ।
- अधिक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में ब्रिक्स की भूमिका को मजबूत किया गया ।
BRICS
ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुपक्षीय समूह है: जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इसकी स्थापना विकासशील देशों के बीच शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार लाने के लिए की गई थी।
प्रमुख विशेषताऐं:
- गठन:
2006 में “ब्रिक” के रूप में इसकी शुरुआत हुई; 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिससे यह ब्रिक्स बन गया। - उद्देश्य:
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत
- संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए प्रयास
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना
- सहयोग के मुख्य स्तंभ:
- राजनीतिक और सुरक्षा
- आर्थिक एवं वित्तीय
- सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आदान-प्रदान
- प्रमुख पहल:
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी): बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराता है
- आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए): वित्तीय संकट के दौरान सदस्य देशों को सहायता प्रदान करती है
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: रणनीतिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं की वार्षिक बैठक
- हालिया विस्तार:
2024-25 में, ब्रिक्स का विस्तार मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया को शामिल करने के लिए किया गया, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव बढ़ गया।
महत्व:
- यह विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% प्रतिनिधित्व करता है।
- ये एक अधिक संतुलित और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में कार्य करता है।
स्रोत: THE HINDU
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ : स्वदेशी 700 मेगावाट भारी जल रिएक्टरों को परिचालन लाइसेंस मिल गया है।
मुख्य तथ्य:
- भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन (केएपीएस) में दो स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) को परिचालन लाइसेंस प्रदान कर दिया है।
- KAPS-3 और KAPS-4 इस पैमाने के पहले भारतीय डिजाइन वाले रिएक्टर हैं। KAPS-3 अगस्त 2023 में पूरी क्षमता पर पहुंच गया; KAPS-4 अगस्त 2024 में इसके बाद आया। सुरक्षा आकलन के बाद जुलाई 2025 में लाइसेंस दिया गया।
महत्व:
- यह भारत की परमाणु आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है , जो बड़े पैमाने पर रिएक्टरों की डिजाइन, निर्माण और संचालन की देश की क्षमता को मजबूत करेगा।
- एनपीसीआईएल अब पूरे भारत में फ्लीट मोड में 700 मेगावाट के 10 और पीएचडब्ल्यूआर का निर्माण कर रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा।
- भारत में पहले से ही 15 PHWR (220 मेगावाट) और 2 PHWR (540 मेगावाट) संचालित हैं। 700 मेगावाट मॉडल एक तकनीकी उन्नयन है।
प्रौद्योगिकी अवलोकन:
- पीएचडब्ल्यूआर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में तथा भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है।
- ये अपनी उच्च सुरक्षा, लागत दक्षता और भारत के संसाधन आधार के लिए उपयुक्तता के लिए जाना जाता है ।
भविष्य की योजनाएं :
- राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 700 मेगावाट के अतिरिक्त पीएचडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं या उनकी योजना बनाई गई है ।
- यह प्रगति भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करती है तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है।
Learning Corner:
भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा
प्रारंभिक नींव:
- दूरदर्शी नेतृत्व: भारत के परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना डॉ. होमी जे. भाभा ने की थी, जिन्होंने भारत के सीमित यूरेनियम और प्रचुर थोरियम संसाधनों का उपयोग करने के लिए तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी।
- संस्थागत ढांचा:
- परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) की स्थापना 1948 में हुई
- परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की स्थापना 1954 में हुई
- भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की स्थापना 1987 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए की गई थी
तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम:
- प्रथम चरण: प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर)
- चरण 2: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) जो प्रयुक्त ईंधन से प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं
- चरण 3: थोरियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले उन्नत रिएक्टर (अभी तक व्यावसायिक रूप से तैनात नहीं किए गए हैं)
प्रमुख उपलब्धियां:
- 1969: पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, चालू हुआ
- 1974 और 1998: परमाणु परीक्षण (पोखरण-I और II) किए, सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया
- 2008: भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से परमाणु अलगाव समाप्त हुआ, जिससे यूरेनियम का आयात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव हुआ
- 2023–25: KAPS-3 और KAPS-4 जैसे स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR पूर्ण शक्ति पर पहुंच गए
वर्तमान स्थिति (2025 तक):
- स्थापित क्षमता: ~7,500 मेगावाट
- प्रचालनरत रिएक्टर: 22 परमाणु रिएक्टर
- निर्माणाधीन रिएक्टर: 10+ PHWRs बेड़े मोड में
- प्रौद्योगिकी मिश्रण: पीएचडब्ल्यूआर, उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर), हल्के पानी रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर), फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)
भविष्य का दृष्टिकोण :
- कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) की स्थापना जल्द ही होने की उम्मीद
- स्वदेशी रिएक्टर प्रौद्योगिकी और थोरियम उपयोग पर जोर
- शुद्ध-शून्य और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है
परमाणु रिएक्टरों के विभिन्न प्रकार
परमाणु रिएक्टरों को ईंधन, मॉडरेटर और इस्तेमाल किए जाने वाले शीतलक के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है । नीचे विश्व स्तर पर और भारत में प्रासंगिक प्रमुख प्रकार दिए गए हैं:
दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR)
- ईंधन: प्राकृतिक यूरेनियम
- मॉडरेटर और शीतलक: भारी जल (D₂O)
- उदाहरण: काकरापार (KAPS), राजस्थान (RAPS)
- विशेषताएँ:
- उच्च न्यूट्रॉन व्यवस्था
- भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों के लिए उपयुक्त
- स्वदेशी डिजाइन (700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर भारत की नवीनतम प्रगति है)
क्वथन जल रिऐक्टर /उबलते जल पर आधारित रिएक्टर (Boiling Water Reactor (BWR)
- ईंधन: संवर्धित यूरेनियम
- मॉडरेटर और शीतलक: हल्का पानी
- उदाहरण: तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन
- विशेषताएँ:
- भाप सीधे रिएक्टर कोर में उत्पन्न होती है
- सरल डिजाइन लेकिन रेडियोधर्मी भाप रिसाव का उच्च जोखिम
दाबयुक्त जल रिएक्टर (Pressurized Water Reactor (PWR)
- ईंधन: संवर्धित यूरेनियम
- मॉडरेटर और शीतलक: हल्का पानी
- उदाहरण: कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (रूसी डिजाइन)
- विशेषताएँ:
- विश्व स्तर पर सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला
- शीतलक को उबलने से रोकने के लिए उच्च दाब में रखा जाता है
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)
- ईंधन: प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX)
- मॉडरेटर: कोई नहीं
- शीतलक: तरल सोडियम
- उदाहरण: प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर), कलपक्कम
- विशेषताएँ:
- यह जितना ईंधन खपत करता है, उससे अधिक पैदा करता है
- भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए आवश्यक
उन्नत भारी जल रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) (विकासाधीन) (Advanced Heavy Water Reactor (AHWR) (Under development))
- ईंधन: थोरियम + यूरेनियम-233
- मॉडरेटर और शीतलक: भारी जल/हल्का जल
- उद्देश्य:
- तीसरे चरण का हिस्सा
- थोरियम भंडार का उपयोग
- उच्च सुरक्षा और निष्क्रिय शीतलन सुविधाएँ
लाइट वाटर रिएक्टर (LWR)
- ईंधन: संवर्धित यूरेनियम
- मॉडरेटर और शीतलक: हल्का पानी
- टिप्पणी:
- BWR और PWR दोनों उपप्रकार शामिल हैं
- अंतर्राष्ट्रीय असैन्य परमाणु कार्यक्रमों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी)
परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) भारत का स्वतंत्र परमाणु विनियामक प्राधिकरण है , जो आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है । यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत कार्य करता है ।
स्थापना:
- स्थापना: 15 नवंबर, 1983
- निम्न के द्वारा: भारत सरकार
- निम्न के अंतर्गत: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
अधिदेश एवं कार्य:
- नियामक निरीक्षण:
- परमाणु सुविधाओं के स्थान निर्धारण, डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और डीकमीशनिंग को मंजूरी देता है।
- विकिरण सुरक्षा:
- चिकित्सा, उद्योग, कृषि और अनुसंधान में विकिरण के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- मानक एवं दिशानिर्देश:
- IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) मानकों के अनुरूप परमाणु और विकिरण सुविधाओं के लिए सुरक्षा कोड, मैनुअल और प्रक्रियाएं तैयार करना।
- लाइसेंसिंग:
- संपूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और विकिरण प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी करता है।
- निरीक्षण एवं प्रवर्तन:
- आवधिक निरीक्षण आयोजित करना तथा आवश्यक होने पर शटडाउन आदेश सहित सुरक्षा अनुपालन लागू करना।
- सार्वजनिक एवं पर्यावरण संरक्षण:
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिकों और आम जनता के लिए विकिरण जोखिम निर्धारित सीमा के भीतर रहे।
संरचना:
- एईआरबी परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) को रिपोर्ट करता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन है।
- यह निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एनपीसीआईएल जैसे परमाणु संयंत्र संचालकों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
स्रोत : THE HINDU
श्रेणी: पर्यावरण
संदर्भ: ग्रेट निकोबार द्वीप अवसंरचना परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) में भूकंपीय जोखिमों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए आलोचना की गई है, जबकि यह क्षेत्र बड़े भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।
प्रमुख आलोचनाएँ:
- भूकंपीय जोखिम को कम आंकना:
ईआईए 2019 के एक सीमित अध्ययन पर निर्भर करता है, जो मुख्य रूप से सुनामी के खतरों पर केंद्रित है और व्यापक भूकंप खतरों को नजरअंदाज करता है, बावजूद इसके कि इस क्षेत्र में बड़े भूकंपों की उच्च संभावना है। - स्वतंत्र अनुसंधान की उपेक्षा:
स्वतंत्र अध्ययनों से पता चलता है कि यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, जहां भूकम्प आने, मृदा द्रवीकरण और भूमि अवतलन की संभावना है, जैसा कि 2004 की सुनामी में देखा गया था। - पारदर्शिता का अभाव:
आलोचकों का दावा है कि मंजूरी प्रक्रिया अपारदर्शी थी और इसमें पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की तुलना में तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को प्राथमिकता दी गई।
आधिकारिक रुख:
- सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी निर्माण कार्यों में भारतीय भूकंपरोधी नियमों का पालन किया जाएगा तथा आपदा प्रबंधन योजना भी लागू की गई है।
- निकट भविष्य में 2004 स्तर के एक और भूकंप के खतरे को कमतर आंकता है।
विशेषज्ञ की अनुशंसाएँ:
- स्वतंत्र समीक्षा:
विशेषज्ञ भूकंपीय संवेदनशीलता पर केन्द्रित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा पारदर्शी पुनर्मूल्यांकन का आग्रह। - नियामक निरीक्षण:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण और तटीय विनियमन मंजूरी के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान करते हुए अस्थायी रोक लगा दी है।
Learning Corner:
पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment (EIA)
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी प्रस्तावित विकास परियोजना के स्वीकृत या कार्यान्वित होने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णयकर्ता आर्थिक और तकनीकी कारकों के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार करें।
पर्यावरण प्रभाव आकलन के उद्देश्य:
- परियोजना नियोजन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना
- प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए शमन उपायों का प्रस्ताव करना
- सतत विकास को बढ़ावा देना
- सूचित एवं पारदर्शी निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना
ईआईए के प्रमुख घटक:
- स्क्रीनिंग – यह निर्धारित करता है कि किसी परियोजना को EIA की आवश्यकता है या नहीं
- स्कोपिंग – अध्ययन किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और प्रभावों की पहचान करता है
- प्रभाव आकलन – संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करता है
- सार्वजनिक परामर्श – निर्णय लेने में हितधारकों को शामिल करना
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) – शमन रणनीतियों का सुझाव देती है
- निगरानी और अनुपालन – यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन करती है
भारत में कानूनी ढांचा:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा शासित
- ईआईए अधिसूचना, 2006 (समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से संचालित
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (SEIAAs) द्वारा विनियमित
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना
ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना एक विशाल बुनियादी ढांचा विकास पहल है जिसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी द्वीप को रणनीतिक रूप से बदलना है। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक, रणनीतिक और पर्यावरणीय निहितार्थ हैं ।
प्रमुख विशेषताऐं:
- स्थान: ग्रेट निकोबार द्वीप, मलक्का जलडमरूमध्य के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है
- परियोजना घटक:
- अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी)
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
- बिजली संयंत्र
- श्रमिकों और निवासियों के लिए टाउनशिप
- कार्यान्वयन एजेंसी: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (एएनआईआईडीसीओ), केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त
सामरिक महत्व:
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति को बढ़ाया गया
- इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीनी प्रभाव को संतुलित करना है
- प्रमुख शिपिंग मार्गों की निकटता के माध्यम से सुरक्षित समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान करता है
पर्यावरणीय चिंता:
- यह द्वीप पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य क्षेत्र है, जो जैव विविधता और जनजातीय विरासत से समृद्ध है
- ईआईए की आलोचनाएँ: भूकंपीय जोखिमों का कथित कम आंकलन, पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त परामर्श
- प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, जनजातीय समुदायों और वन्यजीव आवासों पर संभावित प्रभाव
वर्तमान स्थिति:
- पर्यावरणीय और तटीय विनियमन मंजूरी मिल गई है, हालांकि पर्यावरणविदों और नागरिक समाज समूहों द्वारा इसे चुनौती दी गई है
- अनुपालन और जोखिम पुनर्मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा समीक्षा के अधीन
स्रोत : THE HINDU
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ: केरल में निपाह वायरस के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मलप्पुरम और पलक्कड़ में सतर्कता बढ़ा दी गई है, तथा इसके और फैलने के खतरे के कारण कोझिकोड में अलर्ट जारी किया गया है।
रोकथाम और प्रतिक्रिया उपाय:
- निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग:
तीनों जिलों में 400 से अधिक व्यक्ति निगरानी में हैं। समर्पित टीमें ट्रेसिंग, लक्षण निगरानी और संगरोध का काम कर रही हैं। - चिकित्सा अवसंरचना:
आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू सुविधाएं सक्रिय कर दी गई हैं। मलप्पुरम में 12 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से 5 आईसीयू में हैं, जबकि पलक्कड़ में 4 आइसोलेशन में हैं। - कंटेनमेंट जोन और जागरूकता:
प्रभावित वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मास्क पहनना अनिवार्य है और आवाजाही पर प्रतिबंध है, साथ ही घर-घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। - आपातकालीन समन्वय:
जिला अधिकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से नियंत्रण, हेल्पलाइन और अस्पष्टीकृत मौतों पर नज़र रख रहे हैं। - मंत्रिस्तरीय निगरानी:
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों की निगरानी कर रही हैं।
Learning Corner:
निपाह वायरस
निपाह वायरस (NiV) एक जूनोटिक वायरस (जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला) है जो दूषित भोजन या सीधे मानव-से-मानव संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है । इसे महामारी क्षमता वाला एक अत्यधिक घातक रोगज़नक़ माना जाता है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- कारक एजेंट: निपाह वायरस, पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से संबंधित
- प्राकृतिक मेजबान: टेरोपस प्रजाति के फल चमगादड़ (Fruit bats of the Pteropus genus)
- संचरण:
- चमगादड़ से मनुष्य तक दूषित फल या ताड़ के रस के माध्यम से
- पशुओं (विशेषकर सूअरों) से लेकर मनुष्यों तक
- मानव-से-मानव निकट संपर्क या शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से
लक्षण:
- बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द
- उल्टी और गले में खराश
- चक्कर आना, drowsiness
- गंभीर मामलों में: एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन), कोमा और मृत्यु
मृत्यु दर:
- प्रकोप की प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच के आधार पर यह 40% से 75% तक होता है
भौगोलिक संदर्भ:
- मलेशिया में चिह्नित (1998-99)
- भारत में, पश्चिम बंगाल (2001, 2007) और केरल (2018, 2019, 2021, 2023 और 2025) में इसका प्रकोप हुआ है।
उपचार और रोकथाम:
- कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है
- प्रबंधन सहायक है, लक्षण राहत और महत्वपूर्ण देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है
- रोकथाम में शामिल हैं:
- चमगादड़ों और सूअरों के संपर्क से बचें
- ज़मीन पर गिरे हुए फल या ताड़ के रस का सेवन न करें
- अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण के सख्त उपाय
स्रोत: THE HINDU
(MAINS Focus)
प्रसंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “जय अनुसंधान” (Hail Innovation) के आह्वान, जिसे ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष द्वारा समर्थन प्राप्त है, का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलना है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों को व्यावसायिक रूप से अपनाना आवश्यक है, जो विनियामक तंत्र में फंसी हुई हैं।
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें क्या हैं ?
- आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं, जिनके डीएनए को आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया गया है।
- इसका उद्देश्य पौधे में एक नया गुण लाना है जो उस प्रजाति में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, जैसे कुछ कीटों, रोगों, पर्यावरणीय स्थितियों, शाकनाशियों आदि के प्रति प्रतिरोध। पोषण मूल्य, फार्मास्यूटिकल्स, जैव ईंधन आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी आनुवंशिक संशोधन किया जाता है।
- जीएम फसलों को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर (जीई) पौधे, ट्रांसजेनिक फसलें, जीवित संशोधित जीव (एलएमओ) या बायोटेक फसलें भी कहा जाता है।
जीएम फसलों के लाभ:
- जीएम फसलों से उपज बढ़ सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर हो सकती हैं।
- कुछ जीएम फसलें, जैसे बीटी कपास, सिंथेटिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करती हैं, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है।
- कुछ जीएम फसलों को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि उनकी शेल्फ आयु लंबी हो जाए, जिससे खाद्यान्न की बर्बादी कम हो।
जीएम फसलों की स्थिति
- 2023 तक, 76 देशों में 200 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जीएम सोयाबीन , मक्का, कैनोला आदि की खेती की जा रही है।
- भारत में, केवल बीटी कॉटन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है और 2002 से इसे व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है । भारत के 90 प्रतिशत से अधिक कपास क्षेत्र में बीटी कॉटन की खेती होती है और इसके बीज मवेशियों को खिलाए जाते हैं। इसलिए, एक तरह से, जीएम फसल पहले से ही हमारे खाद्य प्रणाली में है।
- बीटी बैंगन : 2009 में जीईएसी द्वारा अनुमोदित, लेकिन व्यावसायिक रिलीज पर रोक लगी हुई है।
- जीएम सरसों (डीएमएच-11) : 2022 में सशर्त पर्यावरणीय मंज़ूरी दी गई, लेकिन अभी तक इसका व्यावसायीकरण नहीं हुआ है ।
कपास पर प्रभाव
- कपास का उत्पादन 2002-03 में 13.6 मिलियन गांठों से बढ़कर 2013-14 में 39.8 मिलियन गांठों तक पहुंच गया, जो 193 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि है।
- उत्पादकता में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई (302 किग्रा/हेक्टेयर से 566 किग्रा/हेक्टेयर तक)
- खेती का क्षेत्रफल 56 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें बीटी कपास का प्रभुत्व रहा।
- कृषि सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 8 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि हुई।
- भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जिसने 2011-12 के दौरान 4.1 बिलियन डॉलर का शुद्ध निर्यात किया।
- हालांकि, 2015 के बाद, कपास की पैदावार 566 किलोग्राम/हेक्टेयर (2013-14) से घटकर 436 किलोग्राम/हेक्टेयर (2023-24) हो गई । यह वैश्विक औसत (~ 770 किलोग्राम/हेक्टेयर) से कम है और चीन (1,945 किलोग्राम/हेक्टेयर) और ब्राजील (1,839 किलोग्राम/हेक्टेयर) से बहुत पीछे है।
- औसत वार्षिक कपास उत्पादन में 2% की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण गुलाबी / पिंक बॉलवर्म और सफेद मक्खियों जैसे कीटों का प्रकोप, जटिल नियमन, तथा अगली पीढ़ी के कपास बीजों जैसे कि शाकनाशी-सहिष्णु (एचटी) बीटी कपास पर प्रतिबंध है।
कारण:
- ग्लाइफोसेट के छिड़काव से बचने के लिए तैयार की गई एचटी-बीटी कपास को अब तक हटाया नहीं गया है। इसके बावजूद, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना , आंध्र प्रदेश और पंजाब के खेतों में इसके बीज लीक हो गए हैं। उद्योग निकायों और सर्वेक्षणों का अनुमान है कि अवैध एचटी-बीटी कपास के रकबे का 15-25 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है।
- 2015 से, निजी बीज अनुबंधों में सरकारी हस्तक्षेप भारत के कपास क्षेत्र में नवाचार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। कपास बीज मूल्य नियंत्रण आदेश (2015) ने रॉयल्टी शुल्क में कटौती की है, जिससे नवाचार हतोत्साहित हुआ है, विशेषता शुल्क को एमएसपी के 10% पर सीमित कर दिया है, 30 दिनों में अनिवार्य तकनीकी हस्तांतरण के साथ जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक बायोटेक फर्मों की भागीदारी कम हो गई है
- परिणामस्वरूप, 2011-12 के बाद कपास के निर्यात में गिरावट शुरू हो गई और 2024-25 तक भारत कच्चे कपास का शुद्ध आयातक बन गया, जिसका शुद्ध आयात 0.4 बिलियन डॉलर था।
अन्य फसलों की स्थिति
- बीटी के लिए स्वीकृति बैंगन और जीएम सरसों (डीएमएच 11) पर रोक लगी हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्राप्त इन फसलों को अभी तक पूर्ण व्यावसायिक हरी झंडी नहीं मिली है।
- बीटी बैंगन पर 2009 से ही रोक लगी हुई है, जबकि जीएम सरसों को 2022 में सशर्त पर्यावरणीय मंजूरी मिली है – लेकिन आगे की नियामक जांच और संभवतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में इसका व्यावसायीकरण रुका हुआ है।
- व्यवसायीकरण पर रोक लगाकर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा डालकर, भारत के कठोर नियामक रुख ने फसल नवाचार को अवरुद्ध कर दिया है, आयात पर निर्भरता को मजबूर कर दिया है, और जीन क्रांति का नेतृत्व करने का अवसर गंवा दिया है।
आगे की राह
- पारदर्शी और विज्ञान-आधारित विनियामक ढांचा तैयार करना
- सार्वजनिक-निजी अनुसंधान एवं विकास साझेदारी को प्रोत्साहित करना
- जीईएसी द्वारा स्वीकृत जीएम फसलों के लिए पायलट कार्यक्रमों का समर्थन करना
- नवीनता के साथ सामर्थ्य को संतुलित करने के लिए SPCO 2015 की समीक्षा करना
- जी.एम. खाद्य पदार्थों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए जागरूकता फैलाना
- जी.एम. तकनीक को जलवायु-स्मार्ट कृषि के साथ एकीकृत करना
निष्कर्ष
खेत से लेकर निर्यात तक, भारत का भविष्य जीन प्रौद्योगिकी को अपनाने पर निर्भर करता है। अगर जीएम फसलें जिम्मेदारी से इस्तेमाल की जाएं तो उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के प्रति भारत का सतर्क दृष्टिकोण वैज्ञानिक नवाचार और विनियामकीय हिचकिचाहट के बीच गहरे संघर्ष को दर्शाता है।” समालोचनात्मक जांच करें। (250 शब्द, 15 अंक)
प्रसंग:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। 2024-25 के बजट में किए गए वादे के अनुसार इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है।
भारत में रोजगार की स्थिति
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार
-
श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate (LFPR):
- शहरी पुरुष एलएफपीआर 74.3% (2023) से बढ़कर 75.6 % (2024) हो गया।
- शहरी महिला एलएफपीआर 25.5% से मामूली रूप से बढ़कर 25.8% हो गई ।
- समग्र शहरी एलएफपीआर 50.3% से बढ़कर 51.0% हो गया।
- श्रेणीवार भिन्नताओं के बावजूद अखिल भारतीय एलएफपीआर 56.2% पर स्थिर रहा।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio (WPR):
- सभी श्रेणियों में मामूली सुधार देखा गया, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में समग्र WPR (47.0% से 47.6%) में।
- अखिल भारतीय स्तर पर समग्र WPR अपेक्षाकृत अपरिवर्तित (53.4% से 53.5%) रहा।
- बेरोज़गारी के रुझान (पीएलएफ़एस 2023–24)
-
- ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.3% से मामूली रूप से घटकर 4.2% हो गयी ।
- शहरी पुरुष बेरोज़गारी 6.0% से बढ़कर 6.1% हुई
- शहरी महिला बेरोज़गारी 8.9% से घटकर 8.2% हो गयी ।
- समग्र शहरी बेरोजगारी 6.7% पर स्थिर रही ।
- अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 5.0% से मामूली रूप से घटकर 4.9% हो गयी ।
- घरेलू उद्यमों में अवैतनिक महिला सहायकों की संख्या में कमी (19.9% से 18.1% तक) ने ग्रामीण क्षेत्रों में WPR और LFPR को कम करने में योगदान दिया।
योजना के मुख्य प्रावधान
- कौन क्रियान्वयन करेगा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस योजना को लागू करेगा।
- 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
- प्रमुख प्रावधान:
-
- ₹1 लाख तक के वेतन वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को दो किस्तों में ₹15,000 तक एक महीने का ईपीएफ वेतन मिलेगा।
- ईपीएफओ पहली किस्त का भुगतान छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त का भुगतान 12 महीने की सेवा के बाद करेगा – दोनों ही किस्तें सीधे बैंक हस्तांतरण के रूप में होंगी।
- प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा “एक निश्चित अवधि के लिए बचत जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में निकाला जा सकेगा”।
- ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को, “कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए” दो साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक मिलेंगे।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएंगे।
- योजना के भाग ए के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग करके डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से किए जाएंगे। भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
विशेषज्ञ की राय:के.ई. रघुनाथन (भारतीय उद्यमी संघ) सुझाव देते हैं कि:
|
प्रस्तावित लाभ
ईएलआई योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, प्रतिधारण (retention) और कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करके भारत के रोजगार संकट को दूर करना है। इस योजना के उद्देश्य हैं:
- निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि : यह पहल निजी क्षेत्र की कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए वित्तीय पुरस्कार प्रदान करके अतिरिक्त कर्मचारियों, विशेष रूप से कार्यबल में नए प्रवेशकों की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- युवा रोजगार को बढ़ावा देना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायों को युवा व्यक्तियों, विशेषकर पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करके युवा बेरोजगारी को कम करना है।
- नौकरी बनाए रखने को बढ़ावा देना: ईएलआई कार्यक्रम में उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर नौकरी बनाए रखने को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हैं जो समय के साथ उच्च कार्यबल स्तर बनाए रखते हैं, विशेष रूप से वे जो एक विशिष्ट सीमा से परे भर्ती करते हैं।
- कौशल उन्नयन को प्रोत्साहित करना: यह पहल कौशल में सुधार लाने के सरकारी उद्देश्यों के अनुरूप है, विशेष रूप से युवा लोगों के बीच, जो नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को प्रशिक्षण और उन्नत बनाने में निवेश करने के लिए प्रेरित करके है।
- औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना: इस पहल का उद्देश्य रोजगार को औपचारिक बनाना है, खासकर उन उद्योगों में जो ऐतिहासिक रूप से अनौपचारिक श्रम पर निर्भर रहे हैं। इसमें नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना शामिल है जो श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करते हैं, भविष्य निधि (पीएफ) कवरेज जैसे लाभ प्रदान करते हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में सुधार: इस कार्यक्रम में विनिर्माण उद्योग के लिए लक्षित उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कार्यबल में नए व्यक्तियों की भर्ती को बढ़ावा देकर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
- आर्थिक असमानता में कमी: युवा व्यक्तियों, विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता देकर, इस पहल का उद्देश्य आर्थिक असमानता में कमी लाना और सामाजिक गतिशीलता में सुधार करना है।
- नियोक्ताओं को भर्ती में सहायता प्रदान करना: वित्तीय सहायता प्रदान करके, जैसे कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियोक्ताओं को उनके पीएफ अंशदान की प्रतिपूर्ति करना, कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं के व्यय को कम करना और उन्हें अपने स्टाफिंग स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है।
- ईएलआई योजना, दो साल की अवधि में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा । केंद्र को उम्मीद है कि 1.92 करोड़ नए रोज़गार वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई, 2027 को समाप्त होगी।
ट्रेड यूनियनों का दृष्टिकोण
- आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मजदूर संघ (बीएमएस) समेत सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं।
- अन्य यूनियनों को डर है कि श्रमिकों के पैसे का उपयोग नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।
- उन्होंने 2020 के उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन के भाग्य का हवाला दिया, जिसमें कुछ क्षेत्रों को नौकरियां पैदा करने के लिए केंद्र द्वारा छूट दी गई थी, लेकिन पैसा बड़ी कंपनियों की जेब में चला गया था।
- उन्होंने तर्क दिया कि ईपीएफओ को जांच करनी पड़ी तथा कुछ कम्पनियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, क्योंकि यह पाया गया कि योजना का दुरुपयोग नियोक्ताओं के लाभ के लिए किया जा रहा है।
- ईएलआई योजना के साथ, सरकार का इरादा सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अलावा पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल का औपचारिकीकरण भी होगा।
विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताएँ
- चूंकि ईपीएफओ केवल कर्मचारियों की बचत का संरक्षक है, इसलिए वह योजना को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में कैसे कार्य कर सकता है।
- चूंकि ईपीएफओ के खातों में कोई सरकारी फंड नहीं है, इसलिए नियोक्ता या नए भर्ती हुए कर्मचारी को मिलने वाले पैसे की प्रतिपूर्ति पर संदेह है। चूंकि ईपीएफओ कोई एजेंसी नहीं है जिसकी जिम्मेदारी नौकरियां पैदा करना है, इसलिए इस योजना को लागू करने के लिए एक अलग एजेंसी बनाने की मांग की जा रही है।
Value Addition: ईपीएफओ
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी निकाय है ।
- यह भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति बचत योजना, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का प्रबंधन करता है।
- कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने वेतन का एक हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा करते हैं।
- ईपीएफओ इस धन का सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करता है तथा पेंशन और बीमा लाभ के साथ रिटर्न भी प्रदान करता है।
- यह मुख्य रूप से श्रमिकों की बचत के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, न कि रोजगार सृजन या कल्याण वितरण एजेंसी के रूप में।
निष्कर्ष
निष्कर्ष में, रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाओं की शुरूआत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए सरकार के रणनीतिक दृष्टिकोण को उजागर करती है। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके, इन योजनाओं का उद्देश्य अधिक समावेशी और गतिशील रोज़गार बाजार सृजित करना है। ईएलआई पहल न केवल कार्यबल विस्तार और औपचारिकता का समर्थन करती है, बल्कि नियोक्ताओं, विशेष रूप से एसएमई को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत भी प्रदान करती है, जिससे उनके लिए विकास और काम पर रखना आसान हो जाता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ई.एल.आई.) योजना की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों पर चर्चा करें। इसके कार्यान्वयन के संबंध में प्रमुख चिंताएँ क्या हैं? (250 शब्द, 15 अंक)