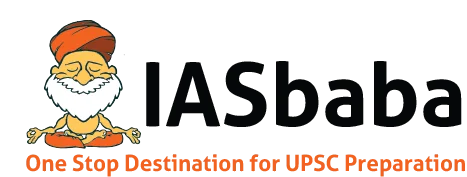IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: कृषि
प्रसंग: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिशुद्ध कृषि (precision farming) को सक्षम बनाकर, उपज अनुमान में सुधार करके, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करके और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके कृषि में क्रांति ला रही है।
प्रमुख अनुप्रयोग:
- परिशुद्ध कृषि: उपग्रह चित्रण और सुदूर संवेदन से फसल के स्वास्थ्य, मृदा नमी और पोषक तत्वों की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर पैदावार और कम अपव्यय के लिए लक्षित सिंचाई और उर्वरक का उपयोग संभव हो पाता है।
- मौसम और जलवायु निगरानी: अंतरिक्ष-आधारित डेटा मौसम पूर्वानुमान में सुधार करता है और किसानों को कृषि गतिविधियों की योजना बनाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करता है।
- संसाधन प्रबंधन: उपग्रह जल संसाधनों के प्रबंधन, सूखे की निगरानी, मिट्टी का मानचित्रण, तथा भूमि क्षरण और वनों की कटाई को रोकने में सहायता करते हैं।
- उपज अनुमान एवं बीमा: फसल और किसान जैसे कार्यक्रम सटीक उपज पूर्वानुमान, बीमा योजनाओं और आपदा नियोजन में सहायता के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हैं।
- कीट एवं रोग का पता लगाना: हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा कीट संक्रमण या रोग के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगा सकते हैं, जिससे फसल की हानि और अत्यधिक रासायनिक उपयोग को कम किया जा सकता है।
- पशुधन और भूमि निगरानी: उपग्रह एकीकरण सतत चराई, पशु ट्रैकिंग और भूमि उपयोग योजना का समर्थन करता है।
- अनुसंधान एवं फसल सुधार: अंतरिक्ष आधारित पौध प्रयोग, पौध जीव विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाते हैं तथा लचीली, उच्च उपज वाली फसल किस्मों को विकसित करने में सहायता करते हैं।
- डिजिटल निर्णय समर्थन: कृषि-डीएसएस जैसे प्लेटफॉर्म भू-स्थानिक डेटा और एआई को जोड़ते हैं ताकि वास्तविक समय में किसानों और नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन किया जा सके।
- खाद्य सुरक्षा एवं सततता: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वैश्विक कृषि प्रवृत्तियों पर नज़र रखने, कमी का पूर्वानुमान लगाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में मदद करती है।
भारत की पहल:
अंतरिक्ष आधारित कृषि सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए FASAL, CHAMAN, NADAMS और महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया है।
Learning Corner:
FASAL (अंतरिक्ष, कृषि – मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान)
- लॉन्च किया गया: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा
- कार्यान्वयनकर्ता: महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी)
- उद्देश्य: रिमोट सेंसिंग, मौसम डेटा और क्षेत्र अवलोकन का उपयोग करके प्रमुख फसलों के लिए फसल-पूर्व उत्पादन पूर्वानुमान।
- महत्व: खाद्यान्न खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और कृषि नीति निर्णयों की सटीक योजना बनाने में मदद करता है।
CHAMAN (भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन)
- लॉन्च किया गया: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा
- कार्यान्वयनकर्ता: एमएनसीएफसी द्वारा इसरो और राज्य बागवानी विभागों के सहयोग से
- उद्देश्य: उपग्रह डेटा और जीआईएस उपकरणों का उपयोग करके बागवानी फसलों का मानचित्रण और मूल्यांकन करना।
- महत्व: यह क्षेत्र आकलन, फसल की स्थिति की निगरानी, तथा फलों और सब्जियों के लिए योजना बनाने में सहायता करता है, तथा बागवानी क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन में सहायता करता है।
NADAMS (राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली)
- विकसितकर्ता: इसरो और कृषि विभाग
- उद्देश्य: वनस्पति सूचकांक, वर्षा और मृदा नमी जैसे उपग्रह-आधारित संकेतकों का उपयोग करके सूखे की वास्तविक समय निगरानी और आकलन करना।
- महत्व: सूखे की घोषणा, आकस्मिक योजना और राहत संसाधनों के समय पर आवंटन में सहायता करता है।
कृषि में प्रौद्योगिकी (एग्री-टेक)
प्रौद्योगिकी ने उत्पादकता, स्थायित्व और लाभप्रदता को बढ़ाकर कृषि में क्रांति ला दी है। यह संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला में – बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक – एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
रिमोट सेंसिंग और जीआईएस
- फसल निगरानी, भूमि उपयोग मानचित्रण और सटीक खेती के लिए उपयोग किया जाता है।
- फसल और चमन जैसे कार्यक्रम वास्तविक समय आकलन के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करते हैं।
परिशुद्ध कृषि
- इसमें जीपीएस, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके साइट-विशिष्ट फसल प्रबंधन शामिल है।
- उर्वरकों, कीटनाशकों और पानी जैसे इनपुट के अनुकूलित उपयोग में मदद करता है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्मार्ट सेंसर
- IoT उपकरण मिट्टी की नमी, तापमान, आर्द्रता और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं।
- वास्तविक समय पर निर्णय लेने और स्वचालित सिंचाई प्रणालियों को सक्षम बनाता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग
- एआई मॉडल मौसम, कीट प्रकोप, उपज अनुमान और बाजार के रुझान की भविष्यवाणी करते हैं।
- किसान सुविधा और एग्रीस्टैक पहल जैसे कृषि -सलाहकार ऐप्स में उपयोग किया जाता है।
ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी)
- हवाई छिड़काव, फसल निगरानी और क्षति आकलन के लिए नियोजित।
- बड़े खेतों में मानव श्रम कम होता है और दक्षता बढ़ती है।
जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग
- उच्च उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल फसल किस्मों का विकास।
- CRISPR जीन संपादन और GM फसलें जैसी प्रौद्योगिकियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
- ई-नाम, पीएम-किसान, एग्रीमार्केट जैसे ऐप बाजार संपर्क, सब्सिडी और मूल्य निर्धारण में मदद करते हैं।
- किसानों को मौसम संबंधी चेतावनियाँ, फसल संबंधी सलाह और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है।
रोबोटिक्स और ऑटोमेशन
- उच्च मूल्य वाली फसलों की कटाई, निराई और पैकेजिंग के लिए रोबोट का उपयोग किया जाता है।
- श्रम निर्भरता कम हो जाती है और एक समान संचालन सुनिश्चित होता है।
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: अर्थशास्त्र
संदर्भ: भास्कर/ BHASKAR (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री) प्लेटफॉर्म एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में सहयोग और नवाचार को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रमुख विशेषताऐं:
- केंद्रीकृत नेटवर्किंग: स्टार्टअप्स, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं को एक ही मंच पर जोड़ता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में निर्बाध सहयोग संभव होता है।
- व्यक्तिगत भास्कर आईडी: उपयोगकर्ताओं को सत्यापित, पूर्ण प्रोफाइल से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होती है – जिससे विश्वसनीयता, खोज योग्यता और सुरक्षित संपर्क में वृद्धि होती है।
- बहु-हितधारक पहुंच: उद्यमियों, निवेशकों, सलाहकारों और सहायक संगठनों सहित विविध भूमिकाओं के लिए खुला, जिससे समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
- उन्नत खोज क्षमता: उन्नत खोज उपकरण उपयोगकर्ताओं को साझेदारों, वित्तपोषण अवसरों, कार्यक्रमों और योजनाओं को शीघ्रता और कुशलता से खोजने में मदद करते हैं।
- संसाधन हब: स्टार्टअप से संबंधित संसाधनों, घटनाओं और ज्ञान-साझाकरण उपकरणों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे सिस्टम विखंडन समाप्त हो जाता है।
- डिजिटल और ऑन-ग्राउंड सहभागिता: संबंध बनाने और बाजार में उपस्थिति बनाने के लिए ऑनलाइन सहयोग और भौतिक आयोजनों दोनों की सुविधा प्रदान करता है।
- बड़े पैमाने पर पहुंच: अगस्त 2025 तक लगभग 200,000 स्टार्टअप पंजीकृत होने के साथ, भास्कर देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप रजिस्ट्री में से एक है।
निष्कर्ष:
भास्कर भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और स्केलेबल डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करता है, जो नवाचार, कनेक्टिविटी और विकास को गति देता है।
Learning Corner:
भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की पहल
भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। नवाचार, रोज़गार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार और संबंधित निकायों ने कई पहल शुरू की हैं:
स्टार्टअप इंडिया पहल (2016)
- लॉन्च किया गया: भारत सरकार द्वारा
- उद्देश्य: उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और वित्तपोषण सहायता प्रदान करना।
- प्रमुख विशेषताऐं:
- 3 वर्षों के लिए कर छूट
- अनुपालन के लिए स्व-प्रमाणन
- ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS)
- एकल-खिड़की समर्थन के लिए स्टार्टअप इंडिया हब
अटल नवाचार मिशन (एआईएम)
- नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया
- अवयव:
- अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल): स्कूली छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी): बुनियादी ढांचे और मार्गदर्शन के साथ प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना
- ARISE: एमएसएमई और सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देना
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन (SIP-EIT)
- अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (2021)
- उद्देश्य: अवधारणा के प्रमाण और उत्पाद विकास के लिए प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को 20 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग (अनुदान और परिवर्तनीय डिबेंचर) प्रदान करना।
स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS)
- सिडबी द्वारा प्रबंधित यह फंड सेबी-पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंडों में निवेश करता है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।
राज्य स्तरीय स्टार्टअप नीतियां
- कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में समर्पित नवाचार केन्द्रों और इनक्यूबेटरों के साथ स्टार्टअप नीतियां हैं।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार
- सामाजिक प्रभाव, ग्रामीण विकास और स्थिरता में योगदान देने वाले स्टार्टअप को मान्यता देना।
डिजिटल प्लेटफॉर्म
- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल: पंजीकरण, शिक्षण कार्यक्रम और नेटवर्किंग के लिए
- GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस): सार्वजनिक खरीद के लिए स्टार्टअप्स को बाजार तक पहुंच प्रदान करता है
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: राजनीति
संदर्भ: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 के बीच प्रमाणित फिल्मों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने मुख्यधारा और क्षेत्रीय फिल्मों में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता का जश्न मनाया।
प्रमुख पुरस्कार:
- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म : 12वीं फेल
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : शाहरुख खान ( जवान ) और विक्रांत मैसी ( 12वीं फेल )
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री : रानी मुखर्जी ( मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे )
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक : सुदीप्तो सेन ( द केरल स्टोरी )
- सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म : कटहल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री
- संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म : रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
- राष्ट्रीय/सामाजिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म : सैम बहादुर
अन्य उल्लेखनीय तथ्य:
- सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म : फ्लावरिंग मैन
- सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र (Documentary) : गॉड वल्चर एंड ह्यूमन
- सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार : सुकृति वेणी बंदरेड्डी , कबीर खानदाने, त्रिश ठोसर
- सर्वश्रेष्ठ पटकथा : बेबी , पार्किंग
- सर्वश्रेष्ठ पुरुष/महिला पार्श्वगायक : पीवीएम स्रोत ( प्रेमिस्टुन्ना ), शिल्पा राव ( छलिया )
- सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी : वैभवी मर्चेंट ( ढिंढोरा बाजे )
- सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन : हनुमान (तेलुगु)
- सर्वश्रेष्ठ संपादन (Editing): पूक्कालम
सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फ़िल्में:
| भाषा | पतली परत |
|---|---|
| असमिया | रोंगाटापु 1982 |
| बंगाली | डीप फ्रिज |
| कन्नड | कंदीलु – आशा की किरण |
| मलयालम | उल्लोझुक्कु |
| मराठी | श्यामची आई |
| ओडिया | पुष्कर |
| पंजाबी | गॉडडे गॉडडे चा |
| तामिल | पार्किंग |
| तेलुगू | भगवंत केसरी |
| गुजराती | वाश |
मुख्य अंश:
- शाहरुख खान ने सिनेमा में 33 साल बाद अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।
- पुरस्कार निर्णायक मंडल की अध्यक्षता फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने की।
- यह मान्यता कलात्मक, तकनीकी और सामाजिक श्रेणियों में फैली हुई थी, जो भारतीय सिनेमा में विविधता को दर्शाती है।
Learning Corner:
भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का इतिहास
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्थापित इन पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्य वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
प्रमुख उपलब्धियां:
- 1954: पहले राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रदान किए गए; शुरुआत में इन्हें “राज्य फ़िल्म पुरस्कार” के नाम से जाना जाता था। केवल कुछ ही श्रेणियाँ थीं, और ” श्यामची आई ” (मराठी) अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक की पहली विजेता थी।
- 1967: पुरस्कारों का नाम बदलकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कर दिया गया और क्षेत्रीय फिल्मों को आधिकारिक तौर पर प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में शामिल किया गया।
- 1973: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) की स्थापना की गई।
- समय के साथ, पुरस्कारों का विस्तार हुआ और इसमें फीचर फिल्मों, गैर-फीचर फिल्मों और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणियां भी शामिल की गईं, जिससे भारत के विविध भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य में सिनेमा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिला।
- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किये जाते हैं और भारतीय फिल्म सम्मानों में इन्हें सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है ।
वर्तमान संरचना:
- तीन वर्गों में विभाजित: फीचर फिल्में, गैर-फीचर फिल्में और सिनेमा पर लेखन।
- इसमें नकद पुरस्कार के साथ स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस) और रजत कमल (रजत कमल) ट्रॉफी शामिल हैं।
- इसमें पिछले कैलेंडर वर्ष में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित फिल्मों का चयन किया जाता है।
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: संस्कृति
प्रसंग: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को “फर्जी आर्य समाज समितियों” के उदय की जांच करने का निर्देश दिया है।
प्रमुख बिंदु:
- आर्य समाज विवाह: सुधारवादी हिंदू मूल्यों पर आधारित, ये विवाह शीघ्र संपन्न होते हैं, कागजी कार्रवाई आसान होती है और अंतर्धार्मिक या भागकर शादी करने वाले जोड़ों के बीच लोकप्रिय हैं। 1875 में स्थापित, आर्य समाज ” शुद्धि ” या हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण को बढ़ावा देता है।
- कानूनी ढाँचा: आर्य विवाह मान्यता अधिनियम, 1937, विभिन्न जातियों और उपजातियों में भी ऐसे विवाहों को संरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, यह राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानूनों या विवाह पंजीकरण नियमों के तहत प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं करता है।
- चिंताएं जो व्यक्त की गईं: न्यायालयों और सरकारों ने ऐसे मामलों को चिन्हित किया है जहां आर्य समाज विवाहों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया:
- विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत जांच से बचना, जिसके तहत 30 दिन की सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है।
- धर्मांतरण विरोधी कानूनों को दरकिनार करना, विशेषकर तब जब धर्मांतरण की रस्में अधूरी हों या जल्दबाजी में की गई हों।
- नाबालिगों से या वैध सहमति के बिना विवाह करना, विशेष रूप से अंतर्धार्मिक मामलों में।
- उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021: धर्मांतरण से पूर्व और बाद की घोषणाओं, स्वैच्छिकता के सत्यापन की आवश्यकता है, और बलपूर्वक या कपटपूर्ण धर्मांतरण पर दंड का प्रावधान है।
- न्यायालय की टिप्पणियां: न्यायपालिका ने आर्य समाज मंदिरों द्वारा बिना उचित दस्तावेज के, विशेषकर अंतरधार्मिक विवाहों में, फर्जी विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर किया।
Learning Corner:
आर्य समाज
आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई (अब मुंबई) में की थी। इसका उद्देश्य वैदिक जीवन पद्धति को पुनर्जीवित करना, अंधविश्वासों, जातिगत भेदभाव और मूर्तिपूजा का खंडन करना और तर्कवाद, समानता और शिक्षा को बढ़ावा देना था।
मुख्य उद्देश्य:
- वेदों की ओर वापसी: ज्ञान के सच्चे स्रोत के रूप में चार वेदों की प्रामाणिकता पर जोर दिया गया।
- रूढ़िवादिता का विरोध: अनुष्ठान, पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया।
- सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना:
- महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह
- बाल विवाह और अस्पृश्यता का उन्मूलन
- राष्ट्रीय जागरण: आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित किया गया।
- शुद्धि आंदोलन: गैर-हिंदुओं का पुनः हिंदू धर्म में धर्मांतरण।
प्रमुख योगदान:
- वैदिक मूल्यों को पश्चिमी शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए दयानंद एंग्लो-वैदिक (डीएवी) स्कूल और कॉलेज स्थापित किए।
- देवनागरी लिपि में हिंदी को एकीकृत राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।
- लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को प्रभावित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई।
स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रसंग: इसरो अपने LVM3 (GSLV Mk III) प्रक्षेपण यान का उपयोग करके अमेरिकी-आधारित AST स्पेसमोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है।
मुख्य तथ्य:
- उद्देश्य: स्थलीय नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में भी स्मार्टफोन पर सीधे मोबाइल वॉयस और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना।
- प्रौद्योगिकी: दूरदराज के क्षेत्रों सहित लगभग सम्पूर्ण भौगोलिक कवरेज प्रदान करने के लिए एक बड़े एंटीना (लगभग 64 वर्ग मीटर) से सुसज्जित।
- प्रभाव: वैश्विक संपर्क को बढ़ाता है, विशेष रूप से आपदा प्रतिक्रिया, दूरस्थ शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए उपयोगी।
- सामरिक मूल्य: भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करता है और इसरो को वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित करता है।
यह मिशन वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाओं में भारत के बढ़ते प्रभाव और गहन होते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है।
Learning Corner:
जीसैट श्रृंखला (भूस्थिर उपग्रह)
भारत की जीसैट (भू-स्थिर उपग्रह) श्रृंखला अंतरिक्ष से भारतीय संचार की रीढ़ है, जिसे इसरो द्वारा दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट सेवाओं, सुरक्षित संचार और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए विकसित किया गया है।
हालिया जीसैट मिशन:
- जीसैट-24 (प्रक्षेपण: जून 2022 एरियनस्पेस द्वारा):
- पूर्णतः वाणिज्यिक उपग्रह, टाटा प्ले द्वारा पट्टे पर लिया गया।
- 24 केयू-बैंड ट्रांसपोंडर के साथ डीटीएच सेवाएं प्रदान करता है।
- जीसैट-20 (जीसैट-एन1) – आगामी :
- इसमें हाई थ्रूपुट सैटेलाइट (एचटीएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
- Ka-बैंड उपग्रह अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड कवरेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- एरियनस्पेस या एलवीएम3 के माध्यम से प्रक्षेपण अपेक्षित है ।
- जीसैट-19 और जीसैट-29 :
- ये उच्च क्षमता वाले उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करते थे।
- आयन प्रणोदन और ऑप्टिकल संचार प्रयोगों जैसे उन्नत पेलोड ले जाया गया।
सीएमएस (संचार उपग्रह) श्रृंखला
- सीएमएस-01 (प्रक्षेपण: दिसंबर 2020 पीएसएलवी-सी50 के माध्यम से):
- जीसैट-12 का स्थान लिया।
- टेली-शिक्षा, टेलीमेडिसिन और आपदा चेतावनी के लिए विस्तारित सी-बैंड सेवाएं प्रदान करता है।
स्रोत: द हिंदू
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
भारत में सरकारी स्कूल अनेक छात्र-हितैषी लाभ जैसे: निःशुल्क शिक्षा, योग्य और बेहतर वेतन वाले शिक्षक, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म, तथा कम या शून्य शुल्क प्रदान करते हैं।
इसके बावजूद भारत के सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट देखी जा रही है, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
इसका उत्तर धारणा, नीतिगत अंतराल, संरचनात्मक असमानताओं और सबसे महत्वपूर्ण, एक प्रवेश परीक्षा प्रणाली के जटिल संयोजन में निहित है, जो अनजाने में निजी संस्थानों और शहरी छात्रों को लाभ पहुंचाती है, जबकि ग्रामीण, सरकारी स्कूल के छात्रों को नुकसान में छोड़ देती है।
आइये इस विवरण का विश्लेषण करें।
नामांकन में गिरावट के पीछे मुख्य मुद्दे
धारणा अंतराल (Perception Gap)
- सरकारी स्कूलों को अक्सर पुराना, खराब प्रबंधन वाला तथा वंचितों के लिए बना माना जाता है, भले ही उनकी वास्तविक क्षमता कुछ भी हो।
- जबकि, निजी स्कूलों में अक्सर बुनियादी ढांचे या योग्य कर्मचारियों की कमी के बावजूद, उन्हें आधुनिक और आकांक्षी के रूप में प्रचारित किया जाता है।
शिक्षण माध्यम विभाजन (Medium of Instruction Divide)
- एनईपी कक्षा 5 तक मातृभाषा आधारित शिक्षा की सिफारिश करता है, जिसके बाद प्रारंभिक वर्षों में बेहतर समझ और वैचारिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए क्रमिक परिवर्तन किया जाता है।
- सरकारी स्कूल आमतौर पर इस नीति का पालन करते हैं। हालाँकि, कई निजी स्कूल कक्षा 1 से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का विज्ञापन देते हैं, जो अक्सर बिना योग्य अंग्रेजी शिक्षकों के होता है।
- इसलिए विज्ञापन और साथियों के दबाव में माता-पिता अपने बच्चों के लिए प्रारंभिक भाषा लाभ के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं
- सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में एनईपी के समान क्रियान्वयन के बिना, यह विभाजन और अधिक बढ़ जाएगा।
प्रवेश परीक्षा पूर्वाग्रह (Entrance Exam Bias)
- प्रमुख परीक्षाएँ (आईआईटी-जेईई, नीट, आदि) केवल STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) विषयों पर केंद्रित होती हैं। भाषा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और नैतिकता जैसे विषयों की उपेक्षा की जाती है, जिससे समग्र शिक्षा का मूल्य कम हो जाता है।
- निजी स्कूल प्रायः प्रारंभिक कोचिंग कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे उनके छात्रों को अनुचित लाभ मिलता है।
- सरकारी स्कूलों के छात्र, जो व्यापक और संतुलित पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, नुकसान में रहते हैं। यह व्यवस्था चुनिंदा शिक्षा को पुरस्कृत करती है और समग्र शिक्षा को दंडित करती है।
आवश्यक कदम
प्रवेश परीक्षाओं में सुधार
- प्रवेश परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए ताकि भाषा, मानविकी, नैतिकता और तर्क सहित सभी प्रमुख स्कूल विषयों की परीक्षा ली जा सके।
- इससे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेंगे, न कि केवल STEM विषयों में प्रशिक्षित विद्यार्थियों को।
एनईपी को समान रूप से लागू करें
- सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के नियमों को लागू करें।
- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल उचित भाषा नीतियों और संतुलित पाठ्यक्रम का पालन करें।
निजी स्कूलों द्वारा भ्रामक ब्रांडिंग को विनियमित करें
- निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली भ्रामक ब्रांडिंग – जैसे कक्षा 1 से आईआईटी और एनईईटी प्रशिक्षण – को बाल शिक्षा की अखंडता की रक्षा के लिए विनियमित किया जाना चाहिए।
सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार
- बदलते समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए सार्वजनिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाना चाहिए।
- स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से शिक्षक सहायता, डिजिटल उपकरण और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया जाना चाहिए।
- जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए सरकारी स्कूलों की सफलता की कहानियों का विज्ञापन किया जाना चाहिए।
सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करें
- अभिभावकों और स्थानीय हितधारकों को शामिल करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को सशक्त बनाना।
- स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और स्वामित्व में सुधार करें।
निष्कर्ष
शैक्षिक समानता और राष्ट्रीय विकास के लिए सरकारी स्कूल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निजी स्कूलों के प्रति वर्तमान रुझान वास्तविक प्रदर्शन का परिणाम कम और व्यवस्थागत पूर्वाग्रहों और धारणा संबंधी समस्याओं का परिणाम ज़्यादा है। प्रवेश नीतियों, परीक्षा प्रणालियों और पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में बदलाव ज़रूरी है ताकि सरकारी स्कूलों को “अंतिम विकल्प” के बजाय “पहली पसंद” बनाया जा सके ।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
कल्याणकारी उपायों और सुदृढ़ शैक्षणिक ढाँचों के बावजूद, भारत में सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट जारी है। इस प्रवृत्ति के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सरकारी स्कूली शिक्षा में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: सरकारी स्कूलों में नामांकन क्यों घट रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है – द हिंदू
परिचय (संदर्भ)
जुलाई 2024 में बिहार के पूर्णिया में जादू-टोना के आरोप में तीन महिलाओं सहित परिवार के पांच सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2000 से अब तक 2,500 से ज़्यादा महिलाओं को डायन/ भूत बताकर उनकी हत्या कर दी गई है। यह संख्या और भी ज़्यादा होने का अनुमान है, क्योंकि कई मामले तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते।
ये घटनाएं अंधविश्वास, पितृसत्ता और जातिवाद में निहित हिंसा के परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाती हैं।
विच हंटिंग /डायन शिकार क्या है?
विच हंटिंग से तात्पर्य किसी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं पर जादू-टोना करने का आरोप लगाने की प्रथा से है।
जादू-टोना करने के आरोप में महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ-साथ फाँसी तक की सज़ा दी जाती है। डायन के आरोप में सज़ा देने के लिए आमतौर पर गंभीर हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है , जिसमें बलात्कार, मारपीट, कोड़े मारना और अंग-भंग करना शामिल हो सकता है।
डेटा
- राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 2015 और 2021 के दौरान कथित तौर पर जादू-टोना करने के आरोप में 663 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार , झारखंड राज्य में जादू-टोना के कारण हत्याओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, जहां 2001 से 2021 के बीच जादू-टोना के आधार पर 593 महिलाओं की हत्या की गई।
- असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में भी डायन बताकर दागने के कई मामले दर्ज किए गए हैं।
डायन-शिकार/ विच हंटिंग अभी भी क्यों जारी है?
- अंधविश्वास – लोगों का मानना है कि चुड़ैलों के पास जादुई शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग वे मनुष्यों पर हमला करने, फसलों को नष्ट करने, जानवरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों के शरीर और दिमाग को प्रभावित करने या चिकित्सा स्पष्टीकरण से परे तरीकों से नियंत्रण पाने के लिए करती हैं।
- ज्ञान का अभाव – दूरदराज, एकांत क्षेत्रों में, जहां सीमित या कोई शैक्षिक सुविधाएं नहीं हैं, या वृद्ध निरक्षर लोगों के बीच, अक्सर महिलाओं को बुरी घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि अन्य लोग इसका कारण नहीं बता पाते।
- संसाधनों की कमी और गरीबी – महिलाओं को गरीबी, यौन संबंध बनाने से इनकार करने और अन्य कमजोरियों के कारण निशाना बनाया जाता है।
- अन्य कारणों में रूढ़िवादी समाज, पितृसत्ता, वित्तीय विवाद, व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष, ईर्ष्या, संपत्ति विवाद, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और अज्ञानता शामिल हैं।
परेशान करने वाले रुझान
- जादू-टोने के आरोप व्यवस्थित रूप से विधवा, बुजुर्ग या अकेली महिलाओं पर लगाए जाते हैं, जिन्हें पुरुषों के उत्तराधिकार या भूमि स्वामित्व में बाधा के रूप में देखा जाता है।
- डायन-ब्रांडिंग पितृसत्तात्मक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- जिन इलाकों में गरीबी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य सुविधाएँ व्याप्त हैं, वहाँ जादू-टोने के आरोप आम हैं। ऐसे मामलों में पशुओं की अकारण मृत्यु, बीमारी या प्राकृतिक घटनाओं को उचित ठहराने के लिए अलौकिक प्रभावों का इस्तेमाल किया जाता है।
- आरोप प्रायः भूमि विवाद, जाति संघर्ष या सामुदायिक तनाव से उत्पन्न होते हैं , विशेष रूप से सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने की चाह रखने वाले प्रमुख जाति के पुरुषों से संबंधित।
डायन शिकार से संबंधित कानून
- आईपीसी की धाराएं 302 (हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) लगाई जाती हैं।
- असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ , बिहार, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने विच हंटिंग विरोधी कानून बनाए हैं। ये कानून विच हंटिंग के अपराधियों को कड़ी सज़ा का प्रावधान करते हैं, लेकिन ये राज्य-स्तरीय कानून विच हंटिंग जैसे जघन्य कृत्य को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- विच हंटिंग और संबंधित अंधविश्वासों के कारण ऐसे अपराध होते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 (3) और 21 जैसे मौलिक अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिन पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है, जैसे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979 और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जुलाई 2021 में “जादू टोना और अनुष्ठान हमलों (एचपीएडब्ल्यूआर) के आरोपों से संबंधित हानिकारक प्रथाओं का उन्मूलन” शीर्षक से प्रस्ताव को अपनाया। इसमें जादू टोना के आरोपों से संबंधित हानिकारक प्रथाओं के अपराधीकरण , जागरूकता अभियान और सामुदायिक संवेदीकरण और गरीबी, अंधविश्वास, निरक्षरता और लैंगिक असमानता जैसे मूल कारणों से निपटने का आह्वान किया गया है।
केंद्रीय कानून की आवश्यकता
- वर्तमान कानून दंडात्मक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते।
- इसे लिंग आधारित हिंसा के बजाय “स्थानीय सांस्कृतिक मामलों” के रूप में देखा जाता है ।
- कम दोषसिद्धि दर , पीड़ितों का खराब पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता चुनौतियां बनी हुई हैं।
- रिपोर्ट करने के तरीके सीमित हैं, और पीड़ित अक्सर डर या स्वीकार्यता के कारण विच हंटिंग की रिपोर्ट करने से बचते हैं।
- विच हंटिंग रोकथाम विधेयक 2016 में पेश किया गया था, लेकिन कभी पारित नहीं हो सका।
भारत सरकार को विच हंटिंग की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सार्वभौमिक कानून बनाना चाहिए, जो समय की मांग है और महिलाओं के शोषण को खत्म करने के लिए चिंता का विषय होने के नाते इस तरह के कृत्यों से शीघ्रता से निपटने के लिए संगठन स्थापित करने चाहिए।
अन्य आवश्यक कदम
- विच हंटिंग कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना।
- ऐसे मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतें और अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण।
- वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में।
- भय-आधारित विश्वास प्रणालियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य साक्षरता की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासकों को प्रशिक्षित करना।
- अंधविश्वास का मुकाबला करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी), पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना।
- बचे हुए लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता, तथा आर्थिक पुनर्वास योजनाएं बनाना।
- कलंक को समाप्त करने के लिए साक्ष्यों और उत्तरजीवियों के नेतृत्व वाले अभियानों को प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष
भारत में विच हंटिंग केवल अंधविश्वास का अवशेष नहीं है, बल्कि जड़ जमाए पितृसत्ता, जातिगत उत्पीड़न और व्यवस्थागत उपेक्षा की हिंसक अभिव्यक्ति है। ऐसी हिंसा को बनाए रखने वाली सामाजिक वैधता को खत्म करने के लिए कानूनी सुधार, सामुदायिक संवेदनशीलता और संरचनात्मक सशक्तिकरण को साथ-साथ चलना होगा। केवल एक अंतर्विषयक और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से ही भारत सभी के लिए सम्मान, समानता और न्याय के अपने संवैधानिक वादे को कायम रख सकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
भारत में विच हंटिंग अंधविश्वास, लिंग-आधारित हिंसा, जातिगत भेदभाव और राज्य की विफलता के अंतर्संबंध को दर्शाती है। इस प्रथा को बनाए रखने वाले संरचनात्मक कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसे समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)