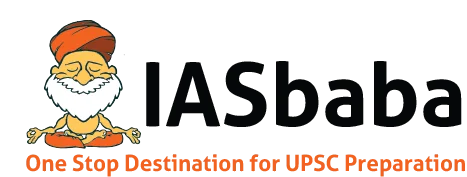IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: राजनीति
प्रसंग: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख विशेषताऐं
- तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन को उन्नत करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, एनईपी 2020 के अनुरूप।
- वित्तपोषण: विश्व बैंक से 2,100 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार से 2,100 करोड़ रुपये का ऋण।
- कवरेज: 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थान, जिनमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं।
- लाभार्थी: लगभग 7.5 लाख छात्र बेहतर बुनियादी ढांचे, डिजिटल पहुंच और कौशल विकास से लाभान्वित होंगे।
उद्देश्य और लाभ
- गुणवत्ता संवर्धन: शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासन और उद्योग प्रासंगिकता में सुधार।
- समानता एवं समावेशन: महिला संकाय, विविध छात्र समूहों और क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना।
- अनुसंधान एवं नवाचार: संस्थागत स्वायत्तता, नवाचार संस्कृति और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- कौशल एवं रोजगार योग्यता: पाठ्यक्रम सुधार, इंटर्नशिप और मिश्रित शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शासन सहायता: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा विभागों के लिए क्षमता निर्माण।
- डिजिटल परिवर्तन: डिजिटल उपकरणों और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों के उपयोग का विस्तार करना।
कार्यान्वयन
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, AICTE, NBA, IITs और IIMs के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा प्रशासित।
Learning Corner:
उच्च शिक्षा पर योजनाएँ – भारत
| योजना / पहल | मंत्रालय / निकाय | उद्देश्य | प्रमुख विशेषताऐं |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) | शिक्षा मंत्रालय | राज्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, पहुंच और समानता में सुधार | बुनियादी ढांचे, संकाय विकास, मान्यता और नवाचार के लिए वित्त पोषण। केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। |
| प्रतिष्ठित संस्थान (Institutions of Eminence- IoE) | शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी | विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों का विकास करना | 10 सार्वजनिक (वित्तपोषित) और 10 निजी (वित्तपोषित नहीं) संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी गई। |
| राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) | शिक्षा मंत्रालय | प्रदर्शन के आधार पर संस्थानों को रैंक करना | शिक्षण, अनुसंधान, आउटरीच जैसे मापदंडों पर आधारित वार्षिक रैंकिंग। |
| अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव (IMPRINT) | शिक्षा मंत्रालय एवं डीएसटी | इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान | उच्चतर संस्थानों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं। |
| शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (GIAN) | शिक्षा मंत्रालय | भारतीय संस्थानों में पढ़ाने के लिए विदेशी संकाय लाना | लघु अवधि पाठ्यक्रम, ज्ञान का आदान-प्रदान। |
| शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC) | शिक्षा मंत्रालय | अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग | शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी। |
| उन्नत भारत अभियान | शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी | उच्च शिक्षा को ग्रामीण विकास से जोड़ना | संकाय एवं छात्र स्थानीय चुनौतियों पर काम करते हैं। |
| राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) | शिक्षा मंत्रालय | स्नातकों/डिप्लोमा धारकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना | वजीफे के साथ उद्योग से जुड़ी प्रशिक्षुता। |
| पीएम रिसर्च फेलोशिप (PMRF) | शिक्षा मंत्रालय | आईआईटी/आईआईएससी
/एनआईटी में पीएचडी के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करना |
अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए उच्च मूल्य वाली फैलोशिप। |
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: राजनीति
संदर्भ: इंडियाएआई (MeitY) और नेशनल कैंसर ग्रिड (NCG) ने पूरे भारत में कैंसर स्क्रीनिंग, निदान और उपचार में एआई-आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कैंसर एआई और प्रौद्योगिकी चुनौती (CATCH) अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है।
मुख्य अंश
- वित्तपोषण: प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक; सफल अभिकर्ताओं को 1 करोड़ रुपये तक का स्केल-अप अनुदान प्राप्त हो सकता है।
- फोकस क्षेत्र: स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स, नैदानिक निर्णय समर्थन, रोगी संलग्नता, परिचालन दक्षता, अनुसंधान और डेटा क्यूरेशन के लिए एआई समाधान।
- पात्रता: भारत में स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी फर्मों, शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए खुला। संयुक्त नैदानिक-तकनीकी अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित किया गया है।
- तैनाती: सत्यापन, पायलट परीक्षण और राष्ट्रव्यापी विस्तार के लिए एनसीजी के 300+ कैंसर केंद्र नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।
समय
- आरंभ तिथि: 2 अगस्त 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 2 सितंबर 2025
- समीक्षा और मैचमेकिंग: सितंबर-अक्टूबर 2025
- अंतिम अनुमोदन: अक्टूबर-नवंबर 2025
- पहला अनुदान वितरण: फरवरी 2026 से
विशेषताएँ
- मार्गदर्शन, विनियामक मार्गदर्शन और नैदानिक सहायता।
- नैतिक, चिकित्सकीय रूप से मान्य और भारत-विशिष्ट एआई समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना।
- इंडियाएआई के नेटवर्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रभाव ।
Learning Corner:
चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करने, निदान में सहायता करने, रोग की प्रगति की भविष्यवाणी करने, उपचार को वैयक्तिकृत करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करने के लिए एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग (एमएल) और डीप लर्निंग (डीएल) का उपयोग।
प्रमुख अनुप्रयोग और उदाहरण
| आवेदन क्षेत्र | एआई की भूमिका | विशिष्ट उदाहरण |
|---|---|---|
| चिकित्सा इमेजिंग और निदान | एआई एल्गोरिदम एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन में असामान्यताओं का पता मनुष्यों की तुलना में अधिक तेजी से और अक्सर अधिक सटीकता से लगाते हैं। | गूगल का डीपमाइंड – रेटिना स्कैन से नेत्र रोगों का पता लगाता है; आईबीएम वॉटसन हेल्थ – कैंसर निदान सहायता; क्यूरे.एआई – भारत में इमेजिंग से टीबी और स्ट्रोक का पता लगाता है। |
| पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और रोग प्रकोप | बड़े डेटासेट का उपयोग करके रोगी की स्थिति में गिरावट या महामारी के प्रसार की भविष्यवाणी करना। | ब्लूडॉट – डब्ल्यूएचओ की चेतावनी से पहले ही कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी कर दी; आईसीयू में एआई-आधारित सेप्सिस भविष्यवाणी उपकरण। |
| दवा की खोज और विकास | एआई दवा अणु स्क्रीनिंग और नैदानिक परीक्षण डिजाइन को गति प्रदान करता है। | बेनेवोलेंट एआई – दुर्लभ रोगों के लिए पुनःप्रयोजनित औषधियाँ; इंसिलिको मेडिसिन – फाइब्रोसिस के लिए एआई द्वारा डिजाइन की गई औषधियाँ। |
| व्यक्तिगत चिकित्सा | रोगी के आनुवंशिक और जीवनशैली संबंधी आंकड़ों के आधार पर उपचार तैयार करना । | टेम्पस – कैंसर जीनोमिक्स के लिए एआई का उपयोग कर चिकित्सा को वैयक्तिकृत करता है। |
| सर्जिकल सहायता और रोबोटिक्स | एआई-संचालित रोबोट सटीकता में सुधार करते हैं और पुनर्प्राप्ति समय को कम करते हैं। | दा विंची सर्जिकल सिस्टम – एआई मार्गदर्शन के साथ न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी; वर्सियस – भारत में रोबोट-सहायता प्राप्त लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। |
| आभासी स्वास्थ्य सहायक | एआई चैटबॉट और वॉयस असिस्टेंट बुनियादी चिकित्सा सलाह और अनुस्मारक प्रदान करते हैं। | बेबीलोन हेल्थ – लक्षण जांचकर्ता; प्रैक्टो एआई – भारत में अपॉइंटमेंट और टेली-परामर्श। |
| प्रशासनिक स्वचालन | कागजी कार्रवाई, बिलिंग और रोगी रिकॉर्ड पर लगने वाले समय को कम करता है। | एपिक सिस्टम्स जैसे एआई-आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) स्वचालन उपकरण। |
स्रोत: पीआईबी
श्रेणी: पर्यावरण
प्रसंग: 5 अरब स्टारफिश की मौत का रहस्य सुलझाया गया ।
पिछले 12 वर्षों में, उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट पर 5 अरब से ज़्यादा स्टारफ़िश सी स्टार क्षय रोग (SSWD) से मर गईं, जिसमें घाव, अंग-क्षय और शरीर का विघटन शामिल था। सबसे ज़्यादा नुकसान सनफ्लॉवर सी स्टार को हुआ, जिसकी आबादी 90% तक कम हो गई। एक प्रमुख शिकारी होने के नाते, इसके लुप्त होने से समुद्री अर्चिन की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिससे केल्प वन तबाह हो गए।
Discovery Journey
- प्रारंभिक अध्ययनों में एक वायरस (डेंसोवायरस) का संदेह था, लेकिन यह असंबंधित साबित हुआ।
- शोधकर्ताओं ने ऊतक के नमूनों के बजाय स्टारफिश के कोइलोमिक द्रव पर ध्यान केंद्रित किया।
- प्रयोगों से पता चला कि संक्रमित तरल को उबालने से रोग पैदा करने वाला कारक नष्ट हो गया, जो कि एक जीवाणु का संकेत था।
कारक की पहचान
- वर्षों के विश्लेषण के बाद, हकाई इंस्टीट्यूट और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि विब्रियो पेक्टेनिसिडा (स्ट्रेन FHCF-3) इसका कारण है।
- डीएनए अनुक्रमण से बीमार स्टारफिश में इसकी उच्च उपस्थिति का पता चला।
- इसके संपर्क में आने से स्वस्थ स्टारफिश में क्षय रोग विकसित हो गया और वे मर गईं।
इसमें एक दशक क्यों लगा?
- लक्षणों के कई संभावित कारण थे।
- प्रारंभिक अनुसंधान में गलत ऊतकों और रोगजनकों को लक्षित किया गया।
- यह जीवाणु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तथा केवल जीवित नमूनों के तरल पदार्थ में ही इसका पता लगाया जा सकता है।
Learning Corner:
सनफ्लॉवर सी स्टार ( पाइक्नोपोडिया हेलियनथोइड्स )
- विवरण: उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे तेज गति से चलने वाले सी स्टार में से एक, जिसमें सूरजमुखी की पंखुड़ियों जैसी 24 भुजाएँ होती हैं।
- पारिस्थितिक भूमिका: एक प्रमुख शिकारी जो समुद्री अर्चिन की आबादी को नियंत्रित करता है, तथा केल्प वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।
- महत्व: इसका शिकार समुद्री अर्चिन के अतिचारण को नियंत्रित करता है, जो अन्यथा समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण केल्प पर्यावासों को नष्ट कर देता है।
- खतरे: 2013 से सी स्टार वेस्टिंग डिजीज (एसएसडब्ल्यूडी) से गंभीर रूप से प्रभावित, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में 90% से अधिक की गिरावट।
- संरक्षण स्थिति: रोग और पर्यावरणीय तनाव के कारण कई क्षेत्रों में गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है।
- पुनर्प्राप्ति प्रयास: चल रहे अनुसंधान का ध्यान जनसंख्या को पुनर्जीवित करने और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बनाए रखने के लिए रोग शमन, कैप्टिव प्रजनन और पर्यावास बहाली पर केंद्रित है।
स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: पर्यावरण
प्रसंग: सरकार ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत बेड़े-स्तरीय उत्सर्जन मानदंडों (fleet-level emission norms) से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहन निर्माताओं को दंडित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है।
प्रमुख विशेषताऐं
- प्राधिकरण: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई) मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करेगा और उल्लंघनों की रिपोर्ट राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) को देगा।
- दंड:
- 0–4.7 ग्राम/किमी CO₂ से अधिक: बेचे गए प्रत्येक वाहन पर ₹25,000
- 4.7 ग्राम/किमी CO₂ से अधिक: बेचे गए प्रत्येक वाहन पर ₹50,000
- आधार जुर्माना: प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए ₹10 लाख
- निधि: जुर्माने का 90% हिस्सा ऊर्जा संरक्षण निधि के माध्यम से राज्यों को जाएगा।
- विवाद समाधान: राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) जहां वाहन निर्माता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
प्रभावित वाहन निर्माता
वित्त वर्ष 2023 में किआ, हुंडई, रेनॉल्ट और होंडा सहित आठ कार निर्माताओं ने मानकों का उल्लंघन किया और उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और टोयोटा ने स्वच्छ बेड़े के कारण नियमों का पालन किया।
नीति संदर्भ
पहले, कोई स्पष्ट दंड प्रक्रिया मौजूद नहीं थी। जनवरी 2023 से प्रभावी नए नियम, पहले के हल्के जुर्माने की जगह लेंगे। उद्योग जगत हाइब्रिड, इथेनॉल और सीएनजी वाहनों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से मुक्त और व्यापक मान्यता चाहता है।
महत्व
यह ढांचा प्रवर्तन को मजबूत करता है, स्वच्छ वाहन अपनाने में तेजी लाता है, तथा भारत के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है, साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता और परिवर्तन समयसीमा पर बहस को भी बढ़ावा देता है।
Learning Corner:
भारत में ऑटोमोटिव उत्सर्जन रोकने की योजनाएँ
भारत स्टेज उत्सर्जन मानक (बीएस मानदंड)
- भारत के उत्सर्जन मानक यूरोपीय मानदंडों के अनुरूप हैं ।
- वर्तमान में बीएस VI (अप्रैल 2020 से) पर, NOx, PM और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों को काफी कम कर रहा है।
- यह स्वच्छ ईंधन और उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों को अनिवार्य बनाता है।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (FAME)
- सब्सिडी, प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना।
- FAME-II (2019 से) मांग सृजन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और EV विनिर्माण को समर्थन देने पर केंद्रित है।
वाहन स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy)
- पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने तथा उनके स्थान पर स्वच्छ वाहन लाने के लिए प्रोत्साहन देकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने को प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य वाहन प्रदूषण को कम करना और ई.वी. को अपनाने को बढ़ावा देना है।
ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहन निर्माताओं की निगरानी करने और उन्हें दंडित करने का अधिकार दिया गया है।
- प्रति वाहन कार्बन उत्सर्जन की अधिकता के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएनजी और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना
- पेट्रोल/डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सीएनजी वाहनों, जैव ईंधन और अन्य स्वच्छ ईंधनों के लिए प्रोत्साहन।
राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन (एनईएमएम)
- विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने तथा जीवाश्म ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक व्यापक पहल।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: पर्यावरण
प्रसंग: भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) की SIGHT योजना (मोड-2ए) के अंतर्गत हरित अमोनिया के लिए अपनी पहली नीलामी आयोजित की।
- रिकॉर्ड कीमत: ₹55.75/किग्रा (~641 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन) पर मिला, जो पिछले साल की H2Global नीलामी में ₹100.28/किग्रा से काफी कम है। ग्रे अमोनिया की कीमत लगभग 515 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन है।
- स्केल: एसईसीआई पारादीप फॉस्फेट्स, ओडिशा के लिए प्रति वर्ष 75,000 मीट्रिक टन की खरीद करेगा। यह 7.24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के लक्ष्य वाली 13 नीलामियों में से पहली है।
- अनुबंध: उर्वरक, शिपिंग और भारी विनिर्माण जैसे उद्योगों को हरित अमोनिया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 10-वर्षीय निश्चित मूल्य।
- प्रभाव: जीवाश्म आधारित अमोनिया के साथ मूल्य समता को दर्शाता है, प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को कम करता है, उर्वरक सब्सिडी को कम करता है, और जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- ग्रीन अमोनिया: ग्रीन हाइड्रोजन (नवीकरणीय ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस से) को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर उत्पादित किया जाता है, जिससे उर्वरकों, समुद्री ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए कार्बन मुक्त अमोनिया प्राप्त होता है।
Learning Corner:
हरित अमोनिया
परिभाषा: ग्रीन अमोनिया, जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित अमोनिया (NH₃) है। मुख्य अंतर हाइड्रोजन स्रोत में है:
- पारंपरिक (ग्रे) अमोनिया में, हाइड्रोजन को स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (एसएमआर) के माध्यम से प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, जिससे CO₂ उत्सर्जित होता है।
- हरित अमोनिया में, हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय बिजली (सौर, पवन, जल) का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, और फिर इसे हैबर-बॉश प्रक्रिया के माध्यम से हवा से नाइट्रोजन के साथ संयोजित किया जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया:
N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)
- हरित अमोनिया के लिए, H₂ नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त होता है।
ग्रीन अमोनिया क्यों महत्वपूर्ण है?
- जलवायु लक्ष्य:
- अमोनिया उत्पादन वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का लगभग 1-2% है (जीवाश्म-आधारित हाइड्रोजन के कारण)।
- हरित अमोनिया का उत्पादन लगभग कार्बन-मुक्त हो सकता है।
- ऊर्जा संक्रमण:
- शिपिंग और उर्वरक जैसे कठिन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है।
- ऊर्जा भंडारण और परिवहन:
- हाइड्रोजन गैस की तुलना में भंडारण और परिवहन आसान है।
- मध्यम दाब और तापमान पर तरल रूप में भेजा जा सकता है।
हरित अमोनिया के अनुप्रयोग
उर्वरक (प्राथमिक उपयोग – अमोनिया उत्पादन का ~80%)
- सीधे उपयोग किया जाता है या यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है।
- हरित अमोनिया कार्बन-तटस्थ कृषि को सक्षम बनाता है।
- प्राकृतिक गैस आधारित अमोनिया पर भारत की आयात निर्भरता कम हो जाती है।
शिपिंग ईंधन
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने 2050 तक उत्सर्जन में 50% की कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ग्रीन अमोनिया लंबी दूरी के जहाजों के लिए एक आशाजनक शून्य-कार्बन बंकर ईंधन है।
- उदाहरण: MAN एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों द्वारा अमोनिया-ईंधन वाले इंजनों का परीक्षण।
विद्युत उत्पादन
- इसका उपयोग सीधे गैस टर्बाइनों में बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है या उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयले के साथ सह-फायरिंग के लिए किया जा सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा को अमोनिया में परिवर्तित करके पुनः बिजली में परिवर्तित करके मौसमी ऊर्जा भंडारण की संभावना।
हाइड्रोजन वाहक
- उपयोग के स्थान पर अमोनिया को पुनः हाइड्रोजन में परिवर्तित किया जा सकता है।
- उच्च ऊर्जा घनत्व और कम क्रायोजेनिक आवश्यकताओं के कारण तरल हाइड्रोजन की तुलना में परिवहन आसान है।
औद्योगिक रसायन
- प्लास्टिक, विस्फोटक (अमोनियम नाइट्रेट) और अन्य रसायनों के लिए फीडस्टॉक।
- कम कार्बन औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम बनाता है।
उभरते उपयोग
- एक शीतलक के रूप में (निम्न-GWP विकल्प)।
- उच्च तापमान औद्योगिक ताप के लिए ईंधन (इस्पात, सीमेंट)।
उत्पादन मार्ग
- इलेक्ट्रोलिसिस: नवीकरणीय ऊर्जा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है।
- वायु पृथक्करण: वायु से नाइट्रोजन निकाला जाता है।
- हेबर-बॉश प्रक्रिया: हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उच्च तापमान और दाब में लौह-आधारित उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं।
चुनौतियां
- लागत: वर्तमान में ग्रे अमोनिया की तुलना में अधिक महंगी (~ 2-4x), लेकिन तेजी से गिर रही है।
- बुनियादी ढांचा: उर्वरक संयंत्रों और बंकरिंग सुविधाओं के पुनरोद्धार की आवश्यकता है।
- ऊर्जा तीव्रता: हेबर-बॉश प्रक्रिया ऊर्जा-गहन है, यहां तक कि हरित इनपुट के साथ भी।
- सुरक्षा: अमोनिया विषैला होता है और इसे सावधानीपूर्वक संभालना आवश्यक है।
ग्रे, नीला और हरित अमोनिया
| अमोनिया के प्रकार | उत्पाद विधि | फीडस्टॉक | कार्बन उत्सर्जन | कार्बन शमन | अनुमानित लागत (2024) | प्रमुख अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रे अमोनिया | स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (एसएमआर) या कोयला गैसीकरण से हाइड्रोजन का उपयोग करके हैबर-बॉश प्रक्रिया | प्राकृतिक गैस (CH₄) या कोयला | उच्च (≈ 2.6 टन CO₂ प्रति टन अमोनिया) | कोई नहीं | ~USD 450–550/एमटी | उर्वरक (यूरिया, डीएपी), विस्फोटक, रसायन |
| नीला अमोनिया | ग्रे के समान, लेकिन कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के साथ | प्राकृतिक गैस/कोयला | मध्यम (≈ 90% CO₂ कैप्चर) | सीसीयूएस प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग | ~USD 600–750/मीट्रिक टन | कम कार्बन वाले उर्वरक, शिपिंग के लिए ईंधन, हाइड्रोजन वाहक |
| हरित अमोनिया | नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन, वायु पृथक्करण से नाइट्रोजन का उपयोग करने वाली हैबर-बॉश प्रक्रिया | जल (H₂ स्रोत) + वायु (N₂ स्रोत) | शून्य प्रत्यक्ष CO₂ उत्सर्जन | 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है | ~USD 600–900/MT | हरित उर्वरक, स्वच्छ समुद्री ईंधन, हाइड्रोजन भंडारण एवं परिवहन, ऊर्जा निर्यात |
स्रोत: पीआईबी
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने 10+2 प्रणाली की जगह 5+3+3+4 स्कूल संरचना लागू की है, जो शिक्षा के चरणों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के साथ संरेखित करती है। हालाँकि यह मॉडल समग्र परिवर्तन का वादा करता है, लेकिन बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की तैयारी, अभिभावकों की जागरूकता आदि में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
एनईपी 2020 का उद्देश्य
- एनईपी 2020 सभी स्तरों – प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक तक – पर स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है।
- व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर इसे यथाशीघ्र सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
5+3+3+4 संरचना का अवलोकन
5+3+3+4 मॉडल पारंपरिक 10+2 प्रणाली का स्थान लेता है और बच्चों की संज्ञानात्मक और विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक यात्रा को चार चरणों में विभाजित करता है:
- आधारभूत चरण (5 वर्ष) :
-
- आयु वर्ग: 3 से 8 वर्ष
- घटक: इस चरण में 3 वर्ष की प्रीस्कूल (आंगनवाड़ी या नर्सरी) और उसके बाद 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 और 2) शामिल है।
- फोकस: सामाजिक संपर्क, भाषा और बुनियादी संख्यात्मकता जैसे आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए खेल-आधारित और गतिविधि-संचालित शिक्षा पर जोर दिया जाता है।
- प्रारंभिक चरण (3 वर्ष) :
-
- आयु वर्ग: 8 से 11 वर्ष
- घटक: कक्षा 3 से 5 तक
- फोकस: जिज्ञासा और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए खोज-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ पढ़ना, लिखना, विज्ञान और गणित जैसे विषयों का परिचय दिया जाता है।
- मध्य चरण (3 वर्ष):
- आयु वर्ग: 11 से 14 वर्ष
- घटक: कक्षा 6 से 8 तक शामिल हैं।
- फोकस: इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में ज्ञान को गहन करना है, साथ ही विद्यार्थियों को अधिक संरचित वातावरण में अपनी रुचियों का पता लगाने और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- माध्यमिक चरण (4 वर्ष):
-
- आयु वर्ग: 14 से 18 वर्ष
- घटक: कक्षा 9 से 12 तक शामिल हैं।
- फोकस: छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना, उन्हें अपनी रुचि और कैरियर आकांक्षाओं के आधार पर विषय चुनने की अनुमति देना।
यह मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे का मस्तिष्क विकास प्रारंभिक वर्षों में सबसे तेजी से होता है, और इसलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए।
अब जोर रटने की बजाय अनुभवात्मक, बहुविषयक, पूछताछ आधारित शिक्षा के साथ-साथ लचीले विषय विकल्पों और समग्र मूल्यांकन पर है।
एनईपी के 5+3+3+4 मॉडल के कार्यान्वयन में प्रमुख अंतराल
- बुनियादी ढांचे की कमी
- कई निजी शहरी स्कूलों ने खेल-आधारित शिक्षा और सॉफ्ट-स्किल मूल्यांकन जैसी एनईपी पद्धतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
- अधिकांश सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जैसे:
- शौचालय और स्वच्छ पेयजल।
- उचित कक्षा-कक्ष कई आंगनवाड़ियों में एकल कमरे में संचालित होते हैं।
- पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं, जो आधारभूत चरण का प्रारंभिक बिंदु हैं।
- पर्याप्त शिक्षण-अधिगम सामग्री।
- शिक्षक की तैयारी
- एनईपी की सफलता अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर करती है, तथापि, इसमें निम्नलिखित चुनौतियाँ शामिल हैं:
- गतिविधि-आधारित और योग्यता-आधारित शिक्षण का सीमित अनुभव।
- पुराने बी.एड. पाठ्यक्रम अभी भी पुरानी 10+2 प्रणाली के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- नियमित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन का अभाव, विशेषकर ग्रामीण विद्यालयों में।
- केवल एक बार के अभिविन्यास की नहीं, बल्कि निरंतर मार्गदर्शन और कक्षा में व्यावहारिक सहायता की आवश्यकता है।
- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में परिवर्तन
- राज्य अलग-अलग गति से एनईपी-संरेखित पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं।
- सामने आने वाली समस्याएं:
- कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने अद्यतनीकरण शुरू कर दिया है, लेकिन अन्य राज्य पिछड़ रहे हैं।
- पाठ्यपुस्तकें प्रायः देरी से आती हैं; कुछ मामलों में तो वर्ष के मध्य में भी।
- शिक्षकों को पुरानी पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे सीखने की गुणवत्ता में असंतुलन पैदा होता है।
- राज्यों में कोई एक समान मानक नहीं है, जो एनईपी के समान शिक्षा पहुंच के उद्देश्य के विरुद्ध है।
- माता-पिता की जागरूकता और सहायता
- कई माता-पिता, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, एनईपी के नए दृष्टिकोण से अवगत नहीं हैं।
- सामान्य मुद्दे:
- माता-पिता अभी भी सीखने का आकलन उच्च अंकों और रटने की आदत से करते हैं।
- वे अक्सर खेल-आधारित शिक्षा, परियोजनाओं और पोर्टफोलियो आकलन के मूल्य पर संदेह करते हैं।
- विश्वास और समझ बनाने में समय और नियमित बातचीत की आवश्यकता होती है।
एनईपी कार्यान्वयन के लिए हालिया पहल
- पीएम श्री स्कूल पहल का लक्ष्य 14,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का उन्नयन करना है । ये स्कूल आधुनिक बुनियादी ढांचे, अनुभवात्मक शिक्षा और डिजिटल कक्षाओं के साथ आदर्श एनईपी स्कूल के रूप में कार्य करेंगे।
- दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा ने नए आधारभूत और प्रारंभिक चरण के पाठ्यक्रमों का परीक्षण शुरू कर दिया है।
- निष्ठा और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
क्या किया जाने की जरूरत है?
एनईपी और इसके 5+3+3+4 मॉडल की सफलता के लिए, हमें यह करना होगा:
- आधारभूत संरचना को मजबूत करना – विशेष रूप से आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों में।
- सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों ही स्तरों पर शिक्षक शिक्षा में सुधार लाना।
- अद्यतन पाठ्यक्रम और सामग्री का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- जागरूकता और विश्वास पैदा करने के लिए माता-पिता और समुदायों को शामिल करना।
- प्रगति की पारदर्शी निगरानी करें और परिवर्तन के दौरान स्कूलों को सहायता प्रदान करना।
निष्कर्ष
5+3+3+4 मॉडल केवल एक संरचनात्मक सुधार नहीं है, बल्कि शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति मानसिकता में बदलाव भी है। इसकी सफलता नीति निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों की सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करती है। बुनियादी ढाँचे, शिक्षक क्षमता और सामुदायिक जागरूकता में निरंतर निवेश के साथ, भारत इस नीति को स्कूली शिक्षा सुधार के लिए एक वैश्विक मानक बना सकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
एनईपी 2020 के तहत 5+3+3+4 स्कूल संरचना क्या है और यह भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) को राजनीतिक दलों तक विस्तारित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला विधायिका और कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्राधिकार में आता है।
POSH अधिनियम क्या है?
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (जिसे POSH अधिनियम कहा जाता है) एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाना है।
यह अधिनियम प्रदान करता है
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा
- रोकथाम
- यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- PoSH अधिनियम लागू होने से पहले , भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का समाधान केवल 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा दिशानिर्देशों के माध्यम से किया जाता था।
- ये दिशानिर्देश ऐतिहासिक मामले विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य से सामने आए, जो भंवरी देवी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद शुरू हुआ था, जिस पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करने पर हमला किया गया था।
- यद्यपि विशाखा दिशानिर्देश एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करते थे, लेकिन वे प्रकृति में वैधानिक नहीं थे, जिसके कारण कार्यस्थलों पर उनका कार्यान्वयन असंगत था।
- इसलिए इन दिशानिर्देशों को कानून के रूप में संहिताबद्ध करने, भारत में सभी कार्यस्थलों पर उनके अनुप्रयोग का विस्तार करने, तथा यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट, प्रवर्तनीय प्रणाली बनाने के लिए PoSH अधिनियम लाया गया।
मुख्य विशेषताएं
- PoSH अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य है, जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों।
- अधिनियम के तहत पीड़ित महिला “किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, चाहे वह [कार्यस्थल पर] कार्यरत हो या नहीं”, जिसने “यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य का आरोप लगाया हो”।
- वास्तव में, यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जो किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी क्षमता में काम कर रही हैं या जा रही हैं।
- 2013 के कानून के तहत, यौन उत्पीड़न में सीधे या निहितार्थ से किए गए निम्नलिखित “अवांछित कृत्यों या व्यवहारों” में से “कोई एक या अधिक” शामिल हैं:
-
- शारीरिक संपर्क और प्रगति
- यौन संबंधों की मांग या अनुरोध
- यौन रूप से अश्लील टिप्पणियाँ
- अश्लील साहित्य दिखाना
- यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
- आईसीसी द्वारा कार्रवाई के लिए पीड़ित महिला के लिए शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है। अगर महिला “शारीरिक या मानसिक अक्षमता, मृत्यु या अन्य किसी कारण” से शिकायत नहीं कर सकती, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है।
- अधिनियम के तहत, शिकायत “घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर” की जानी चाहिए।
- हालांकि, आईसीसी “समय सीमा बढ़ा” सकती है यदि “वह संतुष्ट हो कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके कारण महिला उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कर सकी।”
- आईसीसी “जांच से पहले”, और “पीड़ित महिला के अनुरोध पर, उसके और प्रतिवादी के बीच सुलह के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकती है” – बशर्ते कि “सुलह के आधार के रूप में कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा”।
- आईसीसी या तो पीड़ित की शिकायत पुलिस को भेज सकती है, या फिर जांच शुरू कर सकती है, जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
- जांच पूरी होने पर, आईसीसी को 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट दोनों पक्षों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- महिला, प्रतिवादी, गवाह की पहचान, जांच, सिफारिश और की गई कार्रवाई से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।
- यदि यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हो जाते हैं, तो आईसीसी नियोक्ता को कंपनी के “सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार” कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी । ये नियम अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग हो सकते हैं।
क्या राजनीतिक दल PoSH अधिनियम के अंतर्गत आते हैं?
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, और कहा है कि यह नीति निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र में आता है।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिनियम में “कर्मचारी” और “कार्यस्थल” की व्यापक परिभाषाओं के बावजूद, राजनीतिक कार्यों में लगी महिलाओं, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, को बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तथा इसके समाधान के लिए कोई संरचित तंत्र मौजूद नहीं है।
राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का अभाव है।
किसी राजनीतिक दल के लिए P0SH अधिनियम का निर्धारण करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, पार्टी कार्यकर्ता, जिन्हें पार्टियाँ अक्सर बड़ी संख्या में नियुक्त करती हैं, अक्सर उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ कम ही बातचीत करते हैं और उन्हें बिना किसी निर्धारित “कार्यस्थल” के अस्थायी रूप से मैदान पर काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह विधायी/कार्यकारी नीतिगत मामला है , न्यायिक अधिदेश के लिए नहीं।
केरल उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण (2022)
- संवैधानिक अधिकार अनुसंधान एवं वकालत केंद्र बनाम केरल राज्य मामले (Centre for Constitutional Rights Research and Advocacy v. State of Kerala case) में न्यायालय ने कहा:
- राजनीतिक दलों का अपने सदस्यों के साथ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता।
- वे कोई ऐसा “उद्यम” या “प्रतिष्ठान” नहीं चलाते जो कार्यस्थल की PoSH परिभाषा के अनुरूप हो।
- इसलिए, उन्हें आईसीसी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।
इस तरह के फैसले राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों में खामियों को उजागर करते हैं तथा अनौपचारिक और अनियमित कार्य वातावरण में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाते हैं।
आगे की राह
- POSH की “कार्यस्थल” की परिभाषा का विस्तार करना ताकि इसमें स्पष्ट रूप से राजनीतिक संगठन शामिल हों।
- राजनीतिक दलों में शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाना ।
- सभी स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक करना।
निष्कर्ष
राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार, राजनीतिक स्थानों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने में मौजूदा कानूनी शून्यता को रेखांकित करता है।
यद्यपि यह अधिनियम औपचारिक कार्यस्थलों में सहायक रहा है, परन्तु इसकी सीमित प्रयोज्यता के कारण विशाल अनौपचारिक क्षेत्र – जिनमें राजनीतिक संगठन भी शामिल हैं – इसके दायरे से बाहर हैं।
इस अंतर को पाटने के लिए सक्रिय विधायी हस्तक्षेप, आंतरिक पार्टी सुधारों और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी धमकी, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त हो।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
POSH अधिनियम 2013 ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा को काफ़ी मज़बूत किया है, फिर भी इसकी सीमित प्रयोज्यता राजनीतिक संगठनों में कमियाँ छोड़ती है। व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों और संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)