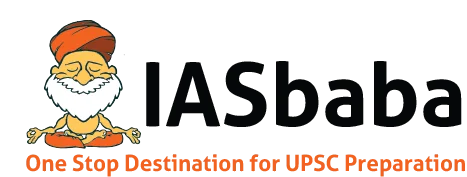IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: राजनीति
संदर्भ: असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए चुनाव हुए, जो भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के पांच जिलों पर शासन से संबंधित है।
बीटीसी चुनाव में यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। 40 सीटों के लिए कुल 316 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें प्रमोद बोरो (यूपीपीएल) और हग्रामा मोहिलरी (बीपीएफ) जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। नतीजे 26 सितंबर को घोषित किए जाएँगे।
Learning Corner:
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी):
- गठन: बीटीसी का गठन 2003 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत किया गया था।
- अधिकार क्षेत्र: यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) पर शासन करता है, जिसमें शुरू में चार जिले (कोकराझार, बक्सा, चिरांग, उदलगुरी) शामिल थे, जिन्हें बाद में पाँच जिलों में पुनर्गठित किया गया। यह क्षेत्र असम की भूटान सीमा से लगा हुआ है।
- संरचना:
- इसमें 40 निर्वाचित सदस्य और 6 असम के राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य हैं।
- बीटीसी को भूमि, वन, कृषि, शिक्षा और संस्कृति सहित 40 विषयों में विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।
- महत्व:
- असम के भीतर बोडो लोगों को स्वायत्तता और स्वशासन प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करते हुए बोडो लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान की रक्षा और संवर्धन करना है।
- नव गतिविधि:
- 2020 बोडो समझौते ने बीटीसी के क्षेत्र का नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) कर दिया और इसके विकास पहलों के दायरे का विस्तार किया।
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची :
- संदर्भ एवं उद्देश्य:
- छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) को पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त प्रशासन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था।
- इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और प्रशासनिक प्रथाओं की रक्षा करना तथा उनका सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
- लागू राज्य:
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
- निर्मित संस्थाएँ:
- स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी): प्रत्येक जिले की अपनी परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं (26 निर्वाचित, 4 राज्यपाल द्वारा नामित)।
- क्षेत्रीय परिषदें: जिलों के भीतर छोटे जनजातीय समूहों के लिए।
- शक्तियाँ एवं कार्य:
- भूमि, वन (आरक्षित वनों के अलावा), झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज आदि जैसे विषयों पर विधायी शक्तियां।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन जैसे विभागों को चलाने के लिए कार्यकारी शक्तियां।
- आदिवासियों से जुड़े मामलों के लिए ग्राम और जिला न्यायालयों के माध्यम से न्यायिक शक्तियां।
- वित्तीय शक्तियों में कर, शुल्क लगाना और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना शामिल है।
- महत्व:
- भारत के संघीय ढांचे के अंतर्गत स्वशासन का एक अनूठा मॉडल प्रदान करता है।
- भारतीय संघ की एकता के साथ जनजातीय स्वायत्तता को संतुलित करना।
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ: वैज्ञानिक पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर एआई के लिए, की गति और ऊर्जा सीमाओं को दूर करने के लिए प्रकाश-आधारित (ऑप्टिकल) कंप्यूटिंग की खोज कर रहे हैं। हाल के शोध में पाया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की अरैखिक अंतःक्रियाएँ एआई कार्यों को तेज़ी से और अधिक कुशलता से कर सकती हैं।
ऑप्टिकल कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनों के बजाय फोटॉन का उपयोग करती है, जिससे यह तेज़, अधिक ऊर्जा-कुशल और विशाल डेटा स्थानांतरण को संभालने में सक्षम हो जाती है। फ़िनलैंड और फ़्रांस के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर में तीव्र प्रकाश स्पंदन पारंपरिक एल्गोरिदम के बजाय भौतिकी का उपयोग करके AI कार्यों को संसाधित कर सकते हैं। उनके प्रयोगों ने ऑप्टिकल संकेतों का उपयोग करके AI मॉडलों को प्रशिक्षित किया, जिससे कम ऊर्जा उपयोग के साथ उच्च सटीकता प्राप्त हुई। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, यह सफलता AI में क्रांति ला सकती है, और भविष्य की कंप्यूटिंग के लिए अभूतपूर्व गति और दक्षता प्रदान कर सकती है।
Learning Corner:
ऑप्टिकल फाइबर:
- परिभाषा: ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के पतले, लचीले धागे होते हैं जो प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचारित करते हैं।
- कार्य सिद्धांत: वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां प्रकाश संकेत फाइबर के कोर के भीतर बिना बाहर निकले उछल जाते हैं, जिससे डेटा न्यूनतम हानि के साथ लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है।
- संरचना:
- कोर: सबसे भीतरी भाग जहां प्रकाश यात्रा करता है।
- क्लैडिंग: यह कोर को घेरता है तथा प्रकाश को वापस इसमें परावर्तित करता है।
- बफर कोटिंग: सुरक्षा और मजबूती प्रदान करती है।
- प्रकार:
- एकल-मोड फाइबर: संकीर्ण कोर, सीधे प्रकाश संचारित करते हैं, लंबी दूरी के संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- मल्टी-मोड फाइबर: बड़ा कोर, एकाधिक प्रकाश पथ, छोटी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है।
- अनुप्रयोग:
- उच्च गति इंटरनेट और दूरसंचार नेटवर्क।
- मेडिकल इमेजिंग (एंडोस्कोपी)
- रक्षा एवं एयरोस्पेस संचार।
- ऑप्टिकल कंप्यूटिंग और एआई में उभरते उपयोग।
- लाभ:
- उच्च बैंडविड्थ और तेज़ डेटा स्थानांतरण।
- कम सिग्नल हानि और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से प्रतिरक्षित।
- हल्का और टिकाऊ
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रसंग: खगोलविदों ने एक नए क्षुद्रग्रह, 2025 PN7 की खोज की है, जो पृथ्वी के समान कक्षा में घूमता है तथा इसे अर्ध-चंद्रमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अर्ध-चंद्रमा और लघु-चंद्रमा छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो अस्थायी रूप से पृथ्वी की कक्षा में साथ रहते हैं। इस गर्मी में देखा गया नया अर्ध-चंद्रमा, 2025 PN7, 52 फीट से कम ऊँचाई के साथ अपनी तरह का सबसे छोटा हो सकता है। ऐसे पिंड अक्सर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट से या चंद्रमा के मलबे के रूप में उत्पन्न होते हैं। स्थायी चंद्रमाओं के विपरीत, ये अस्थायी साथी होते हैं, जो दशकों तक पृथ्वी के साथ रहते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। पृथ्वी के पहले भी ऐसे ही अनुयायी रहे हैं, जहाँ अर्ध-चंद्रमा अनुसंधान और संभावित भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अवसर प्रदान करते हैं।
Learning Corner:
अर्ध-चंद्रमा और लघु-चंद्रमा (Quasi-moons and Mini-moons):
- मिनी-मून:
- छोटी प्राकृतिक वस्तुएं जो अस्थायी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं।
- स्थायी चंद्रमा के विपरीत, वे अल्पकालिक साथी होते हैं, जो प्रायः कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक साथ रहते हैं।
- इनमें से कई तस्वीरें क्षुद्रग्रहों या उल्कापिंडों के टकराने के बाद चंद्रमा के टुकड़ों के रूप में ली गई हैं।
- उदाहरण: 2006 आर.एच.120, एक छोटा-चंद्रमा जो लगभग एक वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा।
- अर्ध-चंद्रमा:
- वे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी की कक्षा के समान पथ का अनुसरण करते हैं, वे पृथ्वी के साथी जैसे प्रतीत होते हैं।
- वे वास्तविक उपग्रह नहीं हैं, बल्कि स्थिर गुरुत्वाकर्षण “नृत्य” में दशकों तक पृथ्वी के आसपास बने रहते हैं।
- उदाहरण: 2025 PN7 (हाल ही में देखा गया), 469219 कामोओलेवा (2016 में खोजा गया)।
- वे पृथ्वी से एक स्थिर औसत दूरी बनाए रखते हैं, तथा प्रायः अनुनादी कक्षीय पैटर्न में रहते हैं।
- महत्व:
- दोनों ही पृथ्वी के अस्थायी साथी हैं।
- वैज्ञानिक अध्ययन, अंतरिक्ष मिशन और संभावित संसाधन अन्वेषण के लिए उपयोगी, क्योंकि वे मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत करीब हैं और उन तक पहुंचना आसान है।
स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
प्रसंग: रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जो फरवरी 2026 में समाप्त होने वाली है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को न्यू स्टार्ट संधि, जो दोनों देशों के बीच आखिरी परमाणु हथियार समझौता है, को एक साल के लिए बढ़ाने की पेशकश की है। यह संधि दोनों पक्षों को 1,550 तैनात सामरिक परमाणु हथियारों तक सीमित करती है। रूस ने कहा कि वह बातचीत जारी रहने तक संधि का पालन जारी रखने को तैयार है, लेकिन चेतावनी दी कि यह प्रस्ताव इस शर्त पर है कि अमेरिका एकतरफा शर्तें न थोपे या रूस की रक्षा क्षमताओं को कम न करे। यह कदम अमेरिका-रूस के बीच बढ़ते तनाव, खासकर यूक्रेन को लेकर, और हथियार नियंत्रण को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच उठाया गया है।
Learning Corner:
अमेरिका और रूस के बीच प्रमुख परमाणु संधियाँ
परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी), 1968
- यह द्विपक्षीय नहीं था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थे।
- इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करना है।
सामरिक हथियार सीमा वार्ता (SALT I और II)
- SALT I (1972): अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) और पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) की संख्या सीमित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाने वाली एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (ABM) संधि भी हुई।
- SALT II (1979): परमाणु वितरण प्रणालियों पर सीमाएँ प्रस्तावित की गईं, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के कारण औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई। हालाँकि, दोनों पक्षों ने अनौपचारिक रूप से इसका बड़े पैमाने पर पालन किया।
मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति (INF) संधि, 1987
- रीगन (अमेरिका) और गोर्बाचेव (सोवियत संघ) द्वारा हस्ताक्षरित।
- 500-5,500 किमी की दूरी तक मार करने वाली सभी भूमि-आधारित मिसाइलों को समाप्त कर दिया गया।
- परमाणु हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करने वाली पहली संधि।
- अमेरिका ने 2019 में रूसी उल्लंघनों का हवाला देते हुए इसे वापस ले लिया था।
सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधियाँ (START I और II)
- स्टार्ट I (1991): दोनों पक्षों पर तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या घटाकर 6,000 कर दी गई।
- स्टार्ट II (1993): आईसीबीएम पर बहु-युद्धक शीर्षों (एमआईआरवी) पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।
सामरिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि (SORT) / मॉस्को संधि, 2002
- बुश (अमेरिका) और पुतिन (रूस) द्वारा हस्ताक्षरित।
- परिचालनात्मक रूप से तैनात वारहेड्स को 1,700-2,200 तक सीमित कर दिया गया।
नई START संधि, 2010
- ओबामा (अमेरिका) और मेदवेदेव (रूस) द्वारा हस्ताक्षरित।
- तैनात सामरिक हथियारों की संख्या 1,550 तथा वितरण प्रणालियों की संख्या 700 तक सीमित कर दी गई।
- 2021 में 5 साल के विस्तार के बाद फरवरी 2026 में इसकी अवधि समाप्त होने वाली है।
- वर्तमान में यह दोनों शक्तियों के बीच अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है।
महत्व:
- इन संधियों से शीत युद्ध के तनाव और विशाल परमाणु भंडार को कम करने में मदद मिली।
- हालाँकि, INF संधि के पतन और न्यू स्टार्ट की समाप्ति के साथ, परमाणु हथियार नियंत्रण का भविष्य अनिश्चित है।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
प्रसंग: सेबी भारत के बाजार को गहरा करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को गैर-कृषि वस्तु डेरिवेटिव्स में व्यापार करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एफपीआई को नकद-निपटान वाले, गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स जैसे सोना, चांदी, जस्ता और अन्य मूल धातुओं में व्यापार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में, एफपीआई केवल वित्तीय अनुबंधों के माध्यम से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल जैसे गैर-कृषि डेरिवेटिव्स में ही भाग ले सकते हैं, लेकिन लौह और कीमती धातुओं में नहीं। इस कदम से तरलता बढ़ने, बाजार की गहराई बढ़ने, मूल्य निर्धारण में सुधार और अधिक संस्थागत भागीदारी आकर्षित होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार हेजिंग लागत को कम करके और उन्हें वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाकर भारत के कमोडिटी बाजारों को बढ़ावा देगा।
Learning Corner:
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई):
- परिभाषा: किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बांड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव में विदेशी निवेशकों द्वारा किया गया निवेश, बिना व्यावसायिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लिए।
- प्रकृति:
- अल्पकालिक, अस्थिर, और अक्सर सट्टा (“हॉट मनी”)।
- एफडीआई की तुलना में प्रवेश और निकास आसान।
- भारत में नियामक: सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)।
- उदाहरण: एक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा इंफोसिस या रिलायंस के शेयर खरीदना।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):
- परिभाषा: किसी विदेशी संस्था द्वारा किसी अन्य देश में स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन भागीदारी के साथ किसी व्यवसाय में निवेश।
- प्रकृति:
- दीर्घकालिक एवं अपेक्षाकृत स्थिर।
- इसमें कारखाने, कार्यालय स्थापित करना या कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल करना शामिल है।
- भारत में नियामक: डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) और आरबीआई।
- उदाहरण: वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करना; हुंडई द्वारा भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
विश्व रोगी सुरक्षा दिवस (17 सितम्बर) अस्पताल-जनित संक्रमणों की रोकथाम सहित जागरूकता बढ़ाने और रोगी सुरक्षा में सुधार पर जोर देता है।
वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में एचएआई एक महत्वपूर्ण नुकसान का स्रोत है, जो रोगी सुरक्षा, रुग्णता, मृत्यु दर और स्वास्थ्य देखभाल लागत को प्रभावित करता है।
अस्पताल-अधिग्रहित संक्रमण क्या है ?
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) (2002) के अनुसार एचएआई एक ऐसा संक्रमण है जो अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में भर्ती मरीज में होता है, जिसमें भर्ती के समय संक्रमण मौजूद नहीं था या विकसित नहीं हो रहा था।
- इनमें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद होने वाले संक्रमण और स्वास्थ्य कर्मचारियों में व्यावसायिक संक्रमण शामिल हैं।
- आमतौर पर, HAIs भर्ती होने के 48 घंटे बाद या सर्जरी के 30 दिनों के भीतर विकसित होते हैं।
संक्रमण के प्रकार
- एचएआई बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण हो सकता है, जिसमें बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण सबसे आम है।
- आम जीवाणु संक्रमणों में स्टैफ और स्ट्रेप बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण शामिल हैं। कुछ बैक्टीरिया आम एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज मुश्किल और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये जीवाणु संक्रमण रक्त, फेफड़ों या मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं।
- फंगल संक्रमण आमतौर पर कैंडिडा प्रजाति के कारण होता है , जिसमें बहु-दवा प्रतिरोध (multi-drug resistance) बढ़ रहा है।
- वायरल संक्रमण, हालांकि कम आम हैं, उनमें हेपेटाइटिस वायरस और एचआईवी शामिल हैं।
संचरण का तरीका
- एचएआई श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है।
- उचित रोक और संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं का पालन न करने पर ये फैल सकते हैं। दूषित उपकरण संक्रमण का स्रोत बन सकते हैं।
- अंतर्जात क्रियाविधि (शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद सूक्ष्मजीव) HAIs का कारण बन सकती हैं।
उदाहरण:
- केंद्रीय लाइन-संबंधी रक्तप्रवाह संक्रमण (सीएलएबीएसआई): संक्रमण तब होता है जब रोगाणु किसी प्रमुख नस में डाली गई केंद्रीय लाइन या कैथेटर के माध्यम से रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं; ये लाइनें परिधीय IVs से अधिक समय तक रहती हैं।
- कैथेटर-संबंधी मूत्र पथ संक्रमण (सीएयूटीआई): संक्रमण तब होता है जब रोगाणु मूत्र पथ में प्रवेश कर जाते हैं; यह मूत्र प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है।
- सर्जिकल साइट संक्रमण (एसएसआई): संक्रमण सर्जरी के स्थान पर होता है; यह त्वचा, ऊतक, अंगों या प्रत्यारोपित सामग्री को प्रभावित कर सकता है।
- वेंटिलेटर-संबंधी निमोनिया (वीएपी): फेफड़ों का संक्रमण जो वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों में विकसित होता है।
भारत में स्थिति
- भारत में, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण (एचएआई) एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बने हुए हैं, विशेष रूप से तृतीयक देखभाल अस्पतालों और गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) में।
- द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत भर के 26 तृतीयक स्तर के अस्पतालों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 89 आईसीयू शामिल थे। इस अध्ययन में मई 2017 से अक्टूबर 2018 की अवधि में 2,622 स्वास्थ्य सेवा-संबंधी रक्तप्रवाह संक्रमण और 737 मूत्र पथ संक्रमण (यूटीआई) दर्ज किए गए।
- इन संक्रमणों में, केंद्रीय लाइन से जुड़े रक्तप्रवाह संक्रमण (सीएलएबीएसआई) नवजात आईसीयू में सबसे अधिक प्रचलित थे , जबकि कैथेटर से जुड़े मूत्र पथ के संक्रमण (सीएयूटीआई) बाल चिकित्सा आईसीयू में सबसे अधिक थे।
- अध्ययन में कार्बापेनेम्स, जो एंटीबायोटिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, के प्रति उच्च स्तर के प्रतिरोध पर भी प्रकाश डाला गया , जिससे उपचार में अतिरिक्त चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।
- भारत एक निम्न एवं मध्यम आय वाला देश (एलएमआईसी) है, तथा उसे उच्च आय वाले देशों की तुलना में एचएआई का जोखिम 20 गुना अधिक हो सकता है।
भारत में चुनौतियाँ
- प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की सीमित उपलब्धता और अनुचित उपयोग।
- अपर्याप्त स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-रक्षा प्रथाएँ।
- अस्पतालों में मरीजों की अत्यधिक भीड़ के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है।
- कई माध्यमिक और जिला स्तर के अस्पतालों, सार्वजनिक और निजी दोनों में, मजबूत संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों का अभाव है, जिससे मरीज नोसोकोमियल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
आवश्यक कदम
- संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में उच्च-गुणवत्ता वाली जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) सेवाएँ सुनिश्चित करें।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य आईपीसी कार्यक्रमों को लागू करें, जिनमें हाथ स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन, नियमित निगरानी और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
- संक्रामक एजेंटों के संदूषण और संचरण को रोकने के लिए उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों का उचित रूप से रोगाणुनाशन बनाए रखें ।
- संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं की नियमित रूप से निगरानी और ऑडिट करें ताकि कमियों की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपाय लागू किए जा सकें।
- संक्रमण के जोखिम, रोकथाम की रणनीतियों और जिम्मेदार रोगाणुरोधी उपयोग के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ।
- स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के भीतर क्रॉस-ट्रांसमिशन को रोकने के लिए संक्रामक संक्रमण वाले रोगियों के लिए अलगाव प्रोटोकॉल स्थापित करें ।
- व्यापक आईपीसी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन के बीच बहु-विषयक समन्वय को प्रोत्साहित करें ।
निष्कर्ष
अस्पताल-जनित संक्रमण (एचएआई) एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है जो रोगी सुरक्षा, रुग्णता, मृत्यु दर और स्वास्थ्य देखभाल लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत में एचएआई को कम करने, रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने और समग्र स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपाय आवश्यक हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
अस्पताल-जनित संक्रमणों के कारणों, जोखिम कारकों और निवारक रणनीतियों पर चर्चा करें। साथ ही, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (आईपीसी) उपायों की भूमिका पर प्रकाश डालें। (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के डॉक्टर भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए, वे स्वास्थ्य सेवा का एकमात्र सुलभ माध्यम हैं।
उनकी भूमिका नैदानिक देखभाल से आगे बढ़कर सामुदायिक स्वास्थ्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन और नीति क्रियान्वयन तक फैली हुई है। वे न केवल डॉक्टर के रूप में, बल्कि योजनाकार, समन्वयक और नेता के रूप में भी कार्य करते हैं।
पीएचसी डॉक्टरों का महत्व
- पीएचसी डॉक्टर केवल स्वास्थ्य प्रदाता ही नहीं हैं; वे सामुदायिक कल्याण के वाहक हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और ग्रामीण आबादी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
- एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमतौर पर लगभग 30,000 लोगों की विविध आबादी को सेवा प्रदान करता है (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में यह संख्या लगभग 20,000 है) और शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 50,000 तक होती है।
- वे सभी आयु समूहों और विशेषज्ञताओं जैसे नवजात शिशु देखभाल, मातृ स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, संक्रामक रोग, आघात, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों में सेवाएं प्रदान करते हैं।
- उनका कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है: समान पहुंच, सामुदायिक भागीदारी, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक उपयोग।
- वे टीकाकरण अभियानों का समन्वय करते हैं, घर-घर जाकर सर्वेक्षण करते हैं, वेक्टर नियंत्रण का प्रबंधन करते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाते हैं, तथा क्षेत्रीय प्रकोपों पर प्रतिक्रिया देते हैं।
- वे स्वास्थ्य शिक्षा सत्र आयोजित करते हैं, अंतर-क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेते हैं, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं में भाग लेते हैं।
- वे आशा, एएनएम और ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और पर्यवेक्षण करते हैं; प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी और उप-केंद्रों का दौरा करते हैं।
- वे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के अंतिम छोर तक कार्यान्वयनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, तथा सरकारी मंशा और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को पाटते हैं।
पीएचसी डॉक्टरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
पीएचसी डॉक्टरों पर अत्यधिक बोझ
- एक पीएचसी डॉक्टर प्रतिदिन लगभग 100 मरीजों को संभालता है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रसवपूर्व मरीज भी शामिल हैं, तथा साथ ही कार्यक्रम के लक्ष्यों को भी पूरा करता है।
- विशेषज्ञों के विपरीत, उन्हें नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धावस्था और आपातकालीन स्थितियों तक सभी क्षेत्रों में नए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उपचार करना होता है।
- भारी कार्यभार के कारण सीखने या शोध के लिए बहुत कम समय बचता है।
प्रशासनिक अधिभार
- डॉक्टरों को 100 से अधिक भौतिक रजिस्टरों का रखरखाव करना पड़ता है, जिसमें बाह्य रोगी (OPD) रिकॉर्ड, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, दवा सूची, स्वच्छता आदि शामिल होते हैं।
- उन्हें एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी), जनसंख्या स्वास्थ्य रजिस्ट्री (पीएचआर), आयुष्मान भारत पोर्टल, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और टीकाकरण के लिए यूडब्ल्यूआईएन जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों में डेटा प्रविष्टि करनी पड़ती है, जिसके कारण डेटा प्रविष्टि दोहरानी पड़ती है।
- डिजिटलीकरण के बावजूद, कागजी रिकॉर्ड बने हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेज़ीकरण का दोहरा बोझ बढ़ गया है।
- कई डॉक्टर रिपोर्टिंग पूरी करने के लिए देर रात तक काम करते हैं, जिससे कागजी कार्रवाई में प्रभावी रूप से “दूसरी पारी” भी जुड़ जाती है।
बर्नआउट
- बर्नआउट शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक थकावट की स्थिति है जो लंबे समय तक तनाव और अधिक काम के कारण होती है।
- चिकित्सकों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने तथा विस्तृत दस्तावेजीकरण का कार्य सौंपा जाता है, जबकि उन्हें स्टाफ, पारिश्रमिक या मान्यता बहुत कम दी जाती है।
- लैंसेट ने चिकित्सकों की थकान को एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया है, जिसमें भावनात्मक थकावट, अलगाव और व्यर्थता की भावना होती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की आईसीडी-11 बर्नआउट को एक व्यावसायिक समस्या मानती है, जिसके लिए केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि प्रणालीगत समाधान की भी आवश्यकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन अध्ययन से पता चलता है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग एक तिहाई प्राथमिक देखभाल चिकित्सक भावनात्मक थकावट से पीड़ित हैं।
- सऊदी अरब के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रशासनिक कार्यभार, पीएचसी डॉक्टरों में थकान का एक प्रमुख कारण है।
वैश्विक अनुभव और सबक
- 25 बाय 5 अभियान (यूएसए) का लक्ष्य स्वचालन और सरलीकरण के माध्यम से 2025 तक चिकित्सकों के दस्तावेज़ीकरण समय को 75% तक कम करना है।
- डेनमार्क और यूके जैसे देशों ने प्रशासनिक कर्मचारियों को गैर-नैदानिक कार्य सौंपकर प्राथमिक देखभाल टीमों को मजबूत किया है।
आवश्यक कदम
- प्रणाली को अनुपालन से सुविधा की ओर स्थानांतरित करें, तथा डॉक्टरों पर चेकलिस्ट और लक्ष्यों का बोझ डालने के बजाय उन्हें सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित करें।
- अनावश्यक कागजी रजिस्टरों को हटा दें तथा दोहरा डेटा प्रविष्टि से बचने के लिए एकल-प्रविष्टि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं।
- डेटा एकत्र करने और मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण को कम करने के लिए स्वचालन, एआई और मोबाइल स्वास्थ्य उपकरणों का उपयोग करें।
- डेटा एंट्री ऑपरेटरों, प्रशासनिक कर्मचारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधकों की भर्ती करें ताकि डॉक्टर रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- नियमित नैदानिक और आउटरीच कार्य को साझा करने के लिए नर्सों, एएनएम और फार्मासिस्टों की भूमिकाओं का विस्तार करें।
- डॉक्टरों को थकान से बचाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, परामर्श सेवाएं और नियमित विश्राम अवकाश प्रदान करें।
निष्कर्ष
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 3.8 में निहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का प्रवेश द्वार है। यह आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षित दवाओं और वित्तीय सुरक्षा तक पहुँच का वादा करता है। मज़बूत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बिना, एसडीजी 3, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है, आकांक्षापूर्ण ही रहेगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरों के सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
परिचय (संदर्भ)
2015 में शुरू की गई भारत की डिजिटल इंडिया पहल, देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाने, शासन को बेहतर बनाने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के एक रणनीतिक प्रयास का प्रतीक है। पिछले एक दशक में, इसने इंटरनेट पहुँच का विस्तार किया है, सेवा वितरण में सुधार किया है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है।
चूंकि अधिकांश अफ्रीकी देश डिजिटल परिवर्तन के लिए तैयार हैं, इसलिए भारतीय अनुभव उन्हें लागत प्रभावी और प्रासंगिक मॉडल प्रदान कर सकता है।
भारत का डिजिटल परिवर्तन डेटा
- इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 में 251 मिलियन से बढ़कर 2024 में लगभग 970 मिलियन हो गई।
- 2,18,000 से अधिक गांव हाई-स्पीड नेटवर्क से जुड़े।
- डिजिटल अवसंरचना ने बड़े पैमाने पर टेलीमेडिसिन, टेली-शिक्षा और ई-गवर्नेंस सेवाओं को सक्षम बनाया
- प्रतिवर्ष लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान; भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 11.74% (2022-23)।
- लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में फिनटेक, ई-कॉमर्स, हेल्थ-टेक और एग्री-टेक शामिल हैं।
अफ्रीका डिजिटल अर्थव्यवस्था
- इंटरनेट की पहुंच 2005 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में लगभग 38 प्रतिशत हो गई।
- 2023 में, मोबाइल उद्योग ने क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 140 बिलियन डॉलर या 7 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसके 2030 तक बढ़कर 170 बिलियन डॉलर हो जाने की उम्मीद है।
- इस महाद्वीप ने स्वयं को मोबाइल वित्तीय सेवाओं में भी अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, तथा विश्व के आधे मोबाइल मनी प्रदाता उप-सहारा अफ्रीका में स्थित हैं।
चुनौतियां
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की कम पहुंच और सीमित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
- डेटा सेंटर, विश्वसनीय बिजली और नेटवर्क कवरेज सहित अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचा
- डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट सेवाओं की उच्च लागत, हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए पहुंच को सीमित करती है।
- डिजिटल शासन के लिए विखंडित एवं अविकसित विनियामक एवं नीतिगत ढाँचे।
- आईसीटी, डेटा विज्ञान, एआई और अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में कुशल कार्यबल की कमी।
- कमजोर साइबर सुरक्षा ढांचे और ऑनलाइन सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण के बारे में सीमित जागरूकता।
- सार्वजनिक सेवा वितरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों के साथ डिजिटल समाधानों का अपर्याप्त एकीकरण।
भारत-अफ्रीका डिजिटल पहल
- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) डिजिटल परियोजनाओं के लिए संवाद, ऋण व्यवस्था, अनुदान और तकनीकी सहायता को सुगम बनाएगा।
- 2009 में, भारत ने टेली-शिक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुगम बनाने वाली एक महाद्वीपव्यापी पहल , पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क की शुरुआत की। इसी के आधार पर, अफ्रीकी छात्रों और रोगियों को भारतीय शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों के साथ और अधिक एकीकृत करने के लिए 2019 में ई-विद्याभारती (टेली-शिक्षा) और ई-आरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) परियोजना (ई-वीबीएबी) शुरू की गई।
- ई-वीबीएबी योजना के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए हजारों छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
- भारत ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए केन्या, बोत्सवाना, युगांडा, तंजानिया और घाना में आईटी केंद्र स्थापित किए हैं।
- आईसीटी अवसंरचना और प्रशिक्षण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मॉरीशस में साइबर टॉवर की स्थापना की गई।
- आईसीटी कौशल विकास को समर्थन देने के लिए घाना में कोफी अन्नान आईसीटी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई ।
- युवाओं में डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई।
- डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्नत कार्यक्रम प्रदान करने वाला विदेशी आईआईटी परिसर स्थापित किया गया ।
- भारती एयरटेल की सहायक कंपनी एक्सटेलीफाई ने 14 अफ्रीकी देशों में एआई-संचालित प्लेटफॉर्म तैनात करने, दूरसंचार अवसंरचना, परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने के लिए नाइजीरिया के साथ बहु-वर्षीय, बहु-मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- अफ्रीकी उद्यमों के साथ सहयोग करने के लिए फिनटेक, स्वास्थ्य-तकनीक और कृषि-तकनीक में भारतीय स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना ।
- भारत के डिजिटल भुगतान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मॉडल को जानने के लिए अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अध्ययन दौरे का आयोजन ।
- समावेशी शासन और वित्तीय समावेशन के मॉडल के रूप में भारत की आधार डिजिटल पहचान प्रणाली को साझा करना ।
- लगभग 19 वर्ष की औसत आयु के साथ, अफ्रीका विश्व स्तर पर सबसे युवा आबादी वाला देश है। हालाँकि, इस जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाने के लिए, डिजिटल कौशल विकास में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। इसलिए, भारत के स्किल इंडिया, डिजिटल साक्षरता अभियान और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं डिजिटल साक्षरता के लिए आईटीईसी से प्रेरित होकर कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आगे की राह
- समावेशी विकास और पारस्परिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत-अफ्रीका सहयोग को मजबूत करना।
- अफ्रीका के डिजिटल बुनियादी ढांचे और शासन प्रणालियों का समर्थन करने के लिए संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- चौथी औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।
- ऐसे नीतिगत ढाँचों को प्रोत्साहित करें जो लचीले, मापनीय और स्थानीय संदर्भों के अनुकूल हों।
- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, शैक्षिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष
समावेशी शासन के लिए डिजिटल तकनीकों का भारत द्वारा सफल उपयोग अफ्रीकी देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, लचीले नीतिगत ढाँचों और रणनीतिक सहयोग के साथ, भारत और अफ्रीका एक ऐसे भविष्य का सह-निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जहाँ डिजिटल नवाचार वैश्विक दक्षिण में सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
जाँच कीजिए कि भारत का डिजिटल परिवर्तन अफ्रीका के लिए किस प्रकार एक आदर्श बन सकता है। पूरे महाद्वीप में समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त अनुभवों और रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)