IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- तेलंगाना विधानमंडल सचिवालय ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के चार और विधायकों को तलब किया है, जिन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने का आरोप है।
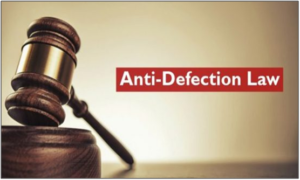
दलबदल विरोधी कानून के बारे में:
- विकास:
- आज़ादी के बाद के भारत में, बार-बार दलबदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 1960 के दशक में हरियाणा के एक विधायक द्वारा एक ही दिन में कई बार दल बदलने के बाद “आया राम, गया राम” मुहावरा प्रचलित हो गया।
- इस मुद्दे को हल करने के लिए, 52वें संविधान संशोधन, 1985 के माध्यम से संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में दलबदल विरोधी कानून को पेश किया गया।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दलबदल को रोकना था। यह संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों पर लागू होता है।
- संशोधन: 91वें संशोधन अधिनियम (2003) ने एक-तिहाई विभाजन प्रावधान को समाप्त करके दलबदल विरोधी कानून में संशोधन किया, जिसके तहत विलय की अनुमति केवल तभी दी गई जब किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य सहमत हों, और दलबदलुओं को मंत्री या भुगतान वाले राजनीतिक पद धारण करने से तब तक अयोग्य घोषित कर दिया गया जब तक कि वे पुनः निर्वाचित नहीं हो जाते।
- अयोग्यता के आधार:
- कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है (इसका अनुमान उसके आचरण से लगाया जा सकता है, न कि केवल त्यागपत्र से)।
- यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- यदि कोई विधायक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायक बनने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- अयोग्यता के अपवाद:
- यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक सहमत हों तो वह किसी अन्य पार्टी के साथ विलय कर सकती है, तथा विलय करने या बने रहने वालों के लिए कोई अयोग्यता नहीं होगी।
- तटस्थ रहने के लिए पार्टी से इस्तीफा देने वाले अध्यक्ष/सभापति/उपसभापति के लिए कोई अयोग्यता नहीं।
- निर्णय लेने वाला प्राधिकारी: अयोग्यता के मामलों का निर्णय अध्यक्ष/सभापति द्वारा किया जाता है। अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के पास कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समय-सीमा नहीं है, जिससे रणनीतिक देरी की गुंजाइश बनी रहती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अध्यक्ष के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इसका अर्थ है कि यदि अध्यक्ष के फैसले में दुर्भावनापूर्ण इरादे, प्रक्रियागत चूक या संवैधानिक उल्लंघन हो, तो अदालतें निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं।
- केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा एवं अन्य (2020) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्षों को दलबदल के मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया और निष्पक्षता एवं गति सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही में देरी दसवीं अनुसूची के उद्देश्य का उल्लंघन करती है और समय पर निर्णय लेने के मानक को बनाए रखने में विफल रहने के कारण अध्यक्ष के कार्यालय में विश्वास को कम करती है।
स्रोत:
श्रेणी: विविध
प्रसंग:
- इस सप्ताह जारी रैंकिंग के अनुसार, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2026 में चीन ने भारत को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला स्थान प्राप्त कर लिया है।
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में:
- प्रकृति: क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग एक वार्षिक क्षेत्रीय मूल्यांकन है जो शैक्षणिक प्रतिष्ठा, रोजगार क्षमता, अनुसंधान उत्पादकता और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एशिया के अग्रणी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है।
- जारीकर्ता: यह रिपोर्ट क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा संकलित की गई है, जो ब्रिटेन स्थित उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म है, जो विश्व स्तर पर अपनी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए जानी जाती है।
- उद्देश्य:
- वैश्विक स्तर पर तुलनीय संकेतकों का उपयोग करके एशियाई विश्वविद्यालयों का मानकीकरण करना।
- क्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार और अनुसंधान प्रभाव को उजागर करना।
- एशियाई उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देना।
- क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 के बारे में:
- 2026 की रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थानों पर हांगकांग, सिंगापुर और चीन के विश्वविद्यालयों का दबदबा रहा।
- इस वर्ष भारत ने सूची में 132 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शामिल किया, जिससे इसकी संख्या रिकॉर्ड 294 पर पहुंच गई, जबकि चीन ने 259 संस्थानों को शामिल किया, जिससे इसकी कुल संख्या 394 हो गई।
- शीर्ष 100 में सात भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली 59वें स्थान पर है।
- शीर्ष 100 में चीन के 25 विश्वविद्यालय हैं, जबकि भारत के संस्थानों की संख्या पिछले वर्ष की तरह ही शीर्ष 100 में बनी हुई है।
स्रोत:
श्रेणी: राजनीति और शासन
प्रसंग:
- भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एपीडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) की पहली निर्यात खेप की सुविधा प्रदान की है।

एपीडा के बारे में:
- स्थापना: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी।
- नोडल मंत्रालय: यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- एनएबी का सचिवालय: यह जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
- उद्देश्य: एपीडा को अनुसूचित उत्पादों जैसे फल, सब्जियां और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद, पुष्प उत्पादन और पुष्प उत्पादन उत्पाद, हर्बल और औषधीय पौधे आदि के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- सर्वेक्षण और अध्ययन करना: यह निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास की देखभाल वित्तीय सहायता प्रदान करके या सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए, सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से भाग लेकर करता है।
- बूचड़खानों (slaughterhouses) का निरीक्षण: यह बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों में मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करता है और अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार करता है।
- एपीडा प्राधिकरण की संरचना : एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष
- भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पूर्व अधिकारी
- नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य
- संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य क्रमशः केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत:
श्रेणी: इतिहास और संस्कृति
प्रसंग:
- तिरुवन्नामलाई में जवाधु पहाड़ियों के ऊपर जमुनामारथुर गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक मिट्टी के बर्तन में विजयनगर काल के 103 अंकित स्वर्ण सिक्के पाए गए।

विजयनगर साम्राज्य के बारे में:
- स्थापना: परंपरा के अनुसार, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पाँच भाइयों के परिवार से थे, जो वारंगल के काकतीय सामंत थे। संगम राजवंश के हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा 1336 में स्थापित, विजयनगर दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया।
- राजधानी: विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जो वर्तमान कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी।
- राजव्यवस्था और प्रशासन: विजयनगर की राजव्यवस्था राजा को सत्ता का केंद्र मानती थी और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। राज्य राज्य या मंडलम (प्रांत) में विभाजित था, जिन्हें आगे नाडु (ज़िला), स्थल (उप-ज़िला) और ग्राम (गाँव) में विभाजित किया गया था।
- अर्थव्यवस्था: विजयनगर शासकों के संरक्षण में कपड़ा, खनन और धातुकर्म जैसे उद्योग फल-फूल रहे थे। व्यापार तेज़ था और फारस, अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे बर्मा, चीन और श्रीलंका के साथ विदेशी व्यापार भी होता था। जहाज़ इन देशों में चावल, लोहा, चंदन, चीनी और मसाले ले जाते थे।
- समाज: मध्यकालीन अन्य सभी समाजों की तरह, विजयनगर का समाज भी तीन मुख्य वर्गों में विभाजित था – कुलीन, मध्यम वर्ग और आम लोग। कुलीन वर्ग अत्यंत सुख-सुविधाओं और विलासिता में जीवन व्यतीत करता था, जबकि मध्यम वर्ग मुख्यतः व्यापारी थे और शहरों में रहते थे। आम लोग साधारण जीवन जीते थे और उन पर भारी कर लगाया जाता था।
- धर्म: संगम शासक अधिकतर शैव धर्म के अनुयायी थे और विरुपाक्ष उनके कुलदेवता थे। बाद के राजवंशों पर वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा, लेकिन शिव की पूजा जारी रही। रामानुज के श्रीवैष्णव धर्म को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। हालाँकि, सभी राजा अन्य धर्मों और उनकी प्रथाओं के प्रति सहिष्णु थे।
- कला और स्थापत्य कला: विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अनेक मंदिर और महल बनवाए। विजयनगर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ ऊँचे राय गोपुरम या प्रवेशद्वार, मंदिर परिसर में नक्काशीदार स्तंभों वाले कल्याण मंडप, गर्भगृह और अम्मन मंदिर का निर्माण थीं।
- साहित्य: विजयनगर के शासकों ने संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल साहित्य को संरक्षण दिया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में साम्राज्य अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के चरम पर था। ‘आंध्र भोज’ के नाम से प्रसिद्ध, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में राजनीति पर एक पुस्तक ‘अमुक्तमाल्यद’ लिखी, जिसमें बताया गया है कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी, हम्पी, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थल कर्नाटक के तुंगभद्रा बेसिन में स्थित 14वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक की राजधानी के अवशेषों से युक्त है। यह विरुपाक्ष मंदिर सहित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।
स्रोत:
श्रेणी: इतिहास और संस्कृति
प्रसंग:
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया, जहां अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उन्हें रम्माण मुखौटा और राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले सदियों पुराने त्योहार पर एक पुस्तक भेंट की।

रम्माण महोत्सव के बारे में:
- स्थान: यह त्यौहार हर साल अप्रैल के अंत में उत्तराखंड के सलूर-डुंगरा नामक जुड़वां गांवों में मनाया जाता है।
- देवता: यह संरक्षक देवता, भूमियाल देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है।
- संबद्ध अनुष्ठान: यह आयोजन अत्यंत जटिल अनुष्ठानों से बना है। इसमें राम महाकाव्य और विभिन्न कथाओं का पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य शामिल हैं। इसमें जटिल अनुष्ठान, रामायण का पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक जाति और समूह अपनी अलग-अलग भूमिकाएँ निभाते हैं।
- मुखौटों पर जोर: भोजपत्र, हिमालयी सन्टी से बने 18 विभिन्न प्रकार के मुखौटे हैं, जिन्हें कलाकार कार्यक्रम के दौरान पहनते हैं।
- सामुदायिक भागीदारी: पूरे गांव के परिवार योगदान करते हैं; भूमिकाएं जाति-आधारित होती हैं (पुजारी, मुखौटा बनाने वाले, ढोल बजाने वाले), धन गांव से आता है, और भागीदारी बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक होती है।
- कला रूपों का सम्मिश्रण: यह वर्णन, मुखौटा नृत्य, अनुष्ठान नाटक, संगीत और मुखौटा शिल्प को एक एकीकृत उत्सव में मिश्रित करता है।
- प्रयुक्त वाद्य यंत्र: प्रलेखित कुछ वाद्य यंत्रों में ढोल (एक प्रकार का ढोल), दमाऊ (छोटा ढोल), मंजीरा (छोटा हाथ का झांझ), झांझर (बड़ा झांझ), भंकोरा (एक प्रकार का तुरही) शामिल हैं।
- महत्व: 2009 में, रम्मन को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था।
स्रोत:
(MAINS Focus)
(जीएस पेपर 3: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन)
पृष्ठभूमि
- 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) की मेजबानी ब्राजील के बेलेम शहर में की जाएगी, जो अमेज़न वर्षावन के मध्य में स्थित है — यह पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है।
- ब्राजील ने इससे पहले 1992 का अर्थ समिट (Earth Summit) आयोजित किया था, जिसने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण से संबंधित तीन प्रमुख वैश्विक कन्वेंशनों को जन्म दिया।
- तीन दशक बाद, COP30 अमेज़न की गोद में वापस लौटते हुए इस बात पर ज़ोर देता है कि अब जलवायु परिवर्तन पर वास्तविक और त्वरित कार्रवाई का समय आ गया है।
- राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के अनुसार, COP30 “सत्य का COP” होगा — ऐसा सम्मेलन जो केवल भाषणों तक सीमित न रहकर ठोस कार्रवाई का उदाहरण बने।
मुख्य विषय और मुद्दे
- भाषणों से आगे बढ़ने की आवश्यकता:
- COP30 को केवल वादों का मंच नहीं, बल्कि कार्रवाई का सम्मेलन बनना चाहिए।
- बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना:
- लूला ने वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता पर चिंता जताई और शासन सुधार की मांग की।
- समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ (CBDR):
- विकसित देशों को, जिन्होंने औद्योगिकीकरण से सर्वाधिक लाभ कमाया, अब विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- वैश्विक दक्षिण (Global South) की भूमिका:
- लूला ने कहा कि जलवायु वित्त तक पहुँच न्याय का प्रश्न है, न कि दान का।
- अमेज़न एक आशा का प्रतीक:
- ब्राजील ने पिछले दो वर्षों में वनों की कटाई को आधा कर दिया है, यह दिखाते हुए कि ठोस जलवायु कार्रवाई संभव है।
ब्राजील की प्रमुख पहलें
- Tropical Forests Forever Facility (TFFF):
- एक अभिनव फंड-आधारित व्यवस्था जो उन देशों को पुरस्कृत करेगी जो अपने वनों को संरक्षित रखते हैं।
- ब्राजील ने इसमें 1 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC):
- ब्राजील ने 59%–67% तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रखा है।
- ऊर्जा संक्रमण:
- ब्राजील की 88% ऊर्जा पहले से नवीकरणीय है (मुख्यतः हाइड्रो, बायोफ्यूल)।
- अब फोकस सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन पर है।
- सामाजिक आयाम:
- COP30 में एक नया घोषणापत्र — “Hunger, Poverty and Climate Declaration” जारी किया जाएगा, जो जलवायु कार्यवाही को गरीबी उन्मूलन से जोड़ेगा।
बहुआयामी विश्लेषण
- पर्यावरणीय आयाम
- अमेज़न की स्थिति जलवायु व जैव विविधता दोनों के लिए निर्णायक है।
- वनों की बहाली से कार्बन अवशोषण और अनुकूलन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।
- आर्थिक आयाम
- जीवाश्म ईंधन से हटना विकासशील देशों के लिए कठिन हो सकता है।
- लेकिन निवेश आधारित मॉडल (TFFF) निजी पूंजी को आकर्षित कर सकता है।
- शासन व राजनीतिक आयाम
- UN सुधार की वकालत की ताकि जलवायु शासन अधिक प्रभावी बने।
- यह वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व के उदय को भी दर्शाता है।
- सामाजिक व नैतिक आयाम
- जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग हैं।
- इसलिए न्यायसंगत और समावेशी विकास जलवायु नीति का केंद्र होना चाहिए।
लाभ
- वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मज़बूती
- जलवायु न्याय और CBDR की पुनर्पुष्टि
- नवीन फंडिंग मॉडल (TFFF) जो अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को जोड़ता है
- गरीबी उन्मूलन को जलवायु नीति से जोड़ना
- बहुपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करना
चुनौतियाँ
- वैश्विक राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
- निवेश आधारित मॉडल में कमज़ोर देशों की भागीदारी सीमित हो सकती है
- घरेलू स्तर पर कृषि व उद्योग लॉबी का दबाव
- विकसित देशों की वित्तीय प्रतिबद्धता में असफलता
- COP30 के “सत्य सम्मेलन” बनने की संभावना केवल शब्दों तक सीमित रह सकती है
आगे की राह
- जवाबदेही और पारदर्शिता को संस्थागत बनाना
- तकनीकी व वित्तीय सहयोग को मजबूत करना
- स्थानीय व आदिवासी समुदायों को नीति निर्माण में शामिल करना
- जलवायु कार्रवाई को गरीबी उन्मूलन व सामाजिक न्याय से जोड़ना
मुख्य अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: COP30 को “सत्य का COP” कहा गया है। अमेज़न क्षेत्र में इसके आयोजन का महत्व स्पष्ट कीजिए और बताइए कि यह वैश्विक जलवायु शासन, समानता और सतत विकास के नए आयामों को कैसे दर्शाता है। (250 शब्द)
(जीएस पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, जीएस पेपर 2: शासन, जीएस पेपर 4: शासन में नैतिकता)
पृष्ठभूमि
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IndiaAI मिशन के तहत IndiaAI Governance Guidelines जारी की हैं।
- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य जिम्मेदार और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करना है।
- यह पहल तेजी से बढ़ते डीपफेक, डेटा दुरुपयोग, भेदभावपूर्ण एल्गोरिद्म और निजता के उल्लंघन जैसे जोखिमों के मद्देनज़र आई है।
- यह मॉडल “टेक्नो-लीगल गवर्नेंस” की दिशा में भारत का कदम है — यानी तकनीक और कानून का संयुक्त नियमन।
मुख्य विशेषताएँ
- चरणबद्ध कार्यान्वयन:
- AI नियमन को तुरंत लागू करने की बजाय धीरे-धीरे लागू करने की योजना ताकि नवाचार बना रहे।
- नए निगरानी निकाय:
- जैसे AI Safety Institute, AI Policy Expert Committee, और AI Governance Group।
- जोखिम वर्गीकरण ढांचा:
- AI अनुप्रयोगों को उनके जोखिम स्तर (निम्न, मध्यम, उच्च) के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा।
- घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रणाली:
- AI से संबंधित त्रुटियों या नैतिक उल्लंघनों की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
- “Automatic by Design” दृष्टिकोण:
- AI सिस्टम में सुरक्षा व पारदर्शिता के उपाय स्वतः अंतर्निहित होंगे।
- मौजूदा कानूनों के साथ समन्वय:
- IT अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम (DPDP), और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों से जोड़ा गया है।
- सात मूल सिद्धांत (IIT मद्रास समिति):
- पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, समझाने योग्य प्रणाली, नवाचार, समानता और समावेशिता।
सरकार का दृष्टिकोण
- आईटी सचिव एस. कृष्णन के अनुसार, भारत “नवाचार-प्रथम दृष्टिकोण” अपनाएगा, और जब आवश्यकता होगी तभी कठोर नियमन किया जाएगा।
- उद्देश्य है — मानव-केंद्रित विकास और विश्वसनीय AI इकोसिस्टम का निर्माण।
बहुआयामी विश्लेषण
- तकनीकी आयाम
- राष्ट्रीय स्तर पर AI सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में कदम।
- यह पहल भारत को EU AI Act और US AI Executive Order जैसे वैश्विक फ्रेमवर्क्स की श्रेणी में खड़ा करती है।
- कानूनी और नैतिक आयाम
- पारदर्शिता, समझाने योग्यता और जवाबदेही को केंद्र में रखता है।
- मौजूदा कानूनों के साथ समन्वित नीति अपनाई गई है।
- आर्थिक आयाम
- यह नीति स्टार्टअप्स और इनोवेशन सेक्टर को प्रोत्साहन देगी।
- निवेशकों को नियामक स्थिरता और विश्वास मिलेगा।
- परन्तु अत्यधिक नियमन से छोटे उद्योगों पर भार बढ़ सकता है।
- सामाजिक व शासन आयाम
- यह नागरिकों के बीच AI पर भरोसा पैदा करेगा।
- चुनावों, सूचना प्रवाह और सामाजिक न्याय में AI के दुरुपयोग को रोकेगा।
- अंतरराष्ट्रीय आयाम
- भारत की यह नीति वैश्विक दक्षिण के लिए वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करती है — जो नैतिकता और विकास दोनों पर आधारित है।
लाभ
- संतुलित और समावेशी ढांचा
- AI दुरुपयोग (Deepfakes आदि) के खिलाफ सक्रिय कदम
- “टेक्नो-लीगल” दृष्टिकोण
- डेटा संरक्षण कानूनों के साथ संगति
- AI पर नागरिकों का विश्वास मजबूत करना
चुनौतियाँ
- कार्यान्वयन में कौशल और संसाधनों की कमी
- कई निकायों से संचालन में जटिलता
- नवाचार और नियमन के बीच संतुलन कठिन
- अंतरराष्ट्रीय मानकों से संगति बनाए रखना
- नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में लागू करना कठिन
आगे की राह
- AI साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
- स्वतंत्र ऑडिट और पारदर्शिता रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना
- शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और नागरिक समाज में सहयोग
- वैश्विक AI सुरक्षा शोध सहयोग को मजबूत करना
- लगातार समीक्षा और अनुकूल शासन मॉडल अपनाना
निष्कर्ष
भारत की नई AI गवर्नेंस गाइडलाइन्स नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए जिम्मेदार AI उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
यह पहल न केवल प्रौद्योगिकीय सुरक्षा बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही और मानव कल्याण को केंद्र में रखती है।
भारत अब नैतिक, समावेशी और विकासोन्मुख AI शासन का वैश्विक उदाहरण बनने की ओर अग्रसर है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: भारत की नई AI शासन दिशानिर्देशों का उद्देश्य जिम्मेदार और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र का निर्माण करना है। विश्लेषण कीजिए कि भारत कैसे नवाचार, नैतिकता और नियमन के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। (250 शब्द)
Source : https://epaper.indianexpress.com/4076464/Delhi/November-06-2025#page/15/2











