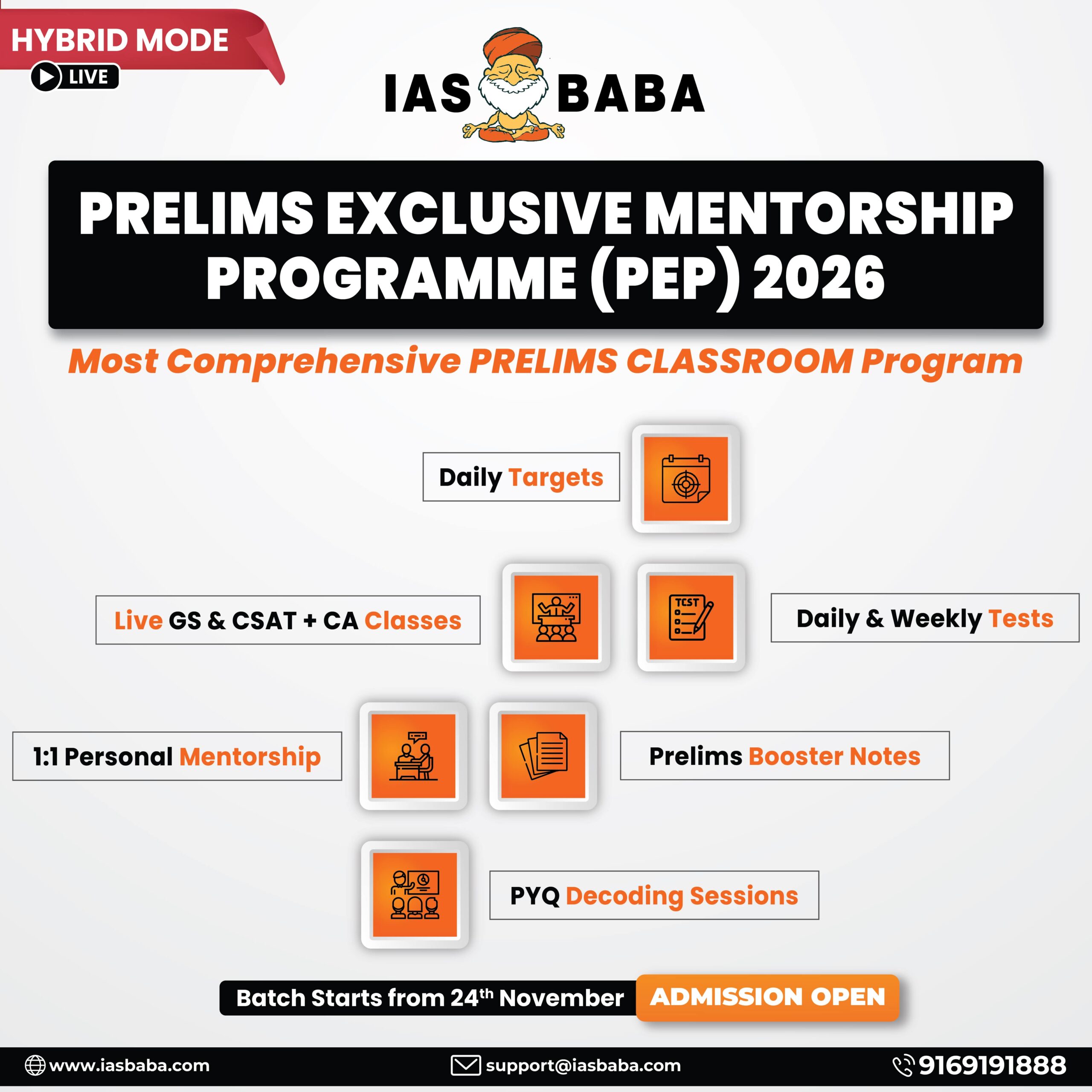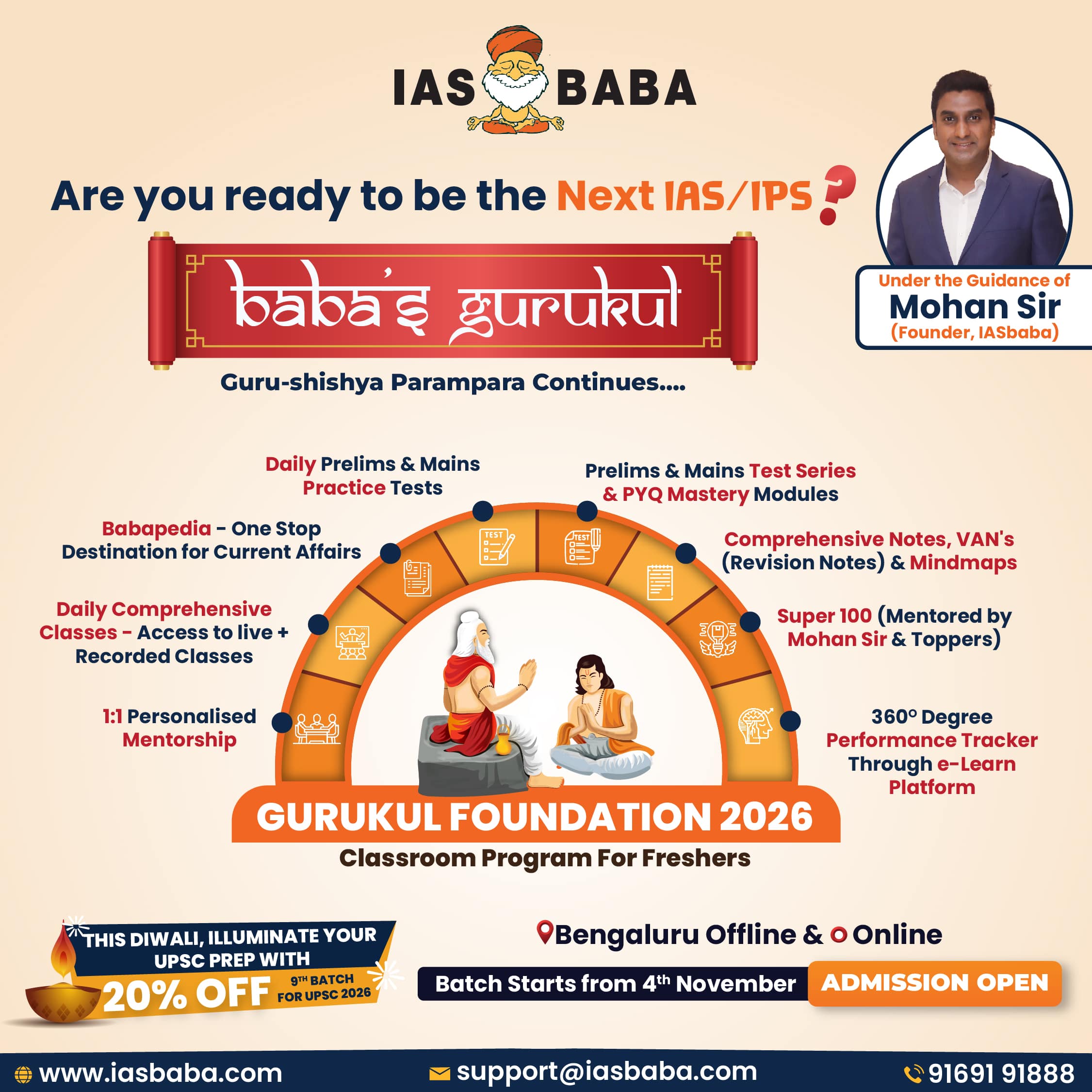IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा
प्रसंग:
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (एसईडी) ने भारत में हैमर वेपन सिस्टम के उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
हैमर वेपन सिस्टम के बारे में:
- नामकरण: हैमर (HAMMER) का पूरा नाम हाइली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज (Highly Agile and Manoeuvrable Munition Extended Range) है। इसे ग्लाइड बम के नाम से भी जाना जाता है।
- प्रकृति: यह एक एयर-टू-ग्राउंड प्रिसिजन-गाइडेड हथियार प्रणाली है और इसे 250 किग्रा, 500 किग्रा और 1,000 किग्रा वजन के मानक बमों पर लगाया जा सकता है।
- विकास: मूल रूप से फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (एसईडी) द्वारा विकसित, अब इसके भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ संयुक्त निर्माण की तैयारी है।
- सीमा: हैमर प्रिसिजन-गाइडेड म्युनिशन्स की सीमा 70 किमी तक है।
- रोकना मुश्किल: यह जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी है, और दुर्गम इलाके में कम ऊंचाई से लॉन्च करने में सक्षम है। इसे रोकना मुश्किल है और यह मजबूत संरचनाओं में भी घुस सकता है।
- गतिशीलता: यह पर्वतीय युद्ध (जैसे, लद्दाख) के लिए अनुकूलित है, जो जटिल स्थलाकृति और उच्च-ऊंचाई वाले वातावरण में भी सटीक हमलों की अनुमति देता है।
- विशिष्टता: यह एक सटीक-निर्देशित हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिजाइन के लिए जानी जाती है, जिससे यह राफेल और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सहित कई प्लेटफार्मों के लिए अनुकूलनीय है।
- समझौते का महत्व: यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के दौरान 2020 में अपने राफेल लड़ाकू विमानों को लैस करने के लिए फ्रांस से अन्य हथियारों के साथ इस हथियार प्रणाली का ऑर्डर दिया था।
स्रोत:
- द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान
प्रसंग:
- हाल ही में, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इनफार्मेशन मैनेजमेंट (APDIM) का 10वां सत्र नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया।
एपीडीआईएम के बारे में:
- नामकरण: एपीडीआईएम (APDIM) का पूरा नाम एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इनफार्मेशन मैनेजमेंट है।
- प्रकृति: यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ESCAP) की एक क्षेत्रीय संस्था है।
- विजन: इसका विजन यह सुनिश्चित करना है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए प्रभावी आपदा जोखिम सूचना का उत्पादन और उपयोग किया जाए।
- जनादेश: इसका लक्ष्य प्राकृतिक खतरों के कारण मानवीय और भौतिक नुकसान को कम करना और आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन नीतियों के प्रभावी डिजाइन, निवेश और कार्यान्वयन में योगदान देना है।
- प्रशासन: इसका संचालन एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है जिसमें आठ ESCAP सदस्य देश तीन साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं (भारत 2022 से 2025 तक की अवधि के लिए सदस्यों में से एक है)।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय तेहरान, ईरान में स्थित है।
- कार्य: यह विज्ञान-नीति इंटरफेस को मजबूत करने के लिए एक क्षेत्रीय सुविधा के रूप में कार्य करता है। यह प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है, संवाद को सुगम बनाता है।
- देशों के बीच आपदा प्रबंधन को सुगम बनाता है: यह क्षेत्र के देशों के बीच और उसके अन्दर स्वयं आपदा सूचना प्रबंधन में विशेषज्ञता, अनुभवों और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है।
- ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है: यह एक क्षेत्रीय ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है, आपदा-संबंधी डेटा को समेकित और साझा करता है, सूचना प्रणालियों को मजबूत करता है और सीमा-पार खतरों पर सहयोग का समर्थन करता है।
स्रोत:
-
- पीआईबी
श्रेणी: भूगोल
प्रसंग:
- इथियोपिया के अफ़ार क्षेत्र में स्थित हायली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद फट गया।
हायली गुब्बी ज्वालामुखी के बारे में:
- स्थान: हायली गुब्बी ज्वालामुखी पूर्वोत्तर इथियोपिया के अफ़ार में, दानाकिल डिप्रेशन के भीतर स्थित है – जो पृथ्वी पर सबसे गर्म और निम्न स्थानों में से एक है।
- भूकंपीय गतिविधि का हॉटस्पॉट: अफ़ार ट्रिपल जंक्शन, जहां रेड सी रिफ्ट, गल्फ ऑफ अदन रिफ्ट और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट मिलते हैं, यह क्षेत्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि का हॉटस्पॉट बनाते हैं।
- विशिष्टता: वर्तमान विस्फोट अद्वितीय है क्योंकि अफ़ार रिफ्ट के भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों के बाद फटा है।
- ज्वालामुखीय प्लम की संरचना: राख के बादल में ज्वालामुखीय राख, सल्फर डाइऑक्साइड, कांच के टुकड़े और चट्टान के टुकड़ों का मिश्रण था, जो 15,000-45,000 फीट की ऊंचाई के बीच उच्च स्तर पर पहुंचाया गया था। ये एरोसोल हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय स्थिरता के आधार पर दिनों से लेकर हफ्तों तक वातावरण में बने रह सकते हैं।
- महत्व: हायली गुब्बी विस्फोट पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट सिस्टम (ईएआरएस) की भूवैज्ञानिक अस्थिरता को उजागर करता है, जहां सक्रिय ज्वालामुखीवाद, दरार विस्फोट और फैलते रिज आम हैं।
- अलग हो रही प्लेटों के जंक्शन पर: यह विश्व की सबसे अधिक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय रिफ्ट प्रणालियों में से एक है जहां अरब, नूबियन और सोमाली प्लेटें अलग हो रही हैं।
- बेसाल्टिक लावा की विशेषता: यह क्षेत्र बेसाल्टिक लावा, फिशर सिस्टम और महाद्वीपीय रिफ्टिंग प्रक्रिया से जुड़ी लगातार भूकंपीय गतिविधि की विशेषता है।
स्रोत:
- द हिंदू
श्रेणी: राज्यव्यवस्था और शासन
प्रसंग:
- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की खारिज होने से आपत्तिजनक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में विलय (merger) नहीं होता है।
विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के बारे में:
- परिभाषा: एक एसएलपी सर्वोच्च न्यायालय से की गई एक अनुरोध है जो किसी भी न्यायालय या अधिकरण (सैन्य अधिकरणों को छोड़कर) के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति मांगता है, भले ही कानून अपील का वैधानिक अधिकार प्रदान नहीं करता हो।
- अधिकार नहीं: विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) एक अधिकार नहीं है – यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विवेक से प्रदान की जाने वाली एक विशेषाधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक विवेकाधीन/वैकल्पिक शक्ति है, और न्यायालय अपने विवेक से अपील स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, अपने विवेक से, भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण या आदेश से अपील की विशेष अनुमति दे सकता है।
- एसएलपी का उपयोग करने की शर्तें: इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न या स्थूल अन्याय हुआ हो। एसएलपी के लिए एक निर्णय, डिक्री, या आदेश अंतिम होना आवश्यक नहीं है। एक अंतरिम या अंतरावर्ती आदेश या डिक्री को भी चुनौती दी जा सकती है।
- कौन दायर कर सकता है: एसएलपी कोई भी पीड़ित पक्ष (व्यक्ति या व्यवसाय), सरकारी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या गैर-सरकारी संगठन या संघ (प्रासंगिक मामलों में) दायर कर सकता है।
- किसके खिलाफ दायर की जा सकती है: एसएलपी उच्च न्यायालयों, अधिकरणों (सशस्त्र बलों के तहत आने वालों को छोड़कर) या अर्ध-न्यायिक निकायों के निर्णयों के खिलाफ दायर की जा सकती है।
- एसएलपी दायर करने की समय सीमा: उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के खिलाफ निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर एसएलपी दायर की जा सकती है या उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र देने से इनकार करता है, के खिलाफ 60 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।
- एसएलपी की प्रक्रिया: एक एसएलपी में उन सभी तथ्यों को शामिल करना होगा जिन पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है, जो उन आधारों के इर्द-गिर्द घूमते हैं जिन पर एसएलपी दायर की जा सकती है। कही गई याचिका पर एक अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दस्तखत किए जाने की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता को एसएलपी के अंतर्गत यह बयान शामिल करना होगा कि उच्च न्यायालय में कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति: एक बार याचिका दायर हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट पीड़ित पक्ष की सुनवाई करेगा और मामले की ताकत के आधार पर, विपरीत पक्ष को एक जवाबी हलफनामे में अपना पक्ष रखने की अनुमति देगा। सुनवाई के बाद, यदि न्यायालय मामले को आगे की सुनवाई के लिए उपयुक्त पाता है, तो वह इसे स्वीकार करेगा; अन्यथा, यह अपील को खारिज कर देगा।
स्रोत:
- लाइव लॉ
श्रेणी: सरकारी योजनाएं
प्रसंग:
- भारत की वाहन सुरक्षा रोडमैप में एक बड़ा उन्नयन होने जा रहा है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत एनसीएपी 2.0 के लिए एक मसौदा जारी किया है।
भारत एनसीएपी के बारे में:
- प्रकृति: भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) कारों की क्रैश टेस्टिंग के लिए एक स्वदेशी स्टार-रेटिंग सिस्टम है, जिसके तहत वाहनों को एक से पांच सितारों के बीच रेटिंग दी जाएगी, जो टक्कर में उनकी सुरक्षा को दर्शाती है।
- साझेदारी: यह भारत सरकार (GoI) और ग्लोबल एनसीएपी, सुरक्षा क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के पीछे नियामक निकाय, के बीच एक महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजना है।
- लॉन्च: इसे 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था और 1 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया था।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कार खरीदने से पहले एक सूचित निर्णय लेने में मदद करना है, जिससे सुरक्षित कारों की मांग बढ़े।
- नोडल मंत्रालय: भारत एनसीएपी सड़क परिवहन मंत्रालय की देखरेख में है, लेकिन एक स्वतंत्र निकाय है।
- परीक्षण प्रोटोकॉल: भारत एनसीएपी के तहत, ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा स्वेच्छा से नामित कारों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 197 में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार क्रैश टेस्ट किया जाएगा।
- सुरक्षा डोमेन: भारत एनसीएपी के तहत परीक्षण किए गए वाहनों का मूल्यांकान तीन महत्वपूर्ण सुरक्षा डोमेन में किया जाता है- वयस्क अधिभोगी सुरक्षा, बाल अधिभोगी सुरक्षा, और सुरक्षा सहायक प्रौद्योगिकियां।
- लागू होना: केवल भारत में बिकने वाले दाएं हाथ वाले यात्री वाहन और 3,500 किग्रा से कम वजन वाले वाहन ही विचार के लिए पात्र हैं। कारों के बेस वेरिएंट का परीक्षण किया जाना है, और रेटिंग चार साल के लिए लागू होंगी।
- पात्र वाहन: आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) मॉडलों के अलावा, सीएनजी कारों के साथ-साथ बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन भी सुरक्षा परीक्षण के लिए पात्र हैं।
- स्वैच्छिक प्रकृति: यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसके तहत स्टार रेटिंग के लिए आकलन के लिए कार की लागत और ऐसे आकलन की लागत संबंधित वाहन निर्माता या आयातक द्वारा वहन की जाती है।
- वैधता: वर्तमान भारत एनसीएपी विनियम 30 सितंबर, 2027 तक वैध हैं, जिसके बाद भारत एनसीएपी 2.0 को अक्टूबर 2027 तक लागू होने की उम्मीद है।
भारत एनसीएपी 2.0 मसौदा दिशानिर्देशों के बारे में:
- 5 स्तंभों पर आधारित: भारत एनसीएपी 2.0 प्रस्ताव पांच स्तंभों- क्रैश प्रोटेक्शन, कमजोर सड़क-उपयोगकर्ता सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटना परिहार, और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी में 100-अंकों की रेटिंग प्रणाली पेश करता है।
- रेटिंग सिस्टम में न्यूनतम स्कोर का उपयोग: 2027-29 से, 5-स्टार रेटिंग के लिए 70 अंकों की आवश्यकता होगी, और यह 2029-31 से बढ़कर 80 अंक हो जाएगी। न्यूनतम स्कोर प्रत्येक स्तंभ में भी लागू होंगे।
- अद्यतन मानदंड: यह ताजा अनिवार्य परीक्षण, संशोधित स्कोरिंग विधियां और अद्यतन सुरक्षा ऊर्ध्वाधर लाता है।
- विशिष्टता: विशेष रूप से, पहली बार, वाहनों का आकलन कमजोर सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा पर किया जाएगा।
- क्रैश टेस्ट का विस्तार: क्रैश टेस्ट को दो से बढ़ाकर पांच कर दिया जाएगा और अब परीक्षण के लिए पुरुष, महिला और बच्चे के डमी होंगे। कारों को ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट, फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट, और रियर इम्पैक्ट से गुजरना होगा।
- पर्दे वाले एयरबैग अनिवार्य: इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी) और पर्दे वाले एयरबैग किसी भी मॉडल के लिए स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होंगे।
स्रोत:
- इंडिया टुडे
(MAINS Focus)
(यूपीएससी जीएस पेपर II -- "कमजोर वर्गों के लिए तंत्र, कानून, संस्थान; महिलाओं से संबंधित मुद्दे")
प्रसंग (परिचय)
चंडीगढ़ का एक हालिया मामला, जहां पॉश अधिनियम के तहत आईसीसी जांच के बाद एक कॉलेज प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया था, ने कम दोषसिद्धि दर, प्रक्रियात्मक कमियों, डिजिटल युग की चुनौतियों और शैक्षणिक संस्थानों में सूचित सहमति और शक्ति असमानता को संबोधित करने में अधिनियम की अक्षमता पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है।
मुख्य तर्क
- वैचारिक स्पष्टता: कार्यस्थलों और विश्वविद्यालयों में हेरफेर, भावनात्मक जबरदस्ती और शक्ति असमानता को नजरअंदाज करते हुए सूचित सहमति को मान्यता दिए बिना अधिनियम का सहमति पर ध्यान केंद्रित करना।
- भावनात्मक शोषण: झूठे रिश्तों से उत्पन्न भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, हालांकि पदानुक्रमित व्यवस्था में दुर्व्यवहार का एक प्रमुख रूप है, अधिनियम के दायरे से बाहर रहता है।
- समय-सीमा से बंधा न्याय: तीन महीने की सीमा अवधि उन पीड़ितों को हतोत्साहित करती है जिन्हें अक्सर हेरफेर को पहचानने, सबूत जुटाने और संस्थागत प्रतिक्रिया के डर पर काबू पाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।
- कमजोर शब्दावली: आरोपी को "अभियुक्त" के बजाय "प्रतिवादी" कहकर कार्यस्थलों के बाहर होने वाले समान कृत्यों की तुलना में यौन उत्पीड़न की गंभीरता को प्रतीकात्मक रूप से कम करके आंका जाता है।
- व्यवहारिक साक्ष्य: अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण आईसीसी सीधे सबूतों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, परिस्थितिजन्य संकेतकों या व्यवहार पैटर्न को नजरअंदाज कर देते हैं जो आमतौर पर उत्पीड़न के मामलों की विशेषता रखते हैं।
चुनौतियाँ / आलोचनाएँ
- अंतर-संस्थागत अनदेखी: शिक्षा जगत में लगातार अंतर-संस्थागत वार्ता के बावजूद, अधिनियम में कई परिसरों में फैले दुर्व्यवहार को संबोधित करने के तंत्र का अभाव है।
- प्रक्रियात्मक आघात: शिकायतकर्ताओं को अक्सर देरी, संस्थागत हिचकिचाहट, भावनात्मक थकान और "दुर्भावनापूर्ण शिकायत" धारा के तहत प्रतिकार के डर का सामना करना पड़ता है।
- डिजिटल साक्ष्यों में कमियाँ: कानूनी और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण आईसीसी गायब होने वाले संदेशों, एन्क्रिप्टेड चैट, सिंगल-व्यू फोटो जैसे आधुनिक डिजिटल सबूतों की व्याख्या करने में संघर्ष करते हैं।
- संस्थागत अप्रस्तुतता: आईसीसी असमान रूप से प्रशिक्षित रहते हैं और अक्सर जोखिम-रोधी होते हैं, जो अनजाने में कमजोर शिकायतकर्ताओं पर शक्तिशाली अपराधियों के लिए सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
- मूक सीरियल अपराधी: सूचना-साझाकरण या अंतर-संस्थागत समन्वय की अनुपस्थिति सीरियल अपराधियों को कई शैक्षणिक वातावरणों का शोषण जारी रखने में सक्षम बनाती है।
आगे की राह
- परिभाषाओं का विस्तार करें: समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए सूचित सहमति, भावनात्मक जबरदस्ती और डिजिटल उत्पीड़न को वैधानिक परिभाषाओं में शामिल करें।
- समयसीमा बढ़ाएँ: विलंबित मान्यता या डर के कारण पीड़ितों को न्याय से वंचित न करने के लिए तीन-माह की सीमा अवधि बढ़ाएँ या हटाएँ।
- साक्ष्य प्रोटोकॉल में सुधार करें: डिजिटल सबूतों को संभालने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित करें और आईसीसी आकलन में पुष्टिकरण या व्यवहार संबंधी संकेतकों के उपयोग का विस्तार करें।
- आईसीसी क्षमता निर्माण: संवेदनशीलता और सबूत मूल्यांकन में सुधार के लिए आईसीसी सदस्यों के लिए नियमित कानूनी, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य करें।
- अंतर-संस्थागत तंत्र: धारावाहिक दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सिद्ध अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने में संस्थानों को सक्षम बनाने वाली एक गोपनीय राष्ट्रीय या क्षेत्रीय रजिस्ट्री बनाएँ।
निष्कर्ष
पॉश अधिनियम 2013 में क्रांतिकारी था, लेकिन विकसित हो रहे शक्ति संरचनाओं, डिजिटल इंटरैक्शन और भावनात्मक हेरफेर के लिए 2025 में एक मजबूत, स्पष्ट, पीड़ित-केंद्रित कानून की मांग करते हैं।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
एक मील का पत्थर होने के बावजूद, पॉश अधिनियम, 2013 उन कमियों का सामना करता है जो इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं। इन चुनौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें और महिलाओं के लिए कार्यस्थल न्याय को मजबूत करने के लिए सुधार सुझाएं। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द हिंदू
(यूपीएससी जीएस पेपर II — “कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ; यूपीएससी की भूमिका”)
प्रसंग (परिचय)
मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति से पहले तमिलनाडु की एक नियमित डीजीपी की नियुक्ति करने में असमर्थता, यूपीएससी पैनल की अस्वीकृति और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अवमानना के आरोपों ने राज्य स्वायत्तता, पुलिस सुधारों और केंद्र-राज्य समन्वय पर बहस को फिर से भड़का दिया है।
मुख्य तर्क: मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है
- प्रकाश सिंह आदेश: 2006 के फैसले में राज्यों को केवल सेवा की लंबाई, रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर तीन वरिष्ठतम पात्र आईपीएस अधिकारियों के यूपीएससी-अनुमोदित पैनल से ही डीजीपी का चयन करना अनिवार्य किया गया है।
- कार्यकाल सुरक्षा: न्यायालय की डीजीपी के लिए न्यूनतम दो वर्ष की निश्चित अवधि की आवश्यकता पुलिस नेतृत्व को अराजनीतिक बनाने और प्रशासनिक निरंतरता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- प्रक्रियात्मक समयसीमा: राज्यों को यूपीएससी को अनुमानित रिक्ति से तीन महीने पहले प्रस्ताव भेजने होते हैं, एक नियम जिसका तमिलनाडु ने सेवानिवृत्ति से केवल एक दिन पहले अपनी सूची जमा करके उल्लंघन किया।
- स्वायत्तता बनाम निगरानी: यूपीएससी पैनल को “अस्वीकार्य” के रूप में राज्य की अस्वीकृति राज्य की पसंद और यूपीएससी-अनिवार्य योग्यता-आधारित चयन के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती है।
- न्यायिक हस्तक्षेप: यूपीएससी की सिफारिशों के बाद तत्काल नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अनुरोध पुलिस सुधार अनुपालन को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
चुनौतियाँ / आलोचनाएँ
- विलंबित अनुपालन: तीन-माह की प्रस्ताव समयसीमा को पूरा करने में तमिलनाडु की विफलता ने चयन प्रक्रिया को बाधित किया और न्यायिक जांच को आमंत्रित किया।
- कैट कार्यवाही: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष लंबित मुकदमेबाजी ने राज्य की कार्रवाइयों में देरी की, फिर भी न्यायालय ने माना कि यह प्रक्रियात्मक अनुपालन न होने का औचित्य नहीं बना सकता।
- पैनल अस्वीकृति: यूपीएससी पैनल पर तमिलनाडु की आपत्ति और एक और बैठक का अनुरोध प्रकाश सिंह में निर्धारित संरचित प्रक्रिया के विपरीत था।
- अवमानना आरोप: एक नियमित के बजाय “प्रभारी” डीजीपी की नियुक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना के आरोपों वाली अवमानना याचिकाओं को जन्म दिया है।
आगे की राह
- सख्त पालन: पुलिस नेतृत्व में पारदर्शिता, स्थिरता और अराजनीतिकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को प्रकाश सिंह ढांचे का पालन करना चाहिए।
- समयसीमा अनुशासन: आंतरिक अनुस्मारक और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को संस्थागत बनाने से अंतिम समय की जमाओं को रोका जा सकता है जो चयन प्रक्रिया को पटरी से उतार देते हैं।
- ईमानदारी पारदर्शिता: ईमानदारी प्रमाणपत्र रोकने के स्पष्ट, दर्ज कारणों को मनमानी को रोकने के लिए यूपीएससी के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- सहयोगात्मक संघवाद: राज्य सरकारों और यूपीएससी के बीच संरचित परामर्श योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया का सम्मान करते हुए संघर्ष को कम कर सकता है।
- निगरानी तंत्र: सर्वोच्च न्यायालय या एक स्वतंत्र निगरानी निकाय द्वारा एक आवधिक अनुपालन ऑडिट देश भर में पुलिस सुधार कार्यान्वयन को मजबूत कर सकता है।
निष्कर्ष
तमिलनाडु में डीजीपी नियुक्ति विवाद राजनीतिक विवेक और न्यायिक रूप से अनिवार्य पुलिस सुधारों के बीच अनसुलझे तनाव को उजागर करता है। एक पेशेवर, स्वतंत्र पुलिस नेतृत्व के निर्माण के लिए योग्यता-आधारित चयन, पारदर्शी प्रक्रियाओं और समय पर समन्वय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्र. प्रकाश सिंह सुधारों का लक्ष्य पारदर्शी और योग्यता-आधारित नियुक्तियों के माध्यम से पुलिस नेतृत्व को अराजनीतिक बनाना था। चर्चा करें। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: द हिंदू
(यूपीएससी जीएस पेपर II — “भारतीय संविधान—विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान; अन्य संविधानों के साथ तुलना”)
प्रसंग (परिचय)
जैसे ही भारत संविधान के अंगीकरण के 76 वर्ष पूरे करता है, नवीन विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे इसके निर्माताओं ने जानबूझकर पश्चिमी संवैधानिक मॉडलों से आगे बढ़कर, एक परिवर्तनकारी चार्टर को डिजाइन किया जिसने भारत के सामाजिक ताने-बाने में निहित सामाजिक पदानुक्रम, समूह अधिकारों और संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित किया।
भारत का संवैधानिक दृष्टिकोण अपने समय से आगे क्यों था
- परिवर्तनकारी समानता: संविधान ने अनुच्छेद 14, 15(2), 17, और 23 के माध्यम से राज्य और निजी अभिकर्ताओं दोनों से जाति-आधारित भेदभाव को मान्यता देकर समानता का पश्चिमी धारणाओं से परे विस्तार किया।
- सामाजिक शक्ति मान्यता: यह स्वीकार करके कि भारत में शक्ति न केवल राज्य बल्कि पुरजोर सामाजिक समूहों द्वारा भी चलाई जाती है, संविधान ने सामाजिक पदानुक्रमों को खत्म करने के लिए राज्य कार्रवाई अनिवार्य की।
- सकारात्मक कार्रवाई नेतृत्व: भारत ने 1950 में संवैधानिक रूप से अनुमोदित आरक्षण शुरू किया, यू.एस. नागरिक अधिकार सुधारों से एक दशक पहले, जिससे यह समूह-विभेदित अधिकारों में एक वैश्विक अग्रणी बन गया।
- धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद: संविधान ने एक सूक्ष्म धर्मनिरपेक्ष ढांचा अपनाया—राज्य धर्म को त्यागते हुए, अनिवार्य धार्मिक करों (अनुच्छेद 27) को प्रतिबंधित किया और व्यक्तिगत (अनुच्छेद 25) और समूह धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26) की रक्षा की।
- अल्पसंख्यक सांस्कृतिक अधिकार: अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से, संविधान ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया, जिससे बहुलवादी राष्ट्र-निर्माण सुनिश्चित हुआ।
चुनौतियाँ / आलोचनाएँ
- आंशिक अधिकार संरक्षण: औपनिवेशिक युग के आपातकालीन प्रावधानों के कारण कुछ स्वतंत्रताएं सीमित रहीं, जिससे सरकारों को व्यापक परिस्थितियों में अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति मिली।
- कार्यपालिका का वर्चस्व: संविधान ने व्यापक विवेकाधीन शक्तियों वाली एक शक्तिशाली कार्यपालिका बनाई, जिससे नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षा उपायों पर चिंताएं बढ़ीं।
- असमान बहुलवाद: हालांकि अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक संरक्षण मौजूद हैं, लेकिन कभी-कभी उनके दायरे को कम कर दिया गया है या असंगत रूप से लागू किया गया है।
- समूह अधिकारों पर बहस: गहन संविधान सभा की बहसों ने समानता और विभेदित संरक्षण के बीच तनाव को दर्शाया, जिससे कुछ अस्पष्टताएं अनसुलझी रह गईं।
- उपचारों की सीमाएँ: न्यायिक समीक्षा मौजूद है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में अधिकारों के निलंबित होने पर उपचारों तक पहुंच सीमित हो सकती है।
संविधान के परिवर्तनकारी वादे को गहरा करना
- सामाजिक समानता को मजबूत करें: अनुच्छेद 15(2) और 17 के मजबूत कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक जनादेशों को सुदृढ़ करें।
- कार्यपालिका शक्ति संतुलन: कार्यपालिका अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपातकालीन प्रावधानों को फिर से देखें और संस्थागत जांच बढ़ाएँ।
- बहुलवादी शासन को बढ़ावा दें: भारत के बहुलवाद को व्यवहार में बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को लगातार कायम रखें।
- अधिकार जागरूकता का विस्तार करें: न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संवैधानिक अधिकारों पर नागरिक शिक्षा और सार्वजनिक साक्षरता बढ़ाएँ।
- परिवर्तनकारी दृष्टि की रक्षा करें: संरचनात्मक असमानता के खिलाफ मूलभूत उपक के रूप में सकारात्मक कार्रवाई और समूह-विभेदित अधिकारों की रक्षा करें।
निष्कर्ष
भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी परियोजना है जो गहरी सामाजिक असमानताओं और बहुल पहचानों को स्वीकार करती है। इसकी स्थायित्व समानता के प्रति एक प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो विविधता का सम्मान करती है, यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक दीर्घायु एकरूपता से नहीं, बल्कि अंतर के समावेशी मान्यता से उत्पन्न होती है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्र. भारतीय संविधान ने जानबूझकर पश्चिमी उदारवादी संवैधानिकता से परे जाने का रास्ता अपनाया। समालोचनात्मक रूप से जांच करें कि कैसे इस परिवर्तनकारी दृष्टि ने भारत के संवैधानिक अनुभव को आकार दिया है। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस