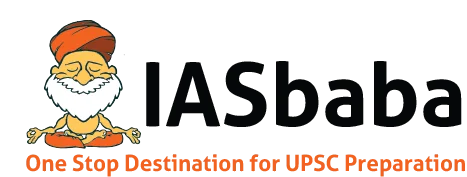IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी
rchives
(PRELIMS Focus)
श्रेणी: कृषि
संदर्भ: कृषि निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव
भारत का बढ़ता कृषि निर्यात
- निर्यात प्रदर्शन: भारत ने 2024-25 में 51.94 बिलियन डॉलर मूल्य की कृषि वस्तुओं का निर्यात किया (अप्रैल-जून डेटा वार्षिकीकृत), जो वर्ष-दर-वर्ष 5.84% अधिक है।
- प्रमुख निर्यात वस्तुएँ: समुद्री उत्पाद, चावल (बासमती और गैर-बासमती), मसाले, भैंस का मांस, कॉफी, फल और सब्जियां, चीनी, तंबाकू, प्रसंस्कृत फल एवं सब्ज़ियां, अरंडी का तेल, तिलहन और ऑयलमील ।
- शीर्ष लाभकर्ता: गैर-बासमती चावल (+11.54%), तंबाकू (+19.29%), कॉफी (+13.87%), और प्रसंस्कृत फल एवं सब्ज़ियां (+12.08%)।
- शीर्ष गिरावट वाले: समुद्री उत्पाद (-19.45%), तिलहन (-12.58%), ऑयलमील (-5.24%)।
- व्यापार अधिशेष: कृषि निर्यात ($51.9B) आयात ($38.5B) से अधिक है, लेकिन अधिशेष एक दशक पहले की तुलना में आधा रह गया है।
- वृद्धि कारक: वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि (एफएओ सूचकांक), कुछ वस्तुओं की मजबूत मांग, निर्यात प्रतिबंधों में ढील, तथा प्याज, कॉफी और तंबाकू की कीमतों में वृद्धि।
- जोखिम: ट्रम्प की नीतियों के तहत संभावित अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट।
- वैश्विक संदर्भ: ब्राजील, जिम्बाब्वे जैसे देशों से मांग में वृद्धि; प्याज निर्यात प्रतिबंध जैसे घरेलू उपाय हटाये गये; कुछ देशों में सूखे के प्रभाव से निर्यात को मदद मिली।
Learning Corner:
भारत का निर्यात
अवलोकन
- भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 20 सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापारिक निर्यात 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जबकि सेवाओं का निर्यात 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जिससे भारत सेवाओं में शुद्ध निर्यातक बन गया।
- प्रमुख निर्यात क्षेत्र: पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि उत्पाद।
प्रमुख योजनाएँ और पहल
- विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023: प्रोत्साहन-आधारित से छूट-आधारित योजनाओं की ओर बदलाव।
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट (RoDTEP): अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट न दिए गए करों की वापसी।
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (ईपीसीजी): निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात।
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई): इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा आदि में विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
- बाजार पहुंच पहल (एमएआई): बाजार विकास के लिए वित्तीय सहायता।
संस्थागत ढांचा
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) – नीतिगत कार्यान्वयन।
- निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) – निर्यात ऋण बीमा।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) – कृषि निर्यात।
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) – समुद्री निर्यात।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- शीर्ष निर्यात गंतव्य (वित्त वर्ष 2024): संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर, चीन।
- शीर्ष निर्यातित वस्तुएँ (2024): पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, चावल, फार्मास्यूटिकल्स।
- आईटी सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक रैंक – प्रथम।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) भारत के कुल निर्यात में 30% से अधिक का योगदान करते हैं।
- यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) से व्यापार मार्गों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विश्व व्यापार संगठन और व्यापार समझौते संदर्भ
- भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।
- संयुक्त अरब अमीरात (सीईपीए), ऑस्ट्रेलिया (ईसीटीए), मॉरीशस (सीईसीपीए), आसियान और जापान जैसे देशों के साथ एफटीए/सीईसीए में शामिल।
- भारत-यूके एफटीए और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए पर वार्ता।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय
संदर्भ: गाजा युद्ध के कारण आई.एम.ई.सी. परियोजना में देरी
- पृष्ठभूमि:
IMEC की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन (2023) के दौरान की गई थी ताकि भारत से यूरोप तक शिपिंग समय को लाल सागर मार्ग की तुलना में लगभग 40% कम किया जा सके। इसमें भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इज़राइल तक समुद्री और रेल संपर्क, फिर जहाज द्वारा ग्रीस और फिर यूरोप के रेल नेटवर्क के माध्यम से आगे की यात्रा शामिल है। इसमें बिजली, इंटरनेट और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पाइपलाइनों के लिए केबल भी शामिल हैं। - महत्व:
यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है; वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 137.41 अरब डॉलर का था। IMEC का उद्देश्य संपर्क को मज़बूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और लागत कम करना है। - प्रारंभिक गति:
मध्य पूर्व में एक दुर्लभ स्थिर भू-राजनीतिक क्षण के दौरान घोषित, बढ़ते सामान्यीकरण (इज़राइल-अरब मेल-मिलाप, सऊदी अरब की सतर्क भागीदारी) के साथ। - गाजा युद्ध का प्रभाव:
- गाजा को लेकर जॉर्डन पर इजरायल-अमेरिकी दबाव के कारण जॉर्डन-इजराइल संबंध टूट गए हैं।
- सऊदी अरब का इजरायल के साथ सामान्यीकरण रुका हुआ है; रियाद फिलिस्तीनी राज्य की मांग पर दोगुना जोर दे रहा है।
- हौथी हमलों के कारण लाल सागर में नौवहन बाधित हो गया है।
- क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण हितधारक बैठकें असंभव हो गई हैं।
Learning Corner:
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) – यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा विशेष
- घोषणा – वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (पीजीआईआई) के हिस्से के रूप में सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा।
- सदस्य – भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजरायल, यूरोपीय संघ, अमेरिका।
- संरचना – दो गलियारे:
- पूर्वी गलियारा – भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है।
- उत्तरी गलियारा – अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
- परिवहन का साधन – बहुविध: रेल, सड़क और शिपिंग लिंक।
- मुख्य उद्देश्य – व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा हस्तांतरण (ग्रीन हाइड्रोजन) और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को बढ़ावा देना।
- भारत के लिए महत्व –
- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का रणनीतिक विकल्प।
- पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप के साथ संपर्क को बढ़ाया जाएगा।
- खाड़ी देशों और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करना।
- चुनौतियाँ – पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और वित्तपोषण संबंधी मुद्दे।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस
श्रेणी: कृषि
प्रसंग: केएलआईपी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग
- KLIP क्या है?
- भूपालपल्ली जिले के कलेश्वरम में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना ।
- 1,800 किमी से अधिक लम्बे नहर नेटवर्क का उपयोग करती है।
- 16 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, मौजूदा आयाकट (ayacut- सिंचाई व्यवस्था) को स्थिर करने तथा सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए 240 टीएमसी फीट गोदावरी जल का भंडारण/वितरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मेडीगड्डा, अन्नाराम, सुंडीला में निर्मित ।
- विवाद:
- संरचनात्मक विफलताएं: तीन वर्षों के भीतर, सुंडिला बैराज के खंभे डूब गए; अन्नाराम और सुंडिला में दरारें आ गईं।
- आरोप: बैराजों का निर्माण ऐसी पारगम्य नींव पर किया गया जो भारी जल प्रवाह को झेलने में असमर्थ थी।
- तुम्मिडीहट्टी से मेडिगड्डा तक स्थान परिवर्तन से लागत बढ़ गई तथा राजनीतिक आलोचना भी हुई।
- तुम्मिडिहट्टी में जल उपलब्धता के संदेह के कारण परिवर्तन हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसके पीछे छिपे उद्देश्य का आरोप लगाया।
- जाँच करना:
- न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है।
- जांच 15 महीने तक चली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और पूर्व मंत्रियों सहित 110 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई।
- निष्पादन एवं निधि निर्गमन में लापरवाही पाई गई।
- 31 जुलाई 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ; विधानसभा में चर्चा होगी।
Learning Corner:
भारत में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ
प्रमुख परिचालन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ
| परियोजना | राज्य | जल का स्रोत | प्रमुख बिंदु |
|---|---|---|---|
| कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) | तेलंगाना | गोदावरी नदी | विश्व की सबसे बड़ी बहु-चरणीय लिफ्ट सिंचाई; 600 मीटर तक पानी उठाती है; सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई। |
| हांड्री -नीवा सुजला श्रावंती (एचएनएसएस) | आंध्र प्रदेश | कृष्णा नदी | बहु-चरणीय; सूखाग्रस्त रायलसीमा तक पानी पहुंचाती है। |
| इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट योजना | राजस्थान | इंदिरा गांधी नहर (सतलज-ब्यास से) | थार रेगिस्तान के ऊंचे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करती है। |
| गंगा नहर लिफ्ट योजना | उत्तर प्रदेश | गंगा नदी | पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रदान करती है; मुख्य गंगा नहर की पूरक। |
| सरदार सरोवर लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ | गुजरात | नर्मदा नदी | गुरुत्वाकर्षण की पहुंच से बाहर के कमांड क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराती है; साथ ही पीने का पानी भी उपलब्ध कराती है। |
| गौरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना | ओडिशा | महानदी नदी | उच्चभूमि जनजातीय क्षेत्रों में कृषि को समर्थन प्रदान करता है। |
| कुंडालिया लिफ्ट सिंचाई योजना | मध्य प्रदेश | नर्मदा नदी | राजगढ़ और आगर-मालवा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई करना है। |
प्रमुख आगामी / निर्माणाधीन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ
| परियोजना | राज्य | स्रोत | स्थिति और महत्व |
|---|---|---|---|
| पलामुरु – रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना | तेलंगाना | कृष्णा नदी | निर्माणाधीन; दक्षिण तेलंगाना को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए। |
| देवदुला लिफ्ट सिंचाई योजना | तेलंगाना | गोदावरी नदी | निर्वहन के संदर्भ में भारत की सबसे अधिक क्षमता वाली लिफ्ट योजना; कई चरणों का कार्यान्वयन जारी। |
| लिफ्ट घटक के साथ मेकेदातु संतुलन जलाशय | कर्नाटक | कावेरी नदी | प्रस्तावित; जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु के साथ विवाद। |
| पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (विस्तार) | आंध्र प्रदेश | गोदावरी नदी | मौजूदा गोदावरी-कृष्णा अंतर्योजन; सूखा निवारण में सुधार के लिए भविष्य में विस्तार। |
| ऊपरी भद्रा परियोजना (लिफ्ट घटक) | कर्नाटक | तुंगा-भद्रा नदी | राष्ट्रीय परियोजना घोषित (2023); सूखाग्रस्त मध्य कर्नाटक में जल वितरण का हिस्सा। |
स्रोत : द हिंदू
श्रेणी: पर्यावरण
प्रसंग: विश्व शेर दिवस 2025 पर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है – जो पांच वर्षों में 32% की वृद्धि और पिछले दशक में 70% से अधिक की वृद्धि है।
भारत ने शेर संरक्षण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, विशेषकर गुजरात के गिर और विस्तृत सौराष्ट्र क्षेत्र में।
इस उपलब्धि के पीछे प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
- दूरदर्शी नेतृत्व : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रोजेक्ट लायन को प्राथमिकता दी, जिससे प्रमुख नीतिगत कार्रवाई, वित्त पोषण और पर्यावास विस्तार को बढ़ावा मिला।
- सामुदायिक भागीदारी : स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से मालधारी चरवाहे, शेरों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व में रहे हैं, अक्सर नुकसान के लिए मुआवजा देने से बचते हैं, जिससे संघर्ष को कम करने और जनसंख्या वृद्धि को सक्षम करने में मदद मिलती है।
- वैज्ञानिक संरक्षण और बुनियादी ढांचा: नए पर्यावास, बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल और पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं – जैसे कि बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का पुनरुद्धार – ने शेरों को स्वाभाविक रूप से तीन से ग्यारह जिलों तक विस्तार करने की अनुमति दी है।
- नीति और वित्तपोषण : 2,900 करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली 10 वर्षीय राष्ट्रीय शेर संरक्षण परियोजना के तहत नए स्वास्थ्य देखभाल और निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- वैश्विक महत्व : एशियाई शेर अब केवल भारत में ही जीवित बचे हैं, जो नीतियों, समर्पित वन कर्मचारियों और सह-अस्तित्व की संस्कृति की सफलता को दर्शाता है।
वैज्ञानिक प्रबंधन, मजबूत नीतियों और सामुदायिक भागीदारी के सम्मिश्रण वाले इस मॉडल को वन्यजीव संरक्षण के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में देखा जाता है।
Learning Corner:
एशियाई शेर बनाम अफ़्रीकी शेर
| विशेषता | एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) | अफ़्रीकी शेर (पैंथेरा लियो लियो) |
|---|---|---|
| वितरण | गिर वन, गुजरात, भारत में एकल जंगली आबादी | उप-सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से वितरित |
| जनसंख्या | ~675 (2024 की जनगणना) | ~20,000 (खंडित आबादी) |
| IUCN स्थिति | संकटग्रस्त/ लुप्तप्राय (EN) | सुभेद्य (VU) |
| शारीरिक बनावट | छोटा, कम मांसल; पेट के साथ प्रमुख त्वचा तह | बड़ा, अधिक मांसल; पेट पर कोई तह नहीं |
| अयाल (Mane) | छोटी, विरल अयाल – कान दिखाई देते हैं | घने, घने बाल – कान अक्सर छिपे रहते हैं |
| सामाजिक संरचना | छोटे झुंड (2-5 मादा) | बड़े झुंड (10-15+ मादा) |
| संरक्षण चुनौतियाँ | प्रतिबंधित आवास, मानव-वन्यजीव संघर्ष, एकल जनसंख्या के कारण रोग का खतरा | आवास की हानि, अवैध शिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष |
| विशेष नोट | अफ्रीका के बाहर केवल जंगली शेर; भारत की वन्यजीव विरासत का हिस्सा | अफ़्रीकी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख शीर्ष शिकारी |
स्रोत: द हिंदू
श्रेणी: पर्यावरण
प्रसंग: तमिलनाडु ने तमिलनाडु स्कूल शिक्षा नीति 2025 का अनावरण किया
मुख्य अंश
दो-भाषा सूत्र
- केवल तमिल और अंग्रेजी में ही शिक्षण की पुष्टि की गई, तथा एनईपी के त्रि-भाषा मॉडल और हिंदी को थोपने को अस्वीकार किया गया।
- तमिल को राज्य की पहचान के रूप में मान्यता दी गई है; तथा अंग्रेजी को वैश्विक कौशल के रूप में मान्यता दी गई है।
दृष्टि और फोकस
- तमिल संस्कृति पर आधारित एक समावेशी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार स्कूल प्रणाली का निर्माण करना।
- समालोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, डिजिटल साक्षरता और तर्कसंगत जांच को बढ़ावा देता है।
- हाशिए पर पड़े समूहों, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।
प्रमुख विशेषताएं
- कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है – केवल कक्षा 10 और 12 की सार्वजनिक परीक्षाएं होंगी।
- स्कूल में प्रवेश की आयु 5 वर्ष ही रहेगी; 10+2 संरचना बरकरार रखी गई, एनईपी के 5+3+3+4 मॉडल को खारिज कर दिया गया।
- कला और विज्ञान के लिए कोई केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा नहीं; प्रवेश कक्षा XI और XII के अंकों के आधार पर होगा।
- योग्यता-आधारित, पूछताछ-संचालित पाठ्यक्रम जिसमें तमिल विरासत, पर्यावरण, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा और डिजिटल कौशल पर जोर दिया जाएगा।
- कला, खेल, जीवन कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
राजनीतिक और नीतिगत रुख
- एसईपी ने सामाजिक न्याय और भाषाई स्वायत्तता के लिए खतरे का हवाला देते हुए एनईपी के प्रतिपक्ष के रूप में अपनी स्थिति बनाई।
- राज्य का कहना है कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और वह एकतरफा केन्द्रीय आदेशों का विरोध करता है।
- एनईपी को न अपनाने से जुड़ी शिक्षा निधि रोके जाने पर केंद्र के साथ विवाद।
कार्यान्वयन लक्ष्य
- व्यापक विचार-विमर्श के बाद 14 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा विकसित।
- स्कूल से उच्च शिक्षा में 100% परिवर्तन का लक्ष्य (वर्तमान में 75%)।
Learning Corner:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 – यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा विशेष
- लॉन्च: 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लेगा।
- विजन: समग्र, लचीली, बहुविषयक शिक्षा जो एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप हो।
- संरचना: 10+2 को 5+3+3+4 मॉडल से प्रतिस्थापित करता है (आयु 3-18)।
- आधारभूत चरण (5 वर्ष) – पूर्व-प्राथमिक + कक्षा 1-2
- प्रारंभिक चरण (3 वर्ष) – ग्रेड 3-5
- मध्य चरण (3 वर्ष) – कक्षा 6-8
- माध्यमिक चरण (4 वर्ष) – कक्षा 9-12
- स्कूल शिक्षा सुधार:
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को 2030 तक सार्वभौमिक बनाया जाएगा।
- आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता में सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन (निपुण भारत)।
- बोर्ड परीक्षाएं आसान और अधिक लचीली होंगी।
- कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी।
- उच्च शिक्षा सुधार:
- सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लक्ष्य: 2035 तक 50%
- बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)
- चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) जिसमें अनेक निकास विकल्प होंगे।
- यूजीसी/एआईसीटीई के स्थान पर भारतीय सामान्य उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना।
- अन्य सुविधा:
- कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा।
- प्रौद्योगिकी का एकीकरण (राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच – एनईटीएफ)।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र – परख ।
- शिक्षक शिक्षा – 2030 तक न्यूनतम डिग्री आवश्यकता 4 वर्षीय बी.एड होगी।
- आलोचना एवं चुनौतियाँ:
- शिक्षा की संघीय प्रकृति के कारण राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में बाधाएं।
- संसाधन की कमी और डिजिटल विभाजन।
स्रोत: द हिंदू
(MAINS Focus)
परिचय (संदर्भ)
25 जुलाई, 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया , जो रासायनिक रूप से दूषित स्थलों के प्रबंधन के लिए भारत का पहला कानूनी ढांचा प्रदान करता है ।
दूषित स्थल (Contaminated Sites) क्या हैं?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार , दूषित स्थल वे स्थान हैं जहां ऐतिहासिक रूप से खतरनाक या अन्य अपशिष्टों को डंप किया जाता था, जिससे मिट्टी, भूजल और सतही जल दूषित होता था , जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा पैदा होता था।
उदाहरण:
- लैंडफिल, अपशिष्ट डंप, रिसाव स्थल
- अपशिष्ट भंडारण और उपचार सुविधाएं
- रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन और भंडारण स्थल
वर्तमान परिदृश्य:
- भारत भर में 103 स्थलों की पहचान की गई।
- केवल 7 स्थलों पर सुधार कार्य शुरू हुआ, जिसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाकर दूषित मिट्टी, भूजल, सतही जल और तलछट को साफ करना शामिल है।
- कई प्रदूषक निष्क्रिय हो चुके हैं या सफाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं
इन नियमों की आवश्यकता क्यों थी?
- 2010 में, MoEFCC ने प्रदूषित स्थलों के उपचार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करने हेतु औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया।
- तीन कार्यों की पहचान की गई:
-
- सूची निर्माण – संभावित दूषित स्थलों की पहचान करना
- मार्गदर्शन विकास – साइट मूल्यांकन और सुधार के लिए मैनुअल तैयार करना
- कानूनी, संस्थागत और वित्तीय ढांचा – बाध्यकारी नियम बनाएं ( 2025 तक लंबित)
- 2025 के नियम कानूनी संहिताकरण प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे संदूषण पर संरचित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
2025 नियमों के प्रावधान
- संदिग्ध स्थलों की रिपोर्टिंग
- जिला प्रशासन को रासायनिक संदूषण के संदिग्ध स्थलों की पहचान करते हुए अर्धवार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
- ये रिपोर्टें आगे की कार्रवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या नामित संदर्भ संगठन को भेजी जाएंगी।
- प्रारंभिक मूल्यांकन
-
- एक बार साइट की सूचना मिलने पर, एसपीसीबी/संदर्भ संगठन के पास प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए 90 दिन का समय होता है।
- इसमें शामिल हैं:
-
-
- साइट के बारे में ऐतिहासिक डेटा की समीक्षा करना
- पिछले औद्योगिक या खतरनाक अपशिष्ट गतिविधि की जाँच करना
- संभावित संदूषण की पुष्टि के लिए सीमित नमूने एकत्र करना
- इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता है।
-
- विस्तृत साइट सर्वेक्षण
-
- यदि प्रारंभिक मूल्यांकन से संदूषण का पता चलता है, तो अगले 90 दिनों में एक व्यापक सर्वेक्षण पूरा किया जाना चाहिए।
- यह सर्वेक्षण:
-
-
- संदूषण के प्रकार और सीमा की पहचान करना
- खतरनाक रसायनों के स्तर को मापना (खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 में 189 रसायनों की सूची से)
- मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिमों का आकलन करना
-
-
- यदि संदूषण सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए:
- साइट का स्थान सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाएगा
- जोखिम को रोकने के लिए प्रवेश प्रतिबंध लगाए जाएंगे
- उपचार योजना
- एक संदर्भ संगठन (विशेषज्ञ निकाय) एक सुधार योजना तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:
-
- उपयोग की जाने वाली सफाई तकनीक (जैसे, मिट्टी की धुलाई, जैव-उपचार, भस्मीकरण)
- सुधार के प्रत्येक चरण के लिए अनुमानित समय-सीमा
- सफाई के दौरान सुरक्षा सावधानियां
- सुधार योजना अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए एसपीसीबी को प्रस्तुत की जाएगी।
- प्रदूषकों की पहचान और लागत वसूली
- एसपीसीबी के पास संदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या कंपनी की पहचान करने के लिए 90 दिन का समय है।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू होता है – प्रदूषकों को उपचार की पूरी लागत वहन करनी होगी।
- यदि प्रदूषक निष्क्रिय हैं, लापता हैं, या भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से सफाई का वित्तपोषण करेंगी।
- कानूनी देयता
-
- भारतीय न्याय संहिता (2023) के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।
- यह सफाई के लिए वित्तीय दायित्व के अतिरिक्त है।
अंतराल
- ये नियम निम्नलिखित से उत्पन्न प्रदूषण पर लागू नहीं होते हैं : रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन कार्य, समुद्र का तेल प्रदूषण और नगरपालिका डंप साइटों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (अन्य कानूनों द्वारा कवर)।
- इसके अलावा, किसी दूषित स्थल की पहचान होने के बाद कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
इसलिए ऐसे अंतरालों को भरने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
नव अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 का उद्देश्य भारत के पर्यावरणीय शासन में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करना है। इनके महत्व, सीमाओं और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
स्रोत: https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/what-are-the-new-rules-on-chemically-contaminated-sites-explained/article69917568.ece
परिचय (संदर्भ)
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी), जिसके लिए भारत ने 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्रतिबद्धता जताई थी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, उच्च स्तर की सेवा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है। हालाँकि, घर के पास स्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में विश्वसनीय निदान सुविधाओं का अभाव सेवा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा दोनों के स्तर को कम करता है।
इसलिए, आइए यूएचसी में निदान की भूमिका, पहुंच में वर्तमान अंतराल, हालिया नीतिगत उपायों (जैसे एनएलईडी) और स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर नैदानिक सेवाओं को मजबूत करने की रणनीतियों को समझें।
डायग्नोस्टिक/ नैदानिक सेवाएं क्या हैं और उनका महत्व क्या है?
नैदानिक सेवाएं चिकित्सा परीक्षणों और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करती हैं जो रोगियों में रोगों और स्थितियों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
इसमें नैदानिक परीक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे चिकित्सा और मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक मूल्यांकन।
महत्व:
- ये सेवाएं रोगी देखभाल में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं।
- शीघ्र पता लगने से रोग की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है और समय पर हस्तक्षेप संभव हो सकता है।
- अनावश्यक या गलत समय पर किए जाने वाले उपचारों में कमी आती है, जिससे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य लागत में बचत होती है।
निदान परीक्षणों तक पहुंच की कमी के कारण विकार की पहचान में देरी हो सकती है या गलत पहचान हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप गलत समय पर या गलत दिशा में उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।
भारत में नैदानिक पहुँच
- निजी बनाम सार्वजनिक
-
- भारत में निजी अस्पताल और प्रयोगशालाएं कई प्रकार के चिकित्सा परीक्षण उपलब्ध कराती हैं, लेकिन शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से में गरीब लोगों के लिए ये सेवाएं बहुत महंगी हैं या बहुत दूर हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्भरता बढ़ती है।
- समाधान: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को वास्तव में काम करने के लिए , लोगों को उनके निवास स्थान के नजदीक आवश्यक परीक्षण कराने में सक्षम होना चाहिए – आदर्श रूप से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप-केंद्र स्तर का स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में।
- निदान का कवरेज
-
- जीवनशैली, आर्थिक, पर्यावरणीय और पोषण संबंधी परिवर्तनों के कारण हृदय रोग और मधुमेह जैसी गैर-संचारी बीमारियाँ (एनसीडी) बढ़ रही हैं।
- टीबी और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- सभी को शीघ्र एवं सटीक निदान सेवाओं की आवश्यकता होती है।
- समाधान: सरकार को देश में बदलती बीमारियों के पैटर्न के बारे में सोचने और उसके अनुसार नैदानिक सेवाओं के पैटर्न में बदलाव करने की आवश्यकता है।
- निदान की लागत प्रभावशीलता
-
- स्वास्थ्य प्रणाली में नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय, हमें लागत-प्रभावशीलता के बारे में सोचना चाहिए ।
- उपलब्ध कराए जाने वाले परीक्षणों, परीक्षणों के क्रम, लागत आदि के बारे में उचित अध्ययन किया जाना चाहिए।
- समाधान: सरकार को साक्ष्य-आधारित नैदानिक दिशानिर्देश प्रदान करने चाहिए । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (एनएलईडी) में हालिया परिवर्तन
आवश्यक निदान की राष्ट्रीय सूची (एनएलईडी) चिकित्सा परीक्षणों की एक सूची है जो पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध होनी चाहिए।
इसे पहली बार 2019 में तैयार किया गया था और अब इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा आज की बीमारी के पैटर्न और आधुनिक तकनीक से मेल खाने के लिए अद्यतन किया गया है।
नए एनएलईडी में प्रमुख अपडेट
- मधुमेह परीक्षण
-
- भारत में लाखों लोग मधुमेह या प्री-डायबिटीज से पीड़ित हैं।
- आईसीएमआर अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर पिछले तीन महीनों के औसत रक्त शर्करा स्तर की जांच के लिए एचबीए1सी रक्त के नमूने एकत्र करने की सिफारिश करता है।
- इन नमूनों को विश्लेषण के लिए बड़े केंद्रों में भेजा जाएगा।
उप-केंद्र स्तर पर परीक्षण (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र)
- सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी और सिफलिस के लिए त्वरित परीक्षण।
- डेंगू परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छर जनित रोग अधिक क्षेत्रों में फैल रहे हैं।
पीएचसी स्तर पर परीक्षण
- रक्त शर्करा, यकृत एंजाइम और कोलेस्ट्रॉल जैसी रक्त रसायन संबंधी जांच अब मौके पर ही की जा सकती है।
सीएचसी स्तर (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) पर परीक्षण
- दंत एक्स-रे की शुरुआत की गई, क्योंकि मौखिक स्वास्थ्य को अब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता माना जाता है।
- टीबी निदान
-
- आणविक टीबी परीक्षण के लिए बलगम के नमूने उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एकत्र किए जाएंगे और उच्चतर केन्द्रों को भेजे जाएंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-जिला और जिला अस्पतालों में ये टीबी परीक्षण घर पर ही किए जाएंगे।
- यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अभी भी टीबी का बोझ बहुत अधिक है, तथा अनेक मामले ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पाता या जिनका पता देर से चलता है।
- ये परिवर्तन इसलिए संभव हो पाए हैं क्योंकि आणविक निदान मशीनें सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई हैं।
आगे की राह
- सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यक नैदानिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।
- तकनीशियनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना।
- स्वास्थ्य बीमा का विस्तार कर बाह्य रोगी निदान को भी कवर किया जाना चाहिए।
- मोबाइल क्लीनिकों और समुदाय-आधारित परीक्षण के माध्यम से अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कौशल और पहुंच के अंतर को पाटने के लिए एआई और टेलीमेडिसिन का उपयोग करना।
निष्कर्ष
विश्वसनीय, किफायती और विकेन्द्रीकृत नैदानिक सेवाओं के बिना, यूएचसी लक्ष्य अप्राप्य रहेंगे। बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के माध्यम से नैदानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना भारत में सार्वभौमिक, समतापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“निदान (Diagnostics) भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की रीढ़ है।” निदान को सुलभ और किफायती बनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)