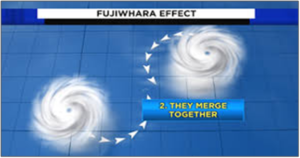(UPSC GS Paper II – “Security Challenges and their Management; Role of State and Non-State Actors)
Context (Introduction)
Recent violence and the subsequent public suspicion directed at Kashmiris highlight deep-seated alienation in Jammu & Kashmir, rooted in perceptions of injustice, civil liberties concerns, and political grievances, making reconciliation dependent on dignity, dialogue, and trust-building.
Main Arguments: Why Reconciliation Requires a Human-Centric Approach
- Collective Suspicion: Media sensationalism and premature attribution of blame stigmatise Kashmiris across India, worsening fear, anxiety, and feelings of being treated as perpetual suspects.
- Punitive Measures: Practices such as demolishing family homes of alleged militants constitute collective punishment, violating fairness norms and deepening resentment.
- Civil Liberties Concerns: Curtailment of liberties, widespread surveillance, arbitrary dismissals from government jobs, and property attachments create suffocation among youth.
- Economic Exclusion: Shrinking employment avenues combined with perceived discriminatory recruitment and reservation policies heighten disempowerment and frustration.
- Political Disempowerment: Abrogation of Article 370, withdrawal of land and job protections, and fears of demographic change fuel sentiments of loss, dispossession, and identity anxiety.
Challenges / Criticisms
- Alienation Spiral: Security actions that emphasise coercion over engagement risk reinforcing alienation and incentivising radicalisation among frustrated youth.
- Identity Insecurity: Perceptions of cultural erosion and erosion of institutional protections hinder emotional integration with the Union.
- Distrust in Institutions: Frequent raids, detentions, and surveillance weaken faith in justice systems and reduce cooperation with authorities.
- Political Vacuum: Limited democratic engagement and absence of meaningful political dialogue allow grievances to fester unaddressed.
- Narrative Polarisation: Media narratives framing the region solely through terrorism ignore lived experiences, limiting empathy and national cohesion.
Way Forward
- End Collective Punishment: Stop punitive demolitions and ensure accused individuals, not families, are subject to due legal process.
- Restore Civil Liberties: Build confidence by curbing excessive surveillance, ensuring fair recruitment, and easing restrictions on peaceful civic activity.
- Reopen Dialogue Channels: Revive a structured political dialogue rooted in insaniyat and jamhooriyat, drawing on the Vajpayee framework.
- Economic Inclusion: Prioritise job creation, equitable recruitment, and targeted youth programmes to strengthen trust in institutions.
- Narrative Correction: Promote responsible media reporting and public communication to prevent stereotyping and encourage national empathy.
Conclusion
Sustainable peace in J&K demands more than security management; it requires dignity, justice, and engagement. When rights are respected, aspirations acknowledged, and communities treated with compassion rather than suspicion, reconciliation becomes a lived reality rather than a distant ideal.
Mains Question
- “Peace in Jammu & Kashmir cannot rest solely on security operations but requires political engagement. Analyse the social and political roots of alienation and suggest measures for sustainable reconciliation.” (250 words, 15 marks)
Source: The Hindu